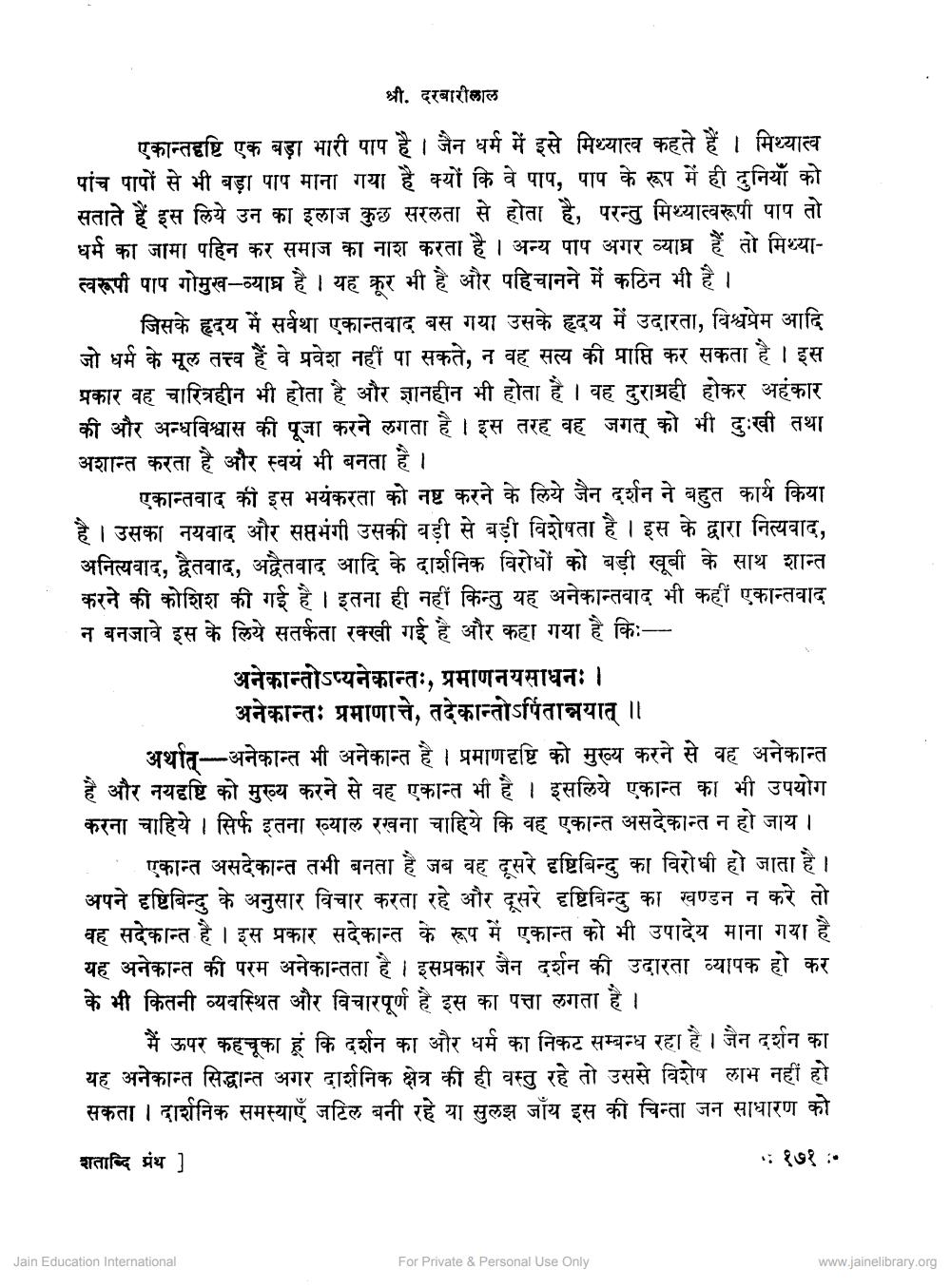________________
श्री. दरबारीलाल एकान्तदृष्टि एक बड़ा भारी पाप है । जैन धर्म में इसे मिथ्यात्व कहते हैं । मिथ्यात्व पांच पापों से भी बड़ा पाप माना गया है क्यों कि वे पाप, पाप के रूप में ही दुनियाँ को सताते हैं इस लिये उन का इलाज कुछ सरलता से होता है, परन्तु मिथ्यात्वरूपी पाप तो धर्म का जामा पहिन कर समाज का नाश करता है । अन्य पाप अगर व्याघ्र हैं तो मिथ्यात्वरूपी पाप गोमुख-व्याघ्र है । यह क्रूर भी है और पहिचानने में कठिन भी है।
जिसके हृदय में सर्वथा एकान्तवाद बस गया उसके हृदय में उदारता, विश्वप्रेम आदि जो धर्म के मूल तत्त्व हैं वे प्रवेश नहीं पा सकते, न वह सत्य की प्राप्ति कर सकता है । इस प्रकार वह चारित्रहीन भी होता है और ज्ञानहीन भी होता है । वह दुराग्रही होकर अहंकार की और अन्धविश्वास की पूजा करने लगता है । इस तरह वह जगत् को भी दुःखी तथा अशान्त करता है और स्वयं भी बनता है ।
एकान्तवाद की इस भयंकरता को नष्ट करने के लिये जैन दर्शन ने बहुत कार्य किया है । उसका नयवाद और सप्तभंगी उसकी बड़ी से बड़ी विशेषता है । इस के द्वारा नित्यवाद, अनित्यवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि के दार्शनिक विरोधों को बड़ी खूबी के साथ शान्त करने की कोशिश की गई है । इतना ही नहीं किन्तु यह अनेकान्तवाद भी कहीं एकान्तवाद न बनजावे इस के लिये सतर्कता रक्खी गई है और कहा गया है किः--
अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः, प्रमाणनयसाधनः।
अनेकान्तः प्रमाणात्ते, तदेकान्तोऽर्पितानयात् ॥ अर्थात-अनेकान्त भी अनेकान्त है । प्रमाणदृष्टि को मुख्य करने से वह अनेकान्त है और नयदृष्टि को मुख्य करने से वह एकान्त भी है । इसलिये एकान्त का भी उपयोग करना चाहिये । सिर्फ इतना ख्याल रखना चाहिये कि वह एकान्त असदेकान्त न हो जाय ।
एकान्त असदेकान्त तभी बनता है जब वह दूसरे दृष्टिबिन्दु का विरोधी हो जाता है। अपने दृष्टिबिन्दु के अनुसार विचार करता रहे और दूसरे दृष्टिबिन्दु का खण्डन न करे तो वह सदेकान्त है । इस प्रकार सदेकान्त के रूप में एकान्त को भी उपादेय माना गया है यह अनेकान्त की परम अनेकान्तता है । इसप्रकार जैन दर्शन की उदारता व्यापक हो कर के भी कितनी व्यवस्थित और विचारपूर्ण है इस का पत्ता लगता है ।
मैं ऊपर कहचूका हूं कि दर्शन का और धर्म का निकट सम्बन्ध रहा है । जैन दर्शन का यह अनेकान्त सिद्धान्त अगर दार्शनिक क्षेत्र की ही वस्तु रहे तो उससे विशेष लाभ नहीं हो सकता । दार्शनिक समस्याएँ जटिल बनी रहे या सुलझ जाँय इस की चिन्ता जन साधारण को शताब्दि ग्रंथ ]
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org