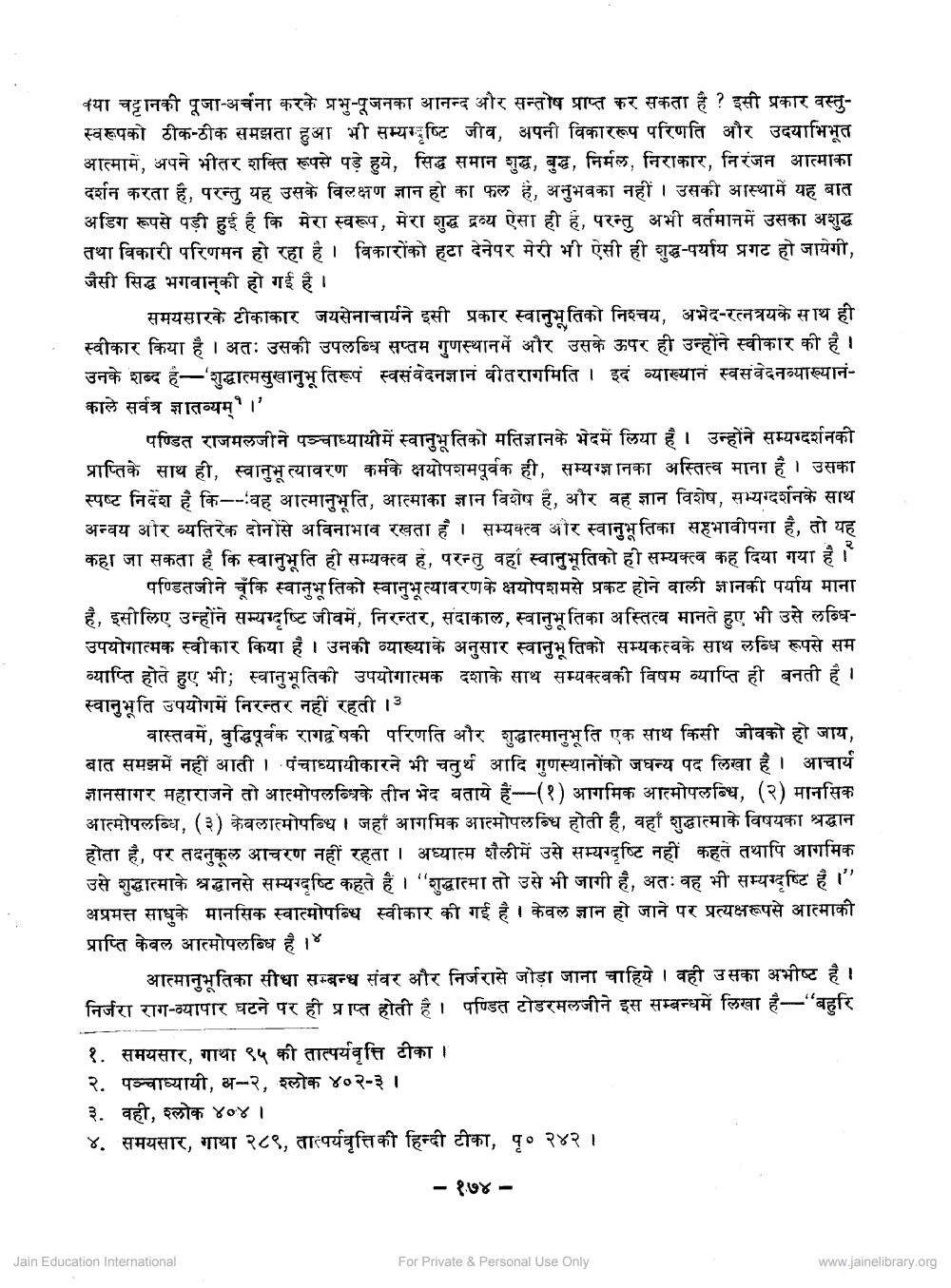________________
क्या चट्टानकी पूजा-अर्चना करके प्रभु-पूजनका आनन्द और सन्तोष प्राप्त कर सकता है ? इसी प्रकार वस्तुस्वरूपको ठीक-ठीक समझता हुआ भी सम्यग्दृष्टि जीव, अपनी विकाररूप परिणति और उदयाभिभूत आत्मामें, अपने भीतर शक्ति रूपसे पड़े हुये, सिद्ध समान शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, निराकार, निरंजन आत्माका दर्शन करता है, परन्तु यह उसके विलक्षण ज्ञान हो का फल है, अनुभवका नहीं। उसकी आस्थामें यह बात अडिग रूपसे पड़ी हुई है कि मेरा स्वरूप, मेरा शुद्ध द्रव्य ऐसा ही है, परन्तु अभी वर्तमानमें उसका अशुद्ध तथा विकारी परिणमन हो रहा है। विकारोंको हटा देनेपर मेरी भी ऐसी ही शुद्ध-पर्याय प्रगट हो जायेगी, जैसी सिद्ध भगवान्की हो गई है।
समयसारके टीकाकार जयसेनाचार्यने इसी प्रकार स्वानुभतिको निश्चय, अभेद-रत्नत्रयके साथ ही स्वीकार किया है । अतः उसकी उपलब्धि सप्तम गुणस्थानमें और उसके ऊपर ही उन्होंने स्वीकार की है। उनके शब्द है-'शुद्धात्मसुखानुभू तिरूपं स्वसंवेदनज्ञानं वीतरागमिति । इदं व्याख्यानं स्वसंवेदनव्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्यम् ।'
पण्डित राजमलजीने पञ्चाध्यायीमें स्वानुभूतिको मतिज्ञानके भेदमें लिया है। उन्होंने सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके साथ ही, स्वानुभू त्यावरण कर्मके क्षयोपशमपूर्वक ही, सम्यग्ज्ञानका अस्तित्व माना है । उसका स्पष्ट निर्देश है कि--वह आत्मानुभूति, आत्माका ज्ञान विशेष है, और वह ज्ञान विशेष, सभ्यग्दर्शनके साथ अन्वय और व्यतिरेक दोनोंसे अविनाभाव रखता है । सम्यक्त्व और स्वानुभूतिका सहभावीपना है, तो यह कहा जा सकता है कि स्वानुभूति ही सम्यक्त्व है, परन्तु वहां स्वानुभूतिको ही सम्यक्त्व कह दिया गया है।
पण्डितजीने चूँकि स्वानुभूतिको स्वानुभूत्यावरण के क्षयोपशमसे प्रकट होने वाली ज्ञानकी पर्याय माना है, इसीलिए उन्होंने सम्यग्दृष्टि जीवमें, निरन्तर, सदाकाल, स्वानुभूतिका अस्तित्व मानते हुए भी उसे लब्धिउपयोगात्मक स्वीकार किया है। उनकी व्याख्याके अनसार स्वानभतिको सम्यकत्वके साथ ल व्याप्ति होते हुए भी; स्वानुभूतिको उपयोगात्मक दशाके साथ सम्यक्त्वकी विषम व्याप्ति ही बनती है । स्वानुभूति उपयोगमें निरन्तर नहीं रहती ।
वास्तवमें, बुद्धिपूर्वक रागद्वषकी परिणति और शुद्धात्मानुभूति एक साथ किसी जीवको हो जाय, बात समझमें नहीं आती। पंचाध्यायीकारने भी चतुर्थ आदि गुणस्थानोंको जघन्य पद लिखा है। आचार्य ज्ञानसागर महाराजने तो आत्मोपलब्धिके तीन भेद बताये हैं-(१) आगमिक आत्मोपलब्धि, (२) मानसिक आत्मोपलब्धि, (३) केबलात्मोपब्धि । जहाँ आगमिक आत्मोपलब्धि होती है, वहाँ शुद्धात्माके विषयका श्रद्धान होता है, पर तदनुकूल आचरण नहीं रहता । अध्यात्म शैलीमें उसे सम्यग्दृष्टि नहीं कहते तथापि आगमिक उसे शुद्धात्माके श्रद्धानसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं । "शुद्धात्मा तो उसे भी जागी है, अतः वह भी सम्यग्दृष्टि है ।' अप्रमत्त साधके मानसिक स्वात्मोपब्धि स्वीकार की गई है। केवल ज्ञान हो जाने पर प्रत्यक्षरूपसे आत्माकी प्राप्ति केवल आत्मोपलब्धि है।४
आत्मानुभूतिका सीधा सम्बन्ध संवर और निर्जरासे जोड़ा जाना चाहिये । वही उसका अभीष्ट है। निर्जरा राग-व्यापार घटने पर ही प्राप्त होती है। पण्डित टोडरमलजीने इस सम्बन्धमें लिखा है-"बहरि
१. समयसार, गाथा ९५ की तात्पर्यवत्ति टीका । २. पञ्चाध्यायी, अ-२, श्लोक ४०२-३ । ३. वही, श्लोक ४०४ ।। ४. समयसार, गाथा २८९, तात्पर्यवृत्तिकी हिन्दी टीका, पृ० २४२ ।
- १७४ -
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org