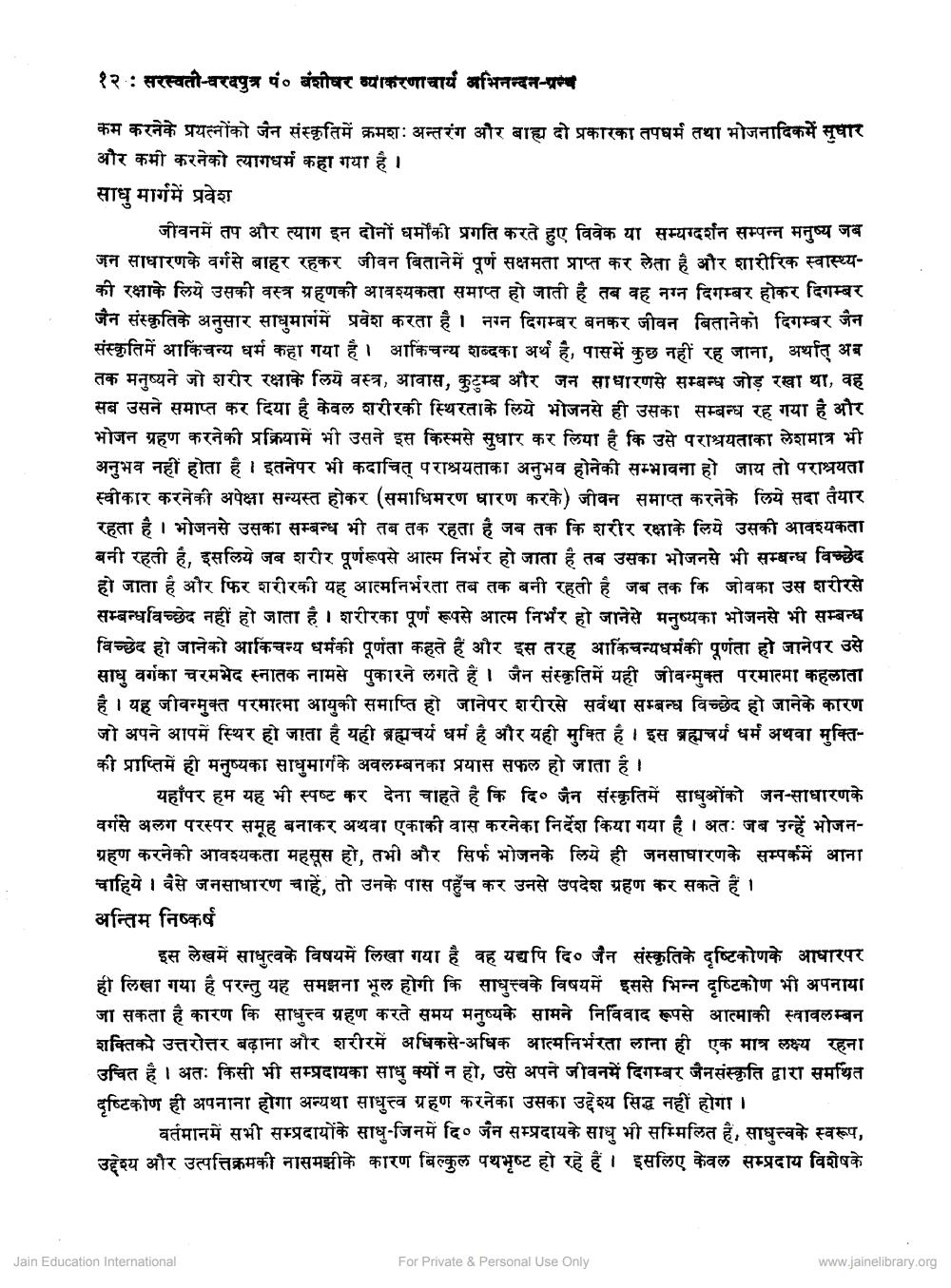________________
१२ : सरस्वती-वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-प्रन्य
कम करनेके प्रयत्नोंको जैन संस्कृतिमें क्रमशः अन्तरंग और बाह्य दो प्रकारका तपधर्म तथा भोजनादिकमें सुधार
और कमी करनेको त्यागधर्म कहा गया है। साधु मार्गमें प्रवेश
जीवनमें तप और त्याग इन दोनों धर्मोंकी प्रगति करते हुए विवेक या सम्यग्दर्शन सम्पन्न मनुष्य जब जन साधारणके वर्गसे बाहर रहकर जीवन बिताने में पूर्ण सक्षमता प्राप्त कर लेता है और शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये उसकी वस्त्र ग्रहणकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तब वह नग्न दिगम्बर होकर दिगम्बर जैन संस्कृतिके अनुसार साधुमार्गमें प्रवेश करता है। नग्न दिगम्बर बनकर जीवन बितानेको दिगम्बर जैन संस्कृतिमें आकिंचन्य धर्म कहा गया है। आकिंचन्य शब्दका अर्थ है, पासमें कुछ नहीं रह जाना, अर्थात् अब तक मनुष्यने जो शरीर रक्षाके लिये वस्त्र, आवास, कुटुम्ब और जन साधारणसे सम्बन्ध जोड़ रखा था, वह सब उसने समाप्त कर दिया है केवल शरीरकी स्थिरताके लिये भोजनसे ही उसका सम्बन्ध रह गया है और भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियामें भी उसने इस किस्मसे सुधार कर लिया है कि उसे पराश्रयताका लेशमात्र भी अनुभव नहीं होता है । इतनेपर भी कदाचित् पराश्रयताका अनुभव होनेकी सम्भावना हो जाय तो पराश्रयता स्वीकार करनेकी अपेक्षा सन्यस्त होकर (समाधिमरण धारण करके) जीवन समाप्त करनेके लिये सदा तैयार रहता है । भोजनसे उसका सम्बन्ध भी तब तक रहता है जब तक कि शरीर रक्षाके लिये उसकी आवश्यकता बनी रहती है, इसलिये जब शरीर पूर्णरूपसे आत्म निर्भर हो जाता है तब उसका भोजनसे भी सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है और फिर शरीरकी यह आत्मनिर्भरता तब तक बनी रहती है जब तक कि जोवका उस शरीरसे सम्बन्धविच्छेद नहीं हो जाता है । शरीरका पूर्ण रूपसे आत्म निर्भर हो जानेसे मनुष्यका भोजनसे भी सम्बन्ध विच्छेद हो जानेको आकिंचन्य धर्मको पूर्णता कहते हैं और इस तरह आकिंचन्यधर्मकी पूर्णता हो जानेपर उसे साधु वर्गका चरमभेद स्नातक नामसे पुकारने लगते हैं। जैन संस्कृतिमें यही जीवन्मुक्त परमात्मा कहलाता है । यह जीवन्मुक्त परमात्मा आयुकी समाप्ति हो जानेपर शरीरसे सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद हो जानेके कारण जो अपने आपमें स्थिर हो जाता है यही ब्रह्मचर्य धर्म है और यही मुक्ति है। इस ब्रह्मचर्य धर्म अथवा मुक्तिकी प्राप्तिमें ही मनुष्यका साधुमार्गके अवलम्बनका प्रयास सफल हो जाता है।
यहाँपर हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते है कि दि० जैन संस्कृतिमें साधुओंको जन-साधारणके वर्गसे अलग परस्पर समूह बनाकर अथवा एकाकी वास करनेका निर्देश किया गया है । अतः जब उन्हें भोजनग्रहण करनेकी आवश्यकता महसूस हो, तभी और सिर्फ भोजनके लिये ही जनसाधारणके सम्पर्कमें आना चाहिये । वैसे जनसाधारण चाहें, तो उनके पास पहुँच कर उनसे उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। अन्तिम निष्कर्ष
इस लेखमें साधुत्वके विषयमें लिखा गया है वह यद्यपि दि० जैन संस्कृतिके दृष्टिकोणके आधारपर ही लिखा गया है परन्तु यह समझना भूल होगी कि साधुत्त्वके विषयमें इससे भिन्न दृष्टिकोण भी अपनाया जा सकता है कारण कि साधुत्त्व ग्रहण करते समय मनुष्यके सामने निर्विवाद रूपसे आत्माकी स्वावलम्बन शक्तिको उत्तरोत्तर बढ़ाना और शरीरमें अधिकसे-अधिक आत्मनिर्भरता लाना ही एक मात्र लक्ष्य रहना उचित है । अतः किसी भी सम्प्रदायका साधु क्यों न हो, उसे अपने जीवनमें दिगम्बर जैनसंस्कृति द्वारा समर्थित दृष्टिकोण ही अपनाना होगा अन्यथा साधुत्त्व ग्रहण करनेका उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।
वर्तमानमें सभी सम्प्रदायोंके साधु-जिनमें दि० जैन सम्प्रदायके साधु भी सम्मिलित हैं, साधुत्त्वके स्वरूप, उद्देश्य और उत्पत्तिक्रमकी नासमझीके कारण बिल्कुल पथभ्रष्ट हो रहे हैं। इसलिए केवल सम्प्रदाय विशेषके
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org