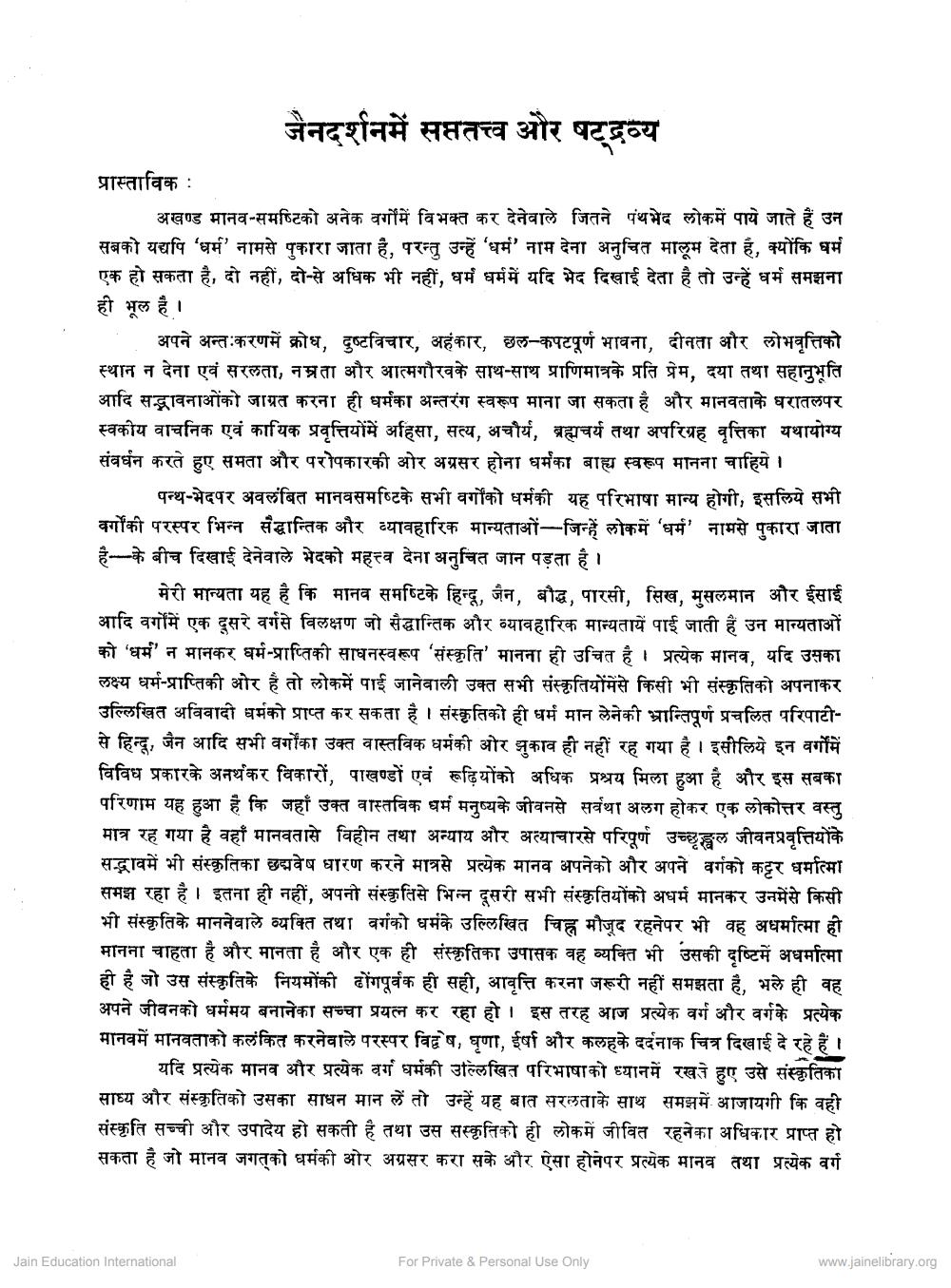________________
जैनदर्शनमें सप्ततत्त्व और षट्द्रव्य
प्रास्ताविक :
अखण्ड मानव-समष्टिको अनेक वर्गोंमें विभक्त कर देनेवाले जितने पंथभेद लोकमें पाये जाते हैं उन सबको यद्यपि 'धर्म' नामसे पुकारा जाता है, परन्तु उन्हें 'धर्म' नाम देना अनुचित मालूम देता है, क्योंकि धर्म एक हो सकता है, दो नहीं, दो से अधिक भी नहीं, धर्मं धर्म में यदि भेद दिखाई देता है तो उन्हें धर्म समझना ही भूल है ।
अपने अन्तःकरणमें क्रोध, दुष्टविचार, अहंकार, छल-कपटपूर्ण भावना, दीनता और लोभवृत्तिको स्थान न देना एवं सरलता, नम्रता और आत्मगौरव के साथ-साथ प्राणिमात्रके प्रति प्रेम, दया तथा सहानुभूति आदि सद्भावनाओं को जाग्रत करना ही धर्मका अन्तरंग स्वरूप माना जा सकता है और मानवताके धरातलपर स्वकीय वाचनिक एवं कायिक प्रवृत्तियोंमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह वृत्तिका यथायोग्य संवर्धन करते हुए समता और परोपकारकी ओर अग्रसर होना धर्मका बाह्य स्वरूप मानना चाहिये ।
पन्थ-भेदपर अवलंबित मानवसमष्टिके सभी वर्गोंको धर्मकी यह परिभाषा मान्य होगी, इसलिये सभी वर्गों की परस्पर भिन्न सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मान्यताओं - जिन्हें लोकमें 'धर्म' नामसे पुकारा जाता है के बीच दिखाई देनेवाले भेदको महत्त्व देना अनुचित जान पड़ता है ।
मेरी मान्यता यह है कि मानव समष्टिके हिन्दू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, मुसलमान और ईसाई आदि वर्गों में एक दुसरे वर्ग से विलक्षण जो सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मान्यतायें पाई जाती हैं उन मान्यताओं को 'धर्म' न मानकर धर्म-प्राप्तिकी साधनस्वरूप 'संस्कृति' मानना ही उचित है । प्रत्येक मानव, यदि उसका लक्ष्य धर्म-प्राप्तिकी ओर हैं तो लोकमें पाई जानेवाली उक्त सभी संस्कृतियोंमेंसे किसी भी संस्कृतिको अपनाकर उल्लिखित अविवादी धर्मको प्राप्त कर सकता है । संस्कृतिको ही धर्म मान लेनेकी भ्रान्तिपूर्ण प्रचलित परिपाटीसे हिन्दू, जैन आदि सभी वर्गोंका उक्त वास्तविक धर्मकी ओर झुकाव ही नहीं रह गया है । इसीलिये इन वर्गों में विविध प्रकारके अनर्थकर विकारों, पाखण्डों एवं रूढ़ियोंको अधिक प्रश्रय मिला हुआ है और इस सबका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ उक्त वास्तविक धर्म मनुष्य के जीवनसे सर्वथा अलग होकर एक लोकोत्तर वस्तु मात्र रह गया है वहाँ मानवतासे विहीन तथा अन्याय और अत्याचारसे परिपूर्ण उच्छृङ्खल जीवनप्रवृत्तियों के सद्भावमें भी संस्कृतिका छद्मवेष धारण करने मात्रसे प्रत्येक मानव अपनेको और अपने वर्गको कट्टर धर्मात्मा समझ रहा है। इतना ही नहीं, अपनी संस्कृति से भिन्न दूसरी सभी संस्कृतियोंको अधर्म मानकर उनमें से किसी भी संस्कृति के माननेवाले व्यक्ति तथा वर्गको धर्मके उल्लिखित चिह्न मौजूद रहनेपर भी वह अधर्मात्मा ही मानना चाहता है और मानता है और एक ही संस्कृतिका उपासक वह व्यक्ति भी उसकी दृष्टिमें अधर्मात्मा ही है जो उस संस्कृतिके नियमोंकी ढोंगपूर्वक ही सही, आवृत्ति करना जरूरी नहीं समझता है, भले ही वह अपने जीवनको धर्ममय बनानेका सच्चा प्रयत्न कर रहा हो। इस तरह आज प्रत्येक वर्ग और वर्ग के प्रत्येक मानव मानवताको कलंकित करनेवाले परस्पर विद्वेष, घृणा, ईर्षा और कलहके दर्दनाक चित्र दिखाई दे रहे हैं । यदि प्रत्येक मानव और प्रत्येक वर्ग धर्मकी उल्लिखित परिभाषाको ध्यान में रखते हुए उसे संस्कृतिका साध्य और संस्कृतिको उसका साधन मान लें तो उन्हें यह बात सरलताके साथ समझमें आजायगी कि वही संस्कृति सच्ची और उपादेय हो सकती है तथा उस सस्कृतिको ही लोकमें जीवित रहने का अधिकार प्राप्त हो सकता है जो मानव जगत्को धर्मकी ओर अग्रसर करा सके और ऐसा होनेपर प्रत्येक मानव तथा प्रत्येक वर्ग
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org