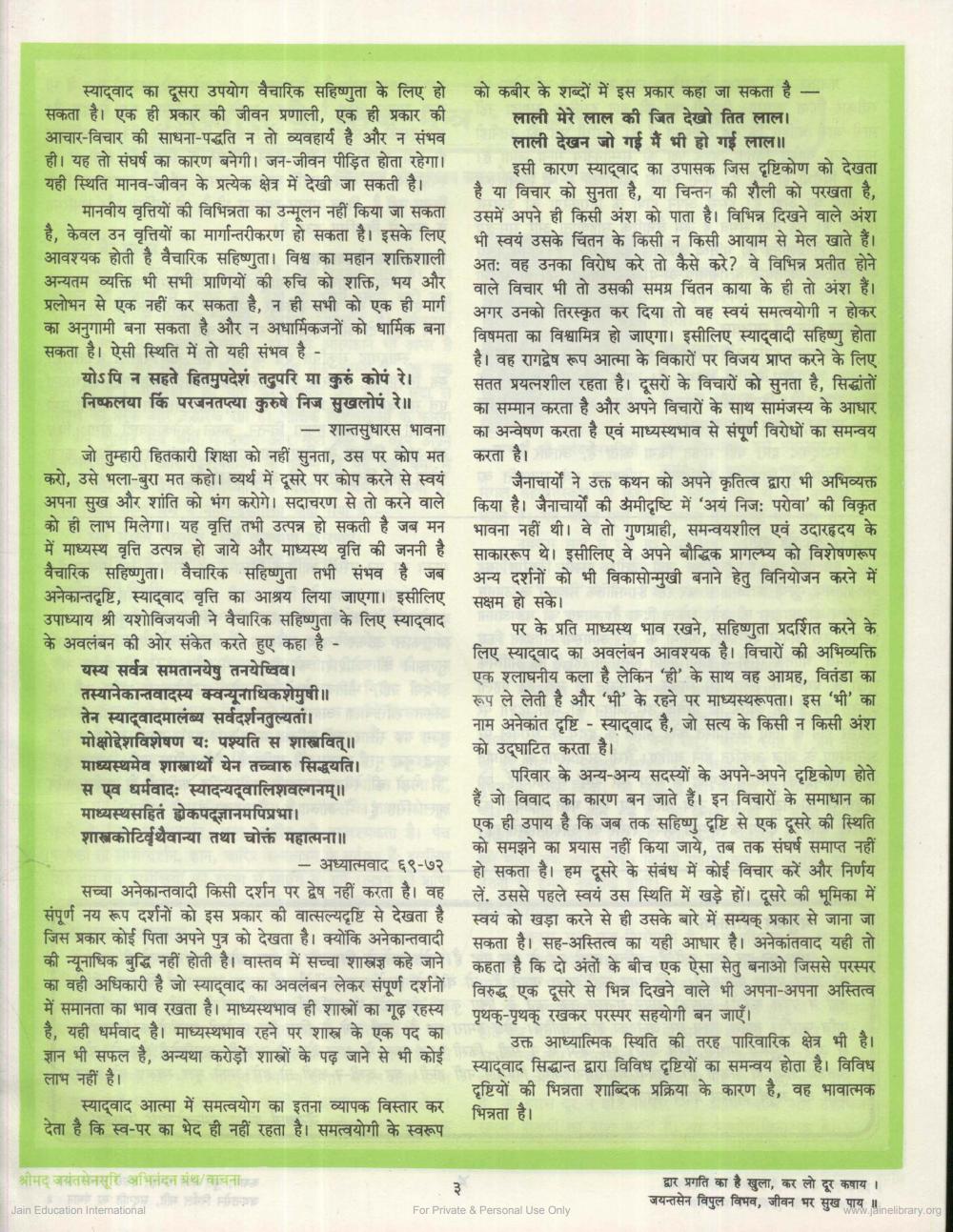________________
स्याद्वाद का दूसरा उपयोग वैचारिक सहिष्णुता के लिए हो को कबीर के शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है - सकता है। एक ही प्रकार की जीवन प्रणाली, एक ही प्रकार की लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। आचार-विचार की साधना-पद्धति न तो व्यवहार्य है और न संभव लाली देखन जो गई मैं भी हो गई लाल॥ ही। यह तो संघर्ष का कारण बनेगी। जन-जीवन पीड़ित होता रहेगा।
इसी कारण स्याद्वाद का उपासक जिस दृष्टिकोण को देखता यही स्थिति मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखी जा सकती है।
है या विचार को सुनता है, या चिन्तन की शैली को परखता है, मानवीय वृत्तियों की विभिन्नता का उन्मूलन नहीं किया जा सकता उसमें अपने ही किसी अंश को पाता है। विभिन्न दिखने वाले अंश है, केवल उन वृत्तियों का मार्गान्तरीकरण हो सकता है। इसके लिए
भी स्वयं उसके चिंतन के किसी न किसी आयाम से मेल खाते हैं। आवश्यक होती है वैचारिक सहिष्णुता। विश्व का महान शक्तिशाली
अत: वह उनका विरोध करे तो कैसे करे? वे विभिन्न प्रतीत होने अन्यतम व्यक्ति भी सभी प्राणियों की रुचि को शक्ति, भय और
वाले विचार भी तो उसकी समग्र चिंतन काया के ही तो अंश हैं। प्रलोभन से एक नहीं कर सकता है, न ही सभी को एक ही मार्ग
अगर उनको तिरस्कृत कर दिया तो वह स्वयं समत्वयोगी न होकर का अनुगामी बना सकता है और न अधार्मिकजनों को धार्मिक बना
विषमता का विश्वामित्र हो जाएगा। इसीलिए स्यावादी सहिष्णु होता सकता है। ऐसी स्थिति में तो यही संभव है -
है। वह रागद्वेष रूप आत्मा के विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए योऽपि न सहते हितमुपदेशं तदुपरि मा कुलं को रे।
सतत प्रयत्नशील रहता है। दूसरों के विचारों को सुनता है, सिद्धांतों निष्कलया किं परजनतप्त्या कुरुषे निज सुखलोपं रे॥ का सम्मान करता है और अपने विचारों के साथ सामंजस्य के आधार
-शान्तसुधारस भावना का अन्वेषण करता है एवं माध्यस्थभाव से संपूर्ण विरोधों का समन्वय जो तुम्हारी हितकारी शिक्षा को नहीं सुनता, उस पर कोप मत करता है। करो, उसे भला-बुरा मत कहो। व्यर्थ में दूसरे पर कोप करने से स्वयं जैनाचार्यों ने उक्त कथन को अपने कृतित्व द्वारा भी अभिव्यक्त अपना सुख और शांति को भंग करोगे। सदाचरण से तो करने वाले किया है। जैनाचार्यों की अमीदृष्टि में 'अयं निजः परोवा' की विकृत को ही लाभ मिलेगा। यह वृत्ति तभी उत्पन्न हो सकती है जब मन भावना नहीं थी। वे तो गुणग्राही, समन्वयशील एवं उदारहृदय के में माध्यस्थ वृत्ति उत्पन्न हो जाये और माध्यस्थ वृत्ति की जननी है साकाररूप थे। इसीलिए वे अपने बौद्धिक प्रागल्भ्य को विशेषणरूप वैचारिक सहिष्णुता। वैचारिक सहिष्णुता तभी संभव है जब अन्य दर्शनों को भी विकासोन्मुखी बनाने हेतु विनियोजन करने में अनेकान्तदृष्टि, स्याद्वाद वृत्ति का आश्रय लिया जाएगा। इसीलिए सक्षम हो सके। उपाध्याय श्री यशोविजयजी ने वैचारिक सहिष्णुता के लिए स्याद्वाद
पर के प्रति माध्यस्थ भाव रखने, सहिष्णुता प्रदर्शित करने के के अवलंबन की ओर संकेत करते हुए कहा है -
लिए स्याद्वाद का अवलंबन आवश्यक है। विचारों की अभिव्यक्ति यस्य सर्वत्र समतानयेषु तनयेष्विव।।
एक श्लाघनीय कला है लेकिन 'ही' के साथ वह आग्रह, वितंडा का तस्यानेकान्तवादस्य क्वन्यूनाधिकशेमुषी॥
रूप ले लेती है और 'भी' के रहने पर माध्यस्थरूपता। इस 'भी' का तेन स्याद्वादमालंब्य सर्वदर्शनतुल्यतां।
नाम अनेकांत दृष्टि - स्याद्वाद है, जो सत्य के किसी न किसी अंश मोक्षोद्देशविशेषण यः पश्यति स शास्ववित्॥
को उद्घाटित करता है। माध्यस्थमेव शास्त्रार्थो येन तच्चारु सिद्धयति।
परिवार के अन्य-अन्य सदस्यों के अपने-अपने दृष्टिकोण होते स एव धर्मवादः स्यादन्यद्वालिशवल्गनम्॥
हैं जो विवाद का कारण बन जाते हैं। इन विचारों के समाधान का माध्यस्थसहितं होकपद्ज्ञानमपिप्रभा।
एक ही उपाय है कि जब तक सहिष्णु दृष्टि से एक दूसरे की स्थिति शास्त्रकोटिर्वथैवान्या तथा चोक्तं महात्मना।
को समझने का प्रयास नहीं किया जाये, तब तक संघर्ष समाप्त नहीं
- अध्यात्मवाद ६९-७२ हो सकता है। हम दूसरे के संबंध में कोई विचार करें और निर्णय सच्चा अनेकान्तवादी किसी दर्शन पर द्वेष नहीं करता है। वह लें. उससे पहले स्वयं उस स्थिति में खड़े हों। दूसरे की भूमिका में संपूर्ण नय रूप दर्शनों को इस प्रकार की वात्सल्यदृष्टि से देखता है स्वयं को खड़ा करने से ही उसके बारे में सम्यक प्रकार से जाना जा जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र को देखता है। क्योंकि अनेकान्तवादी सकता है। सह-अस्तित्व का यही आधार है। अनेकांतवाद यही तो की न्यूनाधिक बुद्धि नहीं होती है। वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहे जाने कहता है कि दो अंतों के बीच एक ऐसा सेतु बनाओ जिससे परस्पर का वही अधिकारी है जो स्याद्वाद का अवलंबन लेकर संपूर्ण दर्शनों
विरुद्ध एक दूसरे से भिन्न दिखने वाले भी अपना-अपना अस्तित्व में समानता का भाव रखता है। माध्यस्थभाव ही शास्त्रों का गूढ रहस्य
पृथक्-पृथक् रखकर परस्पर सहयोगी बन जाएँ। है, यही धर्मवाद है। माध्यस्थभाव रहने पर शास्त्र के एक पद का
उक्त आध्यात्मिक स्थिति की तरह पारिवारिक क्षेत्र भी है। ज्ञान भी सफल है, अन्यथा करोड़ों शास्त्रों के पढ़ जाने से भी कोई
स्याद्वाद सिद्धान्त द्वारा विविध दृष्टियों का समन्वय होता है। विविध लाभ नहीं है।
दृष्टियों की भिन्नता शाब्दिक प्रक्रिया के कारण है, वह भावात्मक स्यादवाद आत्मा में समत्वयोग का इतना व्यापक विस्तार कर मिलता है। देता है कि स्व-पर का भेद ही नहीं रहता है। समत्वयोगी के स्वरूप
श्रीमद् जयंतसेनसूरि अभिनंदन थ/वाचनालय
द्वार प्रगति का है खुला, कर लो दूर कषाय । जयन्तसेन विपुल विभव, जीवन भर सुख पाय linelibrary.org
Jain Education International
For Private & Personal Use Only