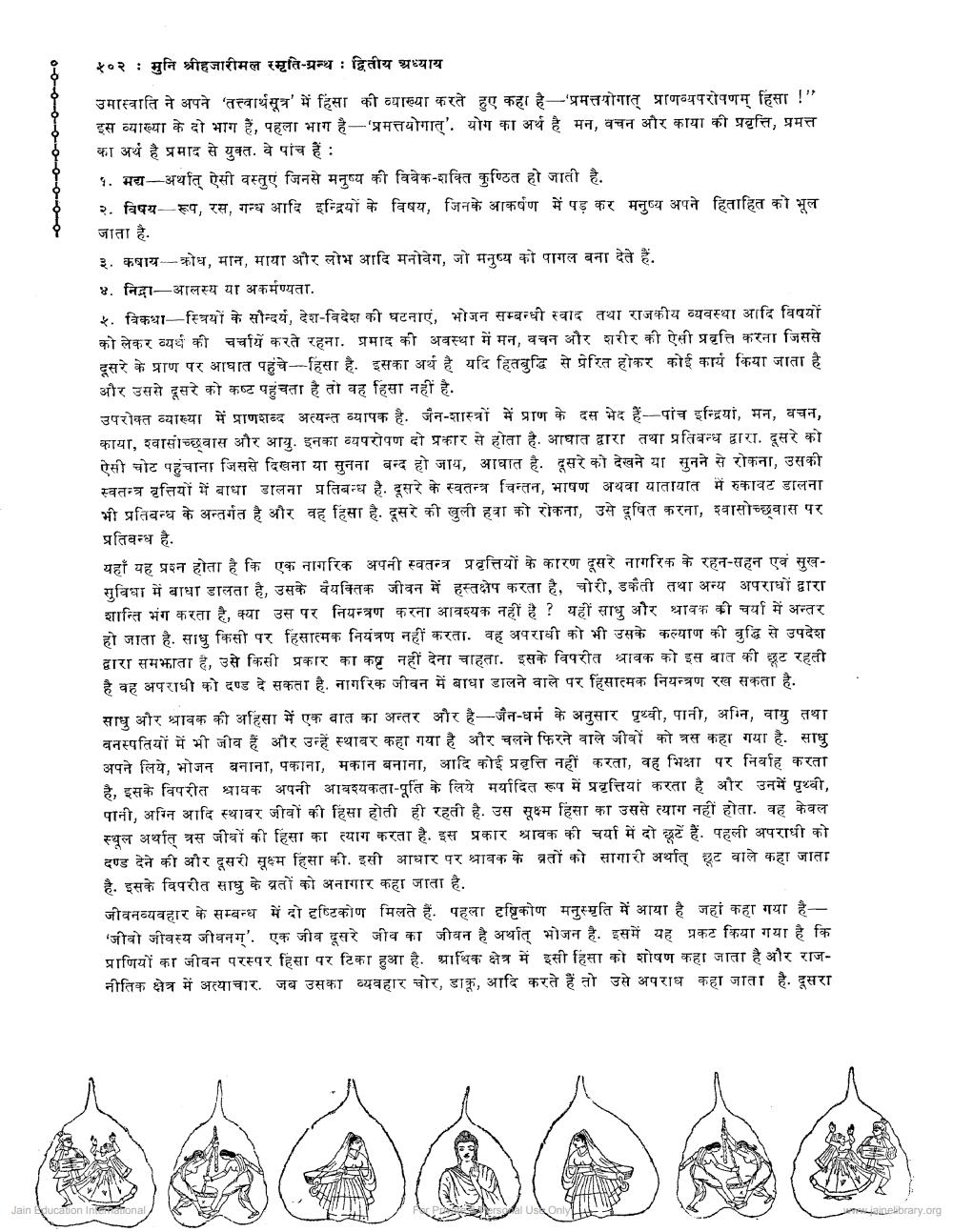________________
२०२ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : द्वितीय अध्याय
-0-0--0--0-0--0--0-0-0-0
उमास्वाति ने अपने 'तत्त्वार्थसूत्र' में हिंसा की व्याख्या करते हुए कहा है-'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणम् हिसा !" इस व्याख्या के दो भाग हैं, पहला भाग है-'प्रमत्तयोगात्'. योग का अर्थ है मन, वचन और काया की प्रवृत्ति, प्रमत्त का अर्थ है प्रमाद से युक्त. वे पांच हैं : १. मद्य-अर्थात् ऐसी वस्तुएं जिनसे मनुष्य की विवेक-शक्ति कुण्ठित हो जाती है. २. विषय-रूप, रस, गन्ध आदि इन्द्रियों के विषय, जिनके आकर्षण में पड़ कर मनुष्य अपने हिताहित को भूल जाता है. ३. कषाय-क्रोध, मान, माया और लोभ आदि मनोवेग, जो मनुष्य को पागल बना देते हैं. ४. निद्रा-आलस्य या अकर्मण्यता. १. विकथा-स्त्रियों के सौन्दर्य, देश-विदेश की घटनाएं, भोजन सम्बन्धी स्वाद तथा राजकीय व्यवस्था आदि विषयों को लेकर व्यर्थ की चर्चायें करते रहना. प्रमाद की अवस्था में मन, वचन और शरीर की ऐसी प्रवृत्ति करना जिससे दूसरे के प्राण पर आघात पहुंचे-हिसा है. इसका अर्थ है यदि हितबुद्धि से प्रेरित होकर कोई कार्य किया जाता है और उससे दूसरे को कष्ट पहुंचता है तो वह हिंसा नहीं है. उपरोक्त व्याख्या में प्राणशब्द अत्यन्त व्यापक है. जैन-शास्त्रों में प्राण के दस भेद हैं-पांच इन्द्रियां, मन, वचन, काया, श्वासोच्छ्वास और आयु. इनका व्यपरोपण दो प्रकार से होता है. आघात द्वारा तथा प्रतिबन्ध द्वारा. दूसरे को ऐसी चोट पहुंचाना जिससे दिखना या सुनना बन्द हो जाय, आघात है. दूसरे को देखने या सुनने से रोकना, उसकी स्वतन्त्र वृत्तियों में बाधा डालना प्रतिबन्ध है. दूसरे के स्वतन्त्र चिन्तन, भाषण अथवा यातायात में रुकावट डालना भी प्रतिबन्ध के अन्तर्गत है और वह हिंसा है. दूसरे की खुली हवा को रोकना, उसे दूषित करना, श्वासोच्छ्वास पर प्रतिबन्ध है. यहाँ यह प्रश्न होता है कि एक नागरिक अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्तियों के कारण दूसरे नागरिक के रहन-सहन एवं सुखसुविधा में बाधा डालता है, उसके वैयक्तिक जीवन में हस्तक्षेप करता है, चोरी, डकैती तथा अन्य अपराधों द्वारा शान्ति भंग करता है, क्या उस पर नियन्त्रण करना आवश्यक नहीं है ? यहीं साधु और श्रावक की चर्या में अन्तर हो जाता है. साधु किसी पर हिंसात्मक नियंत्रण नहीं करता. वह अपराधी को भी उसके कल्याण की बुद्धि से उपदेश द्वारा समझाता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता. इसके विपरीत श्रावक को इस बात की छूट रहती है वह अपराधी को दण्ड दे सकता है. नागरिक जीवन में बाधा डालने वाले पर हिंसात्मक नियन्त्रण रख सकता है. साधु और श्रावक की अहिंसा में एक बात का अन्तर और है-जैन-धर्म के अनुसार पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा वनस्पतियों में भी जीव हैं और उन्हें स्थावर कहा गया है और चलने फिरने वाले जीवों को त्रस कहा गया है. साधु अपने लिये, भोजन बनाना, पकाना, मकान बनाना, आदि कोई प्रवृत्ति नहीं करता, वह भिक्षा पर निर्वाह करता है, इसके विपरीत श्रावक अपनी आवश्यकता-पूर्ति के लिये मर्यादित रूप में प्रवृत्तियां करता है और उनमें पृथ्वी, पानी, अग्नि आदि स्थावर जीवों की हिंसा होती ही रहती है. उस सूक्ष्म हिंसा का उससे त्याग नहीं होता. वह केवल स्थूल अर्थात् त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करता है. इस प्रकार श्रावक की चर्या में दो छूटें हैं. पहली अपराधी को दण्ड देने की और दूसरी सूक्ष्म हिंसा की. इसी आधार पर श्रावक के व्रतों को सागारी अर्थात् छूट वाले कहा जाता है. इसके विपरीत साधु के व्रतों को अनागार कहा जाता है. जीवनव्यवहार के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण मिलते हैं. पहला दृष्टिकोण मनुस्मृति में आया है जहां कहा गया है'जीवो जीवस्य जीवनम्'. एक जीव दूसरे जीव का जीवन है अर्थात् भोजन है. इसमें यह प्रकट किया गया है कि प्राणियों का जीवन परस्पर हिंसा पर टिका हुआ है. आर्थिक क्षेत्र में इसी हिसा को शोषण कहा जाता है और राजनीतिक क्षेत्र में अत्याचार. जब उसका व्यवहार चोर, डाकू, आदि करते हैं तो उसे अपराध कहा जाता है. दूसरा
Jain
ducation
Jainelibrary.org