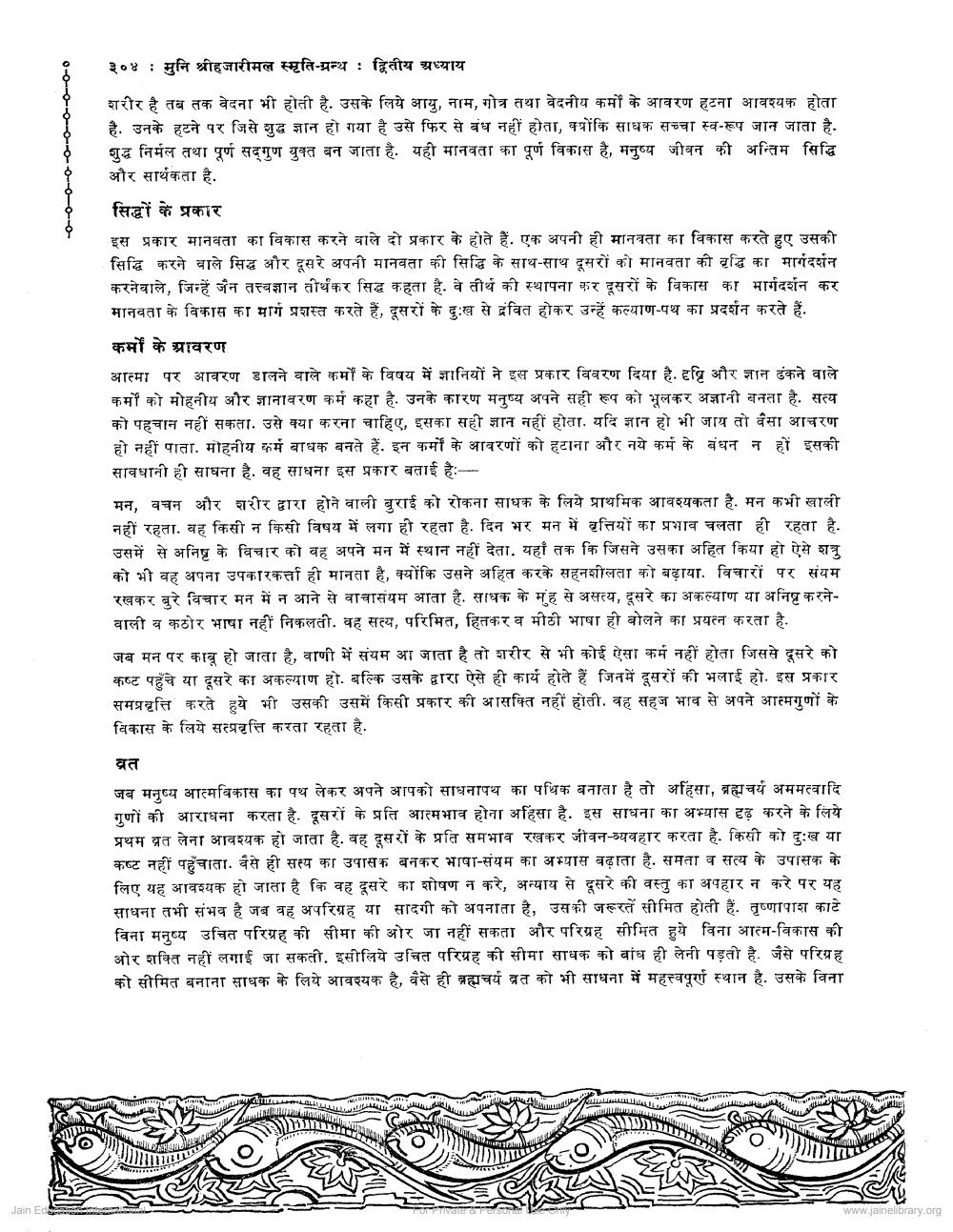________________
Jain Ed
0-0-0-0-0-0
३०४ : मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ : द्वितीय अध्याय
शरीर है तब तक वेदना भी होती है. उसके लिये आयु, नाम, गोत्र तथा वेदनीय कर्मों के आवरण हटना आवश्यक होता है. उनके हटने पर जिसे शुद्ध ज्ञान हो गया है उसे फिर से बंध नहीं होता, क्योंकि साधक सच्चा स्व-रूप जान जाता हैशुद्ध निर्मल तथा पूर्ण सद्गुण युक्त बन जाता है. यही मानवता का पूर्ण विकास है, मनुष्य जीवन की अन्तिम सिद्धि और सार्थकता है.
सिद्धों के प्रकार
इस प्रकार मानवता का विकास करने वाले दो प्रकार के होते हैं. एक अपनी ही मानवता का विकास करते हुए उसकी सिद्धि करने वाले सिद्ध और दूसरे अपनी मानवता की सिद्धि के साथ-साथ दूसरों को मानवता की वृद्धि का मार्गदर्शन करनेवाले, जिन्हें जैन तत्त्वज्ञान तीर्थंकर सिद्ध कहता है. वे तीर्थ की स्थापना कर दूसरों के विकास का मार्गदर्शन कर मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, दूसरों के दुःख से द्रवित होकर उन्हें कल्याण पथ का प्रदर्शन करते हैं.
कर्मों के प्रावरण
आत्मा पर आवरण डालने वाले कर्मों के विषय में ज्ञानियों ने इस प्रकार विवरण दिया है. दृष्टि और ज्ञान ढंकने वाले कर्मों को मोहनीय और ज्ञानावरण कर्म कहा है. उनके कारण मनुष्य अपने सही रूप को भूलकर अज्ञानी बनता है. सत्य को पहचान नहीं सकता. उसे क्या करना चाहिए, इसका सही ज्ञान नहीं होता. यदि ज्ञान हो भी जाय तो वैसा आचरण हो नहीं पाता. मोहनीय कर्म बाधक बनते हैं. इन कर्मों के आवरणों को हटाना और नये कर्म के बंधन न हों इसकी सावधानी ही साधना है. वह साधना इस प्रकार बताई है:
मन, वचन और शरीर द्वारा होने वाली बुराई को रोकना साधक के लिये प्राथमिक आवश्यकता है. मन कभी खाली नहीं रहता. वह किसी न किसी विषय में लगा ही रहता है. दिन भर मन में वृत्तियों का प्रभाव चलता ही रहता है. उसमें से अनिष्ट के विचार को वह अपने मन में स्थान नहीं देता. यहाँ तक कि जिसने उसका अहित किया हो ऐसे शत्रु को भी वह अपना उपकारकर्त्ता ही मानता है, क्योंकि उसने अहित करके सहनशीलता को बढ़ाया. विचारों पर संयम रखकर बुरे विचार मन में न आने से वाचासंयम आता है. साधक के मुंह से असत्य, दूसरे का अकल्याण या अनिष्ट करनेवाली व कठोर भाषा नहीं निकलती. वह सत्य, परिमित, हितकर व मीठी भाषा ही बोलने का प्रयत्न करता है.
जब मन पर काबू हो जाता है, वाणी में संयम आ जाता है तो शरीर से भी कोई ऐसा कर्म नहीं होता जिससे दूसरे को कष्ट पहुँचे या दूसरे का अकल्याण हो. बल्कि उसके द्वारा ऐसे ही कार्य होते हैं जिनमें दूसरों की भलाई हो. इस प्रकार समप्रवृत्ति करते हुये भी उसकी उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती. वह सहज भाव से अपने आत्मगुणों के विकास के लिये सत्प्रवृत्ति करता रहता है.
व्रत
जब मनुष्य आत्मविकास का पथ लेकर अपने आपको साधनापथ का पथिक बनाता है तो अहिंसा, ब्रह्मचर्य अममत्वादि गुणों की आराधना करता है. दूसरों के प्रति आत्मभाव होना अहिंसा है. इस साधना का अभ्यास दृढ़ करने के लिये प्रथम व्रत लेना आवश्यक हो जाता है. वह दूसरों के प्रति समभाव रखकर जीवन व्यवहार करता है. किसी को दुःख या कष्ट नहीं पहुँचाता. वैसे ही सत्य का उपासक बनकर भाषा-संयम का अभ्यास बढ़ाता है. समता व सत्य के उपासक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह दूसरे का शोषण न करे, अन्याय से दूसरे की वस्तु का अपहार न करे पर यह साधना तभी संभव है जब वह अपरिग्रह या सादगी को अपनाता है, उसकी जरूरतें सीमित होती हैं. तृष्णापाश काटे विना मनुष्य उचित परिग्रह की सीमा की ओर जा नहीं सकता और परिग्रह सीमित हुये विना आत्म विकास की ओर शक्ति नहीं लगाई जा सकती. इसीलिये उचित परिग्रह की सीमा साधक को बांध ही लेनी पड़ती है. जैसे परिग्रह को सीमित बनाना साधक के लिये आवश्यक है, वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत को भी साधना में महत्वपूर्ण स्थान है. उसके विना
For Private & Persona
www.jainelibrary.org