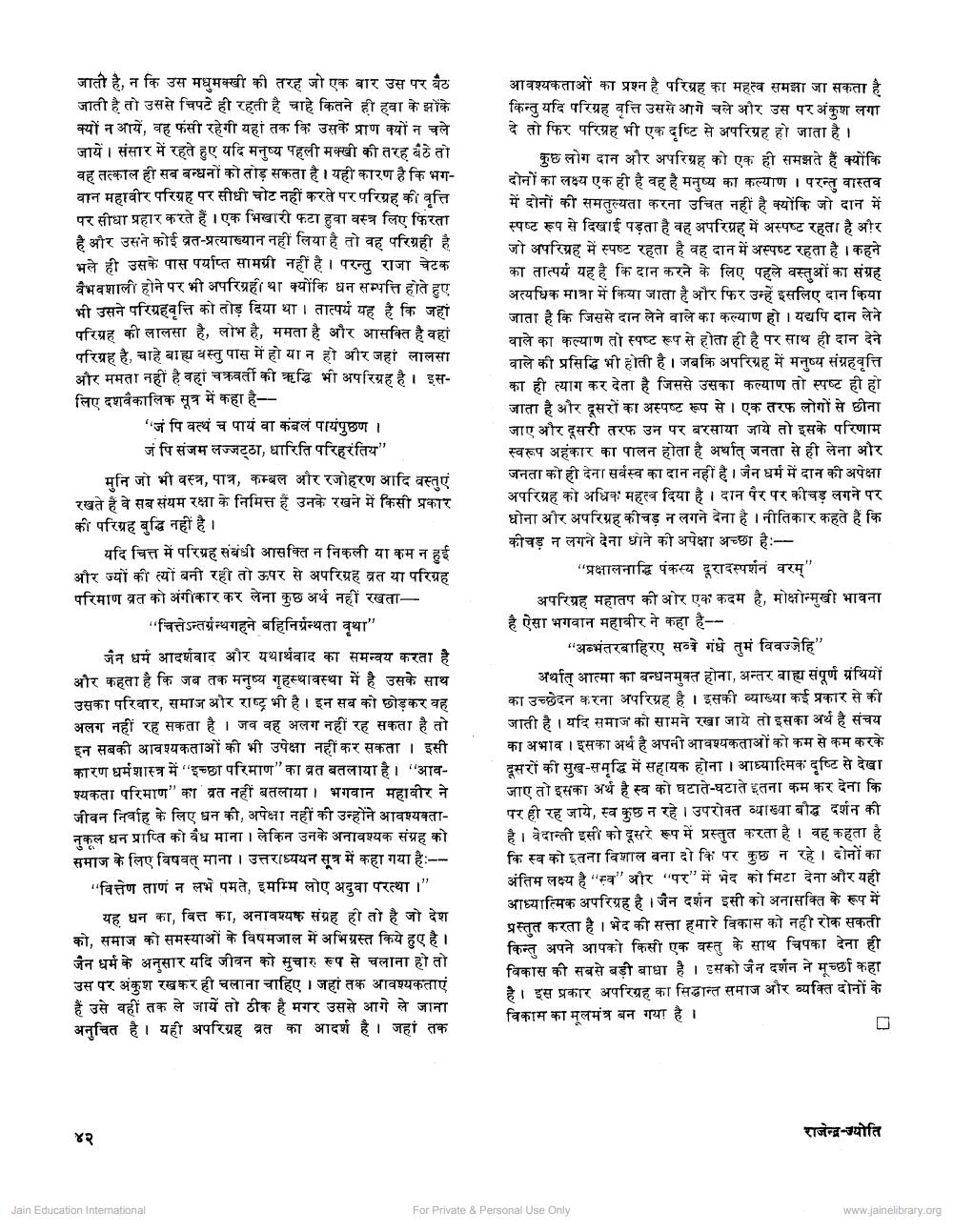________________
जाती है, न कि उस मधुमक्खी की तरह जो एक बार उस पर बैठ जाती है तो उससे चिपटे ही रहती है चाहे कितने ही हवा के झोंके क्यों न आयें, वह फंसी रहेगी यहां तक कि उसके प्राण क्यों न चले जायें। संसार में रहते हुए यदि मनुष्य पहली मक्खी की तरह बैठे तो वह तत्काल ही सब बन्धनों को तोड़ सकता है। यही कारण है कि भगवान महावीर परिग्रह पर सीधी चोट नहीं करते पर परिग्रह की वृत्ति पर सीधा प्रहार करते हैं । एक भिखारी फटा हुवा वस्त्र लिए फिरता है और उसने कोई व्रत-प्रत्याख्यान नहीं लिया है तो वह परिग्रही हैं भले ही उसके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है। परन्तु राजा चेटक वैभवशाली होने पर भी अपरिग्रही था क्योंकि धन सम्पत्ति होते हुए भी उसने परिग्रहवृत्ति को तोड़ दिया था। तात्पर्य यह है कि जहां परिग्रह की लालसा है, लोभ है, ममता है और आसक्ति है वहां परिग्रह है, चाहे बाह्य वस्तु पास में हो या न हो और जहां लालसा
और ममता नहीं है वहां चक्रवर्ती की ऋद्धि भी अपरिग्रह है। इसलिए दशवकालिक सूत्र में कहा है
"ज पि वत्थं च पायं वा कंबलं पायंपुछण ।
जं पि संजम लज्जट्ठा, धारिति परिहरंतिय" मनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण आदि बस्तुएं रखते हैं वे सब संयम रक्षा के निमित्त हैं उनके रखने में किसी प्रकार की परिग्रह बुद्धि नहीं है।
यदि चित्त में परिग्रह संबंधी आसक्ति न निकली या कम न हुई और ज्यों की त्यों बनी रही तो ऊपर से अपरिग्रह व्रत या परिग्रह परिमाण व्रत को अंगीकार कर लेना कुछ अर्थ नहीं रखता
“चित्तेऽन्तर्ग्रन्थगहने बहिनिर्ग्रन्थता वृथा" जैन धर्म आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय करता है और कहता है कि जब तक मनुष्य गृहस्थावस्था में है उसके साथ उसका परिवार, समाज और राष्ट्र भी है। इन सब को छोड़कर वह अलग नहीं रह सकता है । जव वह अलग नहीं रह सकता है तो इन सबकी आवश्यकताओं की भी उपेक्षा नहीं कर सकता । इसी कारण धर्मशास्त्र में "इच्छा परिमाण" का व्रत बतलाया है। "आवश्यकता परिमाण" का व्रत नहीं बतलाया। भगवान महावीर ने जीवन निर्वाह के लिए धन की, अपेक्षा नहीं की उन्होंने आवश्यक्तानकल धन प्राप्ति को वैध माना । लेकिन उनके अनावश्यक संग्रह को समाज के लिए विषवत् माना । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है:-- "वित्तेण ताणं न लभे पमते, इमम्मि लोए अदुवा परत्था।"
यह धन का, वित्त का, अनावश्यक संग्रह ही तो है जो देश को, समाज को समस्याओं के विषमजाल में अभिग्रस्त किये हुए है। जैन धर्म के अनुसार यदि जीवन को सुचारु रूप से चलाना हो तो उस पर अंकुश रख कर ही चलाना चाहिए। जहां तक आवश्यकताएं हैं उसे वहीं तक ले जायें तो ठीक है मगर उससे आगे ले जाना अनुचित है। यही अपरिग्रह व्रत का आदर्श है। जहां तक
आवश्यकताओं का प्रश्न है परिग्रह का महत्व समझा जा सकता है किन्तु यदि परिग्रह बत्ति उससे आगे चले और उस पर अंकुश लगा दे तो फिर परिग्रह भी एक दृष्टि से अपरिग्रह हो जाता है।
कुछ लोग दान और अपरिग्रह को एक ही समझते हैं क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है वह है मनुष्य का कल्याण । परन्तु वास्तव में दोनों की समतुल्यता करना उचित नहीं है क्योंकि जो दान में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है वह अपरिग्रह में अस्पष्ट रहता है और जो अपरिग्रह में स्पष्ट रहता है वह दान में अस्पष्ट रहता है । कहने का तात्पर्य यह है कि दान करने के लिए पहले वस्तुओं का संग्रह अत्यधिक मात्रा में किया जाता है और फिर उन्हें इसलिए दान किया जाता है कि जिससे दान लेने वाले का कल्याण हो । यद्यपि दान लेने वाले का कल्याण तो स्पष्ट रूप से होता ही है पर साथ ही दान देने वाले की प्रसिद्धि भी होती है। जबकि अपरिग्रह में मनुष्य संग्रहवृत्ति का ही त्याग कर देता है जिससे उसका कल्याण तो स्पष्ट ही हो जाता है और दूसरों का अस्पष्ट रूप से । एक तरफ लोगों से छीना जाए और दूसरी तरफ उन पर बरसाया जाये तो इसके परिणाम स्वरूप अहंकार का पालन होता है अर्थात् जनता से ही लेना और जनता को ही देना सर्वस्व का दान नहीं है। जैन धर्म में दान की अपेक्षा अपरिग्रह को अधिक महत्व दिया है । दान पैर पर कीचड़ लगने पर धोना और अपरिग्रह कीचड़ न लगने देना है । नीतिकार कहते हैं कि कीचड़ न लगने देना धोने की अपेक्षा अच्छा है:
"प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम्" अपरिग्रह महातप की ओर एक कदम है, मोक्षोन्मुखी भावना है ऐसा भगवान महावीर ने कहा है--
"अब्भंतरबाहिरए सब्वे गंधे तुम विवज्जेहि" अर्थात् आत्मा का बन्धनमुक्त होना, अन्तर बाह्य संपूर्ण ग्रंथियों का उच्छेदन करना अपरिग्रह है । इसकी व्याख्या कई प्रकार से की जाती है। यदि समाज को सामने रखा जाये तो इसका अर्थ है संचय का अभाव । इसका अर्थ है अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करके दूसरों की सुख-समृद्धि में सहायक होना । आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ है स्व को घटाते-घटाते इतना कम कर देना कि पर ही रह जाये, स्व कुछ न रहे । उपरोक्त व्याख्या बौद्ध दर्शन की है। वेदान्ती इसी को दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है । वह कहता है कि स्व को इतना विशाल बना दो कि पर कुछ न रहे। दोनों का अंतिम लक्ष्य है "स्व" और "पर" में भेद को मिटा देना और यही आध्यात्मिक अपरिग्रह है । जैन दर्शन इसी को अनासक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है । भेद की सत्ता हमारे विकास को नहीं रोक सकती किन्तु अपने आपको किसी एक वस्तु के साथ चिपका देना ही विकास की सबसे बड़ी बाधा है । इसको जैन दर्शन ने मूच्र्छा कहा है। इस प्रकार अपरिग्रह का सिद्धान्त समाज और व्यक्ति दोनों के विकाम का मूलमंत्र बन गया है ।
राजेन्द्र-ज्योति
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org