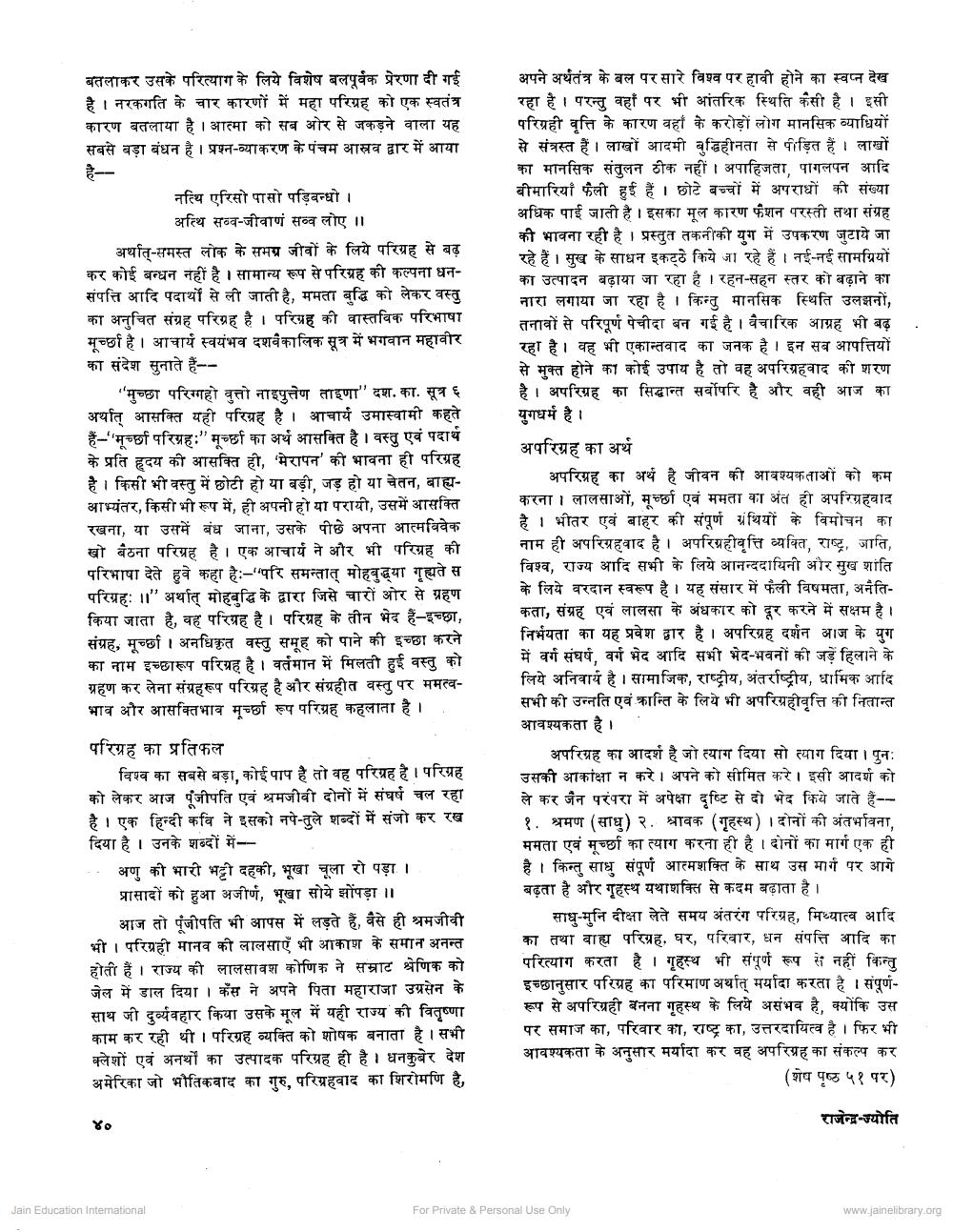________________
बतलाकर उसके परित्याग के लिये विशेष बलपूर्वक प्रेरणा दी गई है। नरकगति के चार कारणों में महा परिग्रह को एक स्वतंत्र कारण बतलाया है । आत्मा को सब ओर से जकड़ने वाला यह सबसे बड़ा बंधन है । प्रश्न-व्याकरण के पंचम आस्रव द्वार में आया
नत्थि एरिसो पासो पड़िबन्धो ।
अत्थि सव्व-जीवाणं सव्व लोए । अर्थात्-समस्त लोक के समग्र जीवों के लिये परिग्रह से बढ़ कर कोई बन्धन नहीं है । सामान्य रूप से परिग्रह की कल्पना धनसंपत्ति आदि पदार्थों से ली जाती है, ममता बुद्धि को लेकर वस्तु का अनुचित संग्रह परिग्रह है । परिग्रह की वास्तविक परिभाषा मूर्छा है। आचार्य स्वयंभव दशवकालिक सूत्र में भगवान महावीर का संदेश सुनाते हैं--
"मुच्छा परिग्गहो वुत्तो नाइपुत्तेण ताइणा" दश. का. सूत्र ६ अर्थात् आसक्ति यही परिग्रह है। आचार्य उमास्वामी कहते हैं-'
मूर्छा परिग्रहः" मूर्छा का अर्थ आसक्ति है । वस्तु एवं पदार्थ के प्रति हृदय की आसक्ति ही, 'मेरापन' की भावना ही परिग्रह है। किसी भी वस्तु में छोटी हो या बड़ी, जड़ हो या चेतन, बाह्यआभ्यंतर, किसी भी रूप में, ही अपनी हो या परायी, उसमें आसक्ति रखना, या उसमें बंध जाना, उसके पीछे अपना आत्मविवेक खो बैठना परिग्रह है। एक आचार्य ने और भी परिग्रह की परिभाषा देते हुवे कहा है:-"परि समन्तात् मोहबुद्ध्या गृह्यते स परिग्रहः ।।" अर्थात् मोहबुद्धि के द्वारा जिसे चारों ओर से ग्रहण किया जाता है, वह परिग्रह है। परिग्रह के तीन भेद हैं-इच्छा, संग्रह, मूर्छा । अनधिकृत वस्तु समूह को पाने की इच्छा करने का नाम इच्छारूप परिग्रह है। वर्तमान में मिलती हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना संग्रहरूप परिग्रह है और संग्रहीत वस्तु पर ममत्वभाव और आसक्तिभाव मूर्छा रूप परिग्रह कहलाता है। . परिग्रह का प्रतिफल
विश्व का सबसे बड़ा, कोई पाप है तो वह परिग्रह है । परिग्रह को लेकर आज पूंजीपति एवं श्रमजीवी दोनों में संघर्ष चल रहा है। एक हिन्दी कवि ने इसको नपे-तुले शब्दों में संजो कर रख दिया है । उनके शब्दों में
अणु की भारी भट्टी दहकी, भूखा चूला रो पड़ा। प्रासादों को हुआ अजीर्ण, भूखा सोये झोंपड़ा।
आज तो पूंजीपति भी आपस में लड़ते हैं, वैसे ही श्रमजीवी भी । परिग्रही मानव की लालसाएँ भी आकाश के समान अनन्त होती हैं। राज्य की लालसावश कोणिक ने सम्राट' श्रेणिक को जेल में डाल दिया। कैंस ने अपने पिता महाराजा उग्रसेन के साथ जी दुर्व्यवहार किया उसके मूल में यही राज्य की वितृष्णा काम कर रही थी। परिग्रह व्यक्ति को शोषक बनाता है । सभी क्लेशों एवं अनर्थों का उत्पादक परिग्रह ही है। धनकुबेर देश अमेरिका जो भौतिकवाद का गुरु, परिग्रहवाद का शिरोमणि है,
अपने अर्थतंत्र के बल पर सारे विश्व पर हावी होने का स्वप्न देख रहा है । परन्तु वहाँ पर भी आंतरिक स्थिति कैसी है । इसी परिग्रही वृत्ति के कारण वहाँ के करोड़ों लोग मानसिक व्याधियों से संत्रस्त हैं । लाखों आदमी बुद्धिहीनता से पीड़ित हैं। लाखों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। अपाहिजता, पागलपन आदि बीमारियां फैली हुई हैं। छोटे बच्चों में अपराधों की संख्या अधिक पाई जाती है । इसका मूल कारण फैशन परस्ती तथा संग्रह की भावना रही है । प्रस्तुत तकनीकी युग में उपकरण जुटाये जा रहे हैं। सुख के साधन इकट्ठे किये जा रहे हैं। नई-नई सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है । रहन-सहन स्तर को बढ़ाने का नारा लगाया जा रहा है । किन्तु मानसिक स्थिति उलझनों, तनावों से परिपूर्ण पेचीदा बन गई है । वैचारिक आग्रह भी बढ़ रहा है। वह भी एकान्तवाद का जनक है। इन सब आपत्तियों से मुक्त होने का कोई उपाय है तो वह अपरिग्रहवाद की शरण है। अपरिग्रह का सिद्धान्त सर्वोपरि है और वही आज का युगधर्म है। अपरिग्रह का अर्थ
अपरिग्रह का अर्थ है जीवन की आवश्यकताओं को कम करना। लालसाओं, मूर्छा एवं ममता का अंत ही अपरिग्रहवाद है । भीतर एवं बाहर की संपूर्ण ग्रंथियों के विमोचन का नाम ही अपरिग्रहवाद है। अपरिग्रहीवृत्ति व्यक्ति, राष्ट्र, जाति, विश्व, राज्य आदि सभी के लिये आनन्ददायिनी और सुख शांति के लिये वरदान स्वरूप है। यह संसार में फैली विषमता, अनैतिकता, संग्रह एवं लालसा के अंधकार को दूर करने में सक्षम है। निर्भयता का यह प्रवेश द्वार है । अपरिग्रह दर्शन आज के युग में वर्ग संघर्ष, वर्ग भेद आदि सभी भेद-भवनों की जड़ें हिलाने के लिये अनिवार्य है । सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, धार्मिक आदि सभी की उन्नति एवं क्रान्ति के लिये भी अपरिग्रहीवृत्ति की नितान्त आवश्यकता है।
अपरिग्रह का आदर्श है जो त्याग दिया सो त्याग दिया। पुनः उसकी आकांक्षा न करे। अपने को सीमित करे। इसी आदर्श को ले कर जैन परंपरा में अपेक्षा दृष्टि से दो भेद किये जाते हैं-- १. श्रमण (साधु) २. श्रावक (गृहस्थ) । दोनों की अंतर्भावना, ममता एवं मूर्छा का त्याग करना ही है । दोनों का मार्ग एक ही है। किन्तु साधु संपूर्ण आत्मशक्ति के साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ता है और गृहस्थ यथाशक्ति से कदम बढ़ाता है। ___साधु-मुनि दीक्षा लेते समय अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व आदि का तथा बाह्य परिग्रह, घर, परिवार, धन संपत्ति आदि का परित्याग करता है । गृहस्थ भी संपूर्ण रूप से नहीं किन्तु इच्छानुसार परिग्रह का परिमाण अर्थात् मर्यादा करता है । संपूर्णरूप से अपरिग्रही बनना गृहस्थ के लिये असंभव है, क्योंकि उस पर समाज का, परिवार का, राष्ट्र का, उत्तरदायित्व है । फिर भी आवश्यकता के अनुसार मर्यादा कर वह अपरिग्रह का संकल्प कर
(शेष पृष्ठ ५१ पर)
४०
राजेन्द्र-ज्योति
Jain Education Interational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org