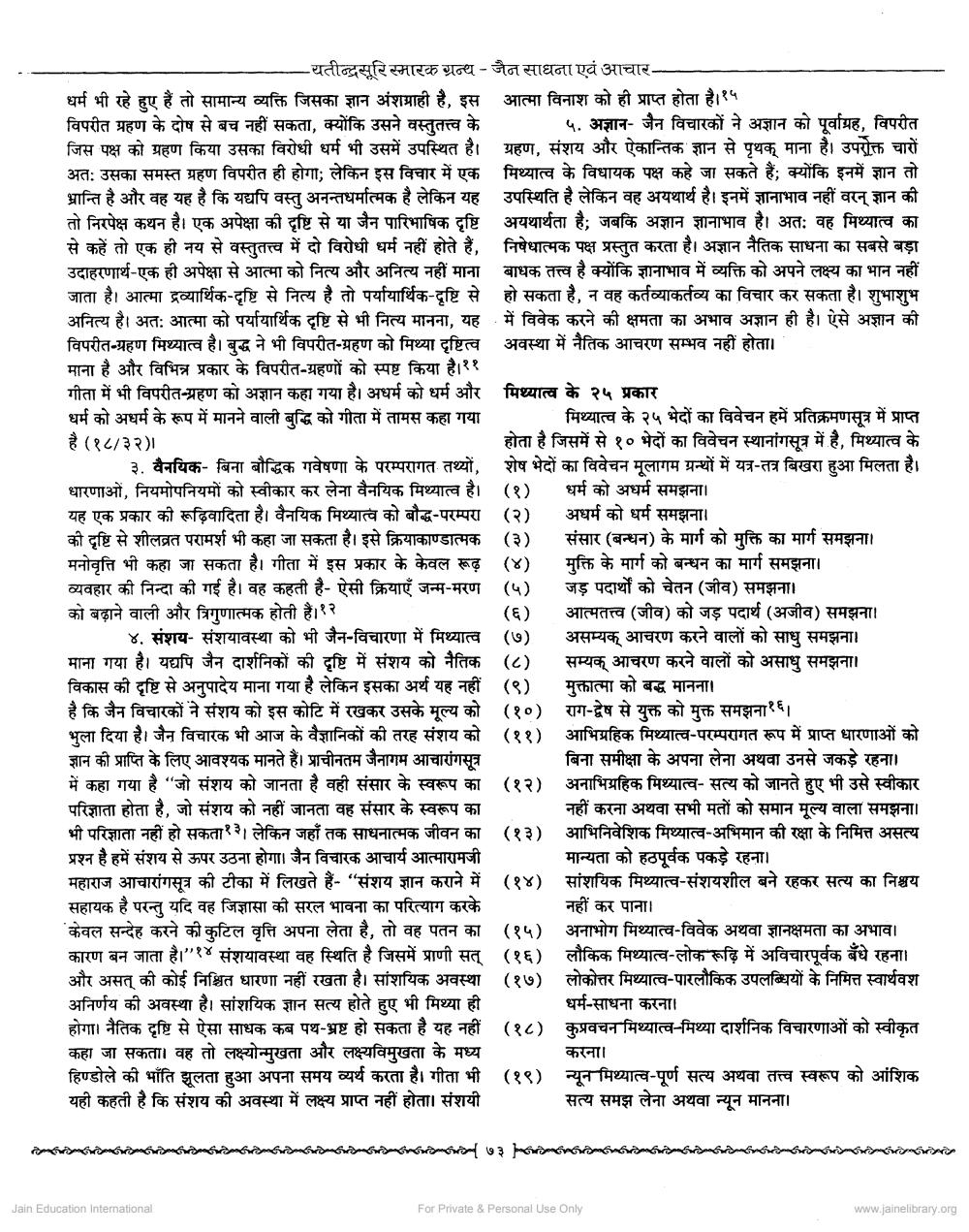________________
-यतीन्द्रसूरिस्मारक ग्रन्थ - जैन साधना एवं आचारधर्म भी रहे हुए हैं तो सामान्य व्यक्ति जिसका ज्ञान अंशग्राही है, इस आत्मा विनाश को ही प्राप्त होता है।१५ विपरीत ग्रहण के दोष से बच नहीं सकता, क्योंकि उसने वस्तुतत्त्व के
५. अज्ञान- जैन विचारकों ने अज्ञान को पूर्वाग्रह, विपरीत जिस पक्ष को ग्रहण किया उसका विरोधी धर्म भी उसमें उपस्थित है। ग्रहण, संशय और ऐकान्तिक ज्ञान से पृथक् माना है। उपरोक्त चारों अत: उसका समस्त ग्रहण विपरीत ही होगा; लेकिन इस विचार में एक मिथ्यात्व के विधायक पक्ष कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान तो भ्रान्ति है और वह यह है कि यद्यपि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है लेकिन यह उपस्थिति है लेकिन वह अयथार्थ है। इनमें ज्ञानाभाव नहीं वरन् ज्ञान की तो निरपेक्ष कथन है। एक अपेक्षा की दृष्टि से या जैन पारिभाषिक दृष्टि अयथार्थता है; जबकि अज्ञान ज्ञानाभाव है। अत: वह मिथ्यात्व का से कहें तो एक ही नय से वस्तुतत्त्व में दो विरोधी धर्म नहीं होते हैं, निषेधात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है। अज्ञान नैतिक साधना का सबसे बड़ा उदाहरणार्थ-एक ही अपेक्षा से आत्मा को नित्य और अनित्य नहीं माना बाधक तत्त्व है क्योंकि ज्ञानाभाव में व्यक्ति को अपने लक्ष्य का भान नहीं जाता है। आत्मा द्रव्यार्थिक-दृष्टि से नित्य है तो पर्यायार्थिक-दृष्टि से हो सकता है, न वह कर्तव्याकर्तव्य का विचार कर सकता है। शुभाशुभ अनित्य है। अत: आत्मा को पर्यायार्थिक दृष्टि से भी नित्य मानना, यह में विवेक करने की क्षमता का अभाव अज्ञान ही है। ऐसे अज्ञान की विपरीत-ग्रहण मिथ्यात्व है। बुद्ध ने भी विपरीत-ग्रहण को मिथ्या दृष्टित्व अवस्था में नैतिक आचरण सम्भव नहीं होता। माना है और विभिन्न प्रकार के विपरीत-ग्रहणों को स्पष्ट किया है।११ गीता में भी विपरीत-ग्रहण को अज्ञान कहा गया है। अधर्म को धर्म और मिथ्यात्व के २५ प्रकार धर्म को अधर्म के रूप में मानने वाली बुद्धि को गीता में तामस कहा गया मिथ्यात्व के २५ भेदों का विवेचन हमें प्रतिक्रमणसूत्र में प्राप्त है (१८/३२)
होता है जिसमें से १० भेदों का विवेचन स्थानांगसूत्र में है, मिथ्यात्व के ३. वैनयिक- बिना बौद्धिक गवेषणा के परम्परागत तथ्यों, शेष भेदों का विवेचन मूलागम ग्रन्थों में यत्र-तत्र बिखरा हुआ मिलता है। धारणाओं, नियमोपनियमों को स्वीकार कर लेना वैनयिक मिथ्यात्व है। (१) धर्म को अधर्म समझना। यह एक प्रकार की रूढ़िवादिता है। वैनयिक मिथ्यात्व को बौद्ध-परम्परा (२) अधर्म को धर्म समझना। की दृष्टि से शीलव्रत परामर्श भी कहा जा सकता है। इसे क्रियाकाण्डात्मक (३) संसार (बन्धन) के मार्ग को मुक्ति का मार्ग समझना। मनोवृत्ति भी कहा जा सकता है। गीता में इस प्रकार के केवल रूढ़ (४) मुक्ति के मार्ग को बन्धन का मार्ग समझना। व्यवहार की निन्दा की गई है। वह कहती है- ऐसी क्रियाएँ जन्म-मरण जड़ पदार्थों को चेतन (जीव) समझना। को बढ़ाने वाली और त्रिगुणात्मक होती है। १२
आत्मतत्त्व (जीव) को जड़ पदार्थ (अजीव) समझना। ४. संशय- संशयावस्था को भी जैन-विचारणा में मिथ्यात्व (७) असम्यक् आचरण करने वालों को साधु समझना। माना गया है। यद्यपि जैन दार्शनिकों की दृष्टि में संशय को नैतिक (८) सम्यक् आचरण करने वालों को असाधु समझना। विकास की दृष्टि से अनुपादेय माना गया है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं (९) मुक्तात्मा को बद्ध मानना। है कि जैन विचारकों ने संशय को इस कोटि में रखकर उसके मूल्य को (१०) राग-द्वेष से युक्त को मुक्त समझना१६। भुला दिया है। जैन विचारक भी आज के वैज्ञानिकों की तरह संशय को (११) आभिग्रहिक मिथ्यात्व-परम्परागत रूप में प्राप्त धारणाओं को ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। प्राचीनतम जैनागम आचारांगसूत्र बिना समीक्षा के अपना लेना अथवा उनसे जकड़े रहना। में कहा गया है “जो संशय को जानता है वही संसार के स्वरूप का (१२) अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व- सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार परिज्ञाता होता है, जो संशय को नहीं जानता वह संसार के स्वरूप का नहीं करना अथवा सभी मतों को समान मूल्य वाला समझना। भी परिज्ञाता नहीं हो सकता१३। लेकिन जहाँ तक साधनात्मक जीवन का (१३) आभिनिवेशिक मिथ्यात्व-अभिमान की रक्षा के निमित्त असत्य प्रश्न है हमें संशय से ऊपर उठना होगा। जैन विचारक आचार्य आत्मारामजी
मान्यता को हठपूर्वक पकड़े रहना। महाराज आचारांगसूत्र की टीका में लिखते हैं- "संशय ज्ञान कराने में (१४) सांशयिक मिथ्यात्व-संशयशील बने रहकर सत्य का निश्चय सहायक है परन्तु यदि वह जिज्ञासा की सरल भावना का परित्याग करके नहीं कर पाना। केवल सन्देह करने की कुटिल वृत्ति अपना लेता है, तो वह पतन का (१५) अनाभोग मिथ्यात्व-विवेक अथवा ज्ञानक्षमता का अभाव। कारण बन जाता है।"१४ संशयावस्था वह स्थिति है जिसमें प्राणी सत् (१६) लौकिक मिथ्यात्व-लोक रूढ़ि में अविचारपूर्वक बँधे रहना।
और असत् की कोई निश्चित धारणा नहीं रखता है। सांशयिक अवस्था (१७) लोकोत्तर मिथ्यात्व-पारलौकिक उपलब्धियों के निमित्त स्वार्थवश अनिर्णय की अवस्था है। सांशयिक ज्ञान सत्य होते हुए भी मिथ्या ही धर्म-साधना करना। होगा। नैतिक दृष्टि से ऐसा साधक कब पथ-भ्रष्ट हो सकता है यह नहीं (१८) कुप्रवचन मिथ्यात्व-मिथ्या दार्शनिक विचारणाओं को स्वीकृत कहा जा सकता। वह तो लक्ष्योन्मुखता और लक्ष्यविमुखता के मध्य
करना। हिण्डोले की भाँति झूलता हुआ अपना समय व्यर्थ करता है। गीता भी (१९) न्यून मिथ्यात्व-पूर्ण सत्य अथवा तत्त्व स्वरूप को आंशिक यही कहती है कि संशय की अवस्था में लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। संशयी सत्य समझ लेना अथवा न्यून मानना।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org