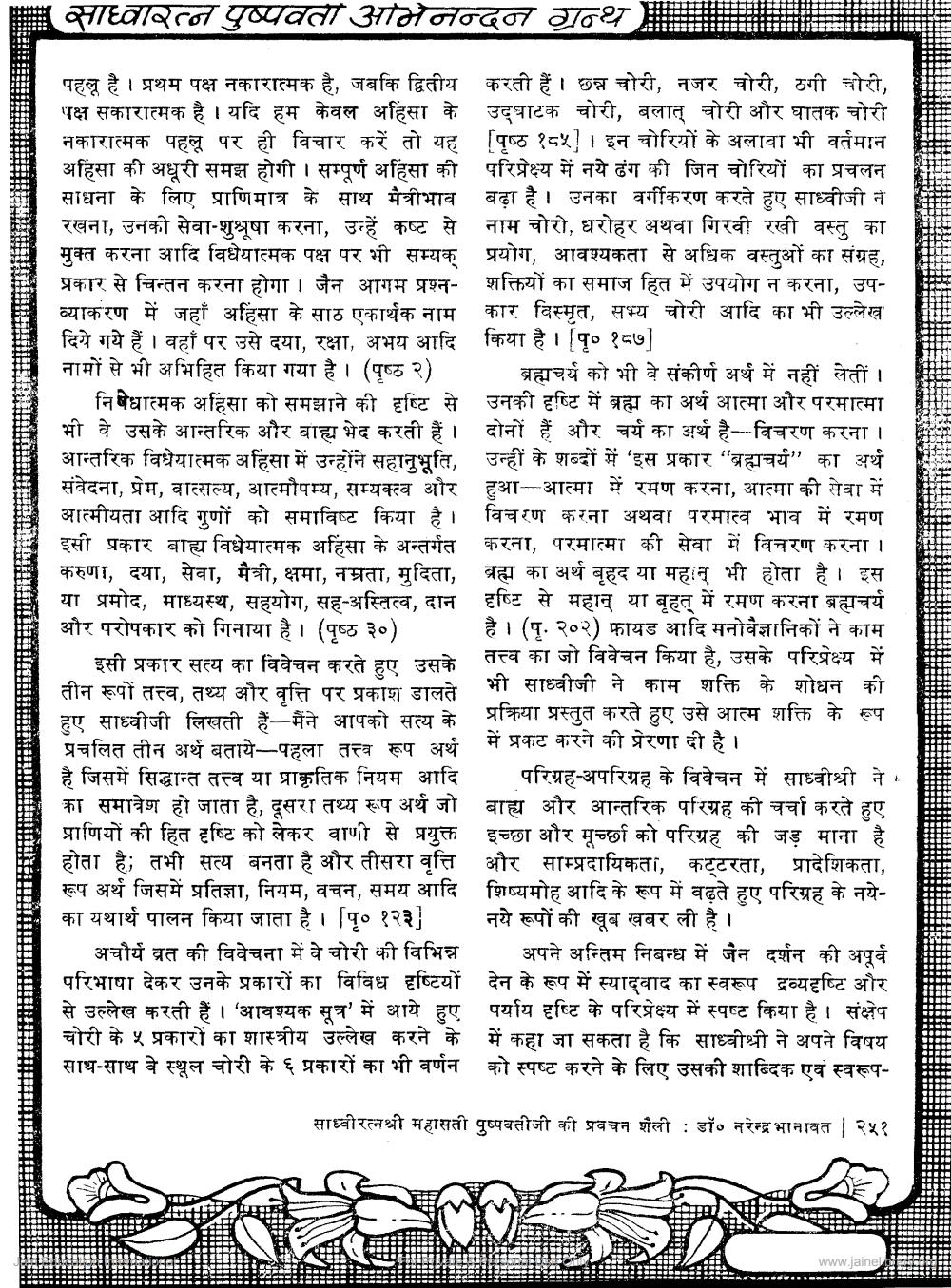________________
साध्वारत्न पुष्पवता आभनन्दन ग्रन्थ
पहल है । प्रथम पक्ष नकारात्मक है, जबकि द्वितीय पक्ष सकारात्मक है । यदि हम केवल अहिंसा के नकारात्मक पहलू पर ही विचार करें तो यह अहिंसा की अधूरी समझ होगी । सम्पूर्ण अहिंसा की साधना के लिए प्राणिमात्र के साथ मैत्रीभाव रखना, उनकी सेवा-शुश्रूषा करना, उन्हें कष्ट से मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी सम्यक् प्रकार से चिन्तन करना होगा। जैन आगम प्रश्नव्याकरण में जहाँ अहिंसा के साठ एकार्थक नाम दिये गये हैं । वहाँ पर उसे दया, रक्षा, अभय आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। (पृष्ठ २) निषेधात्मक अहिंसा को समझाने की दृष्टि से भी वे उसके आन्तरिक और बाह्य भेद करती हैं । आन्तरिक विधेयात्मक अहिंसा में उन्होंने सहानुभूति, संवेदना, प्रेम, वात्सल्य, आत्मौपम्य, सम्यक्त्व और आत्मीयता आदि गुणों को समाविष्ट किया है। इसी प्रकार बाह्य विधेयात्मक अहिंसा के अन्तर्गत करुणा, दया, सेवा, मैत्री, क्षमा, नम्रता, मुदिता, या प्रमोद, माध्यस्थ, सहयोग, सह-अस्तित्व, दान और परोपकार को गिनाया है । ( पृष्ठ ३० ) इसी प्रकार सत्य का विवेचन करते हुए उसके तीन रूपों तत्त्व, तथ्य और वृत्ति पर प्रकाश डालते हुए साध्वीजी लिखती हैं— मैंने आपको सत्य के प्रचलित तीन अर्थ बताये - पहला तत्त्व रूप अर्थ है जिसमें सिद्धान्त तत्त्व या प्राकृतिक नियम आदि का समावेश हो जाता है, दूसरा तथ्य रूप अर्थ जो प्राणियों की हित दृष्टि को लेकर वाणी से प्रयुक्त होता है; तभी सत्य बनता है और तीसरा वृत्ति रूप अर्थ जिसमें प्रतिज्ञा, नियम, वचन, समय आदि का यथार्थ पालन किया जाता है । [ पृ० १२३]
करती हैं । छन्न चोरी, नजर चोरी, ठगी चोरी, उद्घाटक चोरी, बलात् चोरी और घातक चोरी [ पृष्ठ १८५ ] । इन चोरियों के अलावा भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नये ढंग की जिन चोरियों का प्रचलन बढ़ा है। उनका वर्गीकरण करते हुए साध्वीजी ने नाम चोरी, धरोहर अथवा गिरवी रखी वस्तु का प्रयोग, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह, शक्तियों का समाज हित में उपयोग न करना, उपकार विस्मृत, सभ्य चोरी आदि का भी उल्लेख किया है । [ पृ० १८७ ]
अचौर्य व्रत की विवेचना में वे चोरी की विभिन्न परिभाषा देकर उनके प्रकारों का विविध दृष्टियों से उल्लेख करती हैं । 'आवश्यक सूत्र' में आये हुए चोरी के ५ प्रकारों का शास्त्रीय उल्लेख करने के साथ-साथ वे स्थूल चोरी के ६ प्रकारों का भी वर्णन
ब्रह्मचर्य को भी वे संकीर्ण अर्थ में नहीं लेतीं । उनकी दृष्टि में ब्रह्म का अर्थ आत्मा और परमात्मा दोनों हैं और चर्य का अर्थ है -- विचरण करना । उन्हीं के शब्दों में 'इस प्रकार "ब्रह्मचर्य" का अर्थ हुआ - आत्मा में रमण करना, आत्मा की सेवा में विचरण करना अथवा परमात्व भाव में रमण करना, परमात्मा की सेवा में विचरण करना । ब्रह्म का अर्थ बृहद या महान् भी होता है । इस दृष्टि से महान् या बृहत् में रमण करना ब्रह्मचर्य है । (पृ. २०२) फ्रायड आदि मनोवैज्ञानिकों ने काम तत्त्व का जो विवेचन किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी साध्वीजी ने काम शक्ति के शोधन की प्रक्रिया प्रस्तुत करते हुए उसे आत्म शक्ति के रूप में प्रकट करने की प्रेरणा दी है ।
परिग्रह- अपरिग्रह के विवेचन में साध्वीश्री ने बाह्य और आन्तरिक परिग्रह की चर्चा करते हुए इच्छा और मूर्च्छा को परिग्रह की जड़ माना है और साम्प्रदायिकता, कट्टरता, प्रादेशिकता, शिष्यमोह आदि के रूप में बढ़ते हुए परिग्रह के नयेनये रूपों की खूब खबर ली है ।
अपने अन्तिम निबन्ध में जैन दर्शन की अपूर्व देन के रूप में स्याद्वाद का स्वरूप द्रव्यदृष्टि और पर्याय दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया है । संक्षेप में कहा जा सकता है कि साध्वीश्री ने अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए उसकी शाब्दिक एवं स्वरूपसाध्वी रत्नश्री महासती पुष्पवतीजी की प्रवचन शैली : डॉ० नरेन्द्र भानावत | २५१
www.jainel