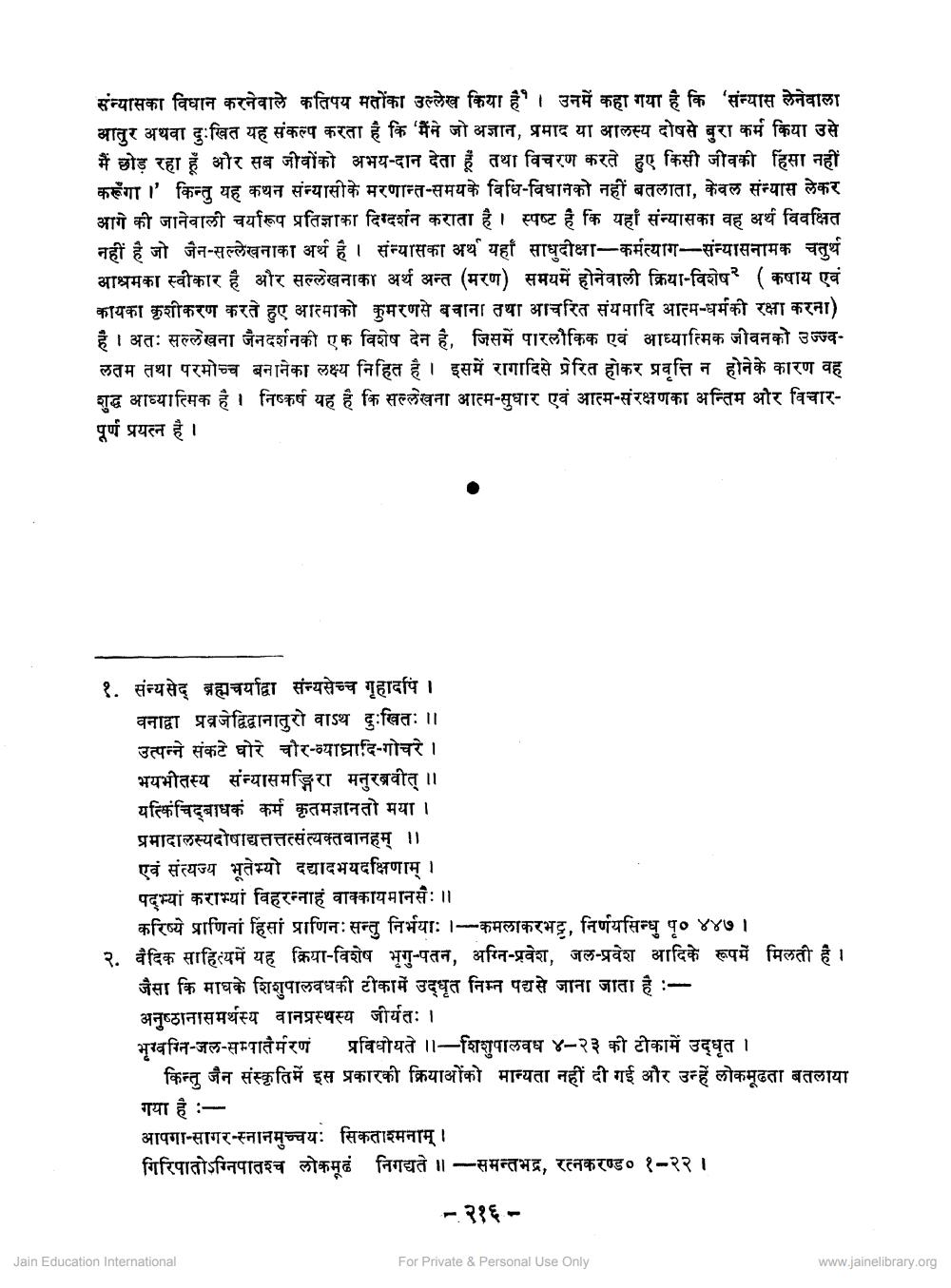________________
संन्यासका विधान करनेवाले कतिपय मतोंका उल्लेख किया है । उनमें कहा गया है कि 'संन्यास लेनेवाला आतुर अथवा दुःखित यह संकल्प करता है कि 'मैंने जो अज्ञान, प्रमाद या आलस्य दोषसे बुरा कर्म किया उसे मैं छोड़ रहा हूँ और सब जीवोंको अभयदान देता हूँ तथा विचरण करते हुए किसी जीवकी हिंसा नहीं करूँगा ।' किन्तु यह कथन संन्यासीके मरणान्त समय के विधि-विधानको नहीं बतलाता, केवल संन्यास लेकर आगे की जानेवाली चर्यारूप प्रतिज्ञाका दिग्दर्शन कराता है। स्पष्ट है कि यहाँ संन्यासका वह अर्थ विवक्षित नहीं है जो जैन- सल्लेखनाका अर्थ है । संन्यासका अर्थ यहाँ साधुदीक्षा - कर्मत्याग —— संन्यासनामक चतुर्थ आश्रमका स्वीकार है और सल्लेखनाका अर्थ अन्त ( मरण ) समय में होनेवाली क्रिया-विशेष २ ( कषाय एवं कायका कृशीकरण करते हुए आत्माको कुमरणसे बचाना तथा आचरित संयमादि आत्म-धर्म की रक्षा करना) है | अतः सल्लेखना जैनदर्शनकी एक विशेष देन है, जिसमें पारलौकिक एवं आध्यात्मिक जीवनको उज्ज्वलतम तथा परमोच्च बनानेका लक्ष्य निहित है । इसमें रागादिसे प्रेरित होकर प्रवृत्ति न होनेके कारण वह शुद्ध आध्यात्मिक है । निष्कर्ष यह है कि सल्लेखना आत्म-सुधार एवं आत्म-संरक्षणका अन्तिम और विचारपूर्ण प्रयत्न है ।
१. संन्यसेद् ब्रह्मचर्याद्वा संन्यसेच्च गृहादपि । वनाद्वा प्रव्रजेद्विद्वानातुरो वाऽथ दुःखितः ।। उत्पन्ने संकटे घोरे चौर- व्याघ्रादि-गोचरे । भयभीतस्य संन्यासमङ्गिरा मनुरब्रवीत् ॥ यत्किंचिद्बाधकं कर्म कृतमज्ञानतो मया । प्रमादालस्यदोषाद्यत्तत्तत्संत्यक्तवानहम् ।।
एवं संत्यज्य भूतेभ्यो दद्यादभयदक्षिणाम् ।
पद्भ्यां कराभ्यां विहरन्नाहं वाक्कायमानसैः ॥
करिष्ये प्राणिनां हिसां प्राणिनः सन्तु निर्भयाः । - कमलाकरभट्ट, निर्णयसिन्धु पृ० ४४७ |
२. वैदिक साहित्य में यह क्रिया-विशेष भृगु-पतन, अग्नि प्रवेश, जल-प्रवेश आदिके रूपमें मिलती है ।
जैसा कि माघके शिशुपालवधकी टीकामें उद्धृत निम्न पद्यसे जाना जाता है। :
अनुष्ठानासमर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः ।
भृग्वग्नि-जल सम्पातैर्मरणं प्रविधोयते ॥ - शिशुपालवध ४-२३ की टीकामें उद्धृत ।
किन्तु जैन संस्कृति में इस प्रकारकी क्रियाओंको मान्यता नहीं दी गई और उन्हें लोकमूढता बतलाया गया है :
आपगा-सागर-स्नानमुच्चयः सिकताश्मनाम् । गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥ - समन्तभद्र, रत्नकरण्ड० १-२२ ।
Jain Education International
1
. २१६ -
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org