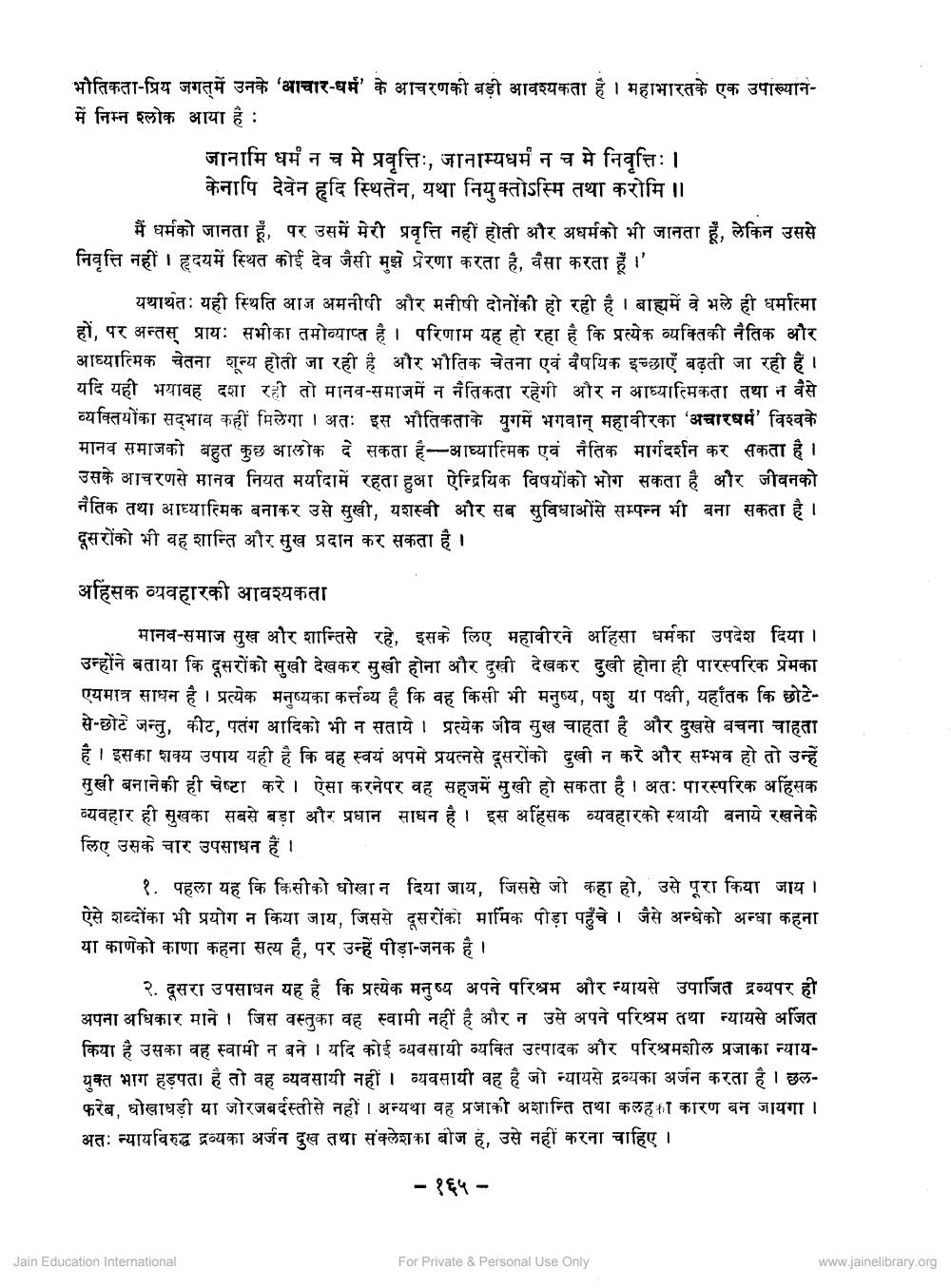________________
भौतिकता-प्रिय जगत्में उनके 'आचार-धर्म' के आचरणकी बड़ी आवश्यकता है । महाभारतके एक उपाख्यानमें निम्न श्लोक आया है :
जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः ।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ मैं धर्मको जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्मको भी जानता हूँ, लेकिन उससे निवृत्ति नहीं । हृदयमें स्थित कोई देव जैसी मुझे प्रेरणा करता है, वैसा करता हूँ।'
यथार्थतः यही स्थिति आज अमनीषी और मनीषी दोनोंकी हो रही है । बाह्यमें वे भले ही धर्मात्मा हों, पर अन्तस् प्रायः सभीका तमोव्याप्त है। परिणाम यह हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्तिकी नैतिक और आध्यात्मिक चेतना शून्य होती जा रही है और भौतिक चेतना एवं वैषयिक इच्छाएँ बढ़ती जा रही हैं। यदि यही भयावह दशा रही तो मानव-समाजमें न नैतिकता रहेगी और न आध्यात्मिकता तथा न वैसे व्यक्तियोंका सद्भाव कहीं मिलेगा । अतः इस भौतिकताके युगमें भगवान महावीरका 'अचारधर्म' विश्वके मानव समाजको बहुत कुछ आलोक दे सकता है-आध्यात्मिक एवं नैतिक मार्गदर्शन कर सकता है। उसके आचरणसे मानव नियत मर्यादामें रहता हआ ऐन्द्रियिक विषयोंको भोग सकता है और जीवनको नैतिक तथा आध्यात्मिक बनाकर उसे सुखी, यशस्वी और सब सुविधाओंसे सम्पन्न भी बना सकता है । दूसरोंको भी वह शान्ति और सुख प्रदान कर सकता है।
अहिंसक व्यवहारकी आवश्यकता
मानव-समाज सुख और शान्तिसे रहे, इसके लिए महावीरने अहिंसा धर्मका उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि दूसरोंको सुखी देखकर सुखी होना और दुखी देखकर दुखी होना ही पारस्परिक प्रेमका एयमात्र साधन है । प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह किसी भी मनुष्य, पशु या पक्षी, यहाँतक कि छोटेसे-छोटे जन्तु, कीट, पतंग आदिको भी न सताये । प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुखसे बचना चाहता है । इसका शक्य उपाय यही है कि वह स्वयं अपने प्रयत्नसे दूसरोंको दुखी न करे और सम्भव हो तो उन्हें सुखी बनाने की ही चेष्टा करे । ऐसा करनेपर वह सहजमें सुखी हो सकता है। अतः पारस्परिक अहिंसक व्यवहार ही सुखका सबसे बड़ा और प्रधान साधन है। इस अहिंसक व्यवहारको स्थायी बनाये रखने के लिए उसके चार उपसाधन हैं।
१. पहला यह कि किसीको धोखा न दिया जाय, जिससे जो कहा हो, उसे पूरा किया जाय। ऐसे शब्दोंका भी प्रयोग न किया जाय, जिससे दूसरोंको मार्मिक पीड़ा पहुँचे । जैसे अन्धेको अन्धा कहना या काणेको काणा कहना सत्य है, पर उन्हें पीड़ा-जनक है ।
२. दूसरा उपसाधन यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने परिश्रम और न्यायसे उपार्जित द्रव्यपर ही अपना अधिकार माने । जिस वस्तुका वह स्वामी नहीं है और न उसे अपने परिश्रम तथा न्यायसे अजित किया है उसका वह स्वामी न बने । यदि कोई व्यवसायी व्यक्ति उत्पादक और परिश्रमशील प्रजाका न्याययुक्त भाग हड़पता है तो वह व्यवसायी नहीं। व्यवसायी वह है जो न्यायसे द्रव्यका अर्जन करता है । छलफरेब, धोखाधड़ी या जोरजबर्दस्तीसे नहीं । अन्यथा वह प्रजाकी अशान्ति तथा कलहका कारण बन जायगा। अतः न्यायविरुद्ध द्रव्यका अर्जन दुख तथा संक्लेशका बीज है, उसे नहीं करना चाहिए ।
-१६५ -
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org