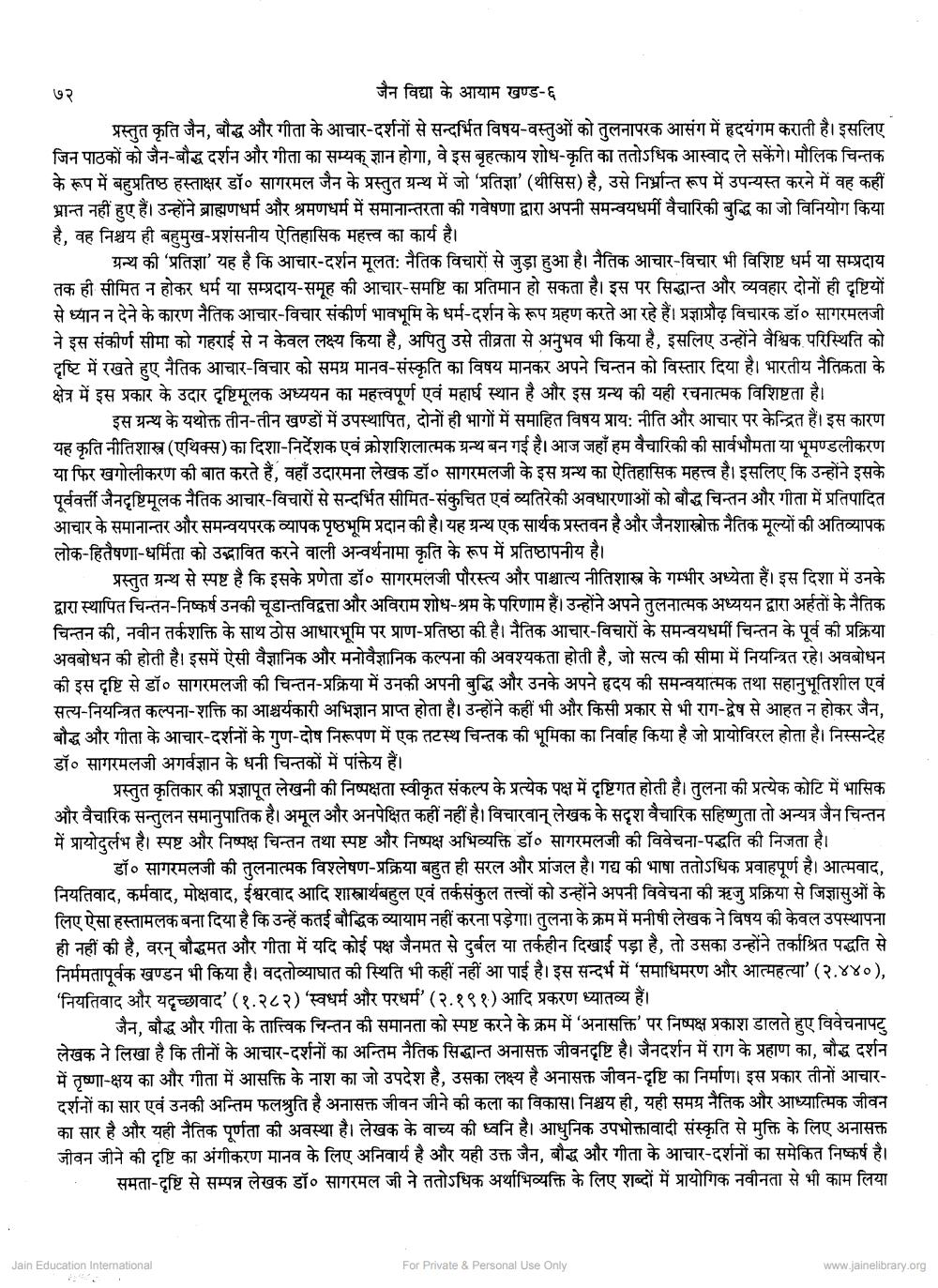________________
जैन विद्या के आयाम खण्ड ६
प्रस्तुत कृति जैन, बौद्ध और गीता के आचार- दर्शनों से सन्दर्भित विषय-वस्तुओं को तुलनापरक आसंग में हृदयंगम कराती है। इसलिए जिन पाठकों को जैन-बौद्ध दर्शन और गीता का सम्यक् ज्ञान होगा, वे इस बृहत्काय शोध कृति का ततोऽधिक आस्वाद ले सकेंगे। मौलिक चिन्तक के रूप में बहुप्रतिष्ठ हस्ताक्षर डॉ० सागरमल जैन के प्रस्तुत ग्रन्थ में जो 'प्रतिज्ञा' (थीसिस) है, उसे निर्भ्रान्त रूप में उपन्यस्त करने में वह कहीं भ्रान्त नहीं हुए हैं। उन्होंने ब्राह्मणधर्म और श्रमणधर्म में समानान्तरता की गवेषणा द्वारा अपनी समन्वयधमीं वैचारिकी बुद्धि का जो विनियोग किया है, वह निश्चय ही बहुमुख- प्रशंसनीय ऐतिहासिक महत्त्व का कार्य है।
ग्रन्थ की ‘प्रतिज्ञा' यह है कि आचार - दर्शन मूलतः नैतिक विचारों से जुड़ा हुआ है। नैतिक आचार-विचार भी विशिष्ट धर्म या सम्प्रदाय तक ही सीमित न होकर धर्म या सम्प्रदाय - समूह की आचार - समष्टि का प्रतिमान हो सकता है। इस पर सिद्धान्त और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से ध्यान न देने के कारण नैतिक आचार-विचार संकीर्ण भावभूमि के धर्म-दर्शन के रूप ग्रहण करते आ रहे हैं। प्रज्ञाप्रौढ़ विचारक डॉ० सागरमलजी ने इस संकीर्ण सीमा को गहराई से न केवल लक्ष्य किया है, अपितु उसे तीव्रता से अनुभव भी किया है, इसलिए उन्होंने वैश्विक परिस्थितिको दृष्टि में रखते हुए नैतिक आचार-विचार को समग्र मानव संस्कृति का विषय मानकर अपने चिन्तन को विस्तार दिया है। भारतीय नैतिकता के क्षेत्र में इस प्रकार के उदार दृष्टिमूलक अध्ययन का महत्त्वपूर्ण एवं महार्ष स्थान है और इस ग्रन्थ की यही रचनात्मक विशिष्टता है।
७२
-
इस ग्रन्थ के यथोक्त तीन-तीन खण्डों में उपस्थापित, दोनों ही भागों में समाहित विषय प्रायः नीति और आचार पर केन्द्रित हैं। इस कारण यह कृति नीतिशास्त्र (एथिक्स) का दिशा-निर्देशक एवं क्रोशशिलात्मक ग्रन्थ बन गई है। आज जहाँ हम वैचारिकी की सार्वभौमता या भूमण्डलीकरण या फिर खगोलीकरण की बात करते हैं, वहाँ उदारमना लेखक डॉ० सागरमलजी के इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक महत्त्व है। इसलिए कि उन्होंने इसके पूर्ववर्ती जैनदृष्टिमूलक नैतिक आचार-विचारों से सन्दर्भित सीमित संकुचित एवं व्यतिरेकी अवधारणाओं को बौद्ध चिन्तन और गीता में प्रतिपादित आचार के समानान्तर और समन्वयपरक व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान की है। यह ग्रन्थ एक सार्थक प्रस्तवन है और जैनशास्त्रोक्त नैतिक मूल्यों की अतिव्यापक लोकहितैषणा धर्मिता को उद्घावित करने वाली अन्वर्थनामा कृति के रूप में प्रतिष्ठापनीय है।
प्रस्तुत ग्रन्थ से स्पष्ट है कि इसके प्रणेता डॉ० सागरमलजी पौरस्त्य और पाश्चात्य नीतिशास्त्र के गम्भीर अध्येता हैं। इस दिशा में उनके द्वारा स्थापित चिन्तन-निष्कर्ष उनकी चूडान्तविद्वत्ता और अविराम शोध-श्रम के परिणाम हैं। उन्होंने अपने तुलनात्मक अध्ययन द्वारा अर्हतों के नैतिक चिन्तन की, नवीन तर्कशक्ति के साथ ठोस आधारभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा की है। नैतिक आचार-विचारों के समन्वयधर्मी चिन्तन के पूर्व की प्रक्रिया अवबोधन की होती है। इसमें ऐसी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कल्पना की अवश्यकता होती है, जो सत्य की सीमा में नियन्त्रित रहे । अवबोधन की इस दृष्टि से डॉ० सागरमलजी की चिन्तन प्रक्रिया में उनकी अपनी बुद्धि और उनके अपने हृदय की समन्वयात्मक तथा सहानुभूतिशील एवं सत्य-नियन्त्रित कल्पना-शक्ति का आश्चर्यकारी अभिज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने कहीं भी और किसी प्रकार से भी राग-द्वेष से आहत न होकर जैन, बौद्ध और गीता के आचार- दर्शनों के गुण-दोष निरूपण में एक तटस्थ चिन्तक की भूमिका का निर्वाह किया है जो प्रायोविरल होता है। निस्सन्देह डॉ० सागरमलजी अगर्वज्ञान के धनी चिन्तकों में पक्तिय है।
प्रस्तुत कृतिकार की प्रज्ञापूत लेखनी की निष्पक्षता स्वीकृत संकल्प के प्रत्येक पक्ष में दृष्टिगत होती है । तुलना की प्रत्येक कोटि में भासिक और वैचारिक सन्तुलन समानुपातिक है अमूल और अनपेक्षित कहीं नहीं है। विचारवान् लेखक के सदृश वैचारिक सहिष्णुता तो अन्यत्र जैन चिन्तन में प्रायोदुर्लभ है। स्पष्ट और निष्पक्ष चिन्तन तथा स्पष्ट और निष्पक्ष अभिव्यक्ति डॉ० सागरमलजी की विवेचना-पद्धति की निजता है।
डॉ० सागरमलजी की तुलनात्मक विश्लेषण प्रक्रिया बहुत ही सरल और प्रांजल है। गद्य की भाषा ततोऽधिक प्रवाहपूर्ण है। आत्मवाद, नियतिवाद, कर्मवाद, मोक्षवाद, ईश्वरवाद आदि शास्त्रार्थबहुल एवं तर्कसंकुल तत्त्वों को उन्होंने अपनी विवेचना की ऋजु प्रक्रिया से जिज्ञासुओं के लिए ऐसा हस्तामलक बना दिया है कि उन्हें कतई बौद्धिक व्यायाम नहीं करना पड़ेगा। तुलना के क्रम में मनीषी लेखक ने विषय की केवल उपस्थापना ही नहीं की है, वरन् बौद्धमत और गीता में यदि कोई पक्ष जैनमत से दुर्बल या तर्कहीन दिखाई पड़ा है, तो उसका उन्होंने तर्काश्रित पद्धति से निर्ममतापूर्वक खण्डन भी किया है वदतोव्याघात की स्थिति भी कहीं नहीं आ पाई है इस सन्दर्भ में 'समाधिमरण और आत्महत्या' (२.४४० ), 'नियतिवाद और यदृच्छावाद' (१.२८२) 'स्वधर्म और परधर्म' (२.१९१) आदि प्रकरण ध्यातव्य हैं।
जैन, बौद्ध और गीता के तात्विक चिन्तन की समानता को स्पष्ट करने के क्रम में 'अनासक्ति' पर निष्पक्ष प्रकाश डालते हुए विवेचनापट् लेखक ने लिखा है कि तीनों के आचार-दर्शनों का अन्तिम नैतिक सिद्धान्त अनासक्त जीवनदृष्टि है जैनदर्शन में राग के प्रहाण का, बौद्ध दर्शन में तृष्णा क्षय का और गीता में आसक्ति के नाश का जो उपदेश है, उसका लक्ष्य है अनासक्त जीवन-दृष्टि का निर्माण इस प्रकार तीनों आचारदर्शनों का सार एवं उनकी अन्तिम फलश्रुति है अनासक्त जीवन जीने की कला का विकास निश्चय ही, यही समग्र नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का सार है और यही नैतिक पूर्णता की अवस्था है। लेखक के वाच्य की ध्वनि है। आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति से मुक्ति के लिए अनासक्त जीवन जीने की दृष्टि का अंगीकरण मानव के लिए अनिवार्य है और यही उक्त जैन, बौद्ध और गीता के आचार- दर्शनों का समेकित निष्कर्ष है। समता-दृष्टि से सम्पन्न लेखक डॉ० सागरमल जी ने ततोऽधिक अर्थाभिव्यक्ति के लिए शब्दों में प्रायोगिक नवीनता से भी काम लिया
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.