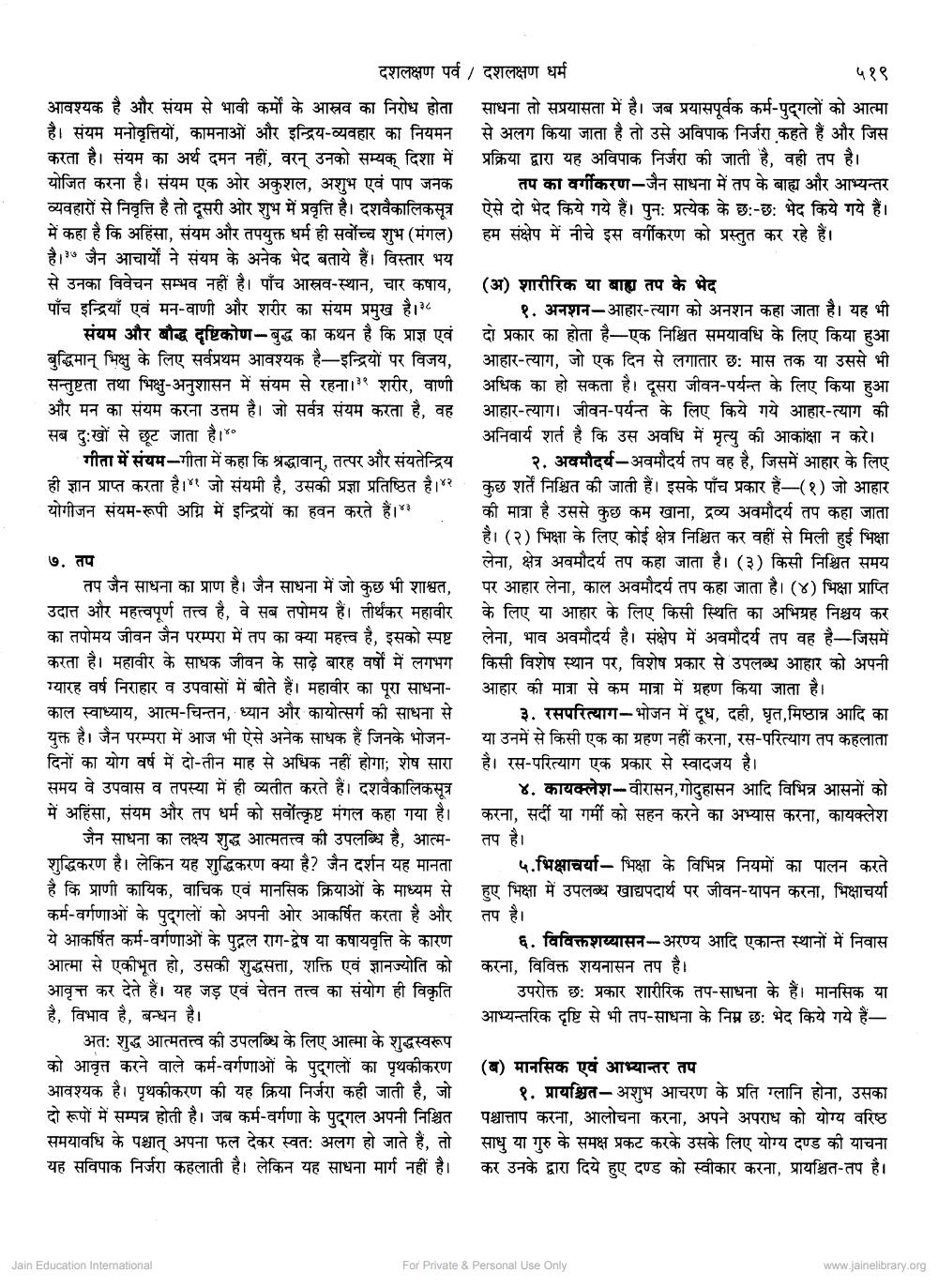________________
दशलक्षण पर्व | दशलक्षण धर्म आवश्यक है और संयम से भावी कर्मों के आस्रव का निरोध होता साधना तो सप्रयासता में है। जब प्रयासपूर्वक कर्म-पुद्गलों को आत्मा है। संयम मनोवृत्तियों, कामनाओं और इन्द्रिय-व्यवहार का नियमन से अलग किया जाता है तो उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं और जिस करता है। संयम का अर्थ दमन नहीं, वरन् उनको सम्यक् दिशा में प्रक्रिया द्वारा यह अविपाक निर्जरा की जाती है, वही तप है। योजित करना है। संयम एक ओर अकुशल, अशुभ एवं पाप जनक तप का वर्गीकरण-जैन साधना में तप के बाह्य और आभ्यन्तर व्यवहारों से निवृत्ति है तो दूसरी ओर शुभ में प्रवृत्ति है। दशवैकालिकसूत्र ऐसे दो भेद किये गये हैं। पुन: प्रत्येक के छ:-छ: भेद किये गये हैं। में कहा है कि अहिंसा, संयम और तपयुक्त धर्म ही सर्वोच्च शुभ (मंगल) हम संक्षेप में नीचे इस वर्गीकरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। है।३७ जैन आचार्यों ने संयम के अनेक भेद बताये हैं। विस्तार भय से उनका विवेचन सम्भव नहीं है। पाँच आस्रव-स्थान, चार कषाय, (अ) शारीरिक या बाह्य तप के भेद पाँच इन्द्रियाँ एवं मन-वाणी और शरीर का संयम प्रमुख है।२८ १. अनशन-आहार-त्याग को अनशन कहा जाता है। यह भी
संयम और बौद्ध दृष्टिकोण-बुद्ध का कथन है कि प्राज्ञ एवं दो प्रकार का होता है—एक निश्चित समयावधि के लिए किया हुआ बुद्धिमान् भिक्षु के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है-इन्द्रियों पर विजय, आहार-त्याग, जो एक दिन से लगातार छ: मास तक या उससे भी सन्तुष्टता तथा भिक्षु-अनुशासन में संयम से रहना।३९ शरीर, वाणी अधिक का हो सकता है। दूसरा जीवन-पर्यन्त के लिए किया हुआ
और मन का संयम करना उत्तम है। जो सर्वत्र संयम करता है, वह आहार-त्याग। जीवन-पर्यन्त के लिए किये गये आहार-त्याग की सब दुःखों से छूट जाता है।४०
अनिवार्य शर्त है कि उस अवधि में मृत्यु की आकांक्षा न करे। गीता में संयम-गीता में कहा कि श्रद्धावान्, तत्पर और संयतेन्द्रिय २. अवमौदर्य-अवमौदर्य तप वह है, जिसमें आहार के लिए ही ज्ञान प्राप्त करता है। जो संयमी है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है।४२ . कुछ शर्ते निश्चित की जाती हैं। इसके पाँच प्रकार हैं-(१) जो आहार योगीजन संयम-रूपी अग्नि में इन्द्रियों का हवन करते हैं। ४३ की मात्रा है उससे कुछ कम खाना, द्रव्य अवमौदर्य तप कहा जाता
है। (२) भिक्षा के लिए कोई क्षेत्र निश्चित कर वहीं से मिली हुई भिक्षा ७. तप
लेना, क्षेत्र अवमौदर्य तप कहा जाता है। (३) किसी निश्चित समय तप जैन साधना का प्राण है। जैन साधना में जो कुछ भी शाश्वत, पर आहार लेना, काल अवमौदर्य तप कहा जाता है। (४) भिक्षा प्राप्ति उदात्त और महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, वे सब तपोमय हैं। तीर्थंकर महावीर के लिए या आहार के लिए किसी स्थिति का अभिग्रह निश्चय कर का तपोमय जीवन जैन परम्परा में तप का क्या महत्त्व है, इसको स्पष्ट लेना, भाव अवमौदर्य है। संक्षेप में अवमौदर्य तप वह है-जिसमें करता है। महावीर के साधक जीवन के साढ़े बारह वर्षों में लगभग किसी विशेष स्थान पर, विशेष प्रकार से उपलब्ध आहार को अपनी ग्यारह वर्ष निराहार व उपवासों में बीते हैं। महावीर का पूरा साधना- आहार की मात्रा से कम मात्रा में ग्रहण किया जाता है। काल स्वाध्याय, आत्म-चिन्तन, ध्यान और कायोत्सर्ग की साधना से ३. रसपरित्याग- भोजन में दूध, दही, घृत,मिष्ठान्न आदि का युक्त है। जैन परम्परा में आज भी ऐसे अनेक साधक हैं जिनके भोजन- या उनमें से किसी एक का ग्रहण नहीं करना, रस-परित्याग तप कहलाता दिनों का योग वर्ष में दो-तीन माह से अधिक नहीं होगा; शेष सारा है। रस-परित्याग एक प्रकार से स्वादजय है। समय वे उपवास व तपस्या में ही व्यतीत करते हैं। दशवैकालिकसूत्र ४. कायक्लेश-वीरासन,गोदुहासन आदि विभिन्न आसनों को में अहिंसा, संयम और तप धर्म को सर्वोत्कृष्ट मंगल कहा गया है। __करना, सर्दी या गर्मी को सहन करने का अभ्यास करना, कायक्लेश
जैन साधना का लक्ष्य शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि है, आत्म- तप है। शुद्धिकरण है। लेकिन यह शुद्धिकरण क्या है? जैन दर्शन यह मानता ५.भिक्षाचर्या-भिक्षा के विभिन्न नियमों का पालन करते है कि प्राणी कायिक, वाचिक एवं मानसिक क्रियाओं के माध्यम से हुए भिक्षा में उपलब्ध खाद्यपदार्थ पर जीवन-यापन करना, भिक्षाचर्या कर्म-वर्गणाओं के पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करता है और तप है। ये आकर्षित कर्म-वर्गणाओं के पुद्गल राग-द्वेष या कषायवृत्ति के कारण ६. विविक्तशय्यासन-अरण्य आदि एकान्त स्थानों में निवास आत्मा से एकीभूत हो, उसकी शुद्धसत्ता, शक्ति एवं ज्ञानज्योति को करना, विविक्त शयनासन तप है। आवृत्त कर देते हैं। यह जड़ एवं चेतन तत्त्व का संयोग ही विकृति उपरोक्त छः प्रकार शारीरिक तप-साधना के हैं। मानसिक या है, विभाव है, बन्धन है।
आभ्यन्तरिक दृष्टि से भी तप-साधना के निम्न छ: भेद किये गये हैंअत: शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि के लिए आत्मा के शुद्धस्वरूप को आवृत्त करने वाले कर्म-वर्गणाओं के पुद्गलों का पृथकीकरण (ब) मानसिक एवं आभ्यान्तर तप आवश्यक है। पृथकीकरण की यह क्रिया निर्जरा कही जाती है, जो १. प्रायश्चित-अशुभ आचरण के प्रति ग्लानि होना, उसका दो रूपों में सम्पन्न होती है। जब कर्म-वर्गणा के पुद्गल अपनी निश्चित पश्चात्ताप करना, आलोचना करना, अपने अपराध को योग्य वरिष्ठ समयावधि के पश्चात् अपना फल देकर स्वत: अलग हो जाते हैं, तो साधु या गुरु के समक्ष प्रकट करके उसके लिए योग्य दण्ड की याचना यह सविपाक निर्जरा कहलाती है। लेकिन यह साधना मार्ग नहीं है। कर उनके द्वारा दिये हुए दण्ड को स्वीकार करना, प्रायश्चित-तप है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org