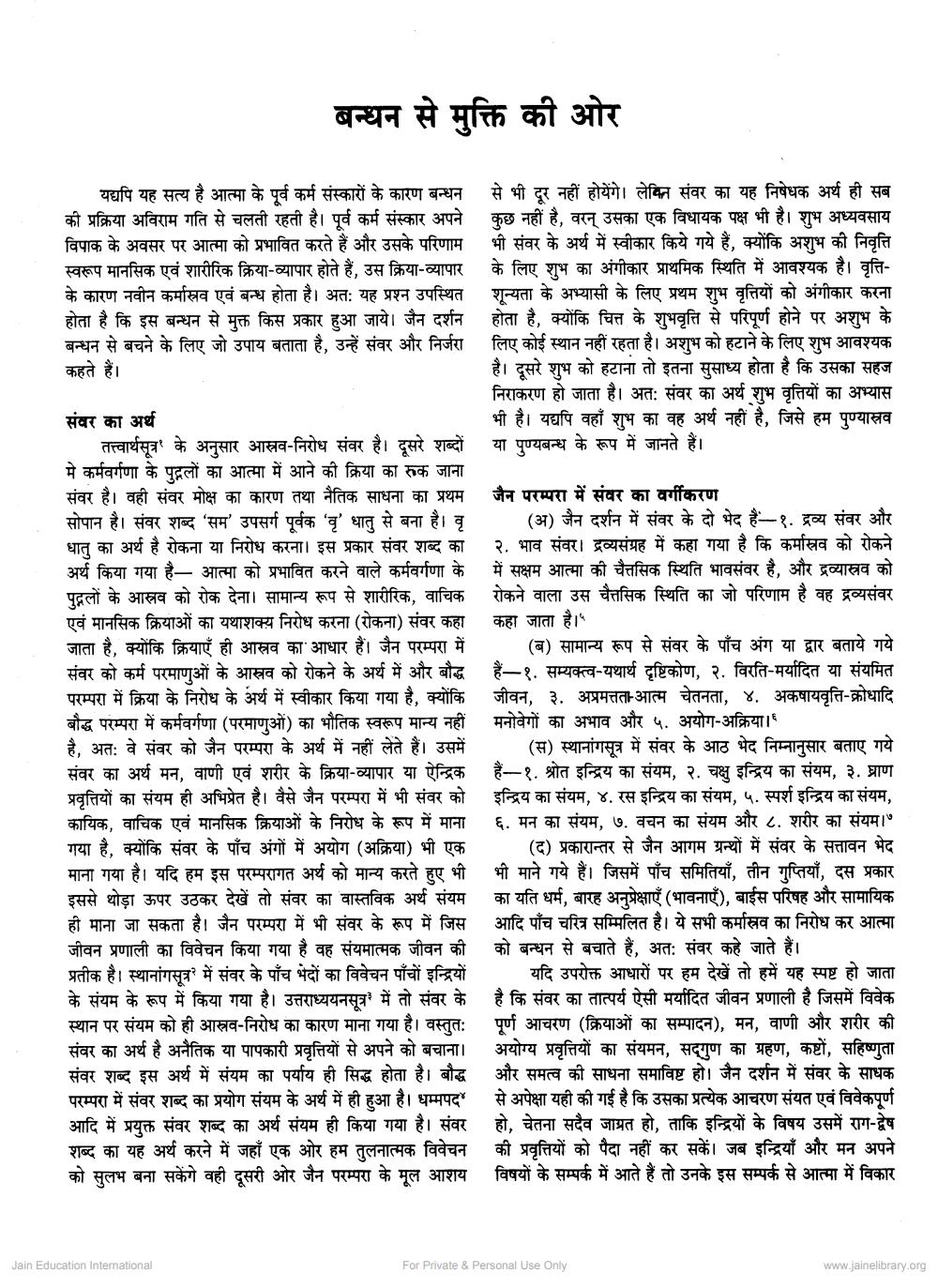________________
यद्यपि यह सत्य है आत्मा के पूर्व कर्म संस्कारों के कारण बन्धन की प्रक्रिया अविराम गति से चलती रहती है। पूर्व कर्म संस्कार अपने विपाक के अवसर पर आत्मा को प्रभावित करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप मानसिक एवं शारीरिक क्रिया व्यापार होते हैं, उस क्रिया व्यापार के कारण नवीन कर्मास्रव एवं बन्ध होता है। अतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस बन्धन से मुक्त किस प्रकार हुआ जाये। जैन दर्शन बन्धन से बचने के लिए जो उपाय बताता है, उन्हें संवर और निर्जरा कहते हैं।
बन्धन से मुक्ति की ओर
-
Jain Education International
संवर का अर्थ
तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार आव निरोध संबर है। दूसरे शब्दों मे कर्मवर्गणा के पुगलों का आत्मा में आने की क्रिया का रूक जाना संवर है। वही संवर मोक्ष का कारण तथा नैतिक साधना का प्रथम सोपान है। संवर शब्द 'सम' उपसर्ग पूर्वक 'वृ' धातु से बना है। वृ धातु का अर्थ है रोकना या निरोध करना। इस प्रकार संवर शब्द का अर्थ किया गया है— आत्मा को प्रभावित करने वाले कर्मवर्गणा के पुद्रलों के आस्रव को रोक देना सामान्य रूप से शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक क्रियाओं का यथाशक्य निरोध करना (रोकना) संवर कहा जाता है, क्योंकि क्रियाएँ ही आस्रव का आधार हैं। जैन परम्परा में संवर को कर्म परमाणुओं के आस्रव को रोकने के अर्थ में और बौद्ध परम्परा में क्रिया के निरोध के अर्थ में स्वीकार किया गया है, क्योंकि बौद्ध परम्परा में कर्मवर्गणा (परमाणुओं) का भौतिक स्वरूप मान्य नहीं है, अतः वे संबर को जैन परम्परा के अर्थ में नहीं लेते हैं। उसमें संवर का अर्थ मन, वाणी एवं शरीर के क्रिया व्यापार या ऐन्द्रिक प्रवृत्तियों का संयम ही अभिप्रेत है। वैसे जैन परम्परा में भी संवर को कायिक, वाचिक एवं मानसिक क्रियाओं के निरोध के रूप में माना गया है, क्योंकि संवर के पाँच अंगों में अयोग (अक्रिया) भी एक माना गया है। यदि हम इस परम्परागत अर्थ को मान्य करते हुए भी इससे थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो संवर का वास्तविक अर्थ संयम ही माना जा सकता है। जैन परम्परा में भी संवर के रूप में जिस जीवन प्रणाली का विवेचन किया गया है वह संयमात्मक जीवन की प्रतीक है। स्थानांगसूत्र में संवर के पाँच भेदों का विवेचन पाँचों इन्द्रियों के संयम के रूप में किया गया है। उत्तराध्ययनसूत्र में तो संवर के स्थान पर संयम को ही आसव-निरोध का कारण माना गया है। वस्तुतः संबर का अर्थ है अनैतिक या पापकारी प्रवृत्तियों से अपने को बचाना। संवर शब्द इस अर्थ में संयम का पर्याय ही सिद्ध होता है। बौद्ध परम्परा में संवर शब्द का प्रयोग संयम के अर्थ में ही हुआ है। धम्मपद' आदि में प्रयुक्त संवर शब्द का अर्थ संयम ही किया गया है। संवर शब्द का यह अर्थ करने में जहाँ एक ओर हम तुलनात्मक विवेचन को सुलभ बना सकेंगे वही दूसरी ओर जैन परम्परा के मूल आशय
से भी दूर नहीं होयेंगे लेकिन संवर का यह निषेधक अर्थ ही सब कुछ नहीं है, वरन् उसका एक विधायक पक्ष भी है शुभ अध्यवसाय भी संवर के अर्थ में स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि अशुभ की निवृत्ति के लिए शुभ का अंगीकार प्राथमिक स्थिति में आवश्यक है। वृत्तिशून्यता के अभ्यासी के लिए प्रथम शुभ वृत्तियों को अंगीकार करना होता है, क्योंकि चित्त के शुभवृत्ति से परिपूर्ण होने पर अशुभ के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। अशुभ को हटाने के लिए शुभ आवश्यक है। दूसरे शुभ को हटाना तो इतना सुसाध्य होता है कि उसका सहज निराकरण हो जाता है। अतः संवर का अर्थ शुभ वृत्तियों का अभ्यास भी है। यद्यपि वहाँ शुभ का वह अर्थ नहीं है, जिसे हम पुण्यासव या पुण्यबन्ध के रूप में जानते हैं।
जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण
(अ) जैन दर्शन में संवर के दो भेद हैं- १. द्रव्य संवर और २. भाव संवर द्रव्यसंग्रह में कहा गया है कि कर्मास्रव को रोकने में सक्षम आत्मा की चैत्तसिक स्थिति भावसंवर है, और द्रव्यास्त्रव को रोकने वाला उस चैत्तसिक स्थिति का जो परिणाम है वह द्रव्यसंवर कहा जाता है । ५
(ब) सामान्य रूप से संवर के पाँच अंग या द्वार बताये गये हैं- १. सम्यक्त्व - यथार्थ दृष्टिकोण, २. विरति मर्यादित या संयमित जीवन, ३ अप्रमत्तता आत्म चेतनता, ४ अकषायवृत्ति-क्रोधादि मनोवेगों का अभाव और ५. अयोग अक्रिया ।
(स) स्थानांगसूत्र में संवर के आठ भेद निम्नानुसार बताए गये हैं - १. श्रोत इन्द्रिय का संयम, २. चक्षु इन्द्रिय का संयम, ३. घ्राण इन्द्रिय का संयम, ४. रस इन्द्रिय का संयम, ५. स्पर्श इन्द्रिय का संयम, ६. मन का संयम, ७ वचन का संयम और ८. शरीर का संयम । *
(द) प्रकारान्तर से जैन आगम ग्रन्थों में संवर के सत्तावन भेद भी माने गये हैं। जिसमें पाँच समितियाँ, तीन गुप्तियाँ, दस प्रकार का यति धर्म, बारह अनुप्रेक्षाएँ (भावनाएँ), बाईस परिषह और सामायिक आदि पाँच चरित्र सम्मिलित है। ये सभी कर्मास्रव का निरोध कर आत्मा को बन्धन से बचाते हैं, अतः संवर कहे जाते हैं।
यदि उपरोक्त आधारों पर हम देखें तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि संवर का तात्पर्य ऐसी मर्यादित जीवन प्रणाली है जिसमें विवेक पूर्ण आचरण ( क्रियाओं का सम्पादन), मन, वाणी और शरीर की अयोग्य प्रवृत्तियों का संयमन, सद्गुण का ग्रहण, कष्टों, सहिष्णुता और समत्व की साधना समाविष्ट हो। जैन दर्शन में संवर के साधक से अपेक्षा यही की गई है कि उसका प्रत्येक आचरण संयत एवं विवेकपूर्ण हो, चेतना सदैव जाग्रत हो, ताकि इन्द्रियों के विषय उसमें राग-द्वेष की प्रवृत्तियों को पैदा नहीं कर सकें। जब इन्द्रियाँ और मन अपने विषयों के सम्पर्क में आते हैं तो उनके इस सम्पर्क से आत्मा में विकार
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.