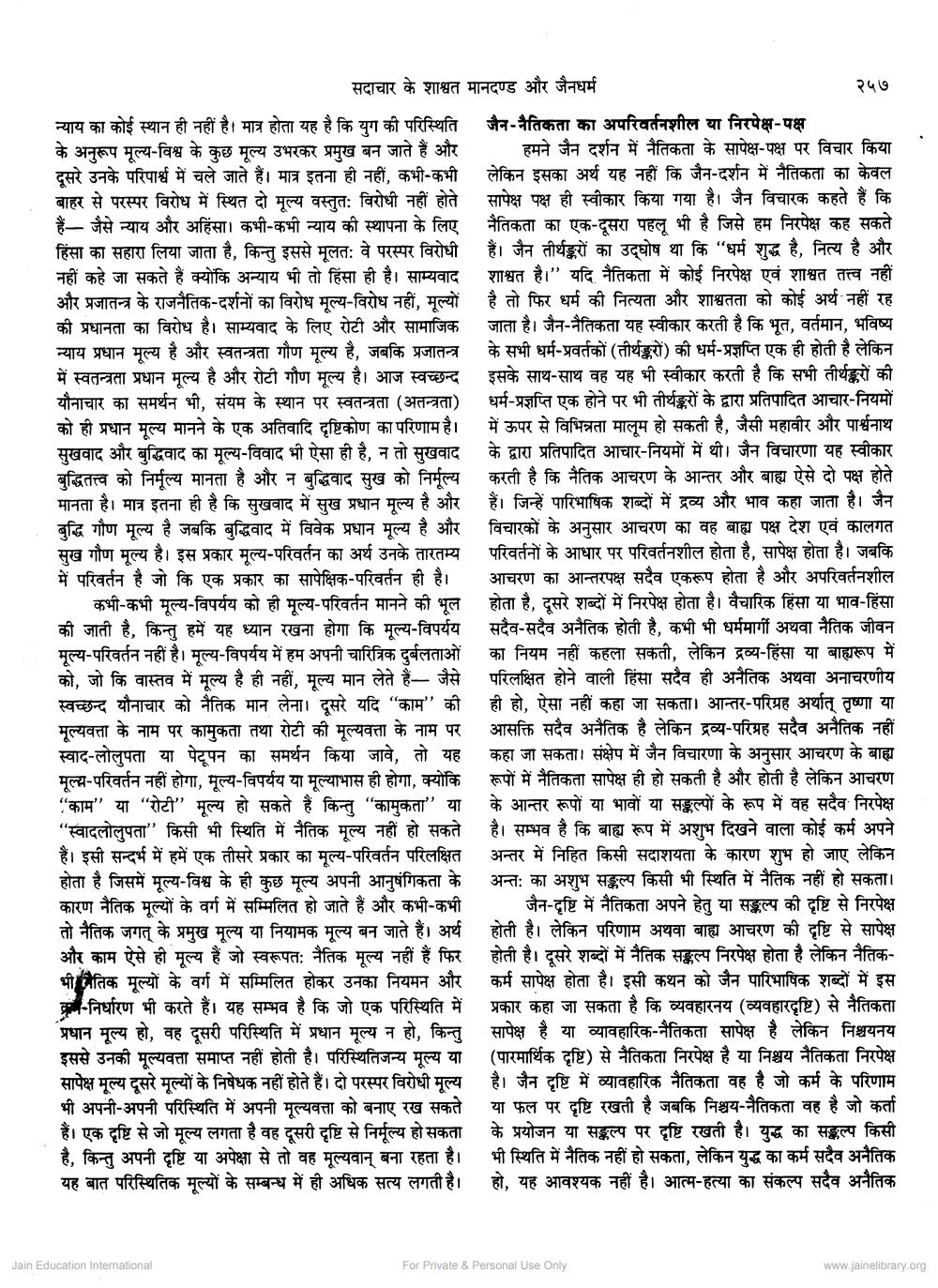________________
सदाचार के शाश्वत मानदण्ड और जैनधर्म
२५७ न्याय का कोई स्थान ही नहीं है। मात्र होता यह है कि युग की परिस्थिति जैन-नैतिकता का अपरिवर्तनशील या निरपेक्ष-पक्ष के अनुरूप मूल्य-विश्व के कुछ मूल्य उभरकर प्रमुख बन जाते हैं और हमने जैन दर्शन में नैतिकता के सापेक्ष-पक्ष पर विचार किया। दूसरे उनके परिपार्श्व में चले जाते हैं। मात्र इतना ही नहीं, कभी-कभी लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जैन-दर्शन में नैतिकता का केवल बाहर से परस्पर विरोध में स्थित दो मूल्य वस्तुत: विरोधी नहीं होते सापेक्ष पक्ष ही स्वीकार किया गया है। जैन विचारक कहते हैं कि हैं- जैसे न्याय और अहिंसा। कभी-कभी न्याय की स्थापना के लिए नैतिकता का एक-दूसरा पहलू भी है जिसे हम निरपेक्ष कह सकते हिंसा का सहारा लिया जाता है, किन्तु इससे मूलत: वे परस्पर विरोधी हैं। जैन तीर्थङ्करों का उद्घोष था कि “धर्म शुद्ध है, नित्य है और नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि अन्याय भी तो हिंसा ही है। साम्यवाद शाश्वत है।" यदि नैतिकता में कोई निरपेक्ष एवं शाश्वत तत्त्व नहीं और प्रजातन्त्र के राजनैतिक-दर्शनों का विरोध मूल्य-विरोध नहीं, मूल्यों है तो फिर धर्म की नित्यता और शाश्वतता को कोई अर्थ नहीं रह की प्रधानता का विरोध है। साम्यवाद के लिए रोटी और सामाजिक जाता है। जैन-नैतिकता यह स्वीकार करती है कि भूत, वर्तमान, भविष्य न्याय प्रधान मूल्य है और स्वतन्त्रता गौण मूल्य है, जबकि प्रजातन्त्र के सभी धर्म-प्रवर्तकों (तीर्थङ्करों) की धर्म-प्रज्ञप्ति एक ही होती है लेकिन में स्वतन्त्रता प्रधान मूल्य है और रोटी गौण मूल्य है। आज स्वच्छन्द इसके साथ-साथ वह यह भी स्वीकार करती है कि सभी तीर्थङ्करों की यौनाचार का समर्थन भी, संयम के स्थान पर स्वतन्त्रता (अतन्त्रता) धर्म-प्रज्ञप्ति एक होने पर भी तीर्थङ्करों के द्वारा प्रतिपादित आचार-नियमों को ही प्रधान मूल्य मानने के एक अतिवादि दृष्टिकोण का परिणाम है। में ऊपर से विभिन्नता मालूम हो सकती है, जैसी महावीर और पार्श्वनाथ सुखवाद और बुद्धिवाद का मूल्य-विवाद भी ऐसा ही है, न तो सुखवाद के द्वारा प्रतिपादित आचार-नियमों में थी। जैन विचारणा यह स्वीकार बुद्धितत्त्व को निर्मूल्य मानता है और न बुद्धिवाद सुख को निर्मूल्य करती है कि नैतिक आचरण के आन्तर और बाह्य ऐसे दो पक्ष होते मानता है। मात्र इतना ही है कि सुखवाद में सुख प्रधान मूल्य है और हैं। जिन्हें पारिभाषिक शब्दों में द्रव्य और भाव कहा जाता है। जैन बुद्धि गौण मूल्य है जबकि बुद्धिवाद में विवेक प्रधान मूल्य है और विचारकों के अनुसार आचरण का वह बाह्य पक्ष देश एवं कालगत सुख गौण मूल्य है। इस प्रकार मूल्य-परिवर्तन का अर्थ उनके तारतम्य परिवर्तनों के आधार पर परिवर्तनशील होता है, सापेक्ष होता है। जबकि में परिवर्तन है जो कि एक प्रकार का सापेक्षिक-परिवर्तन ही है। आचरण का आन्तरपक्ष सदैव एकरूप होता है और अपरिवर्तनशील
कभी-कभी मूल्य-विपर्यय को ही मूल्य-परिवर्तन मानने की भूल होता है, दूसरे शब्दों में निरपेक्ष होता है। वैचारिक हिंसा या भाव-हिंसा की जाती है, किन्तु हमें यह ध्यान रखना होगा कि मूल्य-विपर्यय सदैव-सदैव अनैतिक होती है, कभी भी धर्ममार्गी अथवा नैतिक जीवन मूल्य-परिवर्तन नहीं है। मूल्य-विपर्यय में हम अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं का नियम नहीं कहला सकती, लेकिन द्रव्य-हिंसा या बाह्यरूप में को, जो कि वास्तव में मूल्य है ही नहीं, मूल्य मान लेते हैं- जैसे परिलक्षित होने वाली हिंसा सदैव ही अनैतिक अथवा अनाचरणीय स्वच्छन्द यौनाचार को नैतिक मान लेना। दूसरे यदि “काम' की ही हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आन्तर-परिग्रह अर्थात् तृष्णा या मूल्यवत्ता के नाम पर कामुकता तथा रोटी की मूल्यवत्ता के नाम पर आसक्ति सदैव अनैतिक है लेकिन द्रव्य-परिग्रह सदैव अनैतिक नहीं स्वाद-लोलुपता या पेटूपन का समर्थन किया जावे, तो यह कहा जा सकता। संक्षेप में जैन विचारणा के अनुसार आचरण के बाह्य मूल्य-परिवर्तन नहीं होगा, मूल्य-विपर्यय या मूल्याभास ही होगा, क्योंकि __ रूपों में नैतिकता सापेक्ष ही हो सकती है और होती है लेकिन आचरण “काम' या “रोटी" मूल्य हो सकते हैं किन्तु “कामुकता" या के आन्तर रूपों या भावों या सङ्कल्पों के रूप में वह सदैव निरपेक्ष "स्वादलोलुपता' किसी भी स्थिति में नैतिक मूल्य नहीं हो सकते है। सम्भव है कि बाह्य रूप में अशुभ दिखने वाला कोई कर्म अपने हैं। इसी सन्दर्भ में हमें एक तीसरे प्रकार का मूल्य-परिवर्तन परिलक्षित अन्तर में निहित किसी सदाशयता के कारण शुभ हो जाए लेकिन होता है जिसमें मूल्य-विश्व के ही कुछ मूल्य अपनी आनुषंगिकता के अन्तः का अशुभ सङ्कल्प किसी भी स्थिति में नैतिक नहीं हो सकता। कारण नैतिक मूल्यों के वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं और कभी-कभी जैन-दृष्टि में नैतिकता अपने हेतु या सङ्कल्प की दृष्टि से निरपेक्ष तो नैतिक जगत् के प्रमुख मूल्य या नियामक मूल्य बन जाते हैं। अर्थ होती है। लेकिन परिणाम अथवा बाह्य आचरण की दृष्टि से सापेक्ष और काम ऐसे ही मूल्य हैं जो स्वरूपत: नैतिक मूल्य नहीं हैं फिर होती है। दूसरे शब्दों में नैतिक सङ्कल्प निरपेक्ष होता है लेकिन नैतिकभी नैतिक मूल्यों के वर्ग में सम्मिलित होकर उनका नियमन और कर्म सापेक्ष होता है। इसी कथन को जैन पारिभाषिक शब्दों में इस व-निर्धारण भी करते हैं। यह सम्भव है कि जो एक परिस्थिति में प्रकार कहा जा सकता है कि व्यवहारनय (व्यवहारदृष्टि) से नैतिकता प्रधान मूल्य हो, वह दूसरी परिस्थिति में प्रधान मूल्य न हो, किन्तु सापेक्ष है या व्यावहारिक-नैतिकता सापेक्ष है लेकिन निश्चयनय इससे उनकी मूल्यवत्ता समाप्त नहीं होती है। परिस्थितिजन्य मूल्य या (पारमार्थिक दृष्टि) से नैतिकता निरपेक्ष है या निश्चय नैतिकता निरपेक्ष सापेक्ष मूल्य दूसरे मूल्यों के निषेधक नहीं होते हैं। दो परस्पर विरोधी मूल्य है। जैन दृष्टि में व्यावहारिक नैतिकता वह है जो कर्म के परिणाम भी अपनी-अपनी परिस्थिति में अपनी मूल्यवत्ता को बनाए रख सकते या फल पर दृष्टि रखती है जबकि निश्चय-नैतिकता वह है जो कर्ता हैं। एक दृष्टि से जो मूल्य लगता है वह दूसरी दृष्टि से निर्मूल्य हो सकता के प्रयोजन या सङ्कल्प पर दृष्टि रखती है। युद्ध का सङ्कल्प किसी है, किन्तु अपनी दृष्टि या अपेक्षा से तो वह मूल्यवान् बना रहता है। भी स्थिति में नैतिक नहीं हो सकता, लेकिन युद्ध का कर्म सदैव अनैतिक यह बात परिस्थितिक मूल्यों के सम्बन्ध में ही अधिक सत्य लगती है। हो, यह आवश्यक नहीं है। आत्म-हत्या का संकल्प सदैव अनैतिक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org