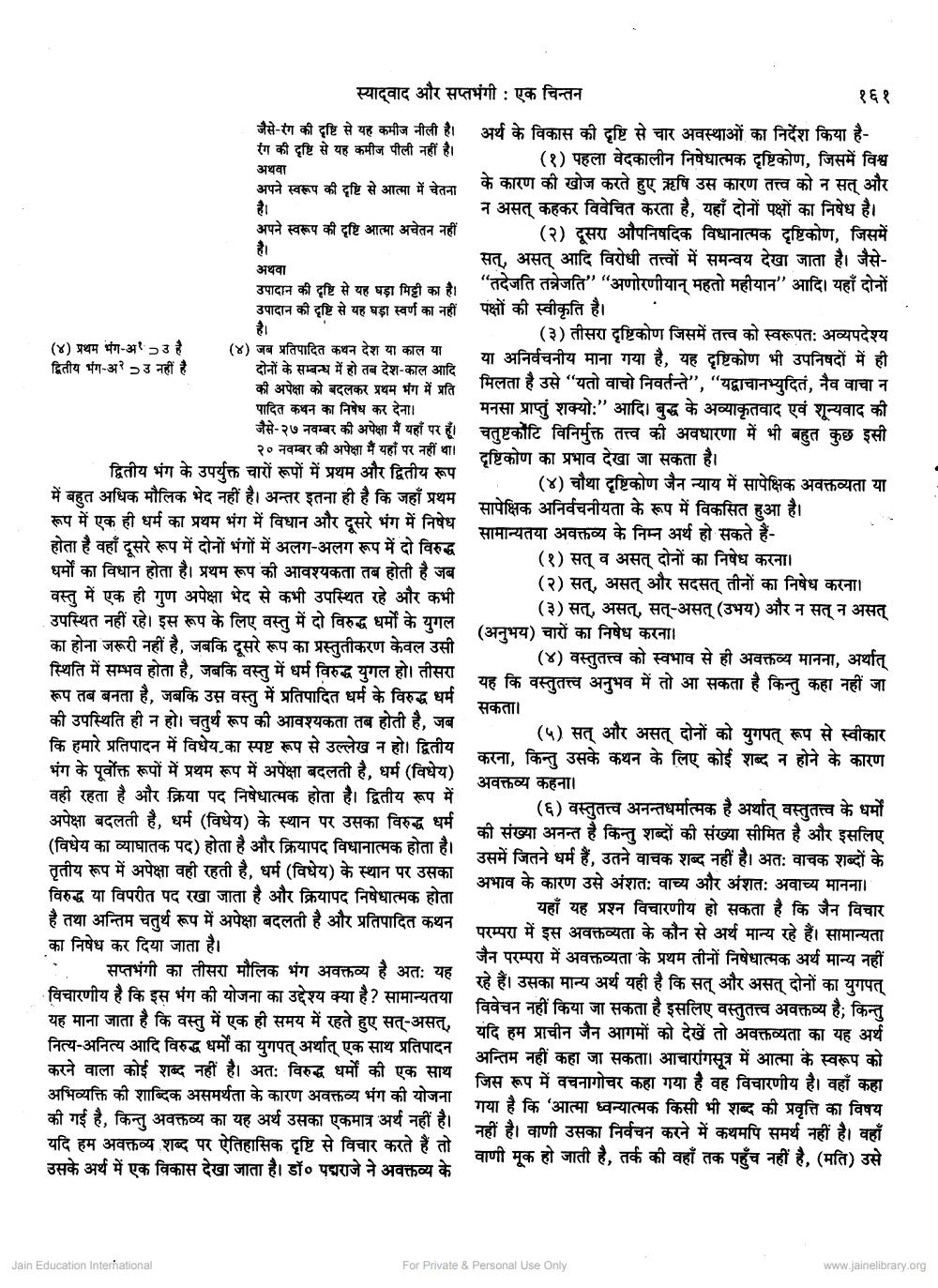________________
स्याद्वाद और सप्तभंगी : एक चिन्तन
१६१ जैसे-रंग की दृष्टि से यह कमीज नीली है। अर्थ के विकास की दृष्टि से चार अवस्थाओं का निर्देश किया हैरंग की दृष्टि से यह कमीज पीली नहीं है।
(१) पहला वेदकालीन निषेधात्मक दृष्टिकोण, जिसमें विश्व अथवा अपने स्वरूप की दृष्टि से आत्मा में चेतना
के कारण की खोज करते हुए ऋषि उस कारण तत्त्व को न सत् और
न असत् कहकर विवेचित करता है, यहाँ दोनों पक्षों का निषेध है। अपने स्वरूप की दृष्टि आत्मा अचेतन नहीं (२) दूसरा औपनिषदिक विधानात्मक दृष्टिकोण, जिसमें
सत, असत् आदि विरोधी तत्त्वों में समन्वय देखा जाता है। जैसेअथवा उपादान की दृष्टि से यह घड़ा मिट्टी का है।
ही “तदेजति तन्नेजति" "अणोरणीयान् महतो महीयान" आदि। यहाँ दोनों
तदजात तन्नजात "अणारणायान् महता महायान" उपादान की दृष्टि से यह घड़ा स्वर्ण का नहीं पक्षों की स्वीकृति है।
(३) तीसरा दृष्टिकोण जिसमें तत्त्व को स्वरूपतः अव्यपदेश्य (४) प्रथम भंग-अ उ है (४) जब प्रतिपादित कथन देश या काल या
या अनिर्वचनीय माना गया है, यह दृष्टिकोण भी उपनिषदों में ही द्वितीय भंग-अ उ नहीं है
दोनों के सम्बन्ध में हो तब देश-काल आदि की अपेक्षा को बदलकर प्रथम भंग में प्रति
मिलता है उसे “यतो वाचो निवर्तन्ते", "यद्वाचानभ्युदितं, नैव वाचा न पादित कथन का निषेध कर देना। मनसा प्राप्तुं शक्योः " आदि। बुद्ध के अव्याकृतवाद एवं शून्यवाद की जैसे-२७ नवम्बर की अपेक्षा मैं यहाँ पर हूँ। चतष्टकोटि विनिर्मुक्त तत्त्व की अवधारणा में भी बहुत कुछ इसी २० नवम्बर की अपेक्षा मैं यहाँ पर नहीं था।
दृष्टिकोण का प्रभाव देखा जा सकता है। द्वितीय भंग के उपर्युक्त चारों रूपों में प्रथम और द्वितीय रूप
(४) चौथा दृष्टिकोण जैन न्याय में सापेक्षिक अवक्तव्यता या में बहुत अधिक मौलिक भेद नहीं है। अन्तर इतना ही है कि जहाँ प्रथम
सापेक्षिक अनिर्वचनीयता के रूप में विकसित हुआ है। रूप में एक ही धर्म का प्रथम भंग में विधान और दूसरे भंग में निषेध
सामान्यतया अवक्तव्य के निम्न अर्थ हो सकते हैंहोता है वहाँ दूसरे रूप में दोनों भंगों में अलग-अलग रूप में दो विरुद्ध
(१) सत् व असत् दोनों का निषेध करना। धर्मों का विधान होता है। प्रथम रूप की आवश्यकता तब होती है जब
(२) सत्, असत् और सदसत् तीनों का निषेध करना। वस्तु में एक ही गुण अपेक्षा भेद से कभी उपस्थित रहे और कभी
(३) सत्, असत्, सत्-असत् (उभय) और न सत् न असत् उपस्थित नहीं रहे। इस रूप के लिए वस्तु में दो विरुद्ध धर्मों के युगल
(अनुभय) चारों का निषेध करना। का होना जरूरी नहीं है, जबकि दूसरे रूप का प्रस्तुतीकरण केवल उसी स्थिति में सम्भव होता है, जबकि वस्तु में धर्म विरुद्ध युगल हो। तीसरा
(४) वस्तुतत्त्व को स्वभाव से ही अवक्तव्य मानना, अर्थात्
यह कि वस्तुतत्त्व अनुभव में तो आ सकता है किन्तु कहा नहीं जा रूप तब बनता है, जबकि उस वस्तु में प्रतिपादित धर्म के विरुद्ध धर्म
सकता। की उपस्थिति ही न हो। चतुर्थ रूप की आवश्यकता तब होती है, जब
(५) सत् और असत् दोनों को युगपत् रूप से स्वीकार कि हमारे प्रतिपादन में विधेय.का स्पष्ट रूप से उल्लेख न हो। द्वितीय
करना, किन्तु उसके कथन के लिए कोई शब्द न होने के कारण भंग के पूर्वोक्त रूपों में प्रथम रूप में अपेक्षा बदलती है, धर्म (विधेय)
अवक्तव्य कहना। वही रहता है और क्रिया पद निषेधात्मक होता है। द्वितीय रूप में
(६) वस्तुतत्त्व अनन्तधर्मात्मक है अर्थात् वस्तुतत्त्व के धर्मों अपेक्षा बदलती है, धर्म (विधेय) के स्थान पर उसका विरुद्ध धर्म
की संख्या अनन्त है किन्तु शब्दों की संख्या सीमित है और इसलिए (विधेय का व्याघातक पद) होता है और क्रियापद विधानात्मक होता है।
उसमें जितने धर्म हैं, उतने वाचक शब्द नहीं है। अत: वाचक शब्दों के तृतीय रूप में अपेक्षा वही रहती है, धर्म (विधेय) के स्थान पर उसका
अभाव के कारण उसे अंशत: वाच्य और अंशत: अवाच्य मानना। विरुद्ध या विपरीत पद रखा जाता है और क्रियापद निषेधात्मक होता
यहाँ यह प्रश्न विचारणीय हो सकता है कि जैन विचार है तथा अन्तिम चतुर्थ रूप में अपेक्षा बदलती है और प्रतिपादित कथन
परम्परा में इस अवक्तव्यता के कौन से अर्थ मान्य रहे हैं। सामान्यता का निषेध कर दिया जाता है।
जैन परम्परा में अवक्तव्यता के प्रथम तीनों निषेधात्मक अर्थ मान्य नहीं • सप्तभंगी का तीसरा मौलिक भंग अवक्तव्य है अत: यह
रहे हैं। उसका मान्य अर्थ यही है कि सत् और असत् दोनों का युगपत् विचारणीय है कि इस भंग की योजना का उद्देश्य क्या है? सामान्यतया ।
विवेचन नहीं किया जा सकता है इसलिए वस्तुतत्त्व अवक्तव्य है; किन्तु यह माना जाता है कि वस्तु में एक ही समय में रहते हुए सत्-असत्,
यदि हम प्राचीन जैन आगमों को देखें तो अवक्तव्यता का यह अर्थ नित्य-अनित्य आदि विरुद्ध धर्मों का युगपत् अर्थात् एक साथ प्रतिपादन
अन्तिम नहीं कहा जा सकता। आचारांगसूत्र में आत्मा के स्वरूप को करने वाला कोई शब्द नहीं है। अत: विरुद्ध धर्मों की एक साथ
जिस रूप में वचनागोचर कहा गया है वह विचारणीय है। वहाँ कहा अभिव्यक्ति की शाब्दिक असमर्थता के कारण अवक्तव्य भंग की योजना
गया है कि 'आत्मा ध्वन्यात्मक किसी भी शब्द की प्रवृत्ति का विषय की गई है, किन्तु अवक्तव्य का यह अर्थ उसका एकमात्र अर्थ नहीं है।
नहीं है। वाणी उसका निर्वचन करने में कथमपि समर्थ नहीं है। वहाँ यदि हम अवक्तव्य शब्द पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते हैं तो
वाणी मूक हो जाती है, तर्क की वहाँ तक पहँच नहीं है, (मति) उसे उसके अर्थ में एक विकास देखा जाता है। डॉ० पद्यराजे ने अवक्तव्य के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org