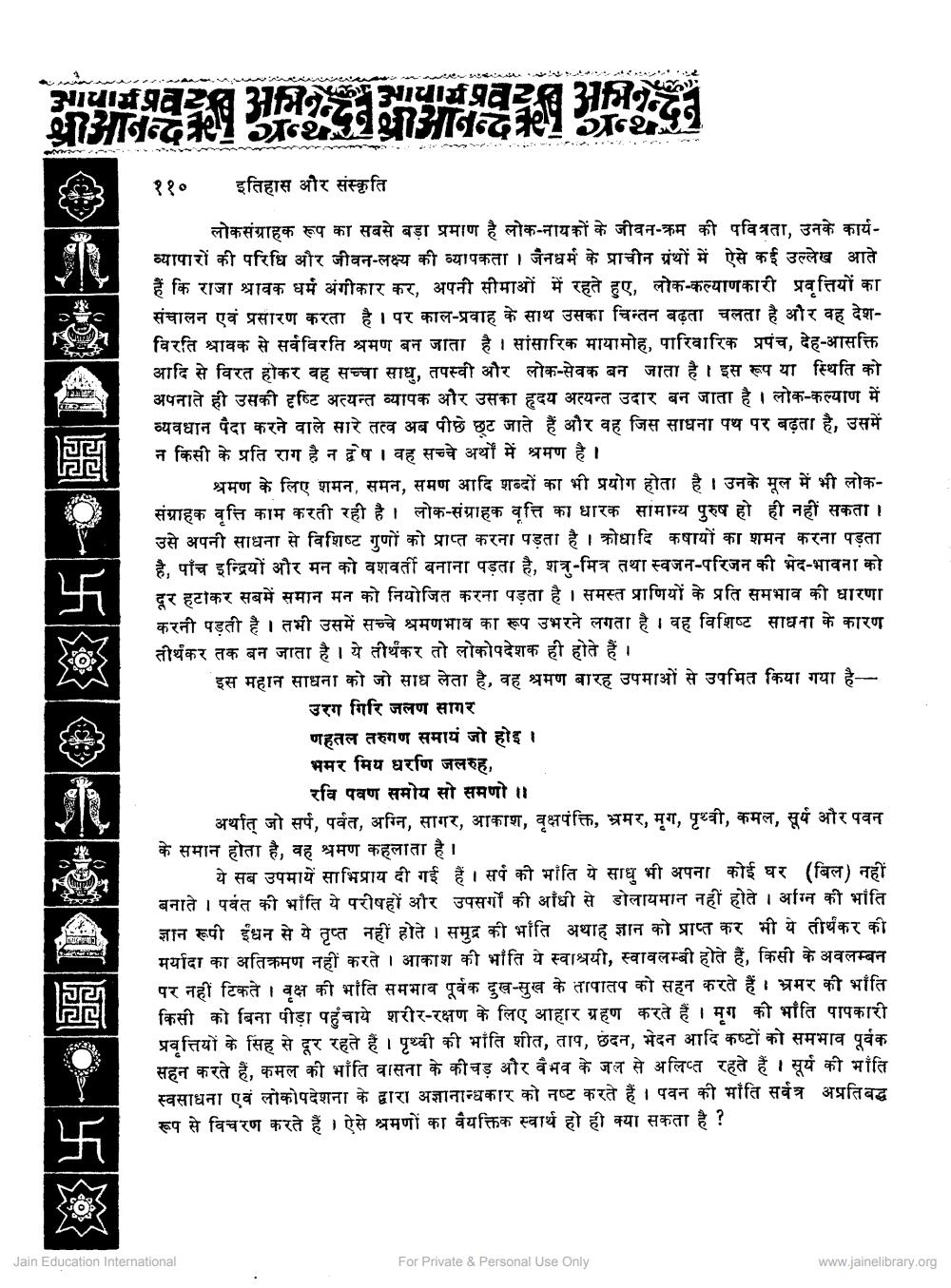________________
आचार्य प्रवास अभि श्री आनन्द ऋ
Ammay
p
११०
अगदी प्रामानन्द आव
ग्रन्थ
इतिहास और संस्कृति
लोकसंग्राहक रूप का सबसे बड़ा प्रमाण है लोक नायकों के जीवन क्रम की पवित्रता, उनके कार्य व्यापारों की परिधि और जीवन-लक्ष्य की व्यापकता जैनधर्म के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई उल्लेख आते हैं कि राजा धावक धर्म अंगीकार कर अपनी सीमाओं में रहते हुए लोक-कल्याणकारी प्रवृत्तियों का संचालन एवं प्रसारण करता है । पर काल-प्रवाह के साथ उसका चिन्तन बढ़ता चलता है और वह देशविरति श्रावक से सर्वविरति श्रमण बन जाता है। सांसारिक मायामोह, पारिवारिक प्रपंच, देह- आसक्ति आदि से विरत होकर वह सच्चा साधु, तपस्वी और लोक सेवक बन जाता है। इस रूप या स्थिति को अपनाते ही उसकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक और उसका हृदय अत्यन्त उदार बन जाता है। लोक-कल्याण में व्यवधान पैदा करने वाले सारे तत्व अब पीछे छूट जाते हैं और वह जिस साधना पथ पर बढ़ता है, उसमें न किसी के प्रति राग है न द्वेष वह सच्चे अर्थों में श्रमण है।
अभिनंदन
Jain Education International
श्रमण के लिए शमन, समन, समण आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। उनके मूल में भी लोकसंग्राहक वृत्ति काम करती रही है। लोक-संग्राहक वृत्ति का धारक सामान्य पुरुष हो ही नहीं सकता। उसे अपनी साधना से विशिष्ट गुणों को प्राप्त करना पड़ता है । क्रोधादि कषायों का शमन करना पड़ता है, पाँच इन्द्रियों और मन को वशवर्ती बनाना पड़ता है, शत्रु-मित्र तथा स्वजन - परिजन की भेद-भावना को दूर हटाकर सबमें समान मन को नियोजित करना पड़ता है । समस्त प्राणियों के प्रति समभाव की धारणा करनी पड़ती है । तभी उसमें सच्चे श्रमणभाव का रूप उभरने लगता है । वह विशिष्ट साधना के कारण तीर्थंकर तक बन जाता है। ये तीर्थंकर तो लोकोपदेशक ही होते हैं ।
इस महान साधना को जो साध लेता है, वह श्रमण बारह उपमाओं से उपभित किया गया है
उरग गिरि जलण सागर
महतल तरुगण समायं जो होइ ।
भमर मिय धरणि जलरुह,
रवि पवण समोय सो समणो ॥
·
अर्थात् जो सर्प, पर्वत, अग्नि, सागर, आकाश, वृक्षपंक्ति, भ्रमर, मृग, पृथ्वी, कमल, सूर्य और पवन के समान होता है, वह भ्रमण कहलाता है।
ये सब उपमायें साभिप्राय दी गई हैं। सर्प की भाँति ये साधु भी अपना कोई घर (बिल) नहीं बनाते । पर्वत की भाँति ये परीषहों और उपसर्गों की आँधी से डोलायमान नहीं होते । अग्नि की भाँति ज्ञान रूपी ईंधन से ये तृप्त नहीं होते। समुद्र की भांति अथाह ज्ञान को प्राप्त कर भी वे तीर्थंकर की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। आकाश की भांति ये स्वाश्रयी, स्वावलम्बी होते हैं, किसी के अवलम्बन पर नहीं टिकते। वृक्ष की भांति समभाव पूर्वक दुख-सुख के तापातप को सहन करते हैं। भ्रमर की भाँति किसी को बिना पीड़ा पहुंचावे शरीर रक्षण के लिए आहार ग्रहण करते हैं। मृग की भाँति पापकारी प्रवृत्तियों के सिंह से दूर रहते हैं। पृथ्वी की भांति शीत, ताप, छंदन, भेदन आदि कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करते हैं, कमल की भाँति वासना के कीचड़ और वैभव के जल से अलिप्त रहते हैं । सूर्य की भाँति स्वसाधना एवं लोकोपदेशना के द्वारा अज्ञानान्धकार को नष्ट करते हैं। पवन की भाँति सर्वत्र अप्रतिबद्ध रूप से विचरण करते हैं। ऐसे श्रमणों का वैयक्तिक स्वार्थ हो ही क्या सकता है ?
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org