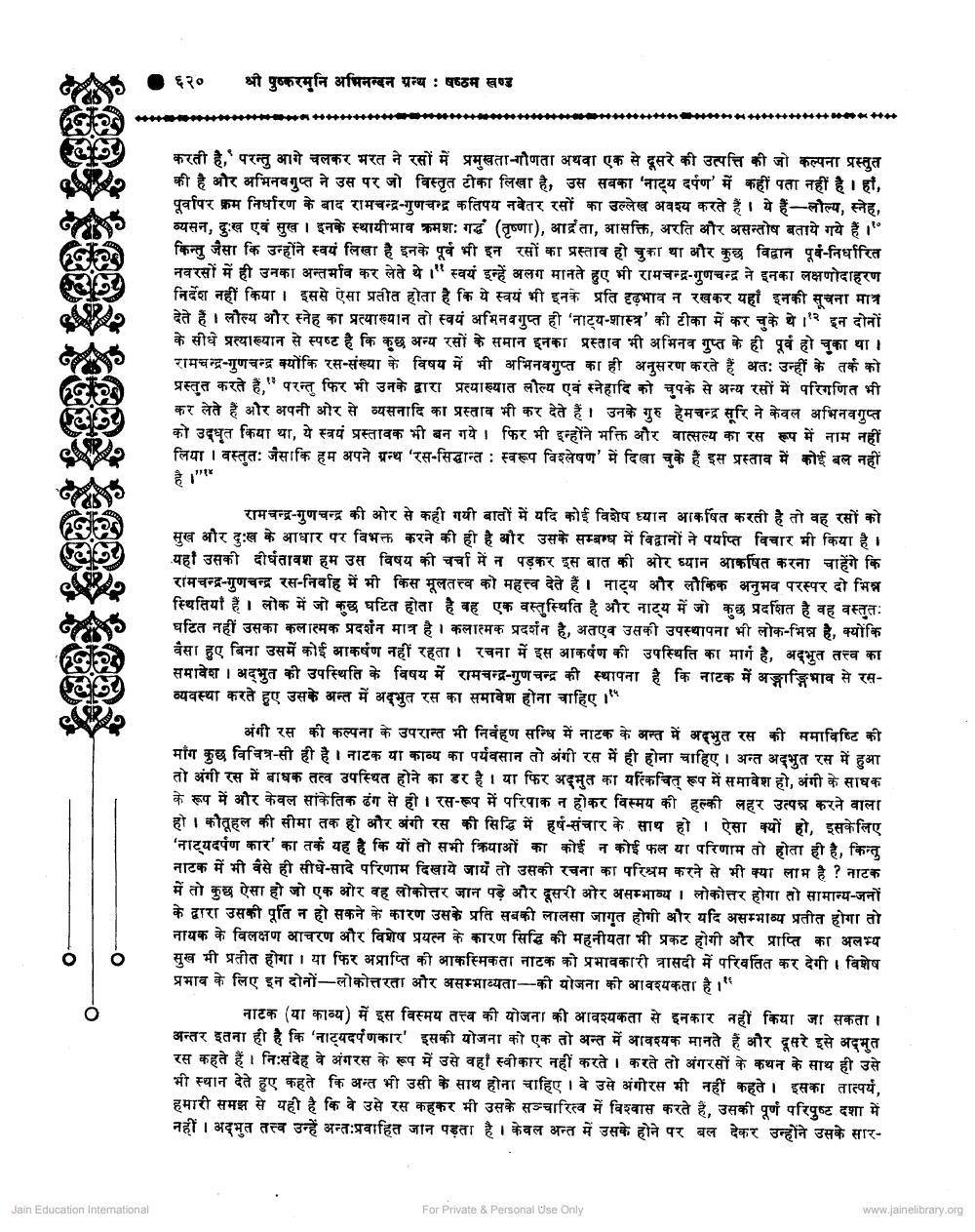________________
०
-०
Jain Education International
६२०
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : षष्ठम खण्ड
**++++
करती है, परन्तु आगे चलकर भरत ने रसों में प्रमुखता - गौणता अथवा एक से दूसरे की उत्पत्ति की जो कल्पना प्रस्तुत की है और अभिनवगुप्त ने उस पर जो विस्तृत टीका लिखा है, उस सबका 'नाट्य दर्पण' में कहीं पता नहीं है। हाँ, पूर्वापर क्रम निर्धारण के बाद रामचन्द्र-गुणचन्द्र कतिपय नवेतर रसों का उल्लेख अवश्य करते हैं। ये हैं-लौल्य, स्नेह, व्यसन, दुःख एवं सुख । इनके स्थायीभाव क्रमश: गद्ध (तृष्णा), आर्द्रता, आसक्ति, अरति और असन्तोष बताये गये हैं । " किन्तु जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है इनके पूर्व भी इन रसों का प्रस्ताव हो चुका था और कुछ विद्वान पूर्व निर्धारित नवरसों में ही उनका अन्तर्भाव कर लेते थे ।" स्वयं इन्हें अलग मानते हुए भी रामचन्द्र गुणचन्द्र ने इनका लक्षणोदाहरण निर्देश नहीं किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वयं भी इनके प्रति दृढ़भाव न रखकर यहाँ इनकी सूचना मात्र देते हैं। लौल्य और स्नेह का प्रत्याख्यान तो स्वयं अभिनवगुप्त ही 'नाट्य शास्त्र' की टीका में कर चुके थे। १२ इन दोनों के सीधे प्रत्याख्यान से स्पष्ट है कि कुछ अन्य रसों के समान इनका प्रस्ताव भी अभिनव गुप्त के ही पूर्व हो चुका था । रामचन्द्र- गुणचन्द्र क्योंकि रस-संख्या के विषय में भी अभिनवगुप्त का ही अनुसरण करते हैं अतः उन्हीं के तर्क को प्रस्तुत करते हैं, " परन्तु फिर भी उनके द्वारा प्रत्याख्यात लौल्य एवं स्नेहादि को चुपके से अन्य रसों में परिगणित भी कर लेते हैं और अपनी ओर से व्यसनादि का प्रस्ताव भी कर देते हैं। उनके गुरु हेमचन्द्र सूरि ने केवल अभिनवगुप्त को उधृत किया था, ये स्वयं प्रस्तावक भी बन गये। फिर भी इन्होंने भक्ति और वात्सल्य का रस रूप में नाम नहीं लिया । वस्तुत: जैसा कि हम अपने ग्रन्थ 'रस- सिद्धान्त: स्वरूप विश्लेषण' में दिखा चुके हैं इस प्रस्ताव में कोई बल नहीं है।
रामचन्द्र- गुणचन्द्र की ओर से कही गयी बातों में यदि कोई विशेष ध्यान आकर्षित करती है तो वह रसों को सुख और दुःख के आधार पर विभक्त करने की ही है और उसके सम्बन्ध में विद्वानों ने पर्याप्त विचार भी किया है । यहाँ उसकी दीर्घतावश हम उस विषय की चर्चा में न पड़कर इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि रामचन्द्र गुणचन्द्र रस- निर्वाह में भी किस मूलतत्त्व को महत्व देते हैं। नाट्य और लौकिक अनुभव परस्पर दो भिन्न स्थितियाँ हैं । लोक में जो कुछ घटित होता है वह एक वस्तुस्थिति है और नाट्य में जो कुछ प्रदर्शित है वह वस्तुतः घटित नहीं उसका कलात्मक प्रदर्शन मात्र है। कलात्मक प्रदर्शन है, अतएव उसकी उपस्थापना भी लोक- भिन्न है, क्योंकि वैसा हुए बिना उसमें कोई आकर्षण नहीं रहता। रचना में इस आकर्षण की उपस्थिति का मार्ग है, अद्भुत तत्त्व का समावेश | अद्भुत की उपस्थिति के विषय में रामचन्द्र गुणचन्द्र की स्थापना है कि नाटक में अङ्गाङ्गिभाव से रसव्यवस्था करते हुए उसके अन्त में अद्भुत रस का समावेश होना चाहिए।"
अंगी रस की कल्पना के उपरान्त भी निर्वहण सन्धि में नाटक के अन्त में अद्भुत रस की समाविष्टि की माँग कुछ विचित्र सी ही है। नाटक या काव्य का पर्यवसान तो अंगी रस में ही होना चाहिए। अन्त अद्भुत रस में हुआ तो अंगी रस में बाधक तत्व उपस्थित होने का डर है। या फिर अद्भुत का यत्किचित् रूप में समावेश हो, अंगी के साधक के रूप में और केवल सांकेतिक ढंग से ही रस रूप में परिपाक न होकर विस्मय की हल्की लहर उत्पन्न करने वाला हो । कौतूहल की सीमा तक हो और अंगी रस की सिद्धि में हर्ष-संचार के साथ हो । ऐसा क्यों हो, इसके लिए 'नाट्यदर्पण कार' का तर्क यह है कि यों तो सभी क्रियाओं का कोई न कोई फल या परिणाम तो होता ही है, किन्तु नाटक में भी वैसे ही सीधे-सादे परिणाम दिखाये जायें तो उसकी रचना का परिश्रम करने से भी क्या लाभ है ? नाटक में तो कुछ ऐसा हो जो एक ओर वह लोकोत्तर जान पड़े और दूसरी ओर असम्भाव्य । लोकोत्तर होगा तो सामान्य जनों के द्वारा उसकी पूर्ति न हो सकने के कारण उसके प्रति सबकी लालसा जागृत होगी और यदि असम्भाव्य प्रतीत होगा तो नायक के विलक्षण आचरण और विशेष प्रयत्न के कारण सिद्धि की महनीयता भी प्रकट होगी और प्राप्ति का अलभ्य सुख भी प्रतीत होगा। या फिर अप्राप्ति की आकस्मिकता नाटक को प्रभावकारी त्रासदी में परिवर्तित कर देगी। विशेष प्रभाव के लिए इन दोनों लोकोत्तरता और असम्भाव्यता - की योजना की आवश्यकता है।"
नाटक ( या काव्य) में इस विस्मय तत्त्व की योजना की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। अन्तर इतना ही है कि 'नाट्यदर्पणकार' इसकी योजना को एक तो अन्त में आवश्यक मानते हैं और दूसरे इसे अद्भुत रस कहते हैं। निःसंदेह वे अंगरस के रूप में उसे वहाँ स्वीकार नहीं करते करते तो अंगरसों के कथन के साथ ही उसे भी स्थान देते हुए कहते कि अन्त भी उसी के साथ होना चाहिए। वे उसे अंगीरस भी नहीं कहते। इसका तात्पर्य, हमारी समझ से यही है कि वे उसे रस कहकर भी उसके सञ्चारित्व में विश्वास करते हैं, उसकी पूर्ण परिपुष्ट दशा में नहीं । अद्भुत तत्त्व उन्हें अन्तःप्रवाहित जान पड़ता है। केवल अन्त में उसके होने पर बल देकर उन्होंने उसके सार
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org