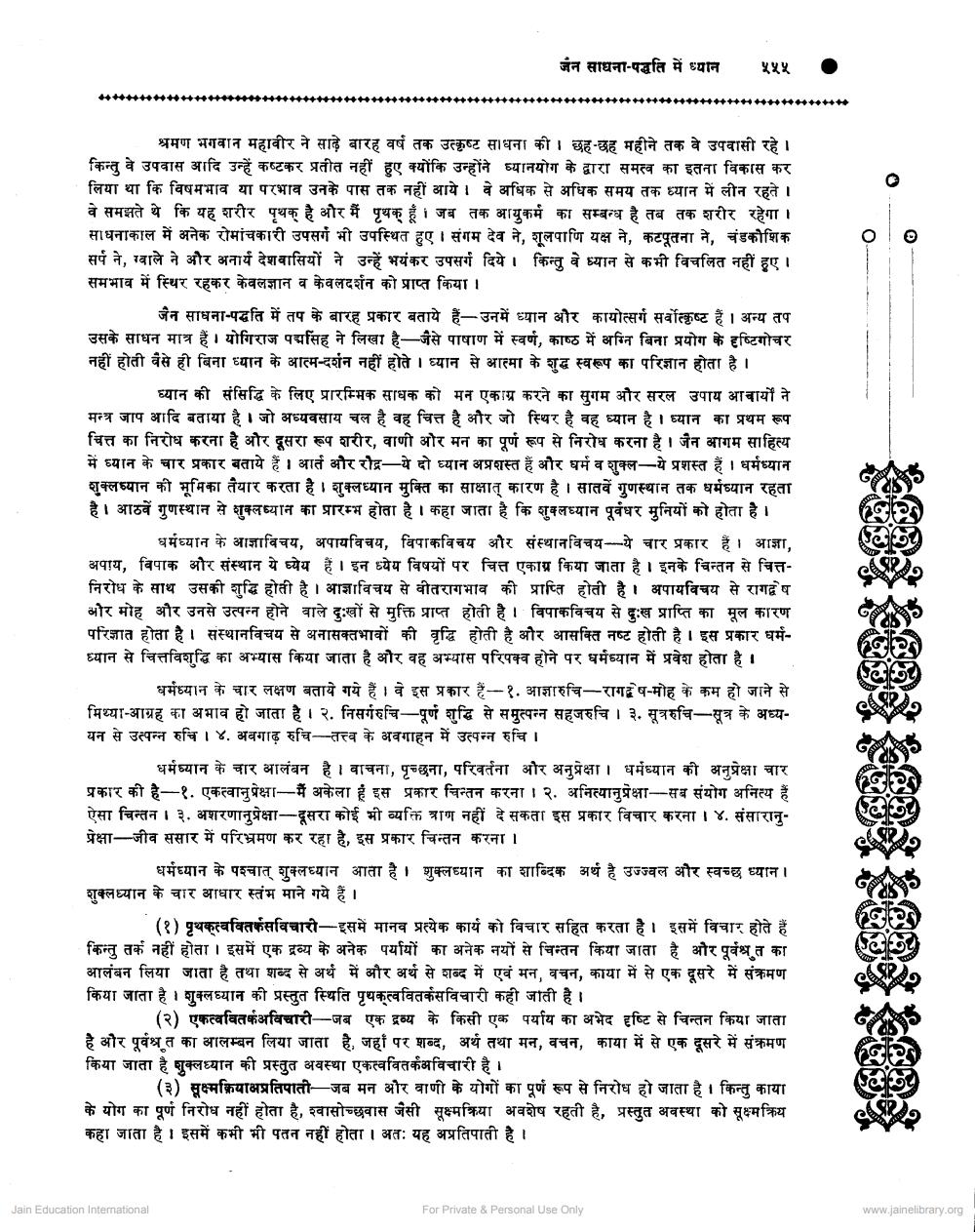________________
जैन साधना-पद्धति में ध्यान
५५५
के द्वारा सा
री उपसा में पृथक् हूँ । जाय। वे अधिक
श्रमण भगवान महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक उत्कृष्ट साधना की। छह-छह महीने तक वे उपवासी रहे । किन्तु वे उपवास आदि उन्हें कष्टकर प्रतीत नहीं हुए क्योंकि उन्होंने ध्यानयोग के द्वारा समत्व का इतना विकास कर लिया था कि विषमभाव या परभाव उनके पास तक नहीं आये। वे अधिक से अधिक समय तक ध्यान में लीन रहते । वे समझते थे कि यह शरीर पृथक् है और मैं पृथक् हूँ। जब तक आयुकर्म का सम्बन्ध है तब तक शरीर रहेगा। साधनाकाल में अनेक रोमांचकारी उपसर्ग भी उपस्थित हुए। संगम देव ने, शूलपाणि यक्ष ने, कटपूतना ने, चंडकौशिक सर्प ने, ग्वाले ने और अनार्य देशवासियों ने उन्हें भयंकर उपसर्ग दिये। किन्तु वे ध्यान से कभी विचलित नहीं हुए। समभाव में स्थिर रहकर केवलज्ञान व केवलदर्शन को प्राप्त किया।
जैन साधना-पद्धति में तप के बारह प्रकार बताये हैं-उनमें ध्यान और कायोत्सर्ग सर्वोत्कृष्ट हैं । अन्य तप उसके साधन मात्र हैं। योगिराज पद्मसिंह ने लिखा है-जैसे पाषाण में स्वर्ण, काष्ठ में अग्नि बिना प्रयोग के दृष्टिगोचर नहीं होती वैसे ही बिना ध्यान के आत्म-दर्शन नहीं होते । ध्यान से आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिज्ञान होता है।
ध्यान की संसिद्धि के लिए प्रारम्भिक साधक को मन एकाग्र करने का सुगम और सरल उपाय आचार्यों ने मन्त्र जाप आदि बताया है। जो अध्यवसाय चल है वह चित्त है और जो स्थिर है वह ध्यान है । ध्यान का प्रथम रूप चित्त का निरोध करना है और दूसरा रूप शरीर, वाणी और मन का पूर्ण रूप से निरोध करना है । जैन आगम साहित्य में ध्यान के चार प्रकार बताये हैं। आर्त और रोद्र—ये दो ध्यान अप्रशस्त हैं और धर्म व शुक्ल-ये प्रशस्त हैं । धर्मध्यान शुक्लध्यान की भूमिका तैयार करता है । शुक्लध्यान मुक्ति का साक्षात् कारण है । सातवें गुणस्थान तक धर्मध्यान रहता है। आठवें गुणस्थान से शुक्लध्यान का प्रारम्भ होता है । कहा जाता है कि शुक्लध्यान पूर्वधर मुनियों को होता है।
धर्मध्यान के आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय-ये चार प्रकार हैं। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान ये ध्येय हैं। इन ध्येय विषयों पर चित्त एकाग्र किया जाता है। इनके चिन्तन से चित्तनिरोध के साथ उसकी शुद्धि होती है । आज्ञाविचय से वीतरागभाव की प्राप्ति होती है। अपायविचय से रागद्वेष
और मोह और उनसे उत्पन्न होने वाले दुःखों से मुक्ति प्राप्त होती है। विपाकविचय से दुःख प्राप्ति का मूल कारण परिज्ञात होता है। संस्थानविचय से अनासक्तभावों की वृद्धि होती है और आसक्ति नष्ट होती है । इस प्रकार धर्मध्यान से चित्तविशुद्धि का अभ्यास किया जाता है और वह अभ्यास परिपक्व होने पर धर्मध्यान में प्रवेश होता है ।
धर्मध्यान के चार लक्षण बताये गये हैं। वे इस प्रकार हैं-१. आज्ञारुचि-रागद्वेष-मोह के कम हो जाने से मिथ्या-आग्रह का अभाव हो जाता है । २. निसर्गरुचिपूर्ण शुद्धि से समुत्पन्न सहजरुचि । ३. सूत्ररुचि-सूत्र के अध्ययन से उत्पन्न रुचि । ४. अवगाढ़ रुचि-तत्त्व के अवगाहन में उत्पन्न रुचि ।
धर्मध्यान के चार आलंबन है। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना और अनुप्रेक्षा। धर्मध्यान की अनुप्रेक्षा चार प्रकार की है-१. एकत्वानुप्रेक्षा-मैं अकेला हूं इस प्रकार चिन्तन करना । २. अनित्यानुप्रेक्षा-सब संयोग अनित्य हैं ऐसा चिन्तन । ३. अशरणानुप्रेक्षा-दूसरा कोई भी व्यक्ति त्राण नहीं दे सकता इस प्रकार विचार करना । ४. संसारानुप्रेक्षा-जीव ससार में परिभ्रमण कर रहा है, इस प्रकार चिन्तन करना ।
धर्मध्यान के पश्चात् शुक्लध्यान आता है। शुक्लध्यान का शाब्दिक अर्थ है उज्ज्वल और स्वच्छ ध्यान । शुक्लध्यान के चार आधार स्तंभ माने गये हैं।
(१) पृथक्त्ववितर्कसविचारो-इसमें मानव प्रत्येक कार्य को विचार सहित करता है। इसमें विचार होते हैं किन्तु तर्क नहीं होता । इसमें एक द्रव्य के अनेक पर्यायों का अनेक नयों से चिन्तन किया जाता है और पूर्वश्रु त का आलंबन लिया जाता है तथा शब्द से अर्थ में और अर्थ से शब्द में एवं मन, वचन, काया में से एक दूसरे में संक्रमण किया जाता है। शुक्लध्यान की प्रस्तुत स्थिति पृथकत्ववितर्कसविचारी कही जाती है।
(२) एकत्ववितर्कअविचारी-जब एक द्रव्य के किसी एक पर्याय का अभेद दृष्टि से चिन्तन किया जाता है और पूर्वश्र त का आलम्बन लिया जाता है, जहाँ पर शब्द, अर्थ तथा मन, वचन, काया में से एक दूसरे में संक्रमण किया जाता है शुक्लध्यान की प्रस्तुत अवस्था एकत्ववितर्कअविचारी है।
(३) सूक्ष्मक्रियामप्रतिपाती-जब मन और वाणी के योगों का पूर्ण रूप से निरोध हो जाता है । किन्तु काया के योग का पूर्ण निरोध नहीं होता है, श्वासोच्छवास जैसी सूक्ष्मक्रिया अवशेष रहती है, प्रस्तुत अवस्था को सूक्ष्म क्रिय कहा जाता है। इसमें कभी भी पतन नहीं होता। अत: यह अप्रतिपाती है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org