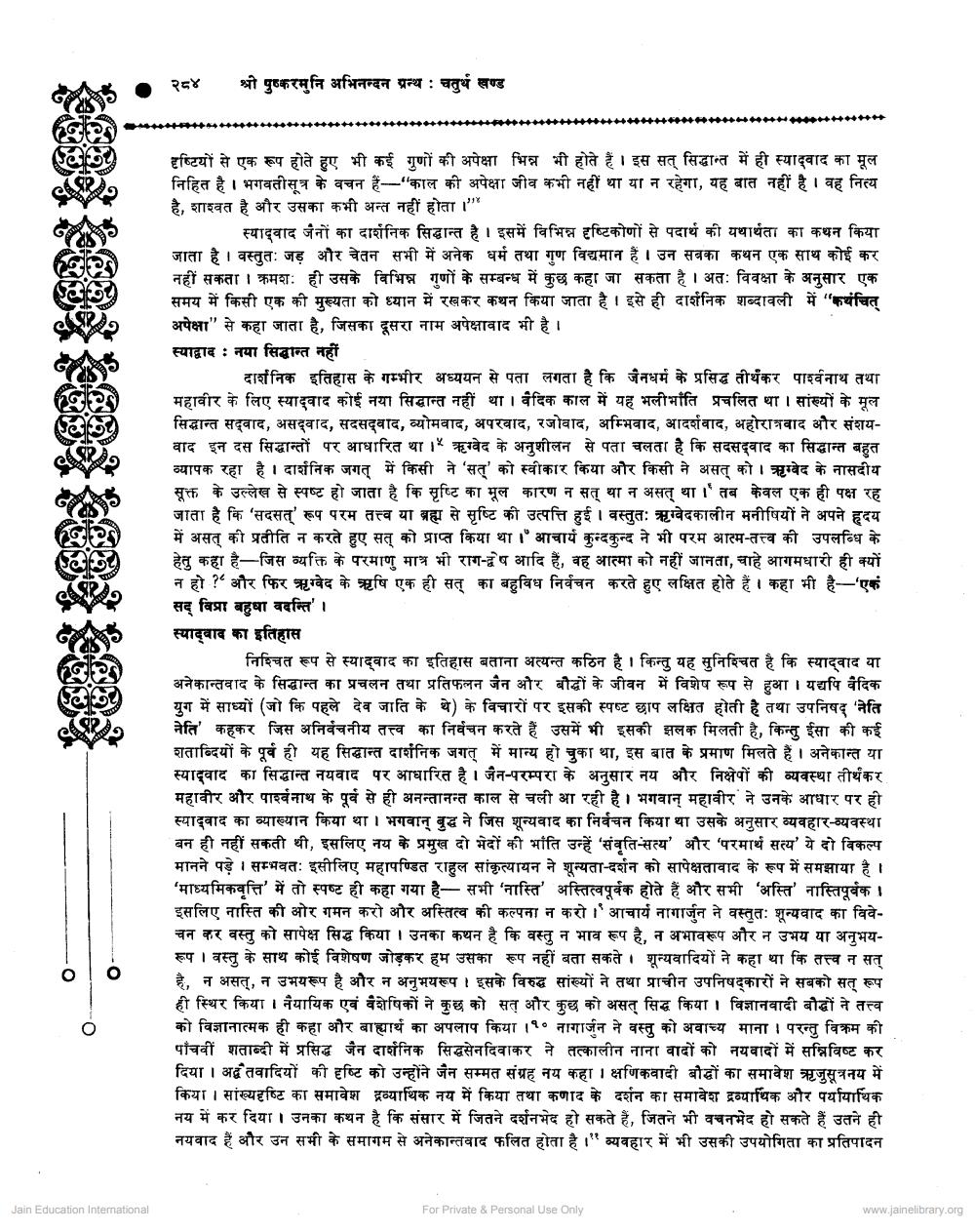________________
२८४
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : चतुर्थ खण्ड
दृष्टियों से एक रूप होते हुए भी कई गुणों की अपेक्षा भिन्न भी होते हैं । इस सत् सिद्धान्त में ही स्याद्वाद का मूल निहित है । भगवतीसूत्र के वचन हैं-"काल की अपेक्षा जीव कभी नहीं था या न रहेगा, यह बात नहीं है । वह नित्य है, शाश्वत है और उसका कभी अन्त नहीं होता।"
स्याद्वाद जैनों का दार्शनिक सिद्धान्त है । इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों से पदार्थ की यथार्थता का कथन किया जाता है। वस्तुतः जड़ और चेतन सभी में अनेक धर्म तथा गुण विद्यमान हैं। उन सबका कथन एक साथ कोई कर नहीं सकता। क्रमशः ही उसके विभिन्न गुणों के सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता है । अत: विवक्षा के अनुसार एक समय में किसी एक की मुख्यता को ध्यान में रखकर कथन किया जाता है । इसे ही दार्शनिक शब्दावली में "कथंचित् अपेक्षा" से कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम अपेक्षावाद भी है । स्याद्वाद : नया सिद्धान्त नहीं
दार्शनिक इतिहास के गम्भीर अध्ययन से पता लगता है कि जैनधर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा महावीर के लिए स्याद्वाद कोई नया सिद्धान्त नहीं था। वैदिक काल में यह भलीभाँति प्रचलित था। सांख्यों के मूल सिद्धान्त सद्वाद, असद्वाद, सदसद्वाद, व्योमवाद, अपरवाद, रजोवाद, अम्भिवाद, आदर्शवाद, अहोरात्रवाद और संशयवाद इन दस सिद्धान्तों पर आधारित था। ऋग्वेद के अनुशीलन से पता चलता है कि सदसद्वाद का सिद्धान्त बहुत व्यापक रहा है । दार्शनिक जगत् में किसी ने 'सत्' को स्वीकार किया और किसी ने असत् को । ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि का मूल कारण न सत् था न असत् था। तब केवल एक ही पक्ष रह जाता है कि 'सदसत्' रूप परम तत्त्व या ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई । वस्तुत: ऋग्वेदकालीन मनीषियों ने अपने हृदय में असत् की प्रतीति न करते हुए सत् को प्राप्त किया था। आचार्य कुन्दकुन्द ने भी परम आत्म-तत्त्व की उपलब्धि के हेतु कहा है-जिस व्यक्ति के परमाणु मात्र भी राग-द्वेष आदि हैं, वह आत्मा को नहीं जानता, चाहे आगमधारी ही क्यों न हो ? और फिर ऋग्वेद के ऋषि एक ही सत् का बहुविध निर्वचन करते हुए लक्षित होते हैं। कहा भी है—'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' । स्याद्वाद का इतिहास
निश्चित रूप से स्याद्वाद का इतिहास बताना अत्यन्त कठिन है । किन्तु यह सुनिश्चित है कि स्याद्वाद या अनेकान्तवाद के सिद्धान्त का प्रचलन तथा प्रतिफलन जैन और बौद्धों के जीवन में विशेष रूप से हुआ। यद्यपि वैदिक युग में साध्यों (जो कि पहले देव जाति के थे) के विचारों पर इसकी स्पष्ट छाप लक्षित होती है तथा उपनिषद् 'नेति नेति' कहकर जिस अनिर्वचनीय तत्त्व का निर्वचन करते हैं उसमें भी इसकी झलक मिलती है, किन्तु ईसा की कई शताब्दियों के पूर्व ही यह सिद्धान्त दार्शनिक जगत् में मान्य हो चुका था, इस बात के प्रमाण मिलते हैं। अनेकान्त या स्याद्वाद का सिद्धान्त नयवाद पर आधारित है । जैन-परम्परा के अनुसार नय और निक्षेपों की व्यवस्था तीर्थंकर महावीर और पार्श्वनाथ के पूर्व से ही अनन्तानन्त काल से चली आ रही है। भगवान् महावीर ने उनके आधार पर ही स्याद्वाद का व्याख्यान किया था। भगवान बुद्ध ने जिस शून्यवाद का निर्वचन किया था उसके अनुसार व्यवहार-व्यवस्था बन ही नहीं सकती थी, इसलिए नय के प्रमुख दो भेदों की भांति उन्हें 'संवृति-सत्य' और 'परमार्थ सत्य' ये दो विकल्प मानने पड़े । सम्भवतः इसीलिए महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने शुन्यता-दर्शन को सापेक्षतावाद के रूप में समझाया है । 'माध्यमिकवृत्ति' में तो स्पष्ट ही कहा गया है- सभी 'नास्ति' अस्तित्वपूर्वक होते हैं और सभी ‘अस्ति' नास्तिपूर्वक । इसलिए नास्ति की ओर गमन करो और अस्तित्व की कल्पना न करो। आचार्य नागार्जुन ने वस्तुतः शून्यवाद का विवेचन कर वस्तु को सापेक्ष सिद्ध किया। उनका कथन है कि वस्तु न भाव रूप है, न अभावरूप और न उभय या अनुभयरूप । वस्तु के साथ कोई विशेषण जोड़कर हम उसका रूप नहीं बता सकते। शून्यवादियों ने कहा था कि तत्त्व न सत् है, न असत्, न उभयरूप है और न अनुभयरूप। इसके विरुद्ध सांख्यों ने तथा प्राचीन उपनिषद्कारों ने सबको सत् रूप ही स्थिर किया । नैयायिक एवं वैशेषिकों ने कुछ को सत् और कुछ को असत् सिद्ध किया। विज्ञानवादी बौद्धों ने तत्त्व को विज्ञानात्मक ही कहा और बाह्यार्थ का अपलाप किया ।१० नागार्जुन ने वस्तु को अवाच्य माना । परन्तु विक्रम की पाँचवीं शताब्दी में प्रसिद्ध जैन दार्शनिक सिद्धसेनदिवाकर ने तत्कालीन नाना वादों को नयवादों में सन्निविष्ट कर दिया। अद्वैतवादियों की दृष्टि को उन्होंने जैन सम्मत संग्रह नय कहा । क्षणिकवादी बौद्धों का समावेश ऋजुसूत्रनय में किया । सांख्यदृष्टि का समावेश द्रव्याथिक नय में किया तथा कणाद के दर्शन का समावेश द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय में कर दिया। उनका कथन है कि संसार में जितने दर्शनभेद हो सकते हैं, जितने भी वचनभेद हो सकते हैं उतने ही नयवाद हैं और उन सभी के समागम से अनेकान्तवाद फलित होता है । " व्यवहार में भी उसकी उपयोगिता का प्रतिपादन
००
पाँचवा
दयों की दृष्टि को उन्हान
किया तथा कणाद के दर्शन
क
वचनभेद हो सकते हैं उतना
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org