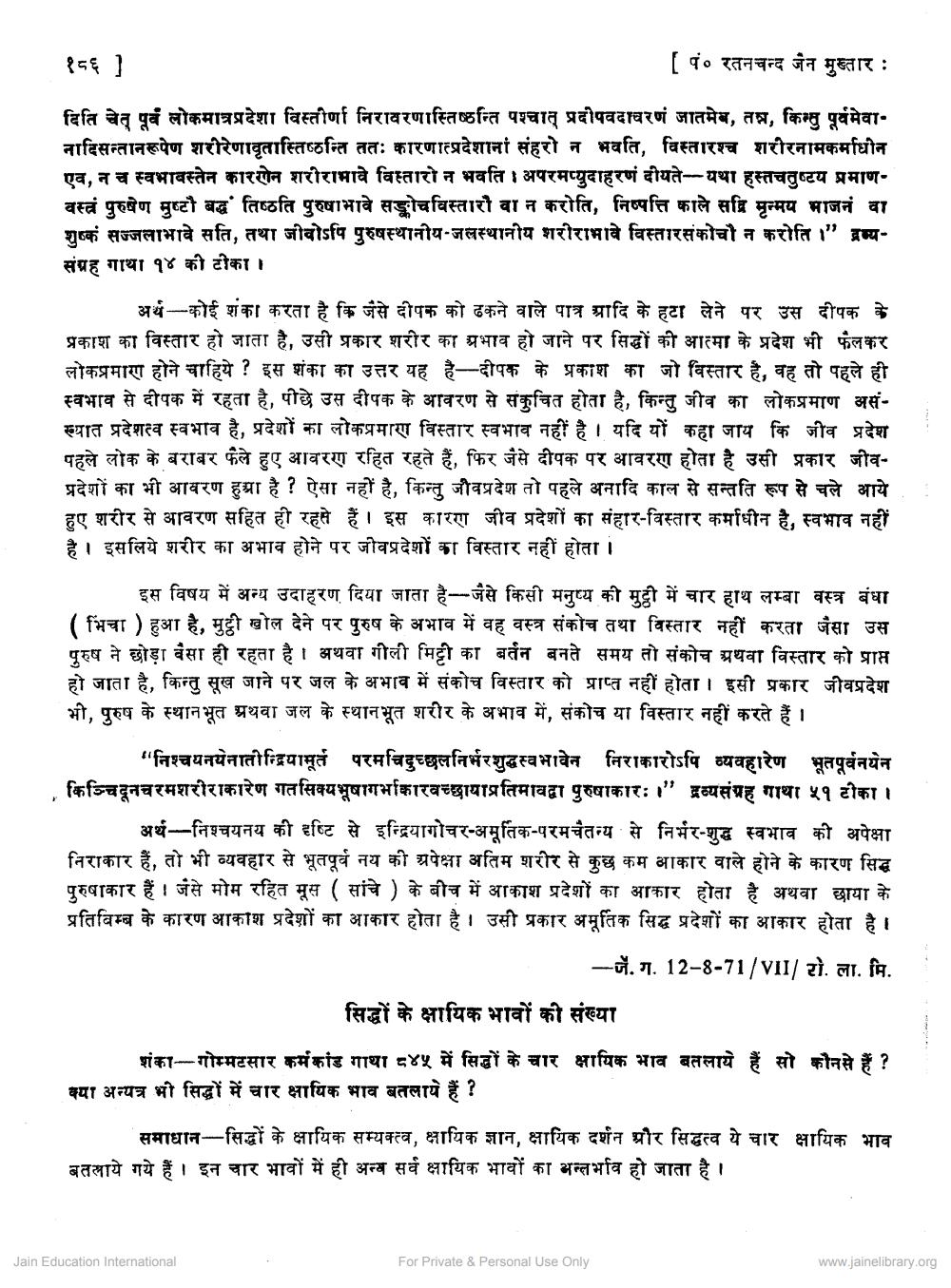________________
१८६ ]
[ पं० रतनचन्द जैन मुख्तार :
दिति चेत् पूर्वं लोकमात्र प्रदेशा विस्तीर्णा निरावरणास्तिष्ठन्ति पश्चात् प्रदीपवदाचरणं जातमेब, तन, किन्तु पूर्वमेवानादिसन्तानरूपेण शरीरेणावृतास्तिष्ठन्ति ततः कारणात्प्रदेशानां संहरो न भवति, विस्तारश्च शरीरनामकर्माधीन एव, न च स्वभावस्तेन कारखेन शरीराभावे विस्तारो न भवति । अपरमप्युदाहरणं दीयते यथा हस्तचतुष्टय प्रमाणवस्त्रं पुरुषेण मुष्टौ बद्ध ं तिष्ठति पुरुषाभावे सङ्कोचविस्तारौ वा न करोति, निष्पत्ति काले सहि मृन्मय भाजनं वा शुष्कं सज्जलाभावे सति तथा जीवोऽपि पुरुषस्थानीय जलस्थानीय शरीराभावे विस्तारसंकोचौ न करोति ।" द्रव्यसंग्रह गाथा १४ की टीका ।
अर्थ – कोई शंका करता है कि जैसे दीपक को ढकने वाले पात्र आदि के हटा लेने पर उस दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार शरीर का प्रभाव हो जाने पर सिद्धों की आत्मा के प्रदेश भी फैलकर लोकप्रमाण होने चाहिये ? इस शंका का उत्तर यह है— दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है, वह तो पहले ही स्वभाव से दीपक में रहता है, पीछे उस दीपक के आवरण से संकुचित होता है, किन्तु जीव का लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है, प्रदेशों का लोकप्रमाण विस्तार स्वभाव नहीं है । यदि यों कहा जाय कि जीव प्रदेश पहले लोक के बराबर फैले हुए आवरण रहित रहते हैं, फिर जैसे दीपक पर आवरण होता है उसी प्रकार जीवप्रदेशों का भी आवरण हुआ है ? ऐसा नहीं है, किन्तु जीवप्रदेश तो पहले अनादि काल से सन्तति रूप से चले आये हुए शरीर से आवरण सहित ही रहते हैं । इस कारण जीव प्रदेशों का संहार विस्तार कर्माधीन है, स्वभाव नहीं है । इसलिये शरीर का अभाव होने पर जीवप्रदेशों का विस्तार नहीं होता ।
इस विषय में अन्य उदाहरण दिया जाता है-जैसे किसी मनुष्य की मुट्ठी में चार हाथ लम्बा वस्त्र बंधा ( भिचा ) हुआ है, मुट्ठी खोल देने पर पुरुष के अभाव में वह वस्त्र संकोच तथा विस्तार नहीं करता जैसा उस पुरुष ने छोड़ा वैसा ही रहता है । अथवा गीली मिट्टी का बर्तन बनते समय तो संकोच अथवा विस्तार को प्राप्त हो जाता है, किन्तु सूख जाने पर जल के अभाव में संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जीवप्रदेश भी, पुरुष के स्थानभूत प्रथवा जल के स्थानभूत शरीर के अभाव में, संकोच या विस्तार नहीं करते हैं ।
" निश्चयनयेनातीन्द्रियामूर्त परमचिदुच्छलनिर्भरशुद्धस्वभावेन निराकारोऽपि व्यवहारेण भूतपूर्वनयेन किञ्चिदूनच रमशरीराकारेण गत सिक्यभूषागर्भाकारवच्छायाप्रतिमावद्वा पुरुषाकारः ।" द्रव्यसंग्रह गाथा ५१ टीका ।
अर्थ - निश्चयनय की दृष्टि से इन्द्रियागोचर- अमूर्तिक- परमचैतन्य से निर्भर - शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा निराकार हैं, तो भी व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा अतिम शरीर से कुछ कम आकार वाले होने के कारण सिद्ध पुरुषाकार हैं । जैसे मोम रहित मूस ( सांचे ) के बीच में आकाश प्रदेशों का आकार होता है अथवा छाया के प्रतिविम्ब के कारण आकाश प्रदेशों का आकार होता है। उसी प्रकार अमूर्तिक सिद्ध प्रदेशों का आकार होता है ।
- जै. ग. 12 - 8 - 71 / VII / रो. ला. मि.
सिद्धों के क्षायिक भावों की संख्या
शंका - गोम्मटसार कर्मकांड गाथा ८४५ में सिद्धों के चार क्षायिक भाव बतलाये हैं सो कौनसे हैं ? क्या अन्यत्र भी सिद्धों में चार क्षायिक भाव बतलाये हैं ?
समाधान - सिद्धों के क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन श्रौर सिद्धत्व ये चार क्षायिक भाव बतलाये गये हैं । इन चार भावों में ही अन्य सर्व क्षायिक भावों का अन्तर्भाव हो जाता है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org