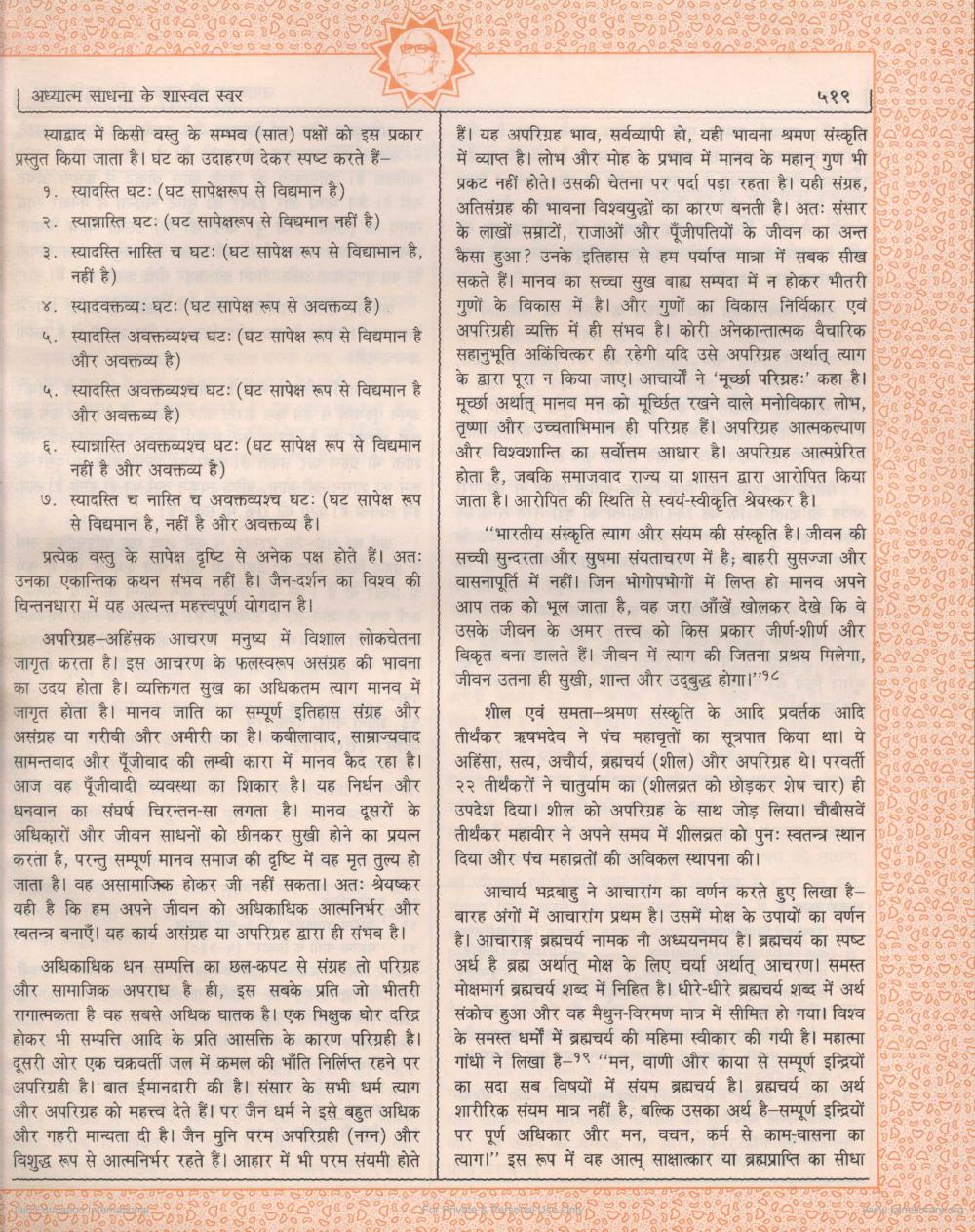________________
अध्यात्म साधना के शास्वत स्वर
स्याद्वाद में किसी वस्तु के सम्भव (सात) पक्षों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। घट का उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं
१. स्यादस्ति घट (घट सापेक्षरूप से विद्यमान है )
२. स्यान्नास्ति घट (घट सापेक्षरूप से विद्यमान नहीं है) ३. स्यादस्ति नास्ति च घटः (घट सापेक्ष रूप से विद्यामान है, नहीं है)
४. स्यादवक्तव्यः घट (घट सापेक्ष रूप से अवक्तव्य है) ५. स्यादस्ति अवक्तव्यश्च घटः (घट सापेक्ष रूप से विद्यमान है और अवक्तव्य है)
५. स्यादस्ति अवक्तव्यश्च घटः (घट सापेक्ष रूप से विद्यमान है और अवक्तव्य है)
६. स्यान्नास्ति अवक्तव्यश्च घटः (घट सापेक्ष रूप से विद्यमान नहीं है और अवक्तव्य है)
७. स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च घटः (घट सापेक्ष रूप से विद्यमान है, नहीं है और अवक्तव्य है।
प्रत्येक वस्तु के सापेक्ष दृष्टि से अनेक पक्ष होते हैं। अतः उनका एकान्तिक कथन संभव नहीं है। जैन दर्शन का विश्व की चिन्तनधारा में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान है।
अपरिग्रह-अहिंसक आचरण मनुष्य में विशाल लोकचेतना जागृत करता है। इस आचरण के फलस्वरूप असंग्रह की भावना का उदय होता है। व्यक्तिगत सुख का अधिकतम त्याग मानव में जागृत होता है। मानव जाति का सम्पूर्ण इतिहास संग्रह और असंग्रह या गरीबी और अमीरी का है। कबीलावाद, साम्राज्यवाद सामन्तवाद और पूँजीवाद की लम्बी कारा में मानव कैद रहा है। आज वह पूँजीवादी व्यवस्था का शिकार है। यह निर्धन और धनवान का संघर्ष चिरन्तन-सा लगता है। मानव दूसरों के अधिकारों और जीवन साधनों को छीनकर सुखी होने का प्रयत्न करता है, परन्तु सम्पूर्ण मानव समाज की दृष्टि में वह मृत तुल्य हो जाता है। वह असामाजिक होकर जी नहीं सकता। अतः श्रेयष्कर यही है कि हम अपने जीवन को अधिकाधिक आत्मनिर्भर और स्वतन्त्र बनाएँ। यह कार्य असंग्रह या अपरिग्रह द्वारा ही संभव है।
अधिकाधिक धन सम्पत्ति का छल-कपट से संग्रह तो परिग्रह और सामाजिक अपराध है ही, इस सबके प्रति जो भीतरी रागात्मकता है वह सबसे अधिक घातक है। एक भिक्षुक घोर दरिद्र होकर भी सम्पत्ति आदि के प्रति आसक्ति के कारण परिग्रही है। दूसरी ओर एक चक्रवर्ती जल में कमल की भाँति निर्लिप्त रहने पर अपरिग्रही है। बात ईमानदारी की है। संसार के सभी धर्म त्याग और अपरिग्रह को महत्त्व देते हैं। पर जैन धर्म ने इसे बहुत अधिक और गहरी मान्यता दी है। जैन मुनि परम अपरिग्रही (नग्न) और विशुद्ध रूप से आत्मनिर्भर रहते हैं। आहार में भी परम संयमी होते
५१९
हैं। यह अपरिग्रह भाव, सर्वव्यापी हो, यही भावना श्रमण संस्कृति में व्याप्त है। लोभ और मोह के प्रभाव में मानव के महान् गुण भी प्रकट नहीं होते। उसकी चेतना पर पर्दा पड़ा रहता है। यही संग्रह, अतिसंग्रह की भावना विश्वयुद्धों का कारण बनती है। अतः संसार के लाखों सम्राटों, राजाओं और पूँजीपतियों के जीवन का अन्त कैसा हुआ ? उनके इतिहास से हम पर्याप्त मात्रा में सबक सीख सकते हैं। मानव का सच्चा सुख बाह्य सम्पदा में न होकर भीतरी । गुणों के विकास में है। और गुणों का विकास निर्विकार एवं अपरिग्रही व्यक्ति में ही संभव है। कोरी अनेकान्तात्मक वैचारिक सहानुभूति अकिंचित्कर ही रहेगी यदि उसे अपरिग्रह अर्थात् त्याग के द्वारा पूरा न किया जाए। आचार्यों ने 'मूर्च्छा परिग्रहः' कहा है। मूर्च्छा अर्थात् मानव मन को मूर्च्छित रखने वाले मनोविकार लोभ, तृष्णा और उच्चताभिमान ही परिग्रह है। अपरिग्रह आत्मकल्याण और विश्वशान्ति का सर्वोत्तम आधार है। अपरिग्रह आत्मप्रेरित होता है, जबकि समाजवाद राज्य या शासन द्वारा आरोपित किया जाता है। आरोपित की स्थिति से स्वयं स्वीकृति श्रेयस्कर है।
"भारतीय संस्कृति त्याग और संयम की संस्कृति है । जीवन की सच्ची सुन्दरता और सुषमा संयताचरण में है; बाहरी सुसज्जा और वासनापूर्ति में नहीं जिन भोगोपभोगों में लिप्त हो मानव अपने आप तक को भूल जाता है, वह जरा आँखें खोलकर देखे कि वे उसके जीवन के अमर तत्त्व को किस प्रकार जीर्ण-शीर्ण और विकृत बना डालते हैं। जीवन में त्याग की जितना प्रश्रय मिलेगा, जीवन उतना ही सुखी, शान्त और उबुद्ध होगा।"१८
शील एवं समता - श्रमण संस्कृति के आदि प्रवर्तक आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने पंच महावृतों का सूत्रपात किया था ये अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य (शील) और अपरिग्रह थे। परवर्ती २२ तीर्थंकरों ने चातुर्याम का ( शीलव्रत को छोड़कर शेष चार) ही उपदेश दिया। शील को अपरिग्रह के साथ जोड़ लिया। चौबीसवें तीर्थंकर महावीर ने अपने समय में शीलव्रत को पुनः स्वतन्त्र स्थान दिया और पंच महाव्रतों की अविकल स्थापना की।
आचार्य भद्रबाहु ने आचारांग का वर्णन करते हुए लिखा हैबारह अंगों में आचारांग प्रथम है। उसमें मोक्ष के उपायों का वर्णन है। आचाराङ्ग ब्रह्मचर्य नामक नौ अध्ययनमय है। ब्रह्मचर्य का स्पष्ट अर्ध हैं ब्रह्म अर्थात् मोक्ष के लिए चर्या अर्थात् आचरण समस्त मोक्षमार्ग ब्रह्मचर्य शब्द में निहित है। धीरे-धीरे ब्रह्मचर्य शब्द में अर्थ संकोच हुआ और वह मैथुन-विरमण मात्र में सीमित हो गया । विश्व के समस्त धर्मों में ब्रह्मचर्य की महिमा स्वीकार की गयी है। महात्मा गांधी ने लिखा है - १९ “ मन, वाणी और काया से सम्पूर्ण इन्द्रियों का सदा सब विषयों में संयम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ शारीरिक संयम मात्र नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है- सम्पूर्ण इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार और मन, वचन, कर्म से काम वासना का त्याग।" इस रूप में वह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मप्राप्ति का सीधा
१७७४