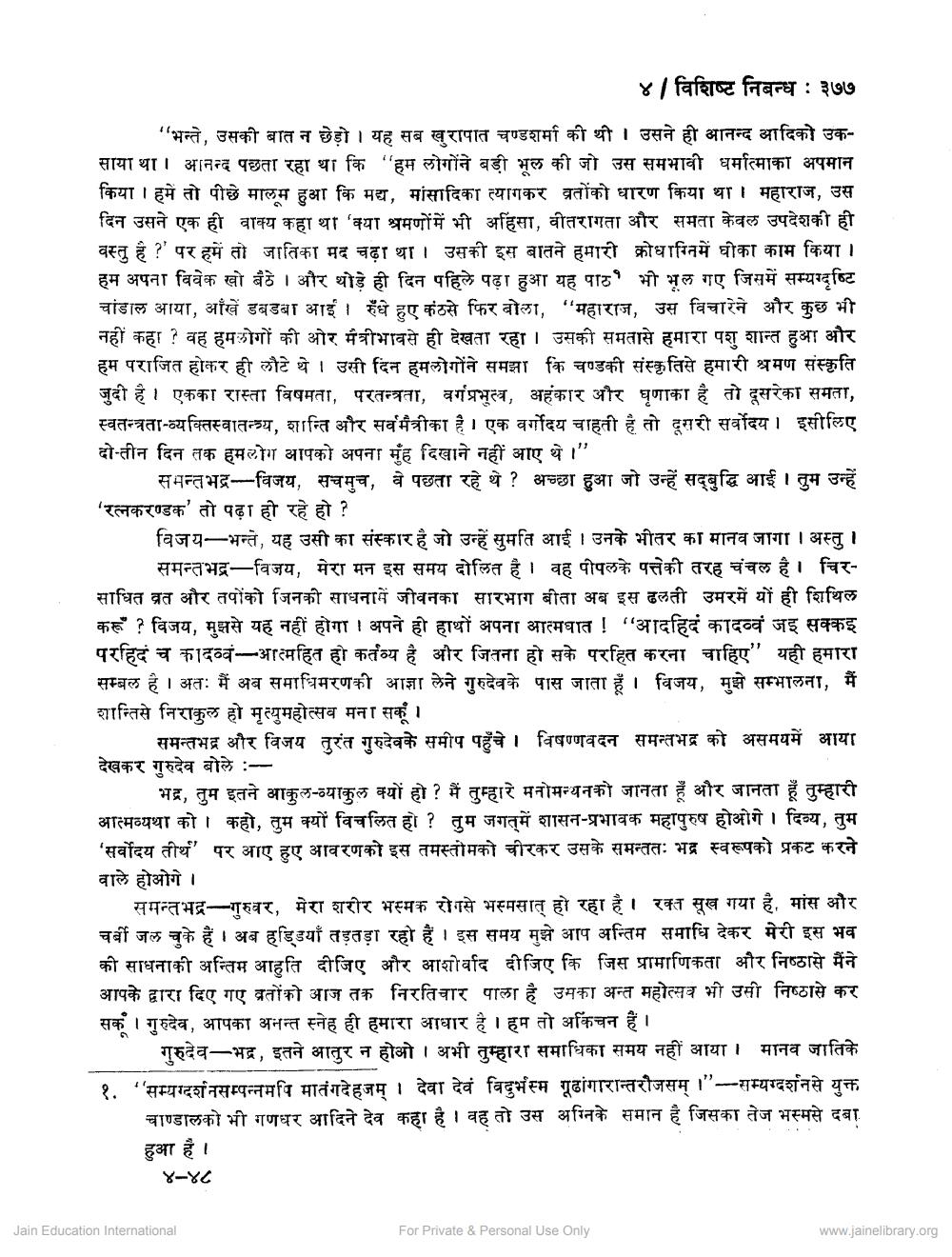________________
४ / विशिष्ट निबन्ध : ३७७
"भन्ते, उसकी बात न छेड़ो। यह सब खुरापात चण्डशर्मा की थी। उसने ही आनन्द आदिको उकसाया था। आनन्द पछता रहा था कि "हम लोगोंने बड़ी भूल की जो उस समभावी धर्मात्माका अपमान किया । हमें तो पीछे मालम हुआ कि मद्य, मांसादिका त्यागकर व्रतोंको धारण किया था। महाराज, उस दिन उसने एक ही वाक्य कहा था 'क्या श्रमणों में भी अहिंसा, वीतरागता और समता केवल उपदेशकी ही वस्तु है ?' पर हमें तो जातिका मद चढ़ा था। उसकी इस बातने हमारी क्रोधाग्निमें घीका काम किया। हम अपना विवेक खो बैठे । और थोड़े ही दिन पहिले पढ़ा हुआ यह पाठ भी भूल गए जिसमें सम्यग्दृष्टि चांडाल आया, आँखें डबडबा आई। रुंधे हए कंठसे फिर बोला, "महाराज, उस विचारेने और कुछ भी नहीं कहा ? वह हमलोगों की ओर मैत्रीभावसे ही देखता रहा। उसकी समतासे हमारा पशु शान्त हुआ और हम पराजित होकर ही लौटे थे । उसी दिन हमलोगोंने समझा कि चण्डकी संस्कृतिसे हमारी श्रमण संस्कृति जुदी है। एकका रास्ता विषमता, परतन्त्रता, वर्गप्रभुत्व, अहंकार और घणाका है तो दूसरेका समता, स्वतन्त्रता-व्यक्तिस्वातन्त्र्य, शान्ति और सर्वमैत्रीका है । एक वर्गोदय चाहती है तो दूसरी सर्वोदय । इसीलिए दो-तीन दिन तक हमलोग आपको अपना मुंह दिखाने नहीं आए थे।"
समन्तभद्र-विजय, सचमुच, वे पछता रहे थे ? अच्छा हुआ जो उन्हें सद्बुद्धि आई । तुम उन्हें 'रत्नकरण्डक' तो पढ़ा हो रहे हो?
विजय-भन्ते, यह उसी का संस्कार है जो उन्हें सुमति आई । उनके भीतर का मानव जागा । अस्तु ।
समन्तभद्र-विजय, मेरा मन इस समय दोलित है। वह पीपलके पत्तेकी तरह चंचल है। चिरसाधित व्रत और तपोंको जिनकी साधनामें जीवनका सारभाग बीता अब इस ढलती उमरमें यों ही शिथिल करूं? विजय, मुझसे यह नहीं होगा । अपने ही हाथों अपना आत्मघात ! "आदहिदं कादव्वं जइ सक्कइ परहिदं च कादव्वं-आत्महित हो कर्तव्य है और जितना हो सके परहित करना चाहिए" यही हमारा सम्बल है । अतः मैं अब समाधिमरणकी आज्ञा लेने गुरुदेवके पास जाता हैं। विजय, मुझे सम्भालना, मैं शान्तिसे निराकुल हो मृत्युमहोत्सव मना सकूँ।
समन्तभद्र और विजय तुरंत गुरुदेवके समीप पहुँचे । विषण्णवदन समन्तभद्र को असमयमें आया देखकर गुरुदेव बोले :
भद्र, तुम इतने आकुल-व्याकुल क्यों हो? मैं तुम्हारे मनोमन्यनको जानता हूँ और जानता हूँ तुम्हारी आत्मव्यथा को। कहो, तुम क्यों विचलित हो ? तुम जगत्में शासन-प्रभावक महापुरुष होओगे । दिव्य, तुम 'सर्वोदय तीर्थ' पर आए हए आवरणको इस तमस्तोमको चीरकर उसके समन्ततः भद्र स्वरूपको प्रकट करने वाले होओगे।
समन्तभद्र-गुरुवर, मेरा शरीर भस्मक रोगसे भस्मसात् हो रहा है। रक्त सूख गया है, मांस और चर्बी जल चुके हैं । अब हड्डियाँ तड़तड़ा रहो है । इस समय मुझे आप अन्तिम समाधि देकर मेरी इस भव की साधनाकी अन्तिम आहति दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि जिस प्रामाणिकता और निष्ठासे मैंने आपके द्वारा दिए गए व्रतोंको आज तक निरतिचार पाला है उसका अन्त महोत्सव भी उसी निष्ठासे कर सर्वं । गुरुदेव, आपका अनन्त स्नेह ही हमारा आधार है । हम तो अकिंचन हैं।
गुरुदेव-भद्र, इतने आतुर न होओ। अभी तुम्हारा समाधिका समय नहीं आया। मानव जातिके १. 'सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातंगदेहजम् । देवा देवं विदुर्भस्म गूढांगारान्तरौजसम् ।"-सम्यग्दर्शनसे युक्त
चाण्डालको भी गणधर आदिने देव कहा है। वह तो उस अग्निके समान है जिसका तेज भस्मसे दबा हुआ है।
४-४८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org