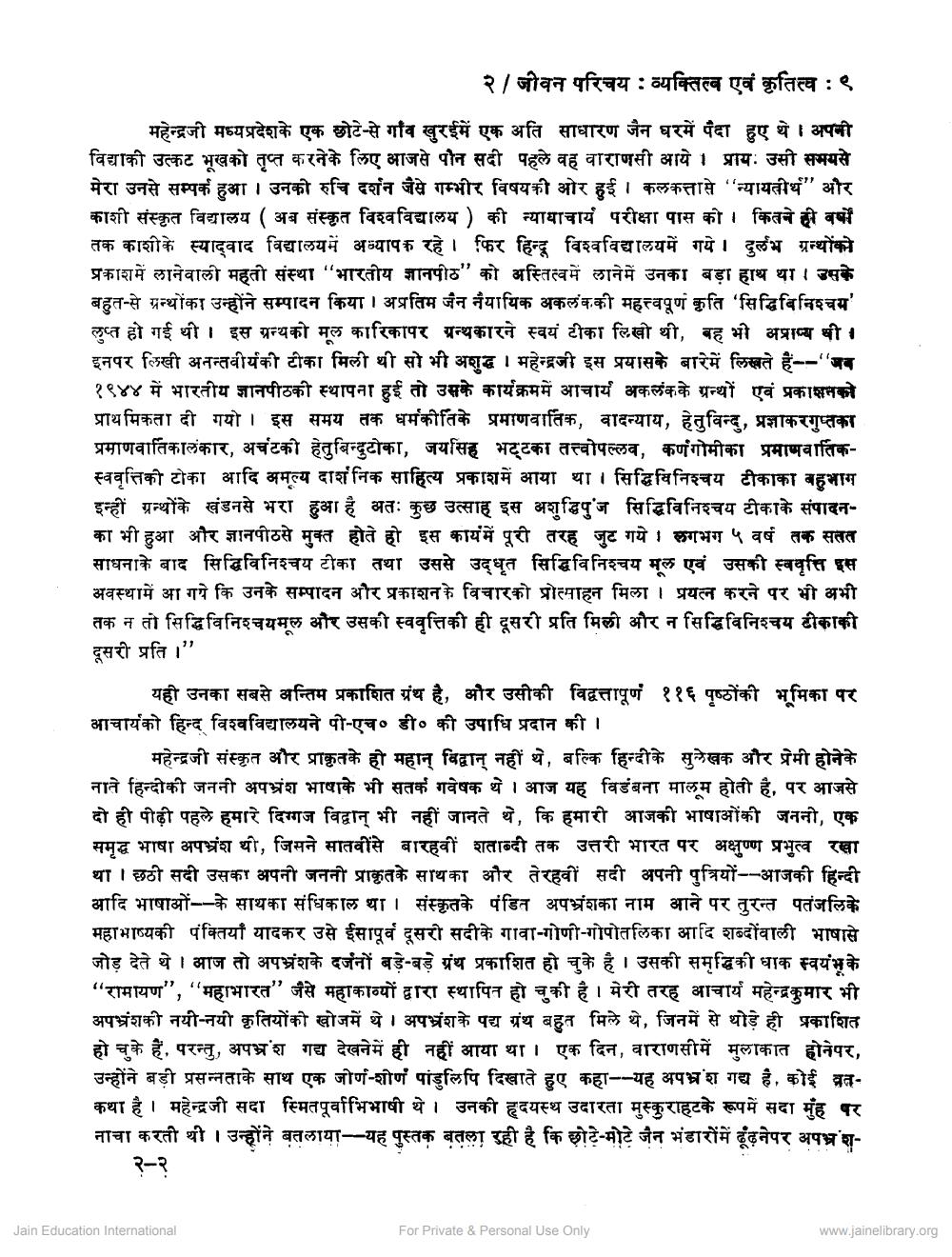________________
२ / जीवन परिचय : व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ९
महेन्द्रजी मध्यप्रदेश के एक छोटे से गाँव खुरईमें एक अति साधारण जैन घरमें पैदा हुए थे । अपनी विद्याकी उत्कट भूखको तृप्त करने के लिए आजसे पौन सदी पहले वह वाराणसी आये । प्रायः उसी समय से मेरा उनसे सम्पर्क हुआ । उनकी रुचि दर्शन जैसे गम्भीर विषयकी ओर हुई । कलकत्तासे " न्यायतीर्थं" और काशी संस्कृत विद्यालय ( अब संस्कृत विश्वविद्यालय ) की न्यायाचार्य परीक्षा पास की। कितने ही वर्षों तक काशी के स्यादवाद विद्यालय में अध्यापक रहे। फिर हिन्दू विश्वविद्यालय में गये । दुर्लभ ग्रन्थोंको प्रकाश में लानेवाली महती संस्था "भारतीय ज्ञानपीठ" को अस्तित्व में लाने में उनका बड़ा हाथ था। उसके बहुत-से ग्रन्थों का उन्होंने सम्पादन किया । अप्रतिम जैन नैयायिक अकलंककी महत्त्वपूर्ण कृति 'सिद्धिविनिश्चय' लुप्त हो गई थी । इस ग्रन्थको मूल कारिकापर ग्रन्थकारने स्वयं टीका लिखी थी, वह भी अप्राप्य थी । इनपर लिखी अनन्तवीर्यकी टीका मिली थी सो भी अशुद्ध । महेन्द्रजी इस प्रयास के बारेमें लिखते हैं-- "जब १९४४ में भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना हुई तो उसके कार्यक्रममें आचार्य अकलंक के ग्रन्थों एवं प्रकाशनको प्राथमिकता दी गयो । इस समय तक धर्मकीर्तिके प्रमाणवार्तिक, वादन्याय हेतुविन्दु, प्रज्ञाकरगुप्तका प्रमाणवार्तिकालंकार, अर्चंटकी हेतुबिन्दुटोका, जयसिंह भट्टका तत्त्वोपल्लव, कर्णंगोमीका प्रमाणवार्तिकस्ववृत्तिकी टोका आदि अमूल्य दार्शनिक साहित्य प्रकाश में आया था । सिद्धिविनिश्चय टीकाका बहुभाग इन्हीं ग्रन्थोंके खंडनसे भरा हुआ है अतः कुछ उत्साह इस अशुद्धिपुज सिद्धिविनिश्चय टीकाके संपादनका भी हुआ और ज्ञानपीठसे मुक्त होते हो इस कार्य में पूरी तरह जुट गये । लगभग ५ वर्ष तक सतत साधना के बाद सिद्धिविनिश्चय टीका तथा उससे उद्धृत सिद्धिविनिश्चय मूल एवं उसकी स्ववृत्ति इस अवस्था में आ गये कि उनके सम्पादन और प्रकाशन के विचारको प्रोत्साहन मिला । प्रयत्न करने पर भी अभी तक न तो सिद्धिविनिश्चयमूल और उसकी स्ववृत्तिकी ही दूसरी प्रति मिली और न सिद्धिविनिश्चय टीकाकी दूसरी प्रति । "
यही उनका सबसे अन्तिम प्रकाशित ग्रंथ है, और उसीकी विद्वत्तापूर्ण ११६ पृष्ठोंकी भूमिका पर आचार्यको हिन्दू विश्वविद्यालयने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की ।
महेन्द्रजी संस्कृत और प्राकृतके हो महान् विद्वान् नहीं थे, बल्कि हिन्दीके सुलेखक और प्रेमी होनेके नाते हिन्दोकी जननी अपभ्रंश भाषाके भी सतर्क गवेषक थे । आज यह विडंबना मालूम होती है, पर आजसे दो ही पीढ़ी पहले हमारे दिग्गज विद्वान् भी नहीं जानते थे, कि हमारी आजकी भाषाओंकी जननी एक समृद्ध भाषा अपभ्रंश थी, जिसने सातवींसे बारहवीं शताब्दी तक उत्तरी भारत पर अक्षुण्ण प्रभुत्व रखा था । छठी सदी उसका अपनी जननी प्राकृतके साथका और तेरहवीं सदी अपनी पुत्रियों -- आजकी हिन्दी आदि भाषाओं - - के साथका संधिकाल था । संस्कृतके पंडित अपभ्रंशका नाम आने पर तुरन्त पतंजलिके महाभाष्यकी पंक्तियाँ यादकर उसे ईसापूर्व दूसरी सदी के गावा-गोणी-गोपोतलिका आदि शब्दोंवाली भाषासे जोड़ देते थे । आज तो अपभ्रंशके दर्जनों बड़े-बड़े ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। उसकी समृद्धिकी धाक स्वयंभू के “रामायण”, “महाभारत” जैसे महाकाव्यों द्वारा स्थापित हो चुकी है । मेरी तरह आचार्य महेन्द्रकुमार भी अपभ्रंशकी नयी-नयी कृतियों की खोजमें थे । अपभ्रंशके पद्य ग्रंथ बहुत मिले थे, जिनमें से थोड़े ही प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु, अपभ्रंश गद्य देखने में ही नहीं आया था । एक दिन, वाराणसी में मुलाकात होनेपर, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक जीर्ण-शीर्णं पांडुलिपि दिखाते हुए कहा -- यह अपभ्रंश गद्य है, कोई व्रतकथा है । महेन्द्रजी सदा स्मितपूर्वाभिभाषी थे । उनकी हृदयस्थ उदारता मुस्कुराहटके रूपमें सदा मुँह पर नाचा करती थी । उन्होंने बतलाया -- यह पुस्तक बतला रही है कि छोटे-मोटे जैन भंडारोंमें ढूंढनेपर अपभ्रं शु२-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org