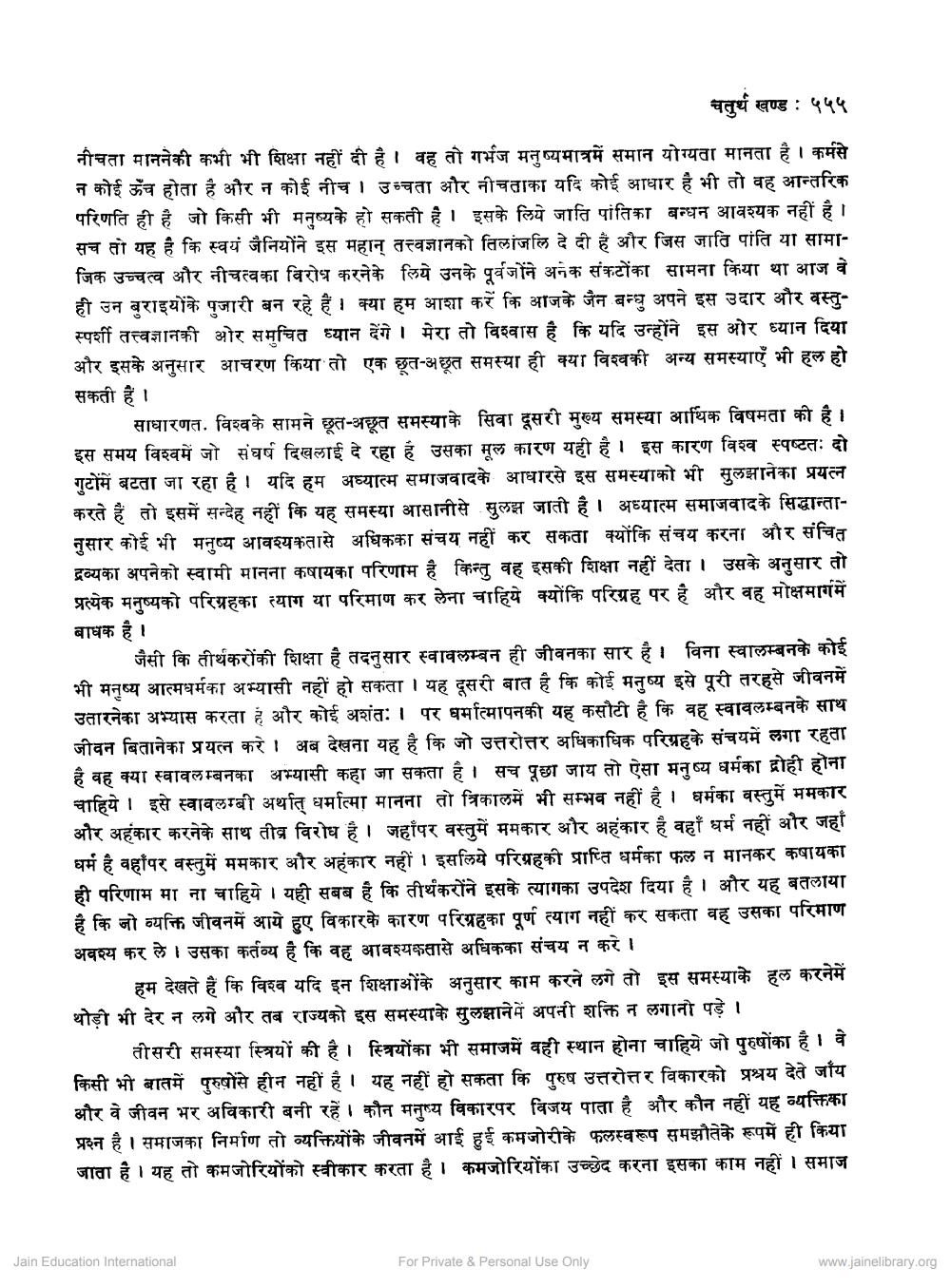________________
चतुर्थ खण्ड : ५५५
नीचता माननेकी कभी भी शिक्षा नहीं दी है। वह तो गर्भज मनुष्यमात्रमें समान योग्यता मानता है। कमसे न कोई ऊँच होता है और न कोई नीच । उच्चता और नीचताका यदि कोई आधार है भी तो वह आन्तरिक परिणति ही है जो किसी भी मनुष्यके हो सकती है। इसके लिये जाति पांतिका बन्धन आवश्यक नहीं है। सच तो यह है कि स्वयं जैनियोंने इस महान् तत्त्वज्ञानको तिलांजलि दे दी है और जिस जाति पांति या सामाजिक उच्चत्व और नीचत्वका विरोध करने के लिये उनके पूर्वजोंने अनेक संकटोंका सामना किया था आज वे ही उन बुराइयोंके पुजारी बन रहे हैं। क्या हम आशा करें कि आजके जैन बन्धु अपने इस उदार और वस्तुस्पर्शी तत्त्वज्ञानकी ओर समचित ध्यान देंगे। मेरा तो विश्वास है कि यदि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और इसके अनुसार आचरण किया तो एक छत-अछूत समस्या ही क्या विश्वकी अन्य समस्याएँ भी हल हो सकती हैं।
साधारणत. विश्वके सामने छत-अछूत समस्याके सिवा दूसरी मुख्य समस्या आर्थिक विषमता की है। इस समय विश्वमें जो संघर्ष दिखलाई दे रहा है उसका मूल कारण यही है। इस कारण विश्व स्पष्टतः दो गुटोंमें बटता जा रहा है। यदि हम अध्यात्म समाजवादके आधारसे इस समस्याको भी सुलझानेका प्रयत्न करते हैं तो इसमें सन्देह नहीं कि यह समस्या आसानीसे सुलझ जाती है। अध्यात्म समाजवादके सिद्धान्तानुसार कोई भी मनुष्य आवश्यकतासे अधिकका संचय नहीं कर सकता क्योंकि संचय करना और संचित द्रव्यका अपनेको स्वामी मानना कषायका परिणाम है किन्तु वह इसकी शिक्षा नहीं देता। उसके अनुसार तो प्रत्येक मनुष्यको परिग्रहका त्याग या परिमाण कर लेना चाहिये क्योंकि परिग्रह पर है और वह मोक्षमार्गमें बाधक है।
जैसी कि तीर्थकरोंकी शिक्षा है तदनुसार स्वावलम्बन ही जीवनका सार है। विना स्वालम्बनके कोई भी मनुष्य आत्मधर्मका अभ्यासी नहीं हो सकता । यह दूसरी बात है कि कोई मनुष्य इसे पूरी तरहसे जीवनमें उतारनेका अभ्यास करता है और कोई अशंतः । पर धर्मात्मापनकी यह कसौटी है कि वह स्वावलम्बनके साथ जीवन बितानेका प्रयत्न करे। अब देखना यह है कि जो उत्तरोत्तर अधिकाधिक परिग्रहके संचयमें लगा रहता है वह क्या स्वावलम्बनका अभ्यासी कहा जा सकता है। सच पूछा जाय तो ऐसा मनुष्य धर्मका द्रोही होना चाहिये। इसे स्वावलम्बी अर्थात धर्मात्मा मानना तो त्रिकालमें भी सम्भव नहीं है। धर्मका वस्तुमें ममकार और अहंकार करनेके साथ तीव्र विरोध है । जहाँपर वस्तुमें ममकार और अहंकार है वहाँ धर्म नहीं और जहाँ धर्म है वहाँपर वस्तुमें ममकार और अहंकार नहीं । इसलिये परिग्रहकी प्राप्ति धर्मका फल न मानकर कषायका ही परिणाम मा ना चाहिये । यही सबब है कि तीर्थंकरोंने इसके त्यागका उपदेश दिया है। और यह बतलाया है कि जो व्यक्ति जीवनमें आये हुए विकारके कारण परिग्रहका पूर्ण त्याग नहीं कर सकता वह उसका परिमाण अवश्य कर ले । उसका कर्तव्य है कि वह आवश्यकतासे अधिकका संचय न करे ।
हम देखते हैं कि विश्व यदि इन शिक्षाओंके अनुसार काम करने लगे तो इस समस्याके हल करने में थोड़ी भी देर न लगे और तब राज्यको इस समस्याके सुलझानेमें अपनी शक्ति न लगानो पड़े ।
तीसरी समस्या स्त्रियों की है। स्त्रियोंका भी समाजमें वही स्थान होना चाहिये जो पुरुषोंका है । वे किसी भी बातमें पुरुषोंसे हीन नहीं है । यह नहीं हो सकता कि पुरुष उत्तरोत्तर विकारको प्रश्रय देते जाँय
और वे जीवन भर अविकारी बनी रहें। कौन मनुष्य विकारपर विजय पाता है और कौन नहीं यह व्यक्तिका प्रश्न है। समाजका निर्माण तो व्यक्तियोंके जीवनमें आई हुई कमजोरीके फलस्वरूप समझौतेके रूपमें ही किया जाता है । यह तो कमजोरियोंको स्वीकार करता है। कमजोरियोंका उच्छेद करना इसका काम नहीं । समाज
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org