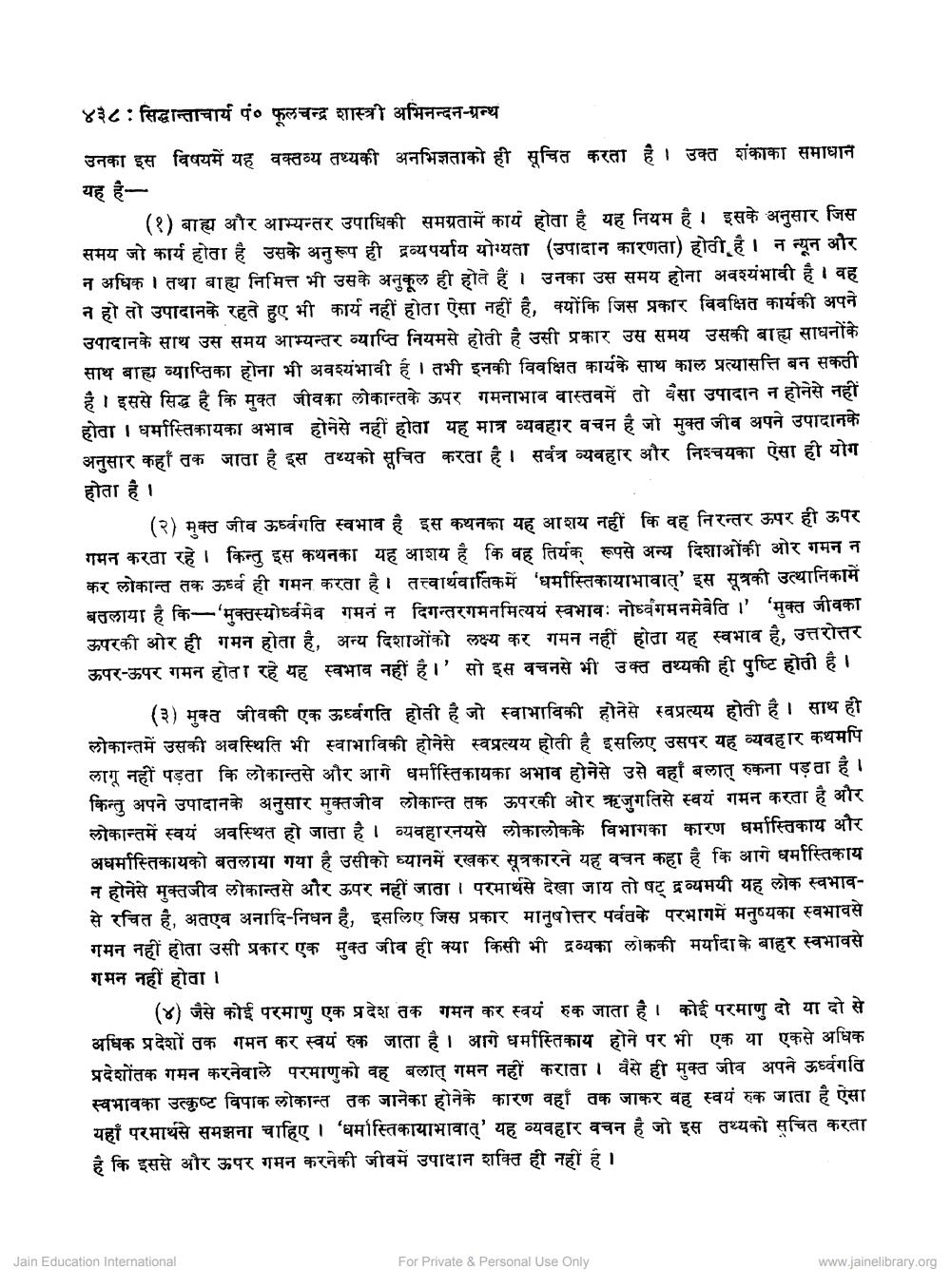________________
४३८ : सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ
उनका इस विषयमें यह वक्तव्य तथ्यकी अनभिज्ञताको ही सूचित करता है। उक्त शंकाका समाधान यह है
(१) बाह्य और आभ्यन्तर उपाधिकी समग्रतामें कार्य होता है यह नियम है। इसके अनुसार जिस समय जो कार्य होता है उसके अनुरूप ही द्रव्यपर्याय योग्यता ( उपादान कारणता होती है। न न्यून और न अधिक तथा बाह्य निमित्त भी उसके अनुकूल ही होते हैं। उनका उस समय होना अवश्यंभावी है। वह न हो तो उपादानके रहते हुए भी कार्य नहीं होता ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार विवक्षित कार्यकी अपने उपादान के साथ उस समय आभ्यन्तर व्याप्ति नियमसे होती है उसी प्रकार उस समय उसकी बाह्य साधनोंके साथ बाह्य व्याप्तिका होना भी अवश्यंभावी है । तभी इनकी विवक्षित कार्यके साथ काल प्रत्यासत्ति बन सकती है । इससे सिद्ध है कि मुक्त जीवका लोकान्तके ऊपर गमनाभाव वास्तवमें तो वैसा उपादान न होनेसे नहीं होता । धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे नहीं होता यह मात्र व्यवहार वचन है जो मुक्त जीव अपने उपादानके अनुसार कहाँ तक जाता है इस तथ्यको सूचित करता है। सर्वत्र व्यवहार और निश्चयका ऐसा ही योग होता है ।
(२) मुक्त जीव ऊर्ध्वगति स्वभाव है इस कथनका यह आशय नहीं कि वह निरन्तर ऊपर ही ऊपर गमन करता रहे। किन्तु इस कथनका यह आशय है कि वह तिर्यक् रूपसे अन्य दिशाओंकी ओर गमन न कर [लोकान्त तक ऊर्ध्व ही गमन करता है। तत्वार्थवार्तिक में 'धर्मास्तिकायाभावात्' इस सूत्र की उत्थानिकामें बतलाया है कि - 'मुक्तस्योर्ध्वमेव गमनं न दिगन्तरगमनमित्ययं स्वभावः नोर्ध्वगमनमेवेति ।' 'मुक्त जीवका ऊपरकी ओर ही गमन होता है, अन्य दिशाओंको लक्ष्य कर गमन नहीं होता यह स्वभाव है, उत्तरोत्तर ऊपर-ऊपर गमन होता रहे यह स्वभाव नहीं है।' सो इस वचनसे भी उक्त तथ्यकी ही पुष्टि होती है।
(३) मुक्त जीवकी एक ऊर्ध्वगति होती है जो स्वाभाविकी होनेसे स्वप्रत्यय होती है। साथ ही लोकान्तमें उसकी अवस्थिति भी स्वाभाविकी होनेसे स्वप्रत्यय होती है इसलिए उसपर यह व्यवहार कथमपि लागू नहीं पड़ता कि लोकान्तसे और आगे धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे उसे वहाँ बलात् रुकना पड़ता है। किन्तु अपने उपादानके अनुसार मुक्तजीव लोकान्त तक ऊपरकी ओर ऋजुगतिसे स्वयं गमन करता है और लोकान्तमें स्वयं अवस्थित हो जाता है। पवहारनयसे लोकालोकके विभागका कारण धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायको बतलाया गया है उसीको ध्यान में रखकर सूत्रकारने यह वचन कहा है कि आगे धर्मास्तिकाय न होनेसे मुक्तजीव लोकान्तसे और ऊपर नहीं जाता। परमार्थसे देखा जाय तो पट् द्रव्यमयी यह लोक स्वभावसे रचित है, अतएव अनादि-निधन है, इसलिए जिस प्रकार मानुषोत्तर पर्वतके परभागमें मनुष्यका स्वभावसे गमन नहीं होता उसी प्रकार एक मुक्त जीव ही क्या किसी भी द्रव्यका लोककी मर्यादा के बाहर स्वभावसे गमन नहीं होता ।
(४) जैसे कोई परमाणु एक प्रदेश तक गमन कर स्वयं रुक जाता है । कोई परमाणु दो या दो से अधिक प्रदेशों तक गमन कर स्वयं रुक जाता है। आगे धर्मास्तिकाय होने पर भी एक या एकसे अधिक प्रदेशोंतक गमन करनेवाले परमाणुको वह बलात् गमन नहीं कराता । वैसे ही मुक्त जीव अपने ऊर्ध्वगति स्वभावका उत्कृष्ट विपाक लोकान्त तक जानेका होनेके कारण वहाँ तक जाकर वह यहाँ परमार्थसे समझना चाहिए। 'धर्मास्तिकायाभावात्' यह व्यवहार वचन है जो इस है कि इससे और ऊपर गमन करनेकी जीवमें उपादान शक्ति ही नहीं है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
स्वयं रुक जाता है ऐसा तथ्य को सूचित करता
www.jainelibrary.org