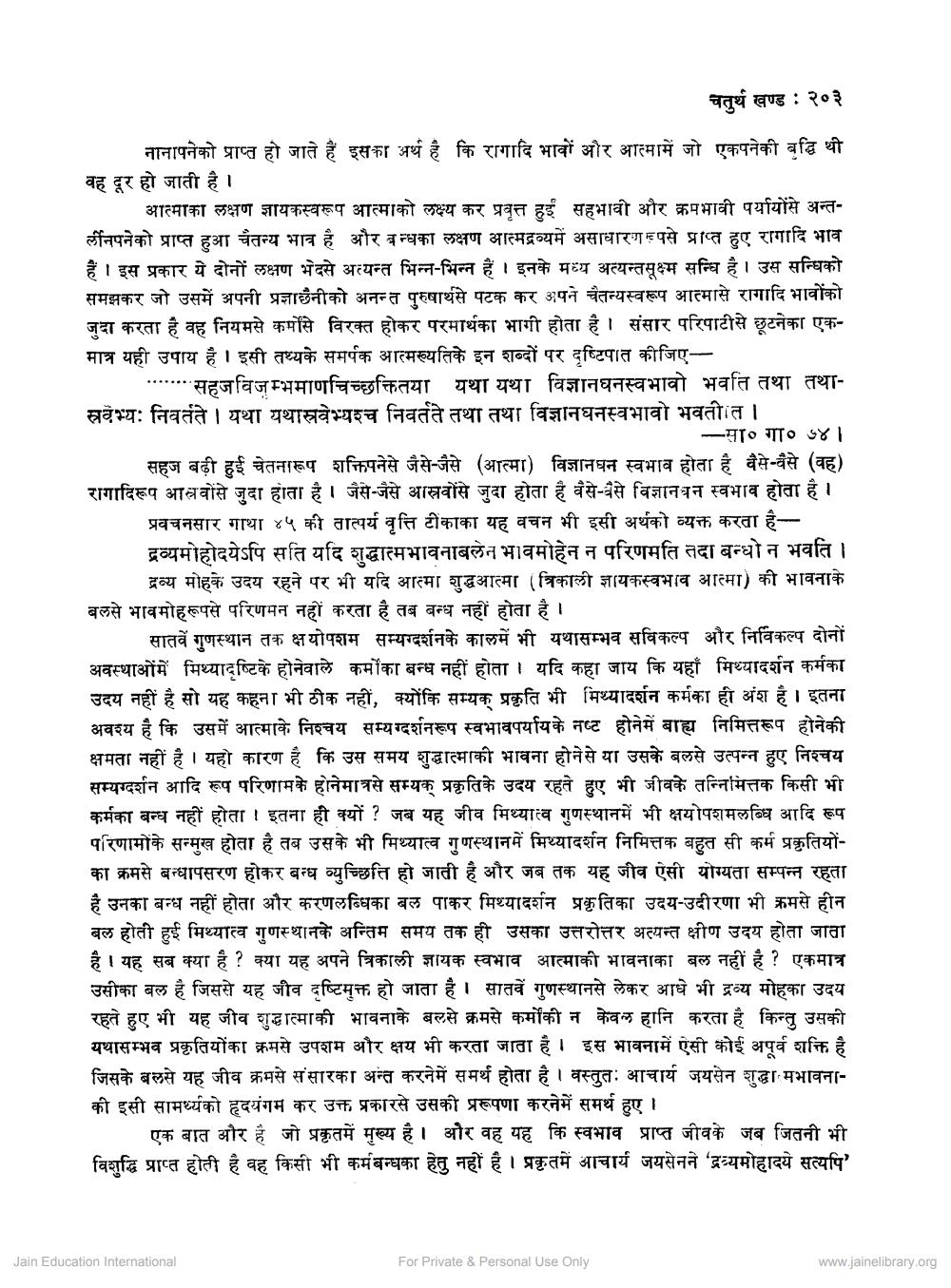________________
चतुर्थ खण्ड : २०३ नानापनेको प्राप्त हो जाते हैं इसका अर्थ है कि रागादि भावों और आत्मामें जो एकपनेकी बुद्धि थी वह दूर हो जाती है।
आत्माका लक्षण ज्ञायकस्वरूप आत्माको लक्ष्य कर प्रवृत्त हुईं सहभावी और क्रमभावी पर्यायोंसे अन्तलीनपनेको प्राप्त हआ चैतन्य भाव है और बन्धका लक्षण आत्मद्रव्यमें असाधारण पसे प्राप्त हुए रागादि भाव हैं । इस प्रकार ये दोनों लक्षण भेदसे अत्यन्त भिन्न-भिन्न हैं । इनके मध्य अत्यन्तसूक्ष्म सन्धि है। उस सन्धिको समझकर जो उसमें अपनी प्रज्ञाछनीको अनन्त पुरुषार्थसे पटक कर अपने चैतन्यस्वरूप आत्मासे रागादि भावोंको जुदा करता है वह नियमसे कर्मोसे विरक्त होकर परमार्थका भागी होता है। संसार परिपाटीसे छुटनेका एकमात्र यही उपाय है । इसी तथ्यके समर्पक आत्मख्यतिके इन शब्दों पर दृष्टिपात कीजिए
...... सहजविज़म्भमाणचिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावो भवति तथा तथास्रवेभ्यः निवर्तते । यथा यथास्रवेभ्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो भवतीति ।
-सा० गा० ७४। सहज बढ़ी हई चेतनारूप शक्तिपनेसे जैसे-जैसे (आत्मा) विज्ञानघन स्वभाव होता है वैसे-वैसे (वह) रागादिरूप आत्रवोंसे जुदा होता है । जैसे-जैसे आस्रवोंसे जुदा होता है वैसे-वैसे विज्ञानवन स्वभाव होता है।
प्रवचनसार गाथा ४५ की तात्पर्य वृत्ति टीकाका यह वचन भी इसी अर्थको व्यक्त करता हैद्रव्यमोहोदयेऽपि सति यदि शुद्धात्मभावनाबलेन भावमोहेन न परिणमति तदा बन्धो न भवति ।
द्रव्य मोहके उदय रहने पर भी यदि आत्मा शुद्धआत्मा (त्रिकाली ज्ञायकस्वभाव आत्मा) की भावनाके बलसे भावमोहरूपसे परिणमन नहीं करता है तब बन्ध नहीं होता है।
सातवें गुणस्थान तक क्षयोपशम सम्यग्दर्शनके कालमें भी यथासम्भव सविकल्प और निर्विकल्प दोनों अवस्थाओंमें मिथ्यादष्टिके होनेवाले कर्मोका बन्ध नहीं होता। यदि कहा जाय कि यहाँ मिथ्यादर्शन कर्मका उदय नहीं है सो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सम्यक् प्रकृति भी मिथ्यादर्शन कर्मका ही अंश है । इतना अवश्य है कि उसमें आत्माके निश्चय सम्यग्दर्शनरूप स्वभावपर्यायके नष्ट होने में बाह्य निमित्तरूप होनेकी क्षमता नहीं है । यही कारण है कि उस समय शुद्धात्माकी भावना होने से या उसके बलसे उत्पन्न हुए निश्चय सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणामके होनेमात्रसे सम्यक् प्रकृतिके उदय रहते हुए भी जीवके तन्निमित्तक किसी भी कर्मका बन्ध नहीं होता। इतना ही क्यों ? जब यह जीव मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी क्षयोपशमलब्धि आदि रूप परिणामोंके सन्मुख होता है तब उसके भी मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यादर्शन निमित्तक बहुत सी कर्म प्रकृतियोंका क्रमसे बन्धापसरण होकर बन्ध व्युच्छित्ति हो जाती है और जब तक यह जीव ऐसी योग्यता सम्पन्न रहता है उनका बन्ध नहीं होता और करणलब्धिका बल पाकर मिथ्यादर्शन प्रकृतिका उदय-उदीरणा भी क्रमसे हीन बल होती हुई मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समय तक ही उसका उत्तरोत्तर अत्यन्त क्षीण उदय होता जाता है । यह सब क्या है ? क्या यह अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव आत्माकी भावनाका बल नहीं है ? एकमात्र उसीका बल है जिससे यह जीव दृष्टिमुक्त हो जाता है । सातवें गुणस्थानसे लेकर आधे भी द्रव्य मोहका उदय रहते हुए भी यह जीव शुद्धात्माकी भावनाके बलसे क्रमसे कर्मोकी न केवल हानि करता है किन्तु उसकी यथासम्भव प्रकृतियोंका क्रमसे उपशम और क्षय भी करता जाता है। इस भावनामें ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है जिसके बलसे यह जीव क्रमसे संसारका अन्त करने में समर्थ होता है । वस्तुतः आचार्य जयसेन शुद्धा मभावनाकी इसी सामर्थ्यको हृदयंगम कर उक्त प्रकारसे उसकी प्ररूपणा करने में समर्थ हुए।
एक बात और है जो प्रकृतमें मुख्य है। और वह यह कि स्वभाव प्राप्त जीवके जब जितनी विशुद्धि प्राप्त होती है वह किसी भी कर्मबन्धका हेतु नहीं है। प्रकृतमें आचार्य जयसेनने 'द्रव्यमोहादये सत्यपि'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org