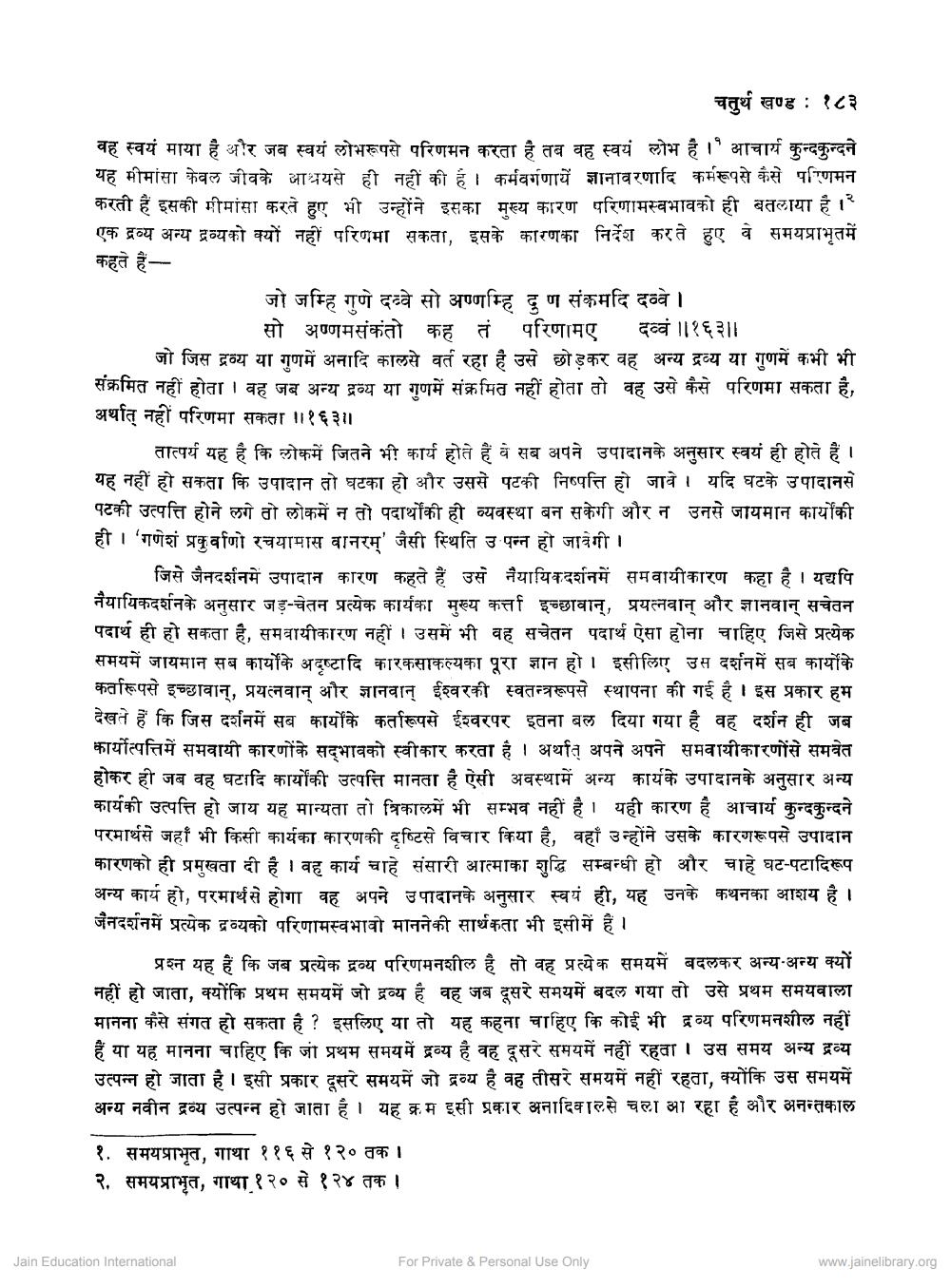________________
चतुर्थ खण्ड: १८३
वह स्वयं माया है और जब स्वयं लोभरूपसे परिणमन करता है तब वह स्वयं लोभ है।' आचार्य कुन्दकुन्दने यह मीमांसा केवल जीवके आथयसे ही नहीं की है। कर्मवगंणायें ज्ञानावरणादि कर्मरूपसे कैसे परिणमन करती हैं इसकी मीमांसा करते हुए भी उन्होंने इसका मुख्य कारण परिणामस्वभावको ही बतलाया है। एक द्रव्य अन्य द्रव्यको क्यों नहीं परिणमा सकता, इसके कारणका निर्देश करते हुए वे समयप्राभूतमें कहते हैं
जो जहि गुणे दवे सो अण्णम्हि दुण संकमदि दध्वे ।
सो अण्णमसंकतो कह तं परिणामए दव्वं ॥ १६३॥
जो जिस द्रव्य या गुणमें अनादि कालसे वर्त रहा है उसे छोड़कर वह अन्य द्रव्य या गुणमें कभी भी संक्रमित नहीं होता। वह जब अन्य द्रव्य या गुणमें संक्रमित नहीं होता तो वह उसे कैसे परिणमा सकता है, अर्थात् नहीं परिणमा सकता ॥ १६३॥
तात्पर्य यह है कि लोकमें जितने भी कार्य होते हैं वे सब अपने उपादानके अनुसार स्वयं ही होते हैं । यह नहीं हो सकता कि उपादान तो घटका हो और उससे पटकी निष्पत्ति हो जावे । यदि घटके उपादान पकी उत्पत्ति होने लगे तो लोकमें न तो पदार्थोंकी ही व्यवस्था बन सकेगी और न उनसे जायमान कार्योंकी ही गणेश प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्' जैसी स्थिति उत्पन्न हो जावेगी ।
जिसे जैनदर्शनमें उपादान कारण कहते हैं उसे नैयायिकदर्शनमें समवायीकारण कहा है । यद्यपि नैयायिकदर्शनके अनुसार जड़-चेतन प्रत्येक कार्यका मुख्य कर्त्ता इच्छावान्, प्रयत्नवान् और ज्ञानवान् सचेतन पदार्थ ही हो सकता है, समवायीकारण नहीं । उसमें भी वह सचेतन पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसे प्रत्येक समयमैं जायमान सब कार्योंके अदृष्टादि कारकसाकल्यका पूरा ज्ञान हो। इसीलिए उस दर्शनमें सब कार्यों के कर्तारूपसे इच्छावान्, प्रयत्नवान् और ज्ञानवान् ईश्वरकी स्वतन्त्ररूपसे स्थापना की गई है । इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस दर्शनमें सब कार्योंके कर्तारूपसे ईश्वरपर इतना बल दिया गया है वह दर्शन ही जब कार्योत्पत्ति में समवायी कारणोंके सद्भावको स्वीकार करता है। अर्थात् अपने अपने समवायीकारणोंसे समयेत होकर ही जब वह घटादि कार्योंकी उत्पत्ति मानता है ऐसी अवस्थामें अन्य कार्यके उपादानके अनुसार अन्य कार्यकी उत्पत्ति हो जाय यह मान्यता तो त्रिकालमें भी सम्भव नहीं है । यही कारण है आचार्य कुन्दकुन्दने परमार्थसे जहाँ भी किसी कार्यका कारणकी दृष्टिसे विचार किया है, वहाँ उन्होंने उसके कारगरूपसे उपादान कारणको ही प्रमुखता दी है। वह कार्य चाहे संसारी आत्माका शुद्धि सम्बन्धी हो और चाहे घटपटादिरूप अन्य कार्य हो, परमार्थ से होगा वह अपने उपादानके अनुसार स्वयं ही, यह उनके कथनका आशय है । जैनदर्शन में प्रत्येक द्रव्यको परिणामस्वभावो मानने की सार्थकता भी इसी में हैं।
प्रश्न यह है कि जब प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है तो वह प्रत्येक समयमें बदलकर अन्य अन्य क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि प्रथम समय में जो द्रव्य है वह जब दूसरे समय में बदल गया तो उसे प्रथम समयवाला मानना कैसे संगत हो सकता है ? इसलिए या तो यह कहना चाहिए कि कोई भी द्रव्य परिणमनशील नहीं हैं या यह मानना चाहिए कि जो प्रथम समय में द्रव्य है वह दूसरे समय में नहीं रहता । उस समय अन्य द्रव्य उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे समयमें जो द्रव्य है वह तीसरे समय में नहीं रहता, क्योंकि उस समय में अन्य नवीन द्रव्य उत्पन्न हो जाता है। यह क्रम इसी प्रकार अनादिकाल से चला आ रहा है और अनन्तकाल
१. समयप्राभूत, गाथा ११६ से १२० तक । २. समयप्राभृत, गाथा १२० से १२४ तक ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org