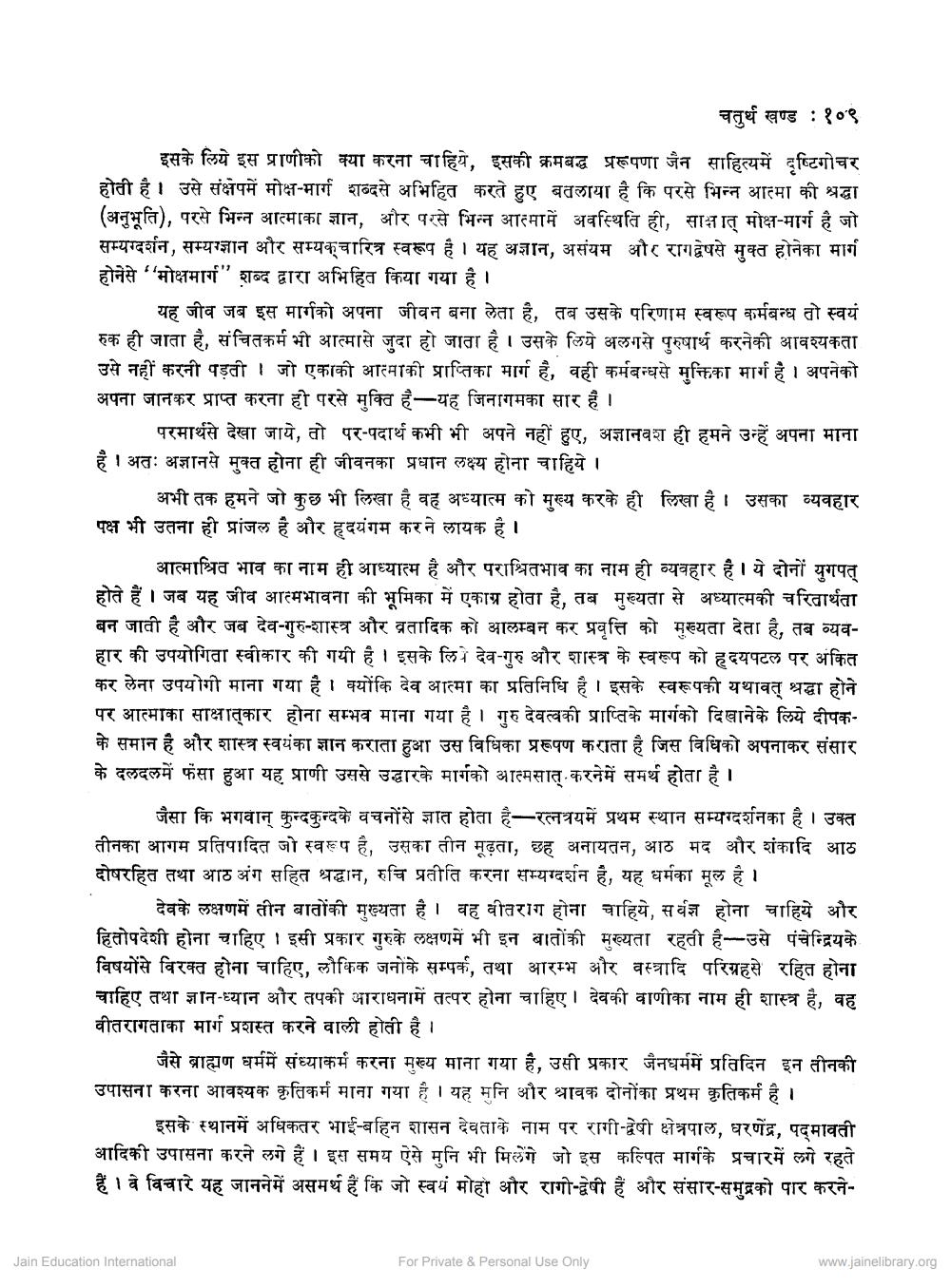________________
चतुर्थ खण्ड : १०९
इसके लिये इस प्राणीको क्या करना चाहिये, इसकी क्रमबद्ध प्ररूपणा जैन साहित्यमें दृष्टिगोचर होती है। उसे संक्षेपमें मोक्ष-मार्ग शब्दसे अभिहित करते हुए बतलाया है कि परसे भिन्न आत्मा की श्रद्धा (अनुभति), परसे भिन्न आत्माका ज्ञान, और परसे भिन्न आत्मामें अवस्थिति ही, साक्षात् मोक्ष-मार्ग है जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र स्वरूप है। यह अज्ञान, असंयम और रागद्वेषसे मुक्त होनेका मार्ग होनेसे "मोक्षमार्ग" शब्द द्वारा अभिहित किया गया है।
यह जीव जब इस मार्गको अपना जीवन बना लेता है. तब उसके परिणाम स्वरूप कर्मबन्ध तो स्वयं रुक ही जाता है, संचितकर्म भी आत्मासे जुदा हो जाता है । उसके लिये अलगसे पुरुषार्थ करनेकी आवश्यकता उसे नहीं करनी पड़ती। जो एकाकी आत्माकी प्राप्तिका मार्ग है, वही कर्मबन्धसे मक्तिका मार्ग है। अपनेको अपना जानकर प्राप्त करना हो परसे मुक्ति है-यह जिनागमका सार हैं ।
परमार्थसे देखा जाये, तो पर-पदार्थ कभी भी अपने नहीं हुए, अज्ञानवश ही हमने उन्हें अपना माना है । अतः अज्ञानसे मुक्त होना ही जीवनका प्रधान लक्ष्य होना चाहिये ।
अभी तक हमने जो कुछ भी लिखा है वह अध्यात्म को मुख्य करके ही लिखा है। उसका व्यवहार पक्ष भी उतना ही प्रांजल है और हृदयंगम करने लायक है ।
__आत्माश्रित भाव का नाम ही आध्यात्म है और पराश्रितभाव का नाम ही व्यवहार है । ये दोनों युगपत् होते हैं । जब यह जीव आत्मभावना की भूमिका में एकाग्र होता है, तब मुख्यता से अध्यात्मकी चरितार्थता बन जाती है और जब देव-गुरु-शास्त्र और व्रतादिक को आलम्बन कर प्रवृत्ति को मुख्यता देता है, तब व्यवहार की उपयोगिता स्वीकार की गयी है। इसके लिये देव-गुरु और शास्त्र के स्वरूप को हृदयपटल पर अकित कर लेना उपयोगी माना गया है । क्योंकि देव आत्मा का प्रतिनिधि है । इसके स्वरूपकी यथावत् श्रद्धा होने पर आत्माका साक्षात्कार होना सम्भव माना गया है। गुरु देवत्वकी प्राप्तिके मार्गको दिखाने के लिये दीपकके समान है और शास्त्र स्वयंका ज्ञान कराता हुआ उस विधिका प्ररूपण कराता है जिस विधिको अपनाकर संसार के दलदलमें फंसा हुआ यह प्राणी उससे उद्धारके मार्गको आत्मसात करने में समर्थ होता है ।
जैसा कि भगवान् कुन्दकुन्दके वचनों से ज्ञात होता है-रत्नत्रयमें प्रथम स्थान सम्यग्दर्शनका है । उक्त तीनका आगम प्रतिपादित जो स्वरूप है, उसका तीन मूढ़ता, छह अनायतन, आठ मद और शंकादि आठ दोषरहित तथा आठ अंग सहित श्रद्धान, रुचि प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है, यह धर्मका मूल है ।
देवके लक्षणमें तीन बातोंकी मुख्यता है । वह वीतराग होना चाहिये, सर्वज्ञ होना चाहिये और हितोपदेशी होना चाहिए । इसी प्रकार गुरुके लक्षणमें भी इन बातोंकी मुख्यता रहती है-उसे पंचेन्द्रियके विषयोंसे विरक्त होना चाहिए, लौकिक जनोंके सम्पर्क, तथा आरम्भ और वस्त्रादि परिग्रहसे रहित होना चाहिए तथा ज्ञान-ध्यान और तपकी आराधनामें तत्पर होना चाहिए। देवकी वाणीका नाम ही शास्त्र है, वह वीतरागताका मार्ग प्रशस्त करने वाली होती है।
जैसे ब्राह्मण धर्ममें संध्याकर्म करना मुख्य माना गया है, उसी प्रकार जैनधर्ममें प्रतिदिन इन तीनकी उपासना करना आवश्यक कृतिकर्म माना गया है । यह मनि और श्रावक दोनोंका प्रथम कृतिकर्म है।
इसके स्थानमें अधिकतर भाई-बहिन शासन देवताके नाम पर रागी-द्वेषी क्षेत्रपाल, धरणेंद्र, पद्मावती आदिकी उपासना करने लगे हैं । इस समय ऐसे मुनि भी मिलेंगे जो इस कल्पित मार्गके प्रचार में लगे रहते हैं । वे विचारे यह जानने में असमर्थ है कि जो स्वयं मोहा और रागो-द्वेषी हैं और संसार-समुद्रको पार करने
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org