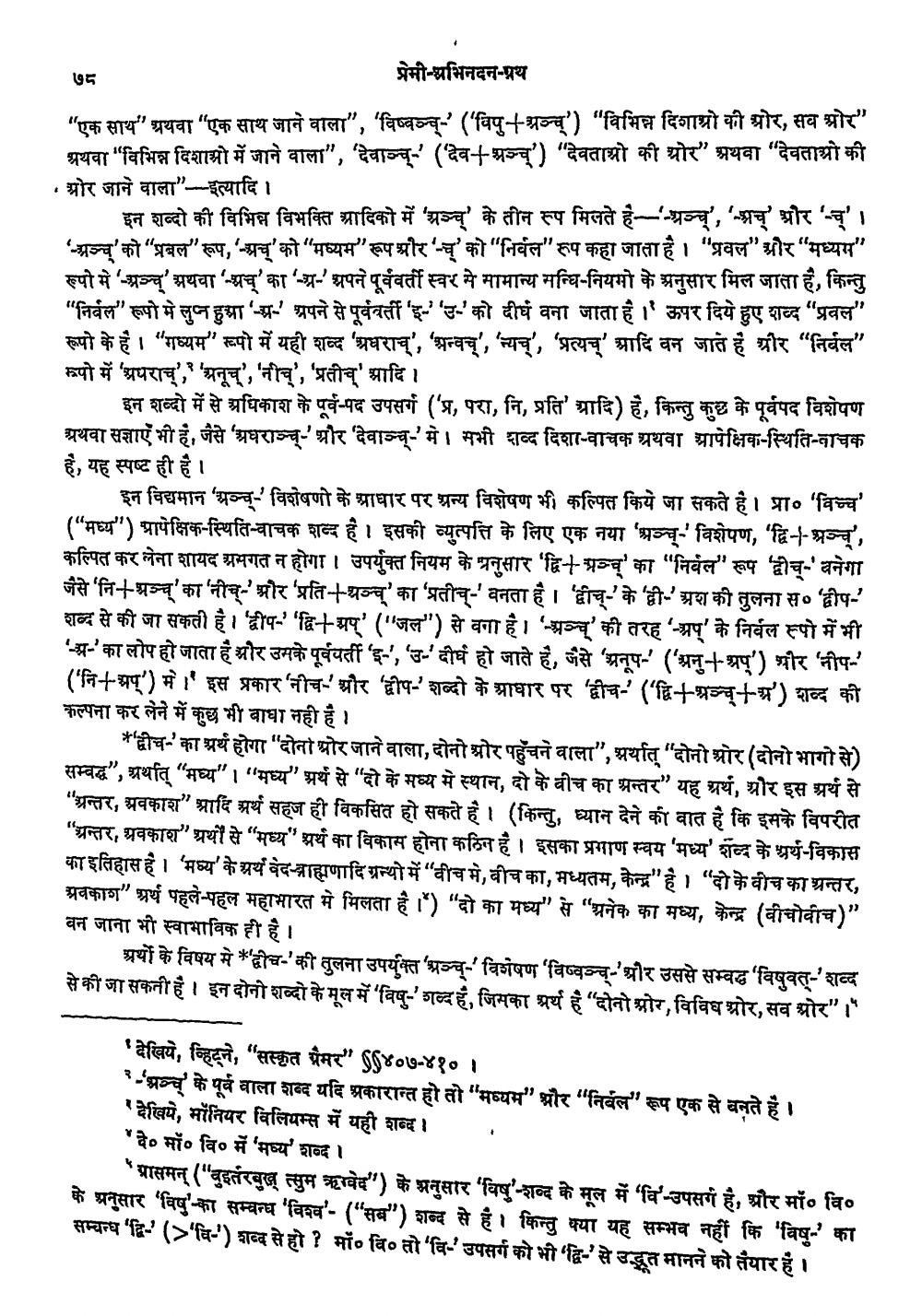________________
प्रेमी-अभिनंदन - प्रथ
"एक साथ” अथवा “एक साथ जाने वाला", "विष्वञ्च्-' ('विपु+ श्रञ्च्') "विभिन्न दिशाश्रो की ओर, सब ओर" अथवा "विभिन्न दिशाओ में जाने वाला', 'देवाञ्च्-' ('देव + अञ्च्') "देवताओ की थोर" अथवा "देवताओ की ओर जाने वाला" इत्यादि ।
#
७८
इन शब्दो की विभिन्न विभक्ति आदिको में 'अञ्च' के तीन रूप मिलते है--' ग्रञ्च', 'अच्' और ' च्' । ‘-अञ्च' को “प्रबल” रूप, 'अच्' को "मध्यम" रूप श्रीर' च्' को " निर्बल" रूप कहा जाता है । "प्रवल" और "मध्यम" रूपो मे ‘-अञ्च् अथवा ‘-अच्' का '--' अपने पूर्ववर्ती स्वर मे मामान्य मन्धि-नियमो के अनुसार मिल जाता है, किन्तु " निर्बल" रूपो मे लुप्न हुआ 'अ- अपने से पूर्ववर्ती 'इ' 'उ' को दीर्घ वना जाता है । ऊपर दिये हुए शब्द "प्रवल" रूपो के हैं । "मध्यम" रूपो में यही शब्द 'घराच्', 'अन्वच्', 'न्यच्', 'प्रत्यच्' आदि वन जाते है श्रीर " निर्बल" रूपो में 'अधराच्', ' 'अनूच्', 'नीच्', 'प्रतीच्' आदि ।
इन शब्दो में से अधिकाश के पूर्व-पद उपसर्ग ('प्र, परा, नि, प्रति ग्रादि) है, किन्तु कुछ के पूर्वपद विशेषण अथवा सज्ञाएँ भी हैं, जैसे 'अघराञ्च्-' श्रौर 'देवाञ्च मे । सभी शब्द दिशा-वाचक प्रथवा आपेक्षिक-स्थिति-वाचक है, यह स्पष्ट ही है ।
इन विद्यमान 'अञ्च् -' विशेषणो के आधार पर अन्य विशेषण भी कल्पित किये जा सकते है । प्रा० 'विच्च' ( " मध्य") प्रापेक्षिक स्थिति - वाचक शब्द है । इसकी व्युत्पत्ति के लिए एक नया 'श्रञ्च विशेषण, 'द्वि--- श्रञ्च', कल्पित कर लेना शायद अभगत न होगा । उपर्युक्त नियम के अनुसार 'द्वि + प्रञ्च' का " निर्बल" रूप 'द्वोच्-' बनेगा जैसे 'नि+अञ्च्' का 'नीच्-' और 'प्रति + थञ्च' का 'प्रतीच्-' बनता है । 'द्वीच्-' के 'द्वी ' अश की तुलना स० 'द्वीप -' शब्द से की जा सकती है। 'द्वीप-' 'द्वि - अप्' ('जल') से बना है। 'अञ्च' की तरह 'अप्' के निर्बल स्पो में भी '--' का लोप हो जाता है और उसके पूर्ववर्ती 'इ', 'उ' दीर्घ हो जाते है, जैसे 'अनूप' ('अनु + श्रप्') श्रर 'नीप-' ('नि+अप्') मे।' इस प्रकार 'नीच' और 'द्वीप -' शब्दो के आधार पर 'द्वीच ' ('द्वि + श्रञ्च् + अ ' ) शब्द की कल्पना कर लेने में कुछ भी बाधा नही है ।
* 'द्वीच ' का अर्थ होगा "दोनो ओर जाने वाला, दोनो ओर पहुँचने वाला", अर्थात् "दोनो श्रोर (दोनो भागो से ) सम्बद्ध”, अर्थात् “मध्य”। “मध्य" अर्थ से "दो के मध्य मे स्थान, दो के बीच का अन्तर" यह अर्थ, और इस अर्थ से "अन्तर, अवकाश” आदि अर्थ सहज ही विकसित हो सकते हैं । ( किन्तु, ध्यान देने की बात है कि इसके विपरीत "अन्तर, श्रवकाश” ग्रथों से "मध्य" श्रर्थ का विकास होना कठिन है । इसका प्रमाण स्वय 'मध्य' शब्द के अर्थ-विकास का इतिहास है । 'मध्य' के अर्थ वेद ब्राह्मणादि ग्रन्थो में "वीच मे, बीच का, मध्यतम, केन्द्र" है । "दो के बीच का ग्रन्तर, अवकाश” अर्थ पहले-पहल महाभारत मे मिलता है । ") "दो का मध्य" से "अनेक का मध्य, केन्द्र ( बीचोबीच )" वन जाना भी स्वाभाविक ही है ।
।
थों के विषय मे * द्वीच ' की तुलना उपर्युक्त 'श्रञ्चु ' विशेषण 'विष्वञ्च्-' और उससे सम्वद्ध 'विषुवत् ' शव्द से की जा सकती है । इन दोनो शब्दो के मूल में 'विषु-' गव्द है, जिसका अर्थ है "दोनो ओर, विविध श्रोर, सव ओर"।"
'देखिये, व्हिट्ने, "संस्कृत प्रेमर " [[४०७ - ४१० ।
'अ' के पूर्व वाला शब्द यदि अकारान्त हो तो "मध्यम" और " निर्बल" रूप एक से बनते हैं ।
देखिये, मॉनियर विलियम्स में यही शब्द |
'दे० मॉ० वि० में 'मध्य' शब्द |
५
'ग्रासमन् ("वुइतंरबुख् त्सुम ऋग्वेद" ) के अनुसार 'विषु' शब्द के मूल में 'वि' उपसर्ग है, और मॉ० वि०
के अनुसार 'विषु' का सम्बन्ध 'विश्व' - ( " सब " ) शब्द से हैं । किन्तु क्या यह सम्भव नहीं कि 'विषु-' का
सम्वन्ध ‘द्वि-' (>'चि-') शब्द से हो ? मॉ० वि० तो 'वि' उपसर्ग को भी 'द्वि-' से उद्भूत मानने को तैयार है ।