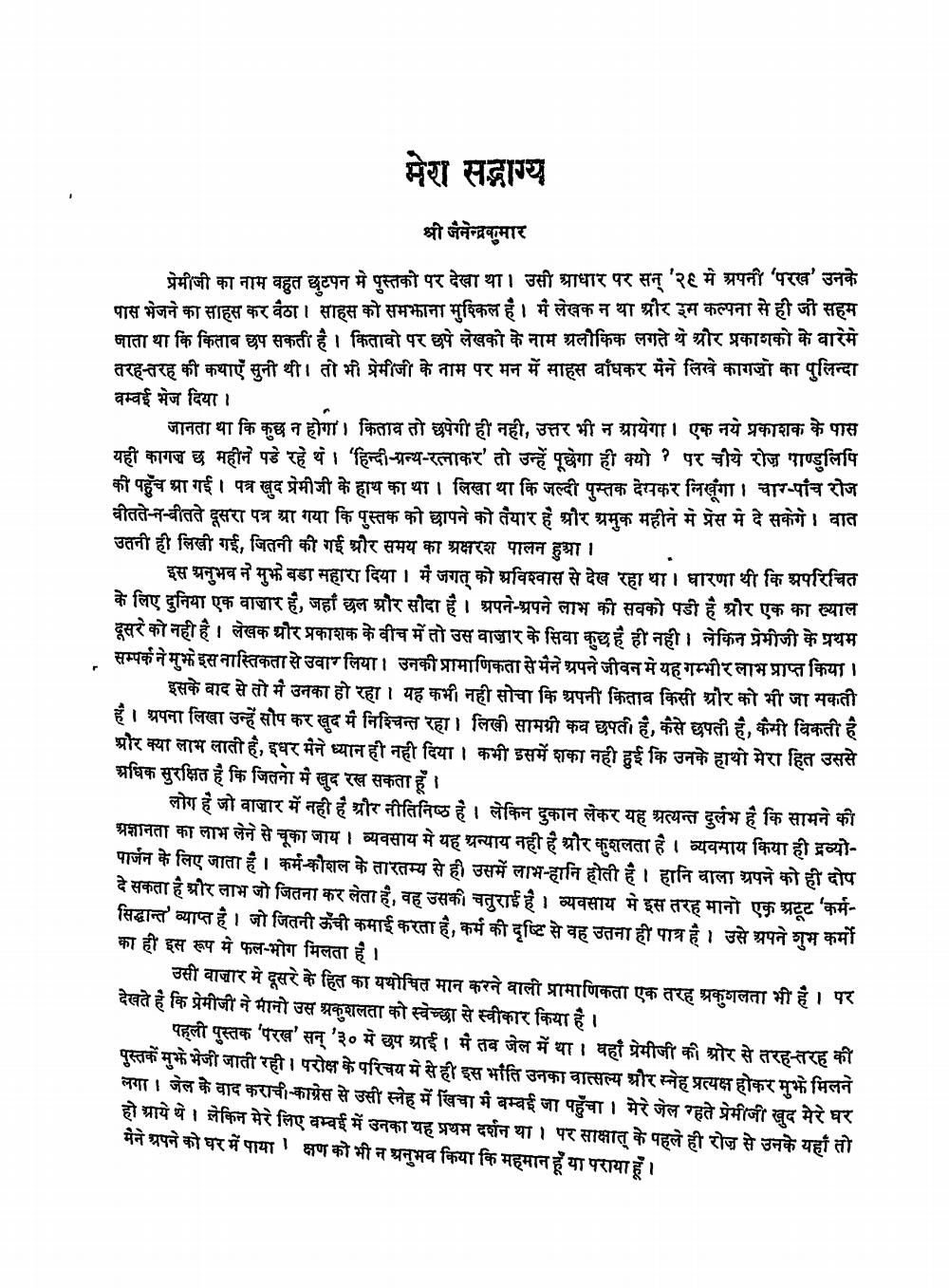________________
मेरा सद्भाग्य
श्री जैनेन्द्रकुमार
प्रेम का नाम बहुत छुटपन मे पुस्तको पर देखा था । उसी आधार पर सन् '२६ मे अपनी 'परख' उनके पास भेजने का साहस कर बैठा । साहस को समझाना मुश्किल है। में लेखक न था और इस कल्पना से ही जी सहम जाता था कि किताब छप सकती है। किताबो पर छपे लेखको के नाम अलौकिक लगते थे और प्रकाशको के बारेमे तरह-तरह की कथाएँ सुनी थी। तो भी प्रेमीजी के नाम पर मन में साहस बांधकर मैंने लिखे कागजों का पुलिन्दा बम्बई भेज दिया ।
जानता था कि कुछ न होगा।
किताव तो छपेगी ही नही, उत्तर भी न आयेगा। एक नये प्रकाशक
।
यही कागज छ महीने पडे रहे थे 'हिन्दी - अन्य - रत्नाकर' तो उन्हें पूछेगा ही क्यो ? पर चौथे रोज पाण्डुलिपि की पहुँच श्रा गई । पत्र खुद प्रेमीजी के हाथ का था । लिखा था कि जल्दी पुस्तक देखकर लिखूंगा। चार-पाँच रोज and - न-बीतते दूसरा पत्र या गया कि पुस्तक को छापने को तैयार है श्रोर श्रमुक महीने में प्रेस में दे सकेगे। वात उतनी ही लिखी गई, जितनी की गई और समय का अक्षरश पालन हुआ ।
-
इस अनुभव ने मुझे बडा महारा दिया। मैं जगत् को अविश्वास से देख रहा था। धारणा थी कि अपरिचित के लिए दुनिया एक बाज़ार है, जहाँ छल और सौदा है । अपने-अपने लाभ की सबको पडी है और एक का ख्याल दूसरे को नही है । लेखक और प्रकाशक के बीच में तो उस बाजार के सिवा कुछ है ही नही। लेकिन प्रेमीजी के प्रथम सम्पर्क ने मुझे इस नास्तिकता से उवार लिया। उनकी प्रामाणिकता से मैने अपने जीवन में यह गम्भीर लाभ प्राप्त किया । इसके बाद से तो मैं उनका हो रहा । यह कभी नही सोचा कि अपनी किताब किसी और को भी जा सकती है । अपना लिखा उन्हें सौप कर खुद में निश्चिन्त रहा। लिखी सामग्री कब छपती है, कैसे छपती है, कैमी विकती है और क्या लाभ लाती है, इधर मैने ध्यान ही नही दिया। कभी इसमें शका नही हुई कि उनके हाथो मेरा हित उससे अधिक सुरक्षित है कि जितना में खुद रख सकता हूँ ।
लोग है जो बाजार में नही है और नीतिनिष्ठ है । लेकिन दुकान लेकर यह अत्यन्त दुर्लभ है कि सामने की अज्ञानता का लाभ लेने से चूका जाय । व्यवसाय मे यह अन्याय नही है और कुशलता है । व्यवसाय किया ही द्रव्योपार्जन के लिए जाता है । कर्म कौशल के तारतम्य से ही उसमें लाभ-हानि होती है। हानि वाला ग्रपने को ही दोप दे सकता है और लाभ जो जितना कर लेता है, वह उसकी चतुराई है । व्यवसाय में इस तरह मानो एक अटूट 'कर्मसिद्धान्त' व्याप्त है । जो जितनी ऊँची कमाई करता है, कर्म की दृष्टि से वह उतना ही पात्र है । उसे अपने का ही इस रूप मे फल भोग मिलता है ।
शुभ कर्मो
उसी बाजार मे दूसरे के हित का यथोचित मान करने वाली प्रामाणिकता एक तरह श्रकुशलता भी है। पर देखते है कि प्रेमीजी ने मानो उस श्रकुशलता को स्वेच्छा से स्वीकार किया है ।
पहली पुस्तक 'परख' सन् '३० मे छप श्रई । मैं तब जेल में था । वहाँ प्रेमीजी की ओर से तरह-तरह की पुस्तकें मुझे भेजी जाती रही । परोक्ष के परिचय मे से ही इस भाँति उनका वात्सल्य और स्नेह प्रत्यक्ष होकर मुझे मिलने लगा । जेल के बाद कराची - काग्रेस से उसी स्नेह में खिचा में बम्बई जा पहुँचा । मेरे जेल रहते प्रेमीजी खुद मेरे घर हो आये थे । लेकिन मेरे लिए बम्बई में उनका यह प्रथम दर्शन था । पर साक्षात् के पहले ही रोज़ से उनके यहाँ तो मैने अपने को घर में पाया । क्षण को भी न अनुभव किया कि महमान हूँ या पराया हूँ ।