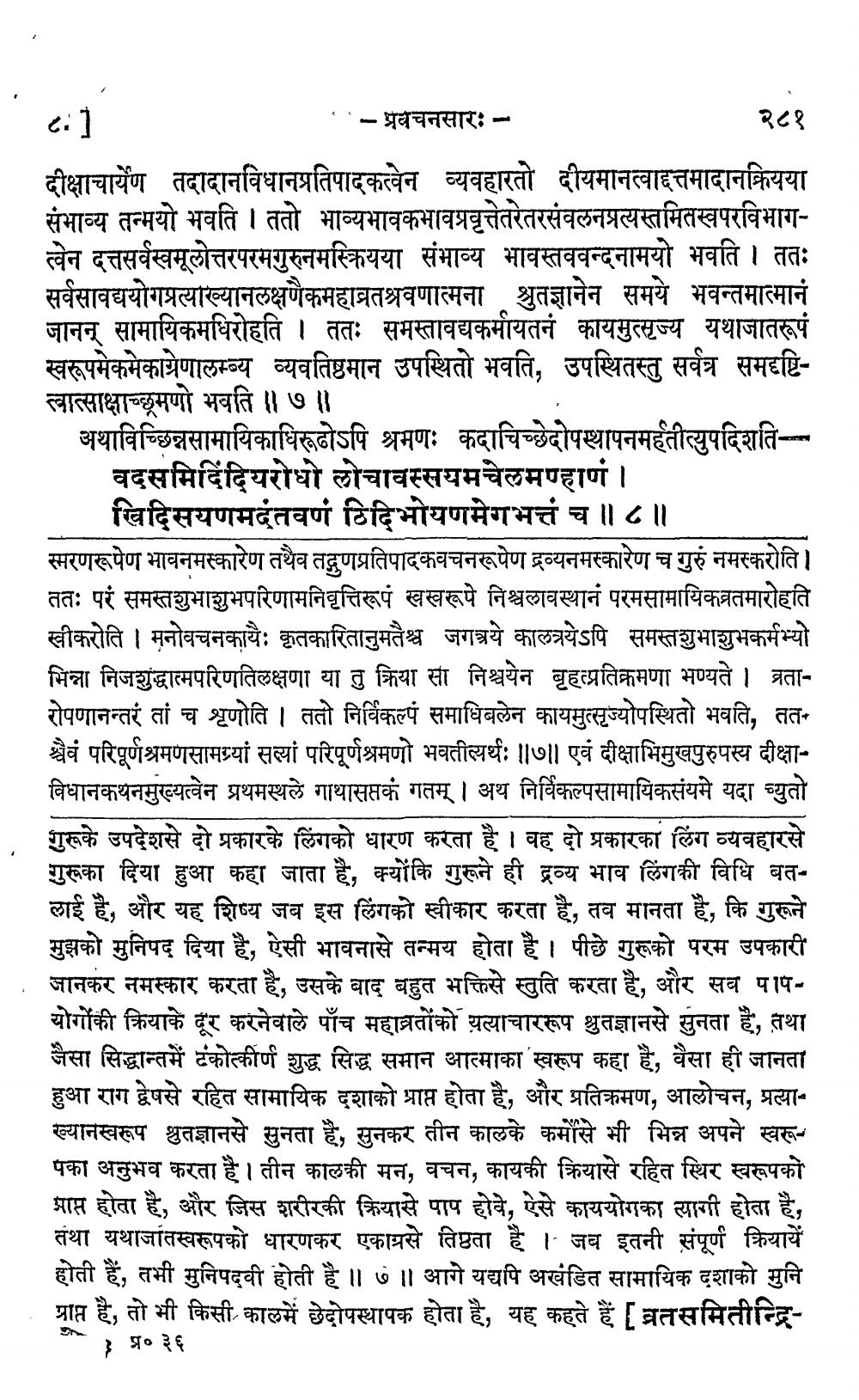________________
८.
--प्रवचनसारः
२८१ दीक्षाचार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वाद्दत्तमादानक्रियया संभाव्य तन्मयो भवति । ततो भाव्यभावकभावप्रवृत्तेतरेतरसंवलनप्रत्यस्तमितवपरविभागत्वेन दत्तसर्वस्वमूलोत्तरपरमगुरुनमस्क्रियया संभाव्य भावस्तववन्दनामयो भवति । ततः सर्वसावधयोगप्रत्याख्यानलक्षणैकमहाव्रतश्रवणात्मना श्रुतज्ञानेन समये भवन्तमात्मानं जानन् सामायिकमधिरोहति । ततः समस्तावद्यकर्मायतनं कायमुत्सृज्य यथाजातरूपं खरूपमेकमेकाग्रेणालम्ब्य व्यवतिष्ठमान उपस्थितो भवति, उपस्थितस्तु सर्वत्र समदृष्टित्वात्साक्षाच्छ्रमणो भवति ॥ ७॥ अथाविच्छिन्नसामायिकाधिरूढोऽपि श्रमणः कदाचिच्छेदोपस्थापनमर्हतीत्युपदिशति--
वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाणं ।।
खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमेगभत्तं च ॥ ८॥ स्मरणरूपेण भावनमस्कारेण तथैव तद्गुणप्रतिपादकवचनरूपेण द्रव्यनमस्कारेण च गुरुं नमस्करोति। ततः परं समस्तशुभाशुभपरिणामनिवृत्तिरूपं स्वस्वरूपे निश्चलावस्थानं परमसामायिकव्रतमारोहति खीकरोति । मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च जगत्रये कालत्रयेऽपि समस्तशुभाशुभकर्मभ्यो भिन्ना निजशुद्धात्मपरिणतिलक्षणा या तु क्रिया सा निश्चयेन बृहत्प्रतिक्रमणा भण्यते । व्रतारोपणानन्तरं तां च शृणोति । ततो निर्विकल्पं समाधिबलेन कायमुत्सृज्योपस्थितो भवति, ततश्चैवं परिपूर्णश्रमणसामग्र्यां सत्यां परिपूर्णश्रमणो भवतीत्यर्थः ॥७॥ एवं दीक्षाभिमुखपुरुपस्य दीक्षाविधानकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथासप्तकं गतम् । अथ निर्विकल्पसामायिकसंयमे यदा च्युतो गुरूके उपदेशसे दो प्रकारके लिंगको धारण करता है । वह दो प्रकारका लिंग व्यवहारसे गुरूका दिया हुआ कहा जाता है, क्योंकि गुरूने ही द्रव्य भाव लिंगकी विधि बतलाई है, और यह शिष्य जब इस लिंगको स्वीकार करता है, तब मानता है, कि गुरूने मुझको मुनिपद दिया है, ऐसी भावनासे तन्मय होता है। पीछे गुरूको परम उपकारी जानकर नमस्कार करता है, उसके बाद बहुत भक्तिसे स्तुति करता है, और सब पापयोगोंकी क्रियाके दूर करनेवाले पाँच महाव्रतोंको अत्याचाररूप श्रुतज्ञानसे सुनता है, तथा जैसा सिद्धान्तमें टंकोत्कीर्ण शुद्ध सिद्ध समान आत्माका स्वरूप कहा है, वैसा ही जानता हुआ राग द्वेषसे रहित सामायिक दशाको प्राप्त होता है, और प्रतिक्रमण, आलोचन, प्रत्याख्यानस्वरूप श्रुतज्ञानसे सुनता है, सुनकर तीन कालके कर्मोंसे भी भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव करता है। तीन कालकी मन, वचन, कायकी क्रियासे रहित स्थिर स्वरूपको प्राप्त होता है, और जिस शरीरकी क्रियासे पाप होवे, ऐसे काययोगका त्यागी होता है, तथा यथाजांतस्वरूपको धारणकर एकाग्रसे तिष्ठता है । जब इतनी संपूर्ण क्रियायें होती हैं, तभी मुनिपदवी होती है ॥ ७ ॥ आगे यद्यपि अखंडित सामायिक दशाको मुनि प्राप्त है, तो भी किसी कालमें छेदोपस्थापक होता है, यह कहते हैं [व्रतसमितीन्द्रि