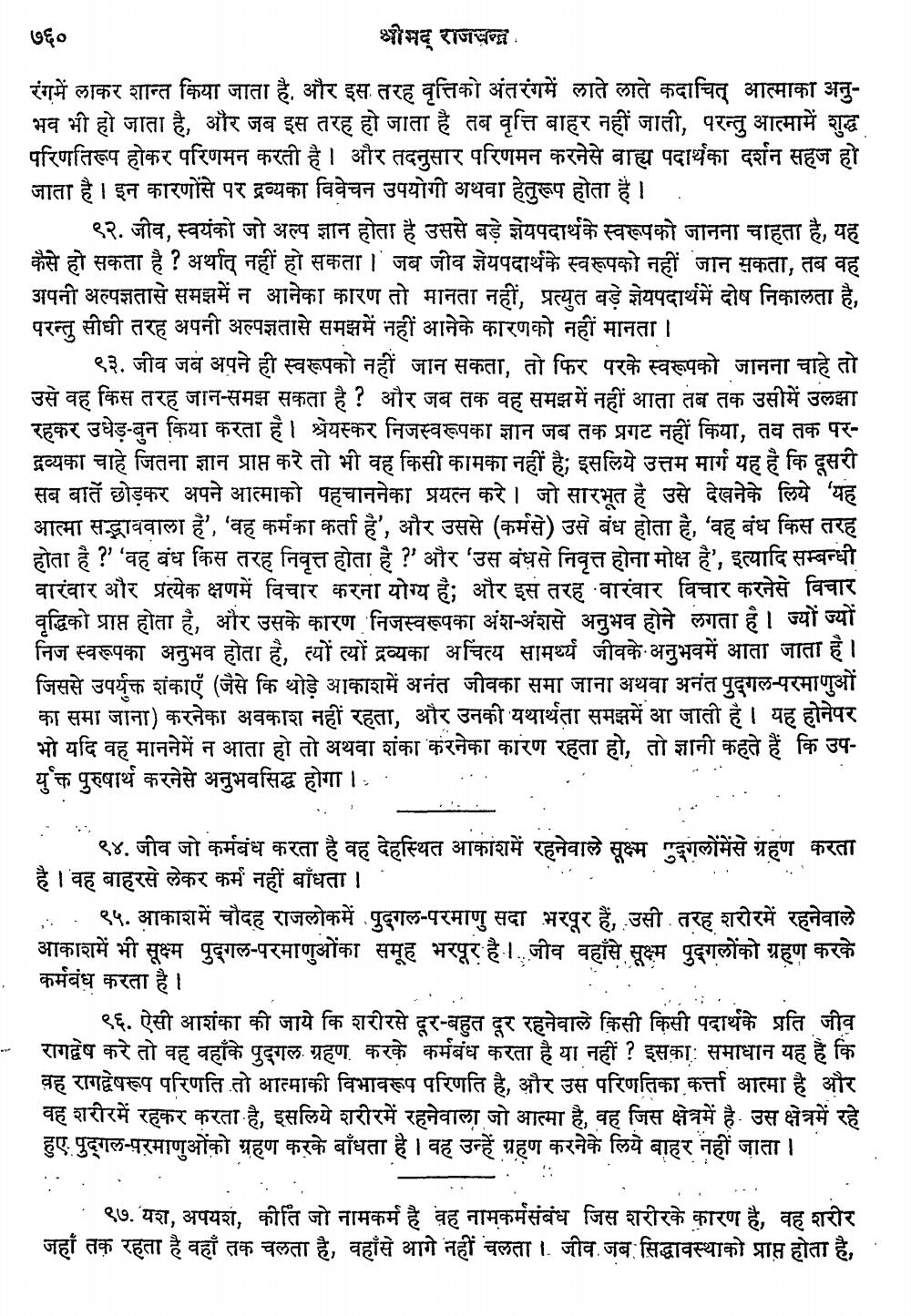________________
७६०
श्रीमद् राजघन्त.
रंगमें लाकर शान्त किया जाता है, और इस तरह वृत्तिको अंतरंगमें लाते लाते कदाचित् आत्माका अनुभव भी हो जाता है, और जब इस तरह हो जाता है तब वृत्ति बाहर नहीं जाती, परन्तु आत्मामें शुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करती है। और तदनुसार परिणमन करनेसे बाह्य पदार्थका दर्शन सहज हो जाता है । इन कारणोंसे पर द्रव्यका विवेचन उपयोगी अथवा हेतुरूप होता है।
९२. जीव, स्वयंको जो अल्प ज्ञान होता है उससे बड़े ज्ञेयपदार्थके स्वरूपको जानना चाहता है, यह कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता। जब जीव ज्ञेयपदार्थके स्वरूपको नहीं जान सकता, तब वह अपनी अल्पज्ञतासे समझमें न आनेका कारण तो मानता नहीं, प्रत्युत बड़े ज्ञेयपदार्थमें दोष निकालता है, परन्तु सीधी तरह अपनी अल्पज्ञतासे समझमें नहीं आनेके कारणको नहीं मानता।
९३. जीव जब अपने ही स्वरूपको नहीं जान सकता, तो फिर परके स्वरूपको जानना चाहे तो उसे वह किस तरह जान-समझ सकता है ? और जब तक वह समझ में नहीं आता तब तक उसीमें उलझा रहकर उधेड़-बुन किया करता है। श्रेयस्कर निजस्वरूपका ज्ञान जब तक प्रगट नहीं किया, तब तक परद्रव्यका चाहे जितना ज्ञान प्राप्त करे तो भी वह किसी कामका नहीं है; इसलिये उत्तम मार्ग यह है कि दूसरी सब बातें छोड़कर अपने आत्माको पहचाननेका प्रयत्न करे। जो सारभूत है उसे देखनेके लिये 'यह आत्मा सद्भाववाला है', 'वह कर्मका कर्ता है', और उससे (कर्मसे) उसे बंध होता है, 'वह बंध किस तरह होता है ?' 'वह बंध किस तरह निवृत्त होता है ?' और 'उस बंधसे निवृत्त होना मोक्ष है', इत्यादि सम्बन्धी वारंवार और प्रत्येक क्षणमें विचार करना योग्य है; और इस तरह वारंवार विचार करनेसे विचार वृद्धिको प्राप्त होता है, और उसके कारण निजस्वरूपका अंश-अंशसे अनुभव होने लगता है। ज्यों ज्यों निज स्वरूपका अनुभव होता है, त्यों त्यों द्रव्यका अचिंत्य सामर्थ्य जीवके अनुभवमें आता जाता है। जिससे उपर्युक्त शंकाएँ (जैसे कि थोड़े आकाशमें अनंत जीवका समा जाना अथवा अनंत पुद्गल-परमाणुओं का समा जाना) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी यथार्थता समझमें आ जाती है। यह होनेपर भो यदि वह मानने में न आता हो तो अथवा शंका करनेका कारण रहता हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि उपयुक्त पुरुषार्थ करनेसे अनुभवसिद्ध होगा।
९४. जीव जो कर्मबंध करता है वह देहस्थित आकाशमें रहनेवाले सूक्ष्म पुद्गलोंमेंसे ग्रहण करता है । वह बाहरसे लेकर कर्म नहीं बाँधता। . . ९५. आकाशमें चौदह राजलोकमें पुद्गल-परमाणु सदा भरपूर हैं, उसी तरह शरीरमें रहनेवाले आकाशमें भी सूक्ष्म पुद्गल-परमाणुओंका समूह भरपूर है। जीव वहाँसे सूक्ष्म पुद्गलोंको ग्रहण करके कर्मबंध करता है।
___ ९६. ऐसी आशंका की जाये कि शरीरसे दूर-बहुत दूर रहनेवाले किसी किसी पदार्थके प्रति जीव रागद्वेष करे तो वह वहाँके पुद्गल ग्रहण करके कर्मबंध करता है या नहीं ? इसका समाधान यह है कि वह रागद्वेषरूप परिणति तो आत्माकी विभावरूप परिणति है, और उस परिणतिका कर्ता आत्मा है और वह शरीरमें रहकर करता है, इसलिये शरीरमें रहनेवाला जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्रमें है. उस क्षेत्रमें रहे हुए. पुद्गल परमाणुओंको ग्रहण करके बाँधता है । वह उन्हें ग्रहण करनेके लिये बाहर नहीं जाता।
९७. यश, अपयश, कीति जो नामकर्म है वह नामकर्मसंबंध जिस शरीरके कारण है, वह शरीर जहाँ तक रहता है वहाँ तक चलता है, वहाँसे आगे नहीं चलता। जीव जब सिद्धावस्थाको प्राप्त होता है,