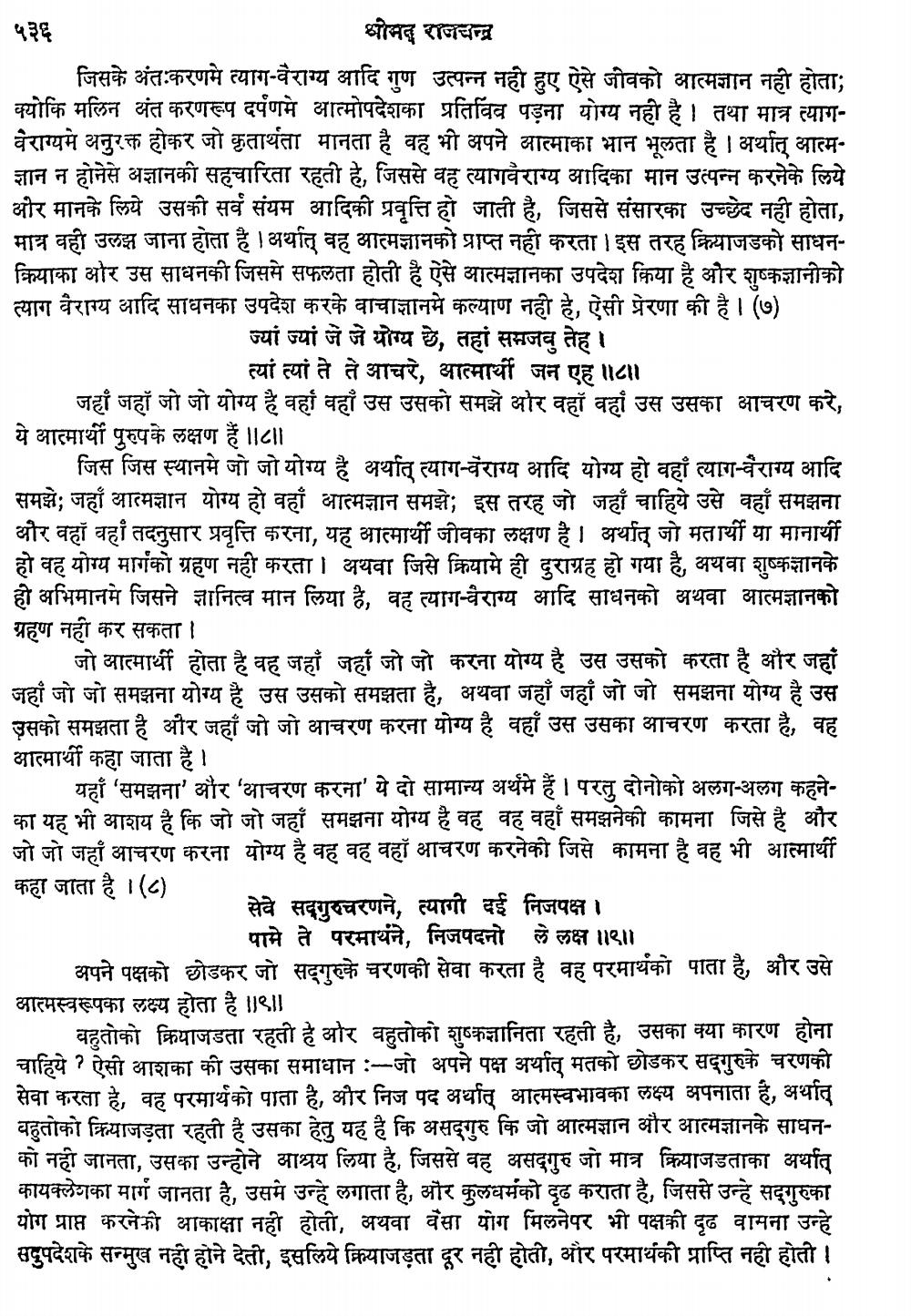________________
५३६
धीमद् राजचन्द्र जिसके अंतःकरणमे त्याग-वैराग्य आदि गुण उत्पन्न नही हुए ऐसे जीवको आत्मज्ञान नही होता; क्योकि मलिन अंत करणरूप दर्पणमे आत्मोपदेशका प्रतिबिंब पड़ना योग्य नहीं है। तथा मात्र त्यागवैराग्यमे अनुरक्त होकर जो कृतार्थता मानता है वह भी अपने आत्माका भान भूलता है । अर्थात् आत्मज्ञान न होनेसे अज्ञानकी सहचारिता रहती है, जिससे वह त्यागवैराग्य आदिका मान उत्पन्न करनेके लिये और मानके लिये उसकी सर्व संयम आदिकी प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे संसारका उच्छेद नहीं होता, मात्र वही उलझ जाना होता है । अर्थात् वह आत्मज्ञानको प्राप्त नहीं करता। इस तरह क्रियाजडको साधनक्रियाका ओर उस साधनकी जिससे सफलता होती है ऐसे आत्मज्ञानका उपदेश किया है और शुष्कज्ञानीको त्याग वैराग्य आदि साधनका उपदेश करके वाचाज्ञानमे कल्याण नही है, ऐसी प्रेरणा की है । (७)
ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजवु तेह।
त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥८॥ जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहां वहाँ उस उसको समझे और वहाँ वहाँ उस उसका आचरण करे, ये आत्मार्थी पुरुपके लक्षण हैं ||८||
जिस जिस स्थानमे जो जो योग्य है अर्थात् त्याग-वैराग्य आदि योग्य हो वहाँ त्याग-वैराग्य आदि समझे; जहाँ आत्मज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझे; इस तरह जो जहाँ चाहिये उसे वहाँ समझना और वहाँ वहाँ तदनुसार प्रवृत्ति करना, यह आत्मार्थी जीवका लक्षण है। अर्थात् जो मतार्थी या मानार्थी हो वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता। अथवा जिसे क्रियामे ही दुराग्रह हो गया है, अथवा शुष्कज्ञानके हो अभिमानमे जिसने ज्ञानित्व मान लिया है, वह त्याग-वैराग्य आदि साधनको अथवा आत्मज्ञानको ग्रहण नहीं कर सकता।
जो आत्मार्थी होता है वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है उस उसको करता है और जहां जहाँ जो जो समझना योग्य है उस उसको समझता है, अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उस उसको समझता है और जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है वहाँ उस उसका आचरण करता है, वह आत्मार्थी कहा जाता है।
यहाँ 'समझना' और 'आचरण करना' ये दो सामान्य अर्थमे हैं। परतु दोनोको अलग-अलग कहनेका यह भी आशय है कि जो जो जहाँ समझना योग्य है वह वह वहाँ समझनेकी कामना जिसे है और जो जो जहाँ आचरण करना योग्य है वह वह वहाँ आचरण करनेको जिसे कामना है वह भी आत्मार्थी कहा जाता है । (८)
___ सेवे सद्गुरुचरणने, त्यागी दई निजपक्ष ।
पामे ते परमार्थने, निजपदनो ले लक्ष ॥९॥ अपने पक्षको छोडकर जो सद्गुरुके चरणकी सेवा करता है वह परमार्थको पाता है, और उसे आत्मस्वरूपका लक्ष्य होता है |९||
बहुतोको क्रियाजडता रहती है और बहुतोको शुष्कज्ञानिता रहती है, उसका क्या कारण होना चाहिये ? ऐसी आशका की उसका समाधान :-जो अपने पक्ष अर्थात् मतको छोडकर सद्गुरुके चरणको सेवा करता है, वह परमार्थको पाता है, और निज पद अर्थात् आत्मस्वभावका लक्ष्य अपनाता है, अर्थात् बहुतोको क्रिन्याजड़ता रहती है उसका हेतु यह है कि असद्गुरु कि जो आत्मज्ञान और आत्मज्ञानके साधनको नहीं जानता, उसका उन्होने आश्रय लिया है, जिससे वह असद्गुरु जो मात्र क्रियाजडताका अर्थात् कायक्लेगका मार्ग जानता है, उसमे उन्हे लगाता है, और कुलधर्मको दृढ कराता है, जिससे उन्हे सद्गुरुका योग प्राप्त करनेकी आकाक्षा नही होती, अथवा वैसा योग मिलनेपर भी पक्षकी दृढ वासना उन्हे सदुपदेशके सन्मुख नहीं होने देती, इसलिये क्रियाजड़ता दूर नहीं होती, और परमार्थको प्राप्ति नहीं होती।