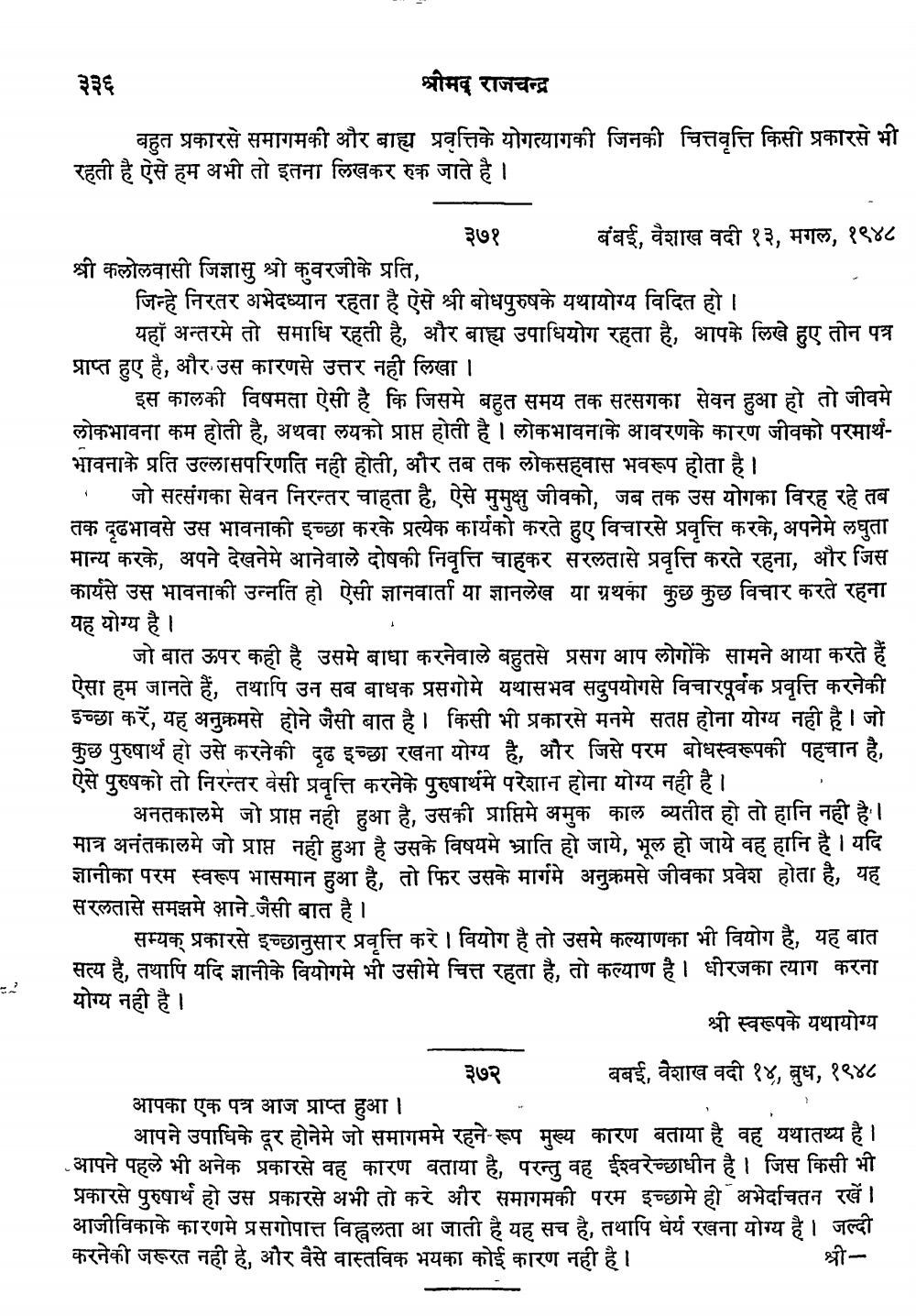________________
३३६
श्रीमद राजचन्द्र __बहुत प्रकारसे समागमकी और बाह्य प्रवृत्तिके योगत्यागकी जिनकी चित्तवृत्ति किसी प्रकारसे भी रहती है ऐसे हम अभी तो इतना लिखकर रुक जाते है।
३७१ बंबई, वैशाख वदी १३, मगल, १९४८ श्री कलोलवासी जिज्ञासु श्री कुवरजीके प्रति,
जिन्हे निरतर अभेदध्यान रहता है ऐसे श्री बोधपुरुषके यथायोग्य विदित हो ।
यहाँ अन्तरमे तो समाधि रहती है, और बाह्य उपाधियोग रहता है, आपके लिखे हुए तोन पत्र प्राप्त हुए है, और उस कारणसे उत्तर नही लिखा।
इस कालकी विषमता ऐसी है कि जिसमे बहुत समय तक सत्सगका सेवन हुआ हो तो जीवमें लोकभावना कम होती है, अथवा लयको प्राप्त होती है । लोकभावनाके आवरणके कारण जीवको परमार्थभावनाके प्रति उल्लासपरिणति नही होती, और तब तक लोकसहवास भवरूप होता है। । जो सत्संगका सेवन निरन्तर चाहता है, ऐसे मुमुक्षु जीवको, जब तक उस योगका विरह रहे तब तक दृढभावसे उस भावनाकी इच्छा करके प्रत्येक कार्यको करते हुए विचारसे प्रवृत्ति करके, अपनेमे लघुता मान्य करके, अपने देखनेमे आनेवाले दोषकी निवृत्ति चाहकर सरलतासे प्रवृत्ति करते रहना, और जिस कार्यसे उस भावनाकी उन्नति हो ऐसी ज्ञानवार्ता या ज्ञानलेख या ग्रथका कुछ कुछ विचार करते रहना यह योग्य है।
___जो बात ऊपर कही है उसमे बाधा करनेवाले बहुतसे प्रसग आप लोगोंके सामने आया करते हैं ऐसा हम जानते हैं, तथापि उन सब बाधक प्रसगोमे यथासभव सदुपयोगसे विचारपूर्वक प्रवृत्ति करनेकी इच्छा करें, यह अनुक्रमसे होने जैसी बात है। किसी भी प्रकारसे मनमे सतप्त होना योग्य नही है । जो कुछ पुरुषार्थ हो उसे करनेकी दृढ इच्छा रखना योग्य है, और जिसे परम बोधस्वरूपकी पहचान है, ऐसे पुरुषको तो निरन्तर वेसी प्रवृत्ति करनेके पुरुषार्थमे परेशान होना योग्य नही है।
अनतकालमे जो प्राप्त नही हुआ है, उसकी प्राप्तिमे अमुक काल व्यतीत हो तो हानि नही है। मात्र अनंतकालमे जो प्राप्त नही हआ है उसके विषयमे भ्राति हो जाये, भूल हो जाये वह हानि है । यदि ज्ञानीका परम स्वरूप भासमान हआ है, तो फिर उसके मार्गमे अनुक्रमसे जीवका प्रवेश होता है, यह सरलतासे समझमे आने जैसी बात है।
सम्यक् प्रकारसे इच्छानुसार प्रवृत्ति करे । वियोग है तो उसमे कल्याणका भी वियोग है, यह बात सत्य है, तथापि यदि ज्ञानीके वियोगमे भी उसीमे चित्त रहता है, तो कल्याण है। धीरजका त्याग करना योग्य नही है।
श्री स्वरूपके यथायोग्य
३७२ बबई, वैशाख वदी १४, बुध, १९४८ आपका एक पत्र आज प्राप्त हुआ।
आपने उपाधिके दूर होनेमे जो समागममे रहने रूप मुख्य कारण बताया है वह यथातथ्य है । आपने पहले भी अनेक प्रकारसे वह कारण बताया है, परन्तु वह ईश्वरेच्छाधीन है। जिस किसी भी प्रकारसे पुरुषार्थ हो उस प्रकारसे अभी तो करे और समागमकी परम इच्छामे ही अभेचतन रखें। आजीविकाके कारणमे प्रसगोपात्त विह्वलता आ जाती है यह सच है, तथापि धेर्य रखना योग्य है। जल्दी करनेकी जरूरत नही है, और वैसे वास्तविक भयका कोई कारण नही है।
श्री