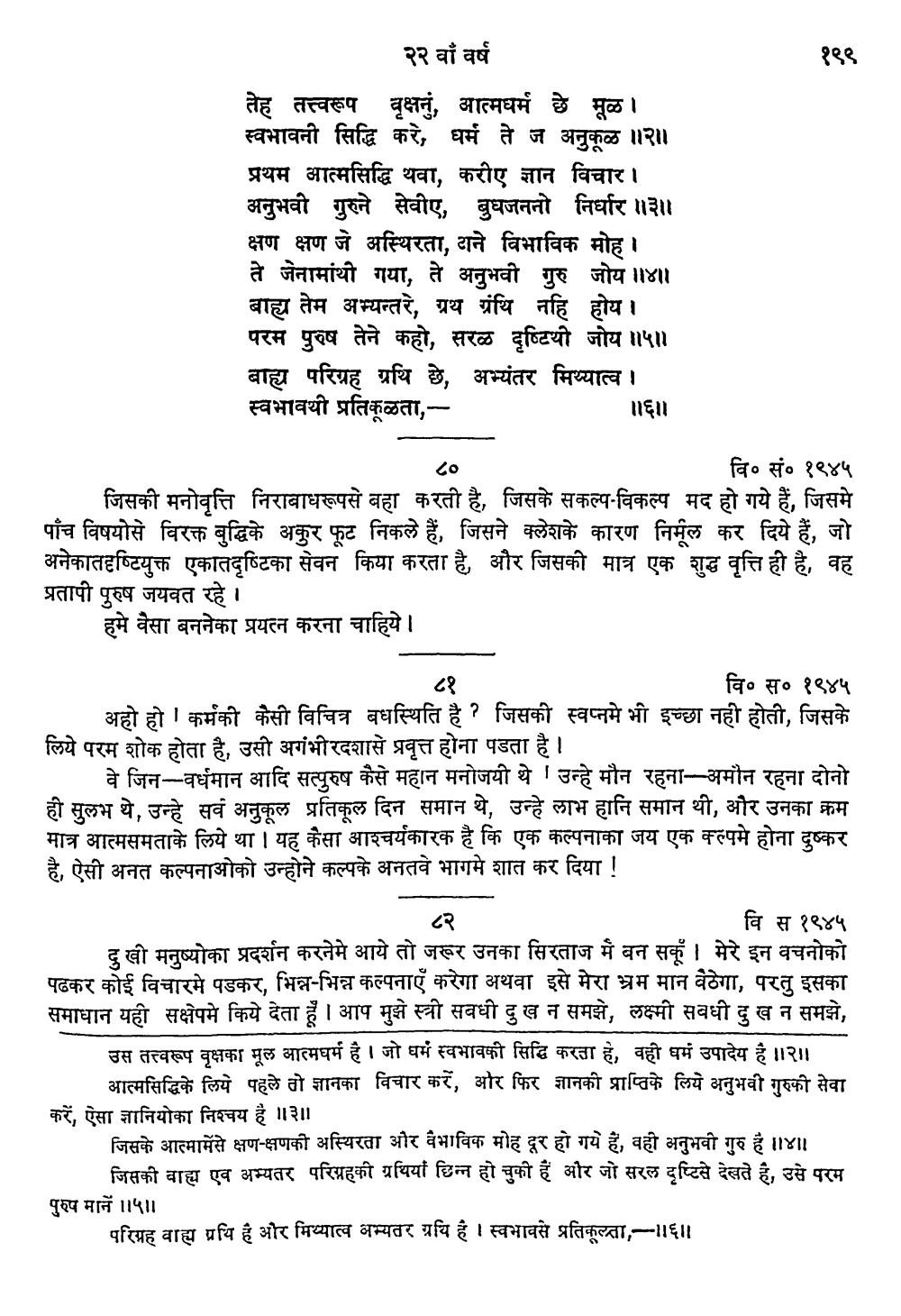________________
१९९
२२ वाँ वर्ष तेह तत्त्वरूप वृक्षन, आत्मधर्म छे मूळ। स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते ज अनुकूळ ॥२॥ प्रथम आत्मसिद्धि थवा, करीए ज्ञान विचार। अनुभवी गुरुने सेवीए, बुधजननो निर्धार ॥३॥ क्षण क्षण जे अस्थिरता, दाने विभाविक मोह। ते जेनामांथो गया, ते अनुभवी गुरु जोय ॥४॥ बाह्य तेम अभ्यन्तरे, ग्रथ ग्रंथि नहि होय । परम पुरुष तेने कहो, सरळ दृष्टियी जोय ॥५॥ बाह्य परिग्रह ग्रथि छे, अभ्यंतर मिथ्यात्व ।। स्वभावथी प्रतिकूळता,
॥६॥
८०
वि० सं० १९४५ जिसकी मनोवृत्ति निराबाधरूपसे बहा करती है, जिसके सकल्प-विकल्प मद हो गये हैं, जिसमे पाँच विषयोसे विरक्त बुद्धिके अकुर फूट निकले हैं, जिसने क्लेशके कारण निर्मूल कर दिये हैं, जो अनेकातदृष्टियुक्त एकातदृष्टिका सेवन किया करता है, और जिसकी मात्र एक शुद्ध वृत्ति ही है, वह प्रतापी पुरुष जयवत रहे।
हमे वैसा बननेका प्रयत्न करना चाहिये।
वि० स० १९४५ अहो हो । कर्मकी कैसी विचित्र बधस्थिति है ? जिसकी स्वप्नमे भी इच्छा नहीं होती, जिसके लिये परम शोक होता है, उसी अगंभीरदशासे प्रवृत्त होना पडता है।।
वे जिन-वर्धमान आदि सत्पुरुष कैसे महान मनोजयी थे | उन्हे मौन रहना-अमौन रहना दोनो ही सुलभ थे, उन्हे सर्व अनुकूल प्रतिकूल दिन समान थे, उन्हे लाभ हानि समान थी, और उनका क्रम मात्र आत्मसमताके लिये था। यह कैसा आश्चर्यकारक है कि एक कल्पनाका जय एक क्ल्पमे होना दुष्कर है, ऐसी अनत कल्पनाओको उन्होने कल्पके अनतवे भागमे शात कर दिया !
८२
वि स १९४५ दुखी मनुष्योका प्रदर्शन करनेमे आये तो जरूर उनका सिरताज में बन सकूँ। मेरे इन वचनोको पढकर कोई विचारमे पडकर, भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ करेगा अथवा इसे मेरा भ्रम मान बैठेगा, परतु इसका समाधान यही सक्षेपमे किये देता हूँ। आप मुझे स्त्री सवधी दुख न समझे, लक्ष्मी सवधी दु ख न समझे,
उस तत्त्वरूप वृक्षका मूल आत्मधर्म है । जो धर्म स्वभावकी सिद्धि करता है, वही धर्म उपादेय है ॥२॥
आत्मसिद्धिके लिये पहले तो ज्ञानका विचार करें, और फिर ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अनुभवी गुरुकी सेवा करें, ऐसा ज्ञानियोका निश्चय है ॥३॥
जिसके आत्मामेंसे क्षण-क्षणकी अस्थिरता और वैभाविक मोह दूर हो गये हैं, वही अनुभवी गुरु है ॥४॥
जिसकी बाह्य एव अभ्यतर परिग्रहकी ग्रथियां छिन्न हो चुकी हैं और जो सरल दृष्टिसे देखते है, उसे परम पुरुष मानें ॥५॥
परिग्रह वाह्य ग्रयि है और मिथ्यात्व अभ्यतर ग्रथि है । स्वभावसे प्रतिकूलता,-॥६॥