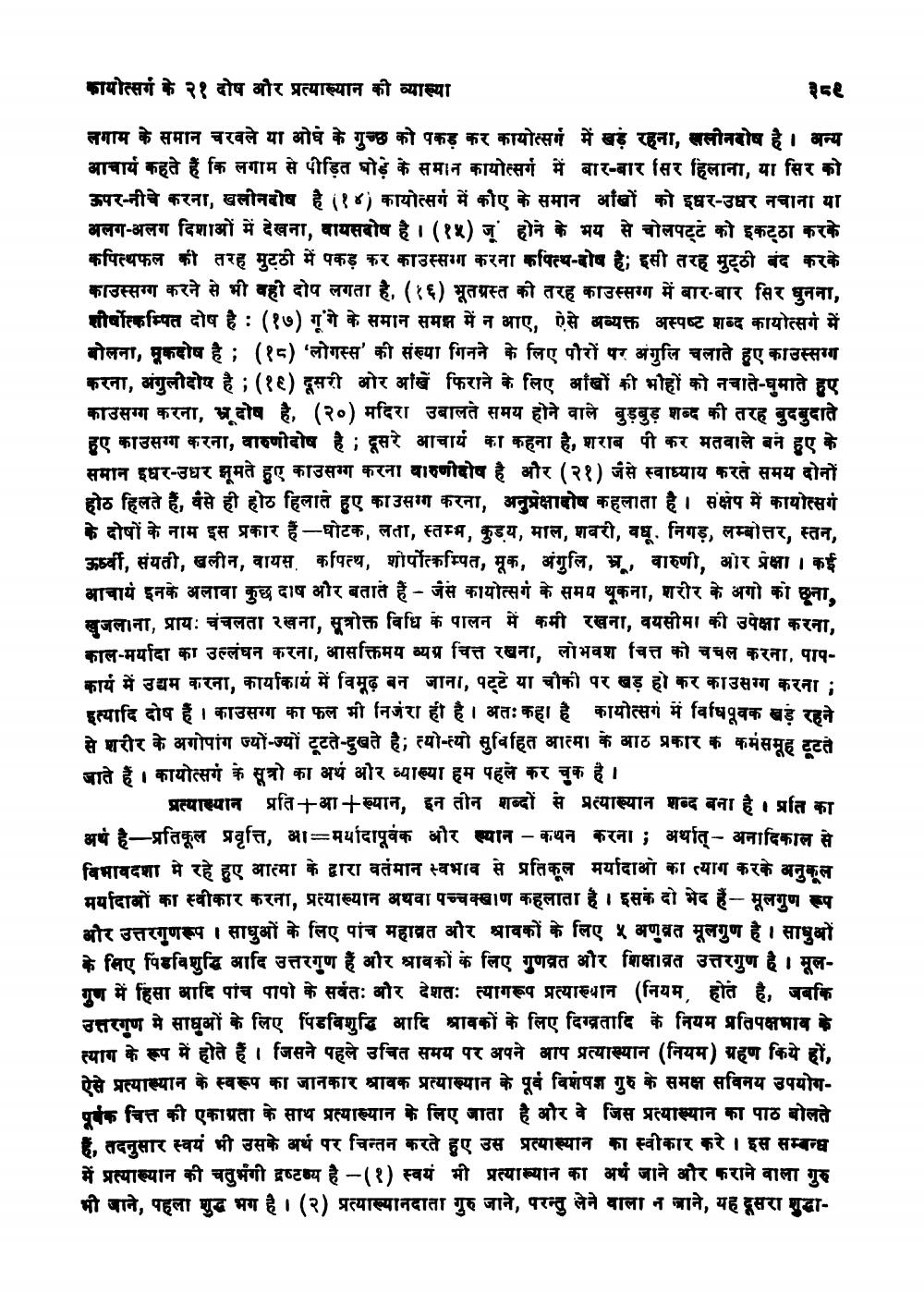________________
कायोत्सर्ग के २१ दोष और प्रत्याख्यान की व्याख्या
३८९ लगाम के समान चरवले या ओघ के गुच्छ को पकड़ कर कायोत्सर्ग में खड़े रहना, खलीनदोष है। अन्य आचार्य कहते हैं कि लगाम से पीड़ित घोड़े के समान कायोत्सर्ग में बार-बार सिर हिलाना, या सिर को ऊपर-नीचे करना, खलीनदोष है (१४) कायोत्सर्ग में कौए के समान आँखों को इधर-उधर नचाना या अलग-अलग दिशाओं में देखना, वायसदोष है । (१५) जू होने के भय से चोलपट्टे को इकट्ठा करके कपित्थफल की तरह मुट्ठी में पकड़ कर काउस्सग्ग करना कपित्थ-दोष है; इसी तरह मुट्ठी बंद करके काउस्सग्ग करने से भी वही दोष लगता है, (१६) भूतग्रस्त की तरह काउस्सग्ग में बार-बार सिर धुनना, शीर्वोत्कम्पित दोष है : (१७) गूगे के समान समझ में न आए, ऐसे अव्यक्त अस्पष्ट शब्द कायोत्सर्ग में बोलना, मूकदोष है ; (१८) 'लोगस्स' की संख्या गिनने के लिए पोरों पर अंगुलि चलाते हुए काउस्सग्ग करना, अंगुलीदोष है ; (१९) दूसरी ओर आंखें फिराने के लिए आँखों की भौहों को नचाते-घुमाते हुए काउसग्ग करना, 5 दोष है, (२०) मदिरा उबालते समय होने वाले बुड़बुड़ शब्द की तरह बुदबुदाते हुए काउसग्ग करना, वारुणोदोष है ; दूसरे आचार्य का कहना है, शराब पी कर मतवाले बने हुए के समान इधर-उधर झमते हुए काउसग्ग करना वारुणीदोष है और (२१) जैसे स्वाध्याय करते समय दोनों होठ हिलते हैं, वैसे ही होठ हिलाते हुए काउसग्ग करना, अनुप्रेक्षादोष कहलाता है। संक्षेप में कायोत्सर्ग के दोषों के नाम इस प्रकार हैं-घोटक, लता, स्तम्भ, कुडय, माल, शबरी, वधू. निगड़, लम्बोत्तर, स्तन, अवी, संयती, खलीन, वायस. कपित्थ, शोर्पोत्कम्पित, मूक, अंगुलि, 5, वारुणी, और प्रेक्षा । कई आचार्य इनके अलावा कुछ दाष और बताते हैं - जैसे कायोत्सर्ग के समय थूकना, शरीर के अगो को छुना, खुजलाना, प्रायः चंचलता रखना, सूत्रोक्त विधि के पालन में कमी रखना, वयसीमा की उपेक्षा करना, काल-मर्यादा का उल्लंघन करना, आसक्तिमय व्यग्र चित्त रखना, लोभवश चित्त को चचल करना, पापकार्य में उद्यम करना, कार्याकार्य में विमूढ़ बन जाना, पट्टे या चौकी पर खड़ हो कर काउसग्ग करना; इत्यादि दोष हैं । काउसग्ग का फल भी निरा ही है। अतः कहा है कायोत्सर्ग में विधिपूर्वक बड़े रहने से शरीर के अगोपांग ज्यों-ज्यों टूटते-दुखते है; त्यो त्यो सुविहित आत्मा के आठ प्रकार के कर्मसमूह दृटते जाते हैं । कायोत्सर्ग के सूत्रो का अर्थ और व्याख्या हम पहले कर चुक है ।
प्रत्याख्यान प्रति+आ+ख्यान, इन तीन शब्दों से प्रत्याख्यान शब्द बना है। प्रति का अर्थ है-प्रतिकूल प्रवृत्ति, आ=मर्यादापूर्वक और ख्यान – कथन करना; अर्थात्- अनादिकाल से विभावदशा मे रहे हुए आत्मा के द्वारा वर्तमान स्वभाव से प्रतिकूल मर्यादाओ का त्याग करके अनुकल मर्यादाओं का स्वीकार करना, प्रत्याख्यान अथवा पच्चक्खाण कहलाता है । इसके दो भेद हैं- मूलगुण रूप
और उत्तरगुणरूप । साधुओं के लिए पांच महावत और श्रावकों के लिए ५ अणुव्रत मूलगुण है। साधुवों के लिए पिंडविशुद्धि आदि उत्तरगुण हैं और श्रावकों के लिए गुणव्रत और शिक्षाव्रत उत्तरगुण है । मूलगुण में हिंसा आदि पांच पापो के सर्वतः और देशतः त्यागरूप प्रत्याख्यान (नियम, होते है, जबकि उत्तरगण मे साधुओं के लिए पिंडविशुद्धि आदि श्रावकों के लिए दिग्वतादि के नियम प्रतिपक्षभाव के त्याग के रूप में होते हैं । जिसने पहले उचित समय पर अपने आप प्रत्याख्यान (नियम) ग्रहण किये हों, ऐसे प्रत्याख्यान के स्वरूप का जानकार श्रावक प्रत्याख्यान के पूर्व विशेषज्ञ गुरु के समक्ष सविनय उपयोगपूर्वक चित्त की एकाग्रता के साथ प्रत्याख्यान के लिए जाता है और वे जिस प्रत्याख्यान का पाठ बोलते है, तदनुसार स्वयं भी उसके अर्थ पर चिन्तन करते हुए उस प्रत्याख्यान का स्वीकार करे । इस सम्बन्ध में प्रत्याख्यान की चतुभंगी द्रष्टव्य है -(१) स्वयं भी प्रत्याख्यान का अर्थ जाने और कराने वाला गुरु भी जाने, पहला शुद्ध भग है । (२) प्रत्याख्यानदाता गुरु जाने, परन्तु लेने वाला न बाने, यह दूसरा शुद्धा