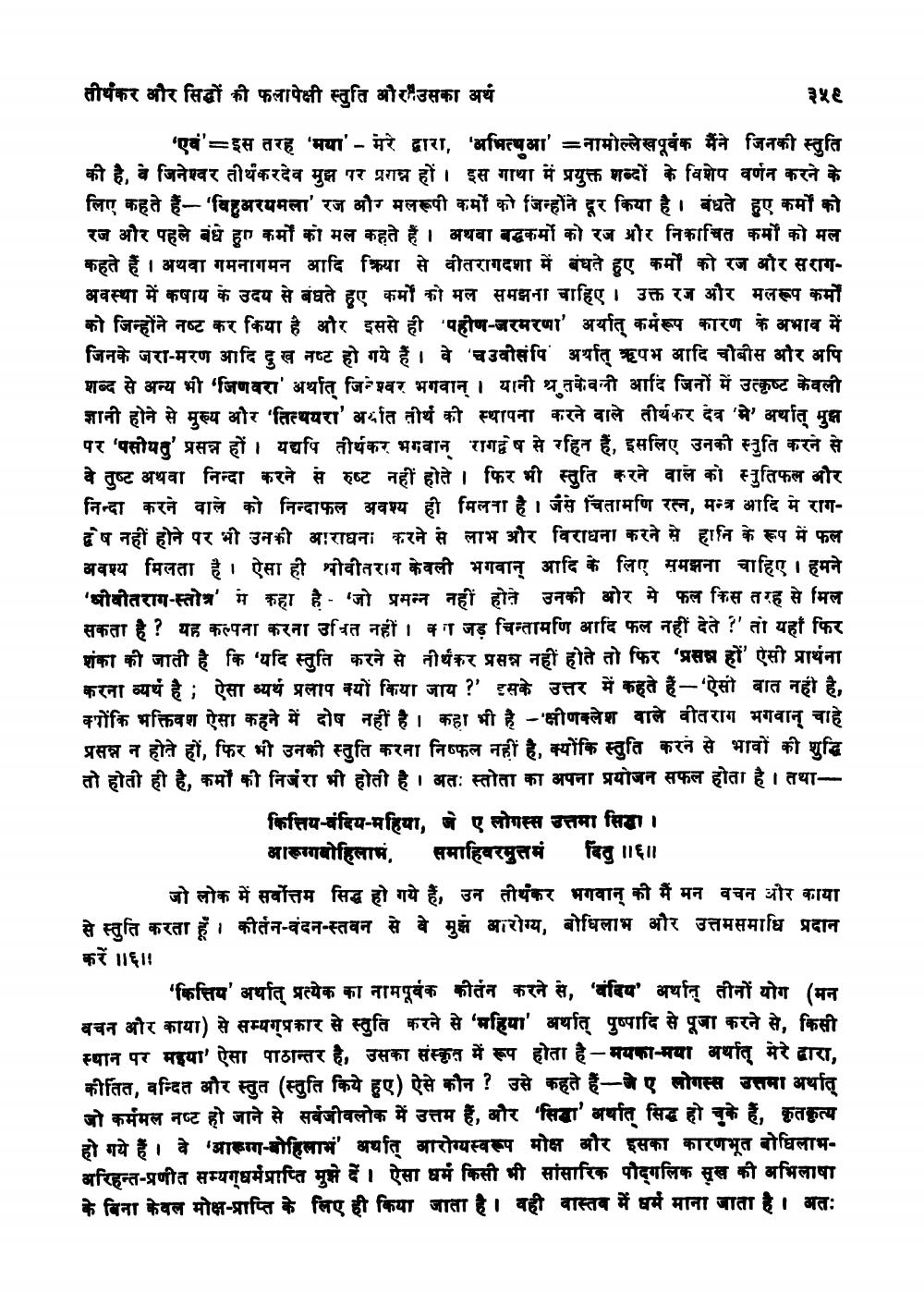________________
तीर्थकर और सिद्धों की फलापेक्षी स्तुति और उसका अर्थ
३५९ "एवं'=इस तरह 'मया' - मेरे द्वारा, 'अभियुमा' =नामोल्लेखपूर्वक मैंने जिनकी स्तुति की है, वे जिनेश्वर तीर्थंकरदेव मुझ पर प्रसन्न हों। इस गाथा में प्रयुक्त शब्दों के विशेप वर्णन करने के लिए कहते हैं- "विहुअरयमला' रज और मलरूपी कर्मों को जिन्होंने दूर किया है। बंधते हुए कर्मों को रज और पहले बंधे हुए कर्मों को मल कहते हैं । अथवा बद्धकर्मों को रज और निकाचित कर्मों को मल कहते हैं । अथवा गमनागमन आदि क्रिया से वीतरागदशा में बंधते हुए कर्मों को रज और सरागअवस्था में कषाय के उदय से बंधते हुए कर्मों को मल समझना चाहिए। उक्त रज और मलरूप कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर किया है और इससे ही 'पहीण-जरमरणा' अर्थात् कर्मरूप कारण के अभाव में जिनके जरा-मरण आदि दुख नष्ट हो गये हैं। वे 'चउवोसंपि अर्थात् ऋषभ आदि चौबीस और अपि शब्द से अन्य भी 'जिणवरा' अर्थात् जितेश्वर भगवान् । यानी श्रु तवली आदि जिनों में उत्कृष्ट केवली ज्ञानी होने से मुख्य और 'तित्ययरा' अर्थात तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थकर देव 'मे' अर्थात् मुझ पर 'पसोयतु' प्रसन्न हों। यद्यपि तीर्थकर भगवान रागद्वेष से रहित हैं, इसलिए उनकी स्तुति करने से वे तुष्ट अथवा निन्दा करने से रुष्ट नहीं होते । फिर भी स्तुति करने वाले को स्तुतिफल और निन्दा करने वाले को निन्दाफल अवश्य ही मिलता है । जैसे चिंतामणि रत्न, मन्त्र आदि मे रागद्वेष नहीं होने पर भी उनकी आराधना करने से लाभ और विराधना करने से हानि के रूप में फल अवश्य मिलता है। ऐसा ही श्रीवीतराग केवली भगवान् आदि के लिए समझना चाहिए । हमने 'धोवीतराग-स्तोत्र' में कहा है - 'जो प्रमन्न नहीं होते उनकी ओर मे फल किस तरह से मिल सकता है ? यह कल्पना करना उचित नहीं। का जड़ चिन्तामणि आदि फल नहीं देते ?' तो यहाँ फिर शंका की जाती है कि 'यदि स्तुति करने से तीर्थंकर प्रसन्न नहीं होते तो फिर 'प्रसन्न हों' ऐसी प्रार्थना करना व्यर्थ है ; ऐसा व्यर्थ प्रलाप क्यों किया जाय ?' इसके उत्तर में कहते हैं- 'ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भक्तिवश ऐसा कहने में दोष नहीं है। कहा भी है - 'क्षीणक्लेश वाले वीतराग भगवान् चाहे प्रसन्न न होते हों, फिर भी उनकी स्तुति करना निष्फल नहीं है, क्योंकि स्तुति करने से भावों की शुद्धि तो होती ही है, कर्मों की निर्जरा भी होती है । अतः स्तोता का अपना प्रयोजन सफल होता है । तथा
कित्तिय-बंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिखा।
आडग्गबोहिलामं, समाहिवरमुत्तमं वितु ॥६॥ जो लोक में सर्वोत्तम सिद्ध हो गये हैं, उन तीर्थकर भगवान् की मैं मन वचन और काया से स्तुति करता हूँ। कीर्तन-वंदन-स्तवन से वे मुझं आरोग्य, बोधिलाभ और उत्तमसमाधि प्रदान करें ॥६॥
_ 'कित्तिय' अर्थात् प्रत्येक का नामपूर्वक कीर्तन करने से, 'बंदिय' अर्थात् तीनों योग (मन वचन और काया) से सम्यगप्रकार से स्तुति करने से 'महिया' अर्थात् पुष्पादि से पूजा करने से, किसी स्थान पर महया' ऐसा पाठान्तर है, उसका संस्कृत में रूप होता है-मयका-मया अर्थात् मेरे द्वारा, कीर्तित, वन्दित और स्तुत (स्तुति किये हुए) ऐसे कौन ? उसे कहते हैं-जे ए लोगस्स उत्तमा अर्थात् जो कर्ममल नष्ट हो जाने से सर्वजीवलोक में उत्तम हैं, और "सिखा' अर्थात् सिद्ध हो चुके हैं, कृतकृत्य हो गये हैं। वे 'आरूग्ग-बोहिलामं' अर्थात आरोग्यस्वरूप मोक्ष और इसका कारणभूत बोधिलाभअरिहन्त-प्रणीत सम्यग्धर्मप्राप्ति मुझे दें। ऐसा धर्म किसी भी सांसारिक पोद्गलिक सुख की अभिलाषा के बिना केवल मोक्ष-प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। वही वास्तव में धर्म माना जाता है। अतः