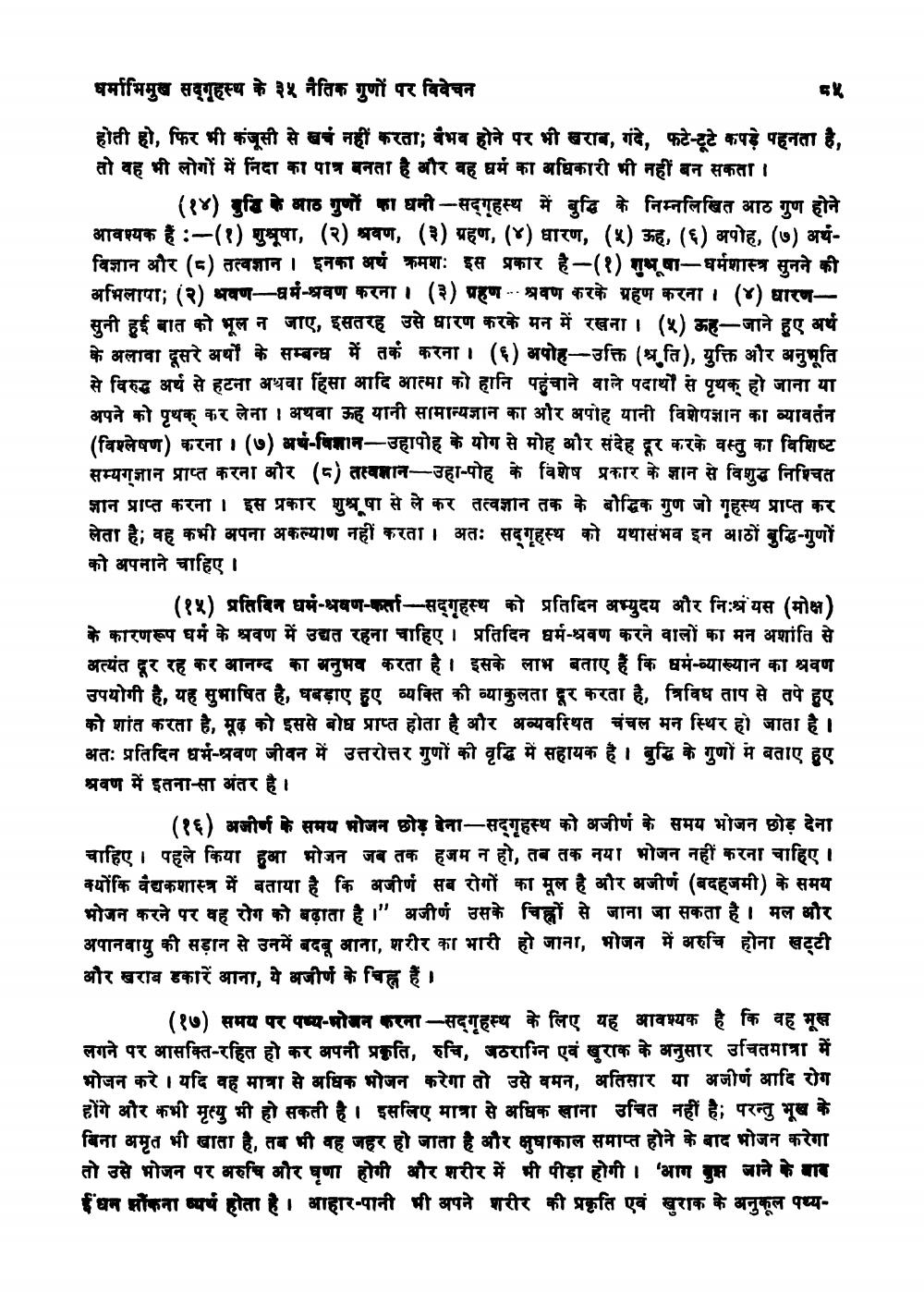________________
धर्माभिमुख सद्गृहस्थ के ३५ नैतिक गुणों पर विवेचन होती हो, फिर भी कंजूसी से खर्च नहीं करता; वैभव होने पर भी खराब, गंदे, फटे-टूटे कपड़े पहनता है, तो वह भी लोगों में निंदा का पात्र बनता है और वह धर्म का अधिकारी भी नहीं बन सकता।
(१४) बुद्धि के माठ गुणों का धनी-सद्गृहस्थ में बुद्धि के निम्नलिखित आठ गुण होने आवश्यक हैं :-(१) शुश्रूषा, (२) श्रवण, (३) ग्रहण, (४) धारण, (५) ऊह, (६) अपोह, (७) अर्थविज्ञान और (6) तत्वज्ञान । इनका अर्थ क्रमशः इस प्रकार है-(१) गुभूषा-धर्मशास्त्र सुनने की अभिलाषा; (२) श्रवण-धर्म-श्रवण करना। (३) ग्रहण ... श्रवण करके ग्रहण करना। (४) धारणसनी हई बात को भूल न जाए, इसतरह उसे धारण करके मन में रखना। (५) मह-जाने हुए अर्थ के अलावा दूसरे अर्थों के सम्बन्ध में तकं करना। (६) अपोह-उक्ति (श्र ति), युक्ति और अनुभूति से विरुद्ध अर्थ से हटना अथवा हिंसा आदि आत्मा को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों से पृथक हो जाना या अपने को पृथक् कर लेना । अथवा ऊह यानी सामान्यज्ञान का और अपोह यानी विशेषज्ञान का व्यावर्तन (विश्लेषण) करना । (७) अर्थ-विज्ञान-उहापोह के योग से मोह और संदेह दूर करके वस्तु का विशिष्ट सम्यग्ज्ञान प्राप्त करना और (८) तस्वज्ञान-उहा-पोह के विशेष प्रकार के ज्ञान से विशुद्ध निश्चित ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार शुश्रूषा से ले कर तत्वज्ञान तक के बौद्धिक गुण जो गृहस्थ प्राप्त कर लेता है; वह कभी अपना अकल्याण नहीं करता। अतः सद्गृहस्थ को यथासंभव इन आठों बुद्धि-गुणों को अपनाने चाहिए।
(१५) प्रतिदिन धर्म-श्रवण-कर्ता-सद्गृहस्थ को प्रतिदिन अभ्युदय और निःश्रेयस (मोक्ष) के कारणरूप धर्म के श्रवण में उद्यत रहना चाहिए। प्रतिदिन धर्म-श्रवण करने वालों का मन अशांति से अत्यंत दूर रह कर आनन्द का अनुभव करता है। इसके लाभ बताए हैं कि धर्म-व्याख्यान का श्रवण उपयोगी है, यह सुभाषित है, घबड़ाए हुए व्यक्ति की व्याकुलता दूर करता है, त्रिविध ताप से तपे हुए को शांत करता है, मूढ़ को इससे बोध प्राप्त होता है और अव्यवस्थित चंचल मन स्थिर हो जाता है। अतः प्रतिदिन धर्म-श्रवण जीवन में उत्तरोत्तर गुणों को वृद्धि में सहायक है। बुद्धि के गुणों में बताए हुए श्रवण में इतना-सा अंतर है।
(१६) अजीर्ण के समय भोजन छोड़ देना-सद्गृहस्थ को अजीर्ण के समय भोजन छोड़ देना चाहिए। पहले किया हुमा भोजन जब तक हजम न हो, तब तक नया भोजन नहीं करना चाहिए । क्योंकि वैद्यकशास्त्र में बताया है कि अजीर्ण सब रोगों का मूल है और अजीर्ण (बदहजमी) के समय भोजन करने पर वह रोग को बढ़ाता है।" अजीर्ण उसके चिह्नों से जाना जा सकता है। मल और अपानवायु की सड़ान से उनमें बदबू आना, शरीर का भारी हो जाना, भोजन में अरुचि होना खट्टी और खराब हकारें आना, ये अजीर्ण के चिह्न हैं।
(१७) समय पर पण्य-मोजन करना-सद्गृहस्थ के लिए यह आवश्यक है कि वह भूख लगने पर आसक्ति-रहित हो कर अपनी प्रकृति, रुचि, जठराग्नि एवं खुराक के अनुसार उचितमात्रा में भोजन करे । यदि वह मात्रा से अधिक भोजन करेगा तो उसे वमन, अतिसार या अजीणं आदि रोग होंगे और कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मात्रा से अधिक खाना उचित नहीं है। परन्तु भूख के बिना अमृत भी खाता है, तब भी वह जहर हो जाता है और भुषाकाल समाप्त होने के बाद भोजन करेगा तो उसे भोजन पर अरुचि और घृणा होगी और शरीर में भी पीड़ा होगी। 'भाग बुझ जाने के बाद धम झोंकना व्यर्थ होता है। आहार-पानी भी अपने शरीर की प्रकृति एवं खुराक के अनुकूल पथ्य