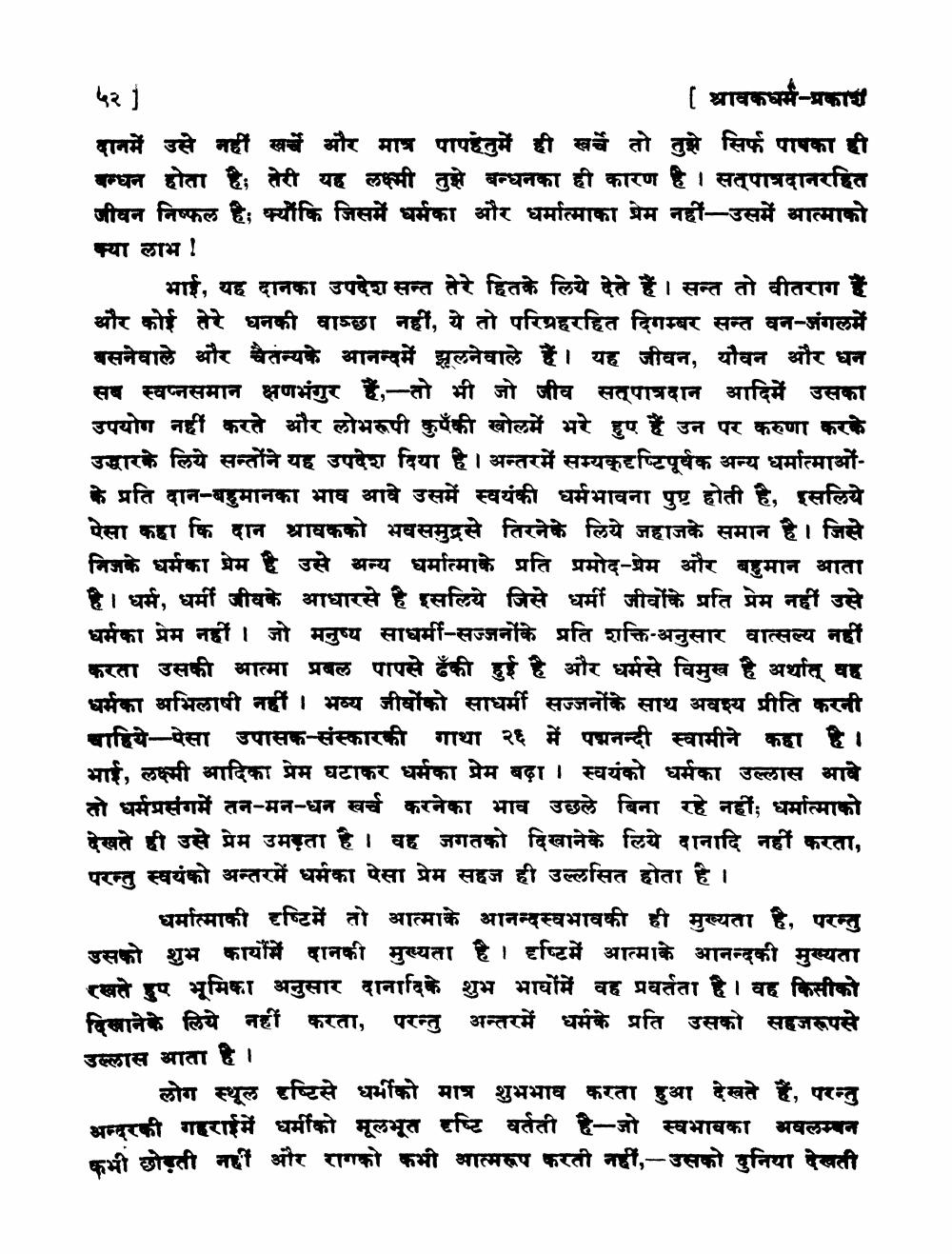________________
५२)
[ श्रावकधर्म-प्रकाश दानमें उसे नहीं स्वर्चे और मात्र पापहंतुमें ही खर्चे तो तुझे सिर्फ पापका ही बन्धन होता है; तेरी यह लक्ष्मी तुझे बन्धनका ही कारण है । सत्पात्रदानरहित जीवन निष्फल है, क्योंकि जिसमें धर्मका और धर्मात्माका प्रेम नहीं-उसमें आत्माको क्या लाभ!
भाई, यह दानका उपदेश सन्त तेरे हितके लिये देते हैं। सन्त तो वीतराग है और कोई तेरे धनकी वाञ्छा नहीं, ये तो परिग्रहरहित दिगम्बर सन्त वन-जंगलमें बसनेवाले और चैतन्यके आनन्दमें झुलनेवाले हैं। यह जीवन, यौवन और धन सब स्वप्नसमान क्षणभंगुर हैं, तो भी जो जीव सत्पात्रदान आदिमें उसका उपयोग नहीं करते और लोभरूपी कुएँकी खोलमें भरे हुए हैं उन पर करुणा करके उद्धारके लिये सन्तोंने यह उपदेश दिया है। अन्तरमें सम्यक्दृष्टिपूर्वक अन्य धर्मात्माओंके प्रति दान-बहुमानका भाव आवे उसमें स्वयंकी धर्मभावना पुष्ट होती है, इसलिये ऐसा कहा कि दान श्रावकको भवसमुद्रसे तिरनेके लिये जहाजके समान है। जिसे निजके धर्मका प्रेम है उसे अन्य धर्मात्माके प्रति प्रमोद-प्रेम और बहुमान आता है। धर्म, धर्मी जीवके आधारसे है इसलिये जिसे धर्मी जीवोंके प्रति प्रेम नहीं उसे धर्मका प्रेम नहीं। जो मनुष्य साधर्मी-सज्जनोंके प्रति शक्ति-अनुसार वात्सल्य नहीं करता उसकी आत्मा प्रबल पापसे ढंकी हुई है और धर्मसे विमुख है अर्थात् वह धर्मका अभिलाषी नहीं। भव्य जीवोंको साधर्मी सज्जनोंके साथ अवश्य प्रीति करनी चाहिये-ऐसा उपासक-संस्कारकी गाथा २६ में पननन्दी स्वामीने कहा है। भाई, लक्ष्मी आदिका प्रेम घटाकर धर्मका प्रेम बढ़ा। स्वयंको धर्मका उल्लास आवे तो धर्मप्रसंगमें तन-मन-धन खर्च करनेका भाव उछले बिना रहे नहीं; धर्मात्माको देखते ही उसे प्रेम उमड़ता है। वह जगतको दिखानेके लिये दानादि नहीं करता, परन्तु स्वयंको अन्तरमें धर्मका ऐसा प्रेम सहज ही उल्लसित होता है।
__ धर्मात्माकी दृष्टि में तो आत्माके आनन्दस्वभावकी ही मुख्यता है, परन्तु उसको शुभ कार्यों में दानकी मुख्यता है। दृष्टिमें आत्माके आनन्दकी मुख्यता रखते हुए भूमिका अनुसार दानादिके शुभ भायोंमें वह प्रवर्तता है। वह किसीको दिखानेके लिये नहीं करता, परन्तु अन्तरमें धर्मके प्रति उसको सहजरूपसे उल्लास आता है।
लोग स्थूल दृष्टिसे धर्मीको मात्र शुभभाष करता हुआ देखते हैं, परन्तु अन्दरकी गहराई में धर्मीको मूलभूत दृष्टि वर्तती है-जो स्वभावका अवलम्बन कभी छोड़ती नहीं और रागको कभी आत्मरूप करती नहीं, उसको दुनिया देखती