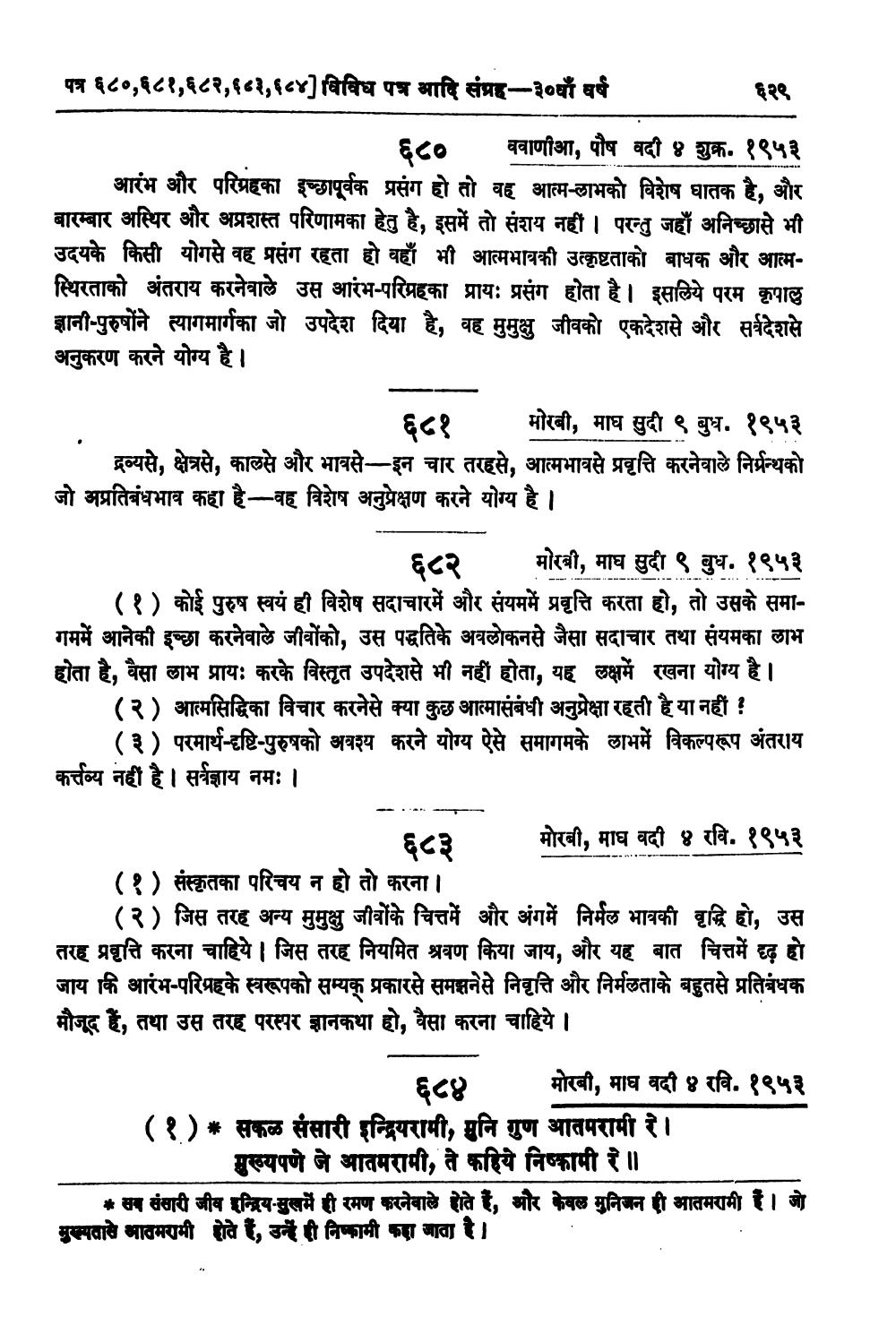________________
पत्र ६८०,६८१,६८२,६८३,६८४] विविध पत्र आदि संग्रह-३०याँ वर्ष
६२९
६८० ववाणीआ, पौष वदी १ शुक्र. १९५३ आरंभ और परिग्रहका इच्छापूर्वक प्रसंग हो तो वह आत्म-लाभको विशेष घातक है, और बारम्बार अस्थिर और अप्रशस्त परिणामका हेतु है, इसमें तो संशय नहीं। परन्तु जहाँ अनिच्छासे भी उदयके किसी योगसे वह प्रसंग रहता हो वहाँ भी आत्मभावकी उत्कृष्टताको बाधक और आत्मस्थिरताको अंतराय करनेवाले उस आरंभ-परिग्रहका प्रायः प्रसंग होता है। इसलिये परम कृपाल ज्ञानी-पुरुषोंने त्यागमार्गका जो उपदेश दिया है, वह मुमुक्षु जीवको एकदेशसे और सर्वदेशसे अनुकरण करने योग्य है।
६८१ मोरबी, माघ सुदी ९ बुध. १९५३ द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे-इन चार तरहसे, आत्मभावसे प्रवृत्ति करनेवाले निर्ग्रन्थको जो अप्रतिबंधभाव कहा है-वह विशेष अनुप्रेक्षण करने योग्य है।
६८२ मोरबी, माघ सुदी ९ बुध. १९५३ (१) कोई पुरुष स्वयं ही विशेष सदाचारमें और संयममें प्रवृत्ति करता हो, तो उसके समागममें आनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंको, उस पद्धतिके अवलोकनसे जैसा सदाचार तथा संयमका लाभ होता है, वैसा लाभ प्रायः करके विस्तृत उपदेशसे भी नहीं होता, यह लक्षमें रखना योग्य है ।
(२) आत्मसिद्धिका विचार करनेसे क्या कुछ आत्मासंबंधी अनुप्रेक्षा रहती है या नहीं !
(३) परमार्थ-दृष्टि-पुरुषको अवश्य करने योग्य ऐसे समागमके लाभमें विकल्परूप अंतराय कर्त्तव्य नहीं है। सर्वज्ञाय नमः ।
मोरबी, माघ वदी १ रवि. १९५३ (१) संस्कृतका परिचय न हो तो करना।
(२) जिस तरह अन्य मुमुक्षु जीवोंके चित्तमें और अंगमें निर्मल भावकी वृद्धि हो, उस तरह प्रवृत्ति करना चाहिये । जिस तरह नियमित श्रवण किया जाय, और यह बात चित्तमें दृढ़ हो जाय कि आरंभ-परिग्रहके स्वरूपको सम्यक् प्रकारसे समझनेसे निवृत्ति और निर्मलताके बहुतसे प्रतिबंधक मौजूद हैं, तथा उस तरह परस्पर ज्ञानकथा हो, वैसा करना चाहिये ।
६८४ मोरबी, माघ वदी १ रवि. १९५३ (१) * सकळ संसारी इन्द्रियरामी, मुनि गुण आतमरामी रे।
मुख्यपणे जे आतमरामी, ते कहिये निष्कामी रे॥ * सब संसारी जीव इन्द्रिय-मुखमें ही रमण करनेवाले होते है, और केवल मुनिजन ही आतमरामी है। जो मुस्मतासे मातमरामी होते हैं, उन ही निकामी कहा जाता है।