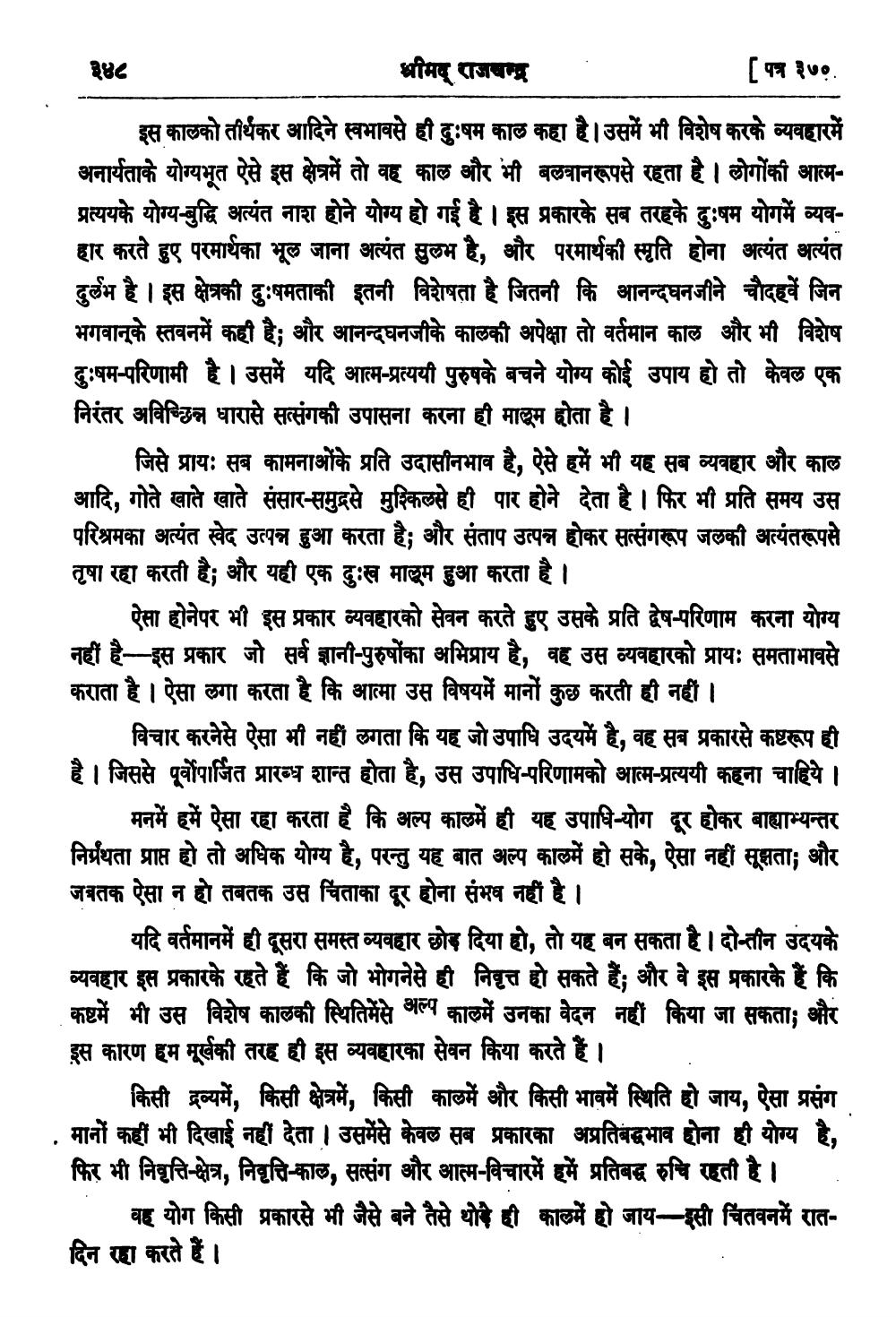________________
३४८
श्रीमद् राजचन्द्र
[पत्र ३७०. इस कालको तीर्थकर आदिने स्वभावसे ही दुःषम काल कहा है। उसमें भी विशेष करके व्यवहारमें अनार्यताके योग्यभूत ऐसे इस क्षेत्रमें तो वह काल और भी बलवानरूपसे रहता है। लोगोंकी आत्मप्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यंत नाश होने योग्य हो गई है। इस प्रकारके सब तरहके दुःषम योगमें व्यवहार करते हुए परमार्थका भूल जाना अत्यंत सुलभ है, और परमार्थकी स्मृति होना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है । इस क्षेत्रकी दुःषमताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दघनजीने चौदहवें जिन भगवान्के स्तवनमें कही है; और आनन्दघनजीके कालकी अपेक्षा तो वर्तमान काल और भी विशेष दुःषम-परिणामी है। उसमें यदि आत्म-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केवल एक निरंतर अविच्छिन्न धारासे सत्संगकी उपासना करना ही मालूम होता है ।
जिसे प्रायः सब कामनाओंके प्रति उदासीनभाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काल आदि, गोते खाते खाते संसार-समुद्रसे मुश्किलसे ही पार होने देता है। फिर भी प्रति समय उस परिश्रमका अत्यंत खेद उत्पन्न हुआ करता है और संताप उत्पन्न होकर सत्संगरूप जलकी अत्यंतरूपसे तृषा रहा करती है; और यही एक दुःख मालूम हुआ करता है।
ऐसा होनेपर भी इस प्रकार व्यवहारको सेवन करते हुए उसके प्रति द्वेष-परिणाम करना योग्य नहीं है इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अभिप्राय है, वह उस व्यवहारको प्रायः समताभावसे कराता है। ऐसा लगा करता है कि आत्मा उस विषयमें मानों कुछ करती ही नहीं।
विचार करनेसे ऐसा भी नहीं लगता कि यह जो उपाधि उदयमें है, वह सब प्रकारसे कष्टरूप ही है । जिससे पूर्वोपार्जित प्रारब्ध शान्त होता है, उस उपाधि-परिणामको आत्म-प्रत्ययी कहना चाहिये ।
मनमें हमें ऐसा रहा करता है कि अल्प कालमें ही यह उपाधि-योग दूर होकर बाह्याभ्यन्तर निग्रंथता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह बात अल्प कालमें हो सके, ऐसा नहीं सूझता; और जबतक ऐसा न हो तबतक उस चिंताका दूर होना संभव नहीं है।
___ यदि वर्तमानमें ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह बन सकता है। दो-तीन उदयके व्यवहार इस प्रकारके रहते हैं कि जो भोगनेसे ही निवृत्त हो सकते हैं; और वे इस प्रकारके हैं कि कष्टमें भी उस विशेष कालकी स्थिति से अल्प कालमें उनका वेदन नहीं किया जा सकता और इस कारण हम मूर्खकी तरह ही इस व्यवहारका सेवन किया करते हैं।
किसी द्रव्यमें, किसी क्षेत्रमें, किसी कालमें और किसी भावमें स्थिति हो जाय, ऐसा प्रसंग . मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता । उसमेंसे केवल सब प्रकारका अप्रतिबद्धभाव होना ही योग्य है, फिर भी निवृत्ति-क्षेत्र, निवृत्ति-काल, सत्संग और आत्म-विचारमें हमें प्रतिबद्ध रुचि रहती है।
वह योग किसी प्रकारसे भी जैसे बने तैसे थोड़े ही कालमें हो जाय-इसी चितवनमें रातदिन रहा करते हैं।