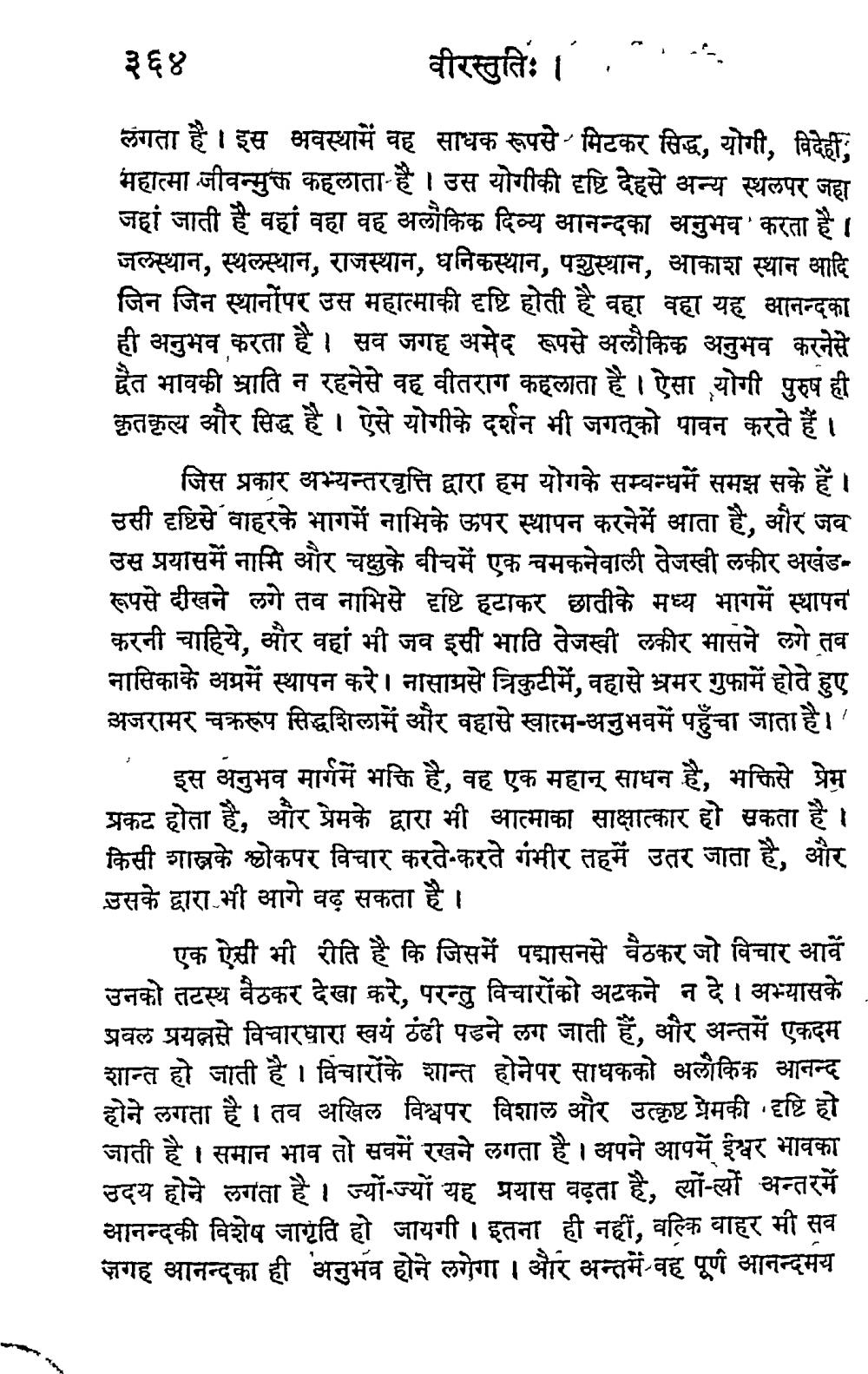________________
३६४
वीरस्तुतिः । . " . ...
अनुभव करता है।
राजस्थान, धनिकस्थान,
जिन जिन स्थान
लगता है । इस अवस्थामें वह साधक रूपसे मिटकर सिद्ध, योगी, विदेही; महात्मा जीवन्मुक्त कहलाता है । उस योगीकी दृष्टि देहसे अन्य स्थलपर जहा जहां जाती है वहां वहा वह अलौकिक दिव्य आनन्दका अनुभव करता है । जलस्थान, स्थलस्थान, राजस्थान, धनिकस्थान, पशुस्थान, आकाश स्थान आदि जिन जिन स्थानोंपर उस महात्माकी दृष्टि होती है वहा वहा यह आनन्दका ही अनुभव करता है। सब जगह अमेद रूपसे अलौकिक अनुभव करनेसे द्वैत भावकी भ्राति न रहनेसे वह वीतराग कहलाता है। ऐसा योगी पुरुष ही कृतकृत्य और सिद्ध है। ऐसे योगीके दर्शन भी जगत्को पावन करते हैं।
जिस प्रकार अभ्यन्तरवृत्ति द्वारा हम योगके सम्बन्धमें समझ सके हैं। उसी दृष्टि से वाहरके भागमें नाभिके ऊपर स्थापन करनेमें आता है, और जव उस प्रयासमें नामि और चक्षुके बीचमें एक चमकनेवाली तेजखी लकीर अखंडरूपसे दीखने लगे तव नाभिसे दृष्टि हटाकर छातीके मध्य भागमें स्थापन करनी चाहिये, और वहां भी जव इसी भाति तेजखी लकीर भासने लगे तव नासिकाके अग्रमें स्थापन करे। नासाग्रसे त्रिकुटीमें, वहासे भ्रमर गुफामें होते हुए अजरामर चक्ररूप सिद्धशिलामें और वहासे खात्म-अनुभवमें पहुँचा जाता है।' ' इस अनुभव मार्गमें भक्ति है, वह एक महान् साधन है, भक्तिसे प्रेम प्रकट होता है, और प्रेमके द्वारा भी आत्माका साक्षात्कार हो सकता है। किसी शास्त्रके श्लोकपर विचार करते-करते गंभीर तहमें उतर जाता है, और उसके द्वारा भी आगे बढ़ सकता है।
एक ऐसी भी रीति है कि जिसमें पद्मासनसे वैठकर जो विचार आ उनको तटस्थ वैठकर देखा करे, परन्तु विचारोंको अटकने न दे । अभ्यासके प्रवल प्रयत्नसे विचारधारा स्वयं ठंढी पडने लग जाती हैं, और अन्तमें एकदम शान्त हो जाती है। विचारोंके शान्त होनेपर साधकको अलौकिक आनन्द होने लगता है । तव अखिल विश्वपर विशाल और उत्कृष्ट प्रेमकी दृष्टि हो जाती है। समान भाव तो सवमें रखने लगता है। अपने आपमें ईश्वर भावका उदय होने लगता है। ज्यों-ज्यों यह प्रयास बढ़ता है, त्यों-त्यों अन्तरमें आनन्दकी विशेष जागृति हो जायगी । इतना ही नहीं, बल्कि बाहर मी सव जगह आनन्दका ही अनुभव होने लगेगा । और अन्तमें वह पूर्ण आनन्दमय