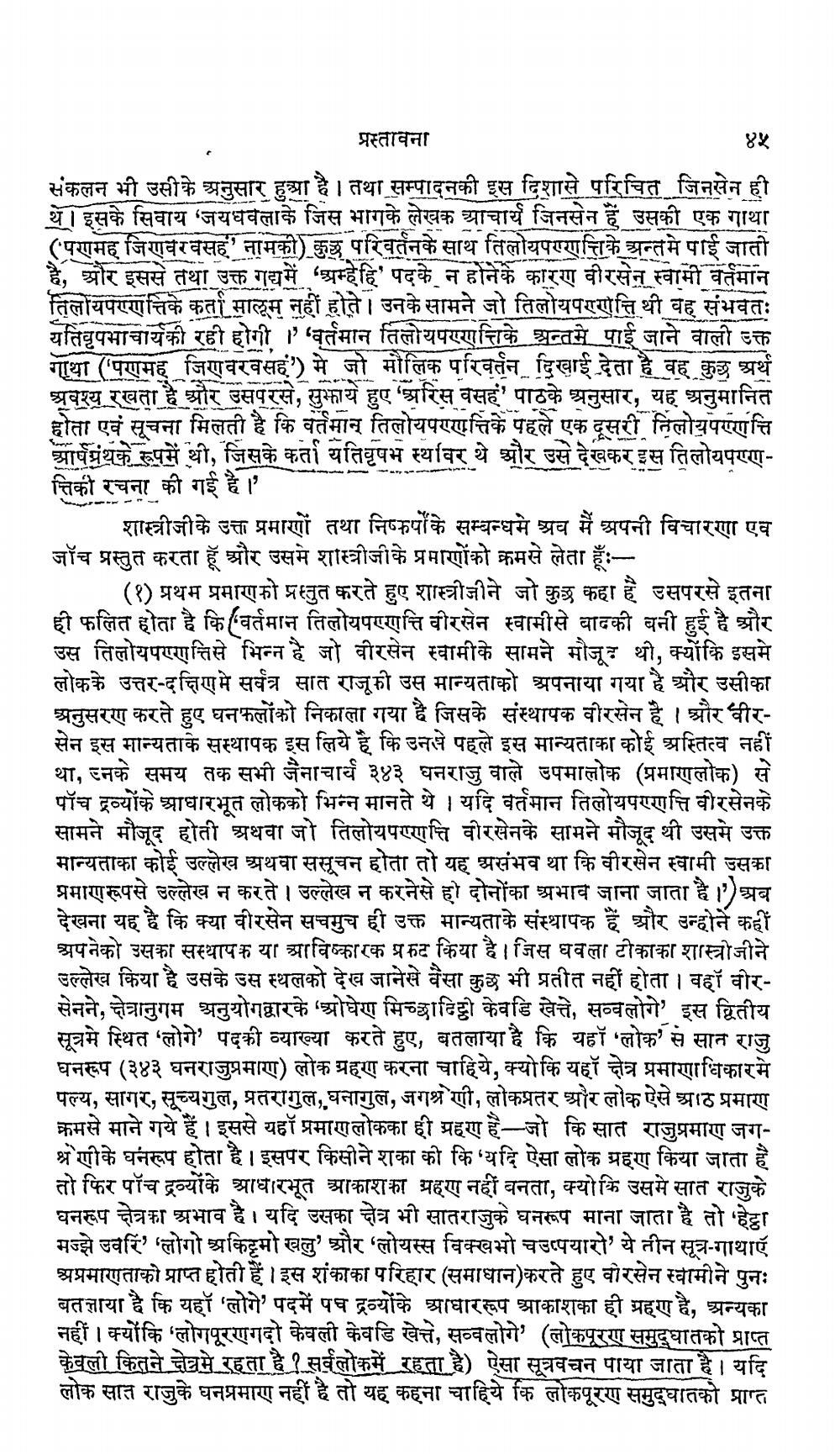________________
प्रस्तावना
संकलन भी उसी के अनुसार हुआ है । तथा सम्पादनकी इस दिशासे परिचित जिनसेन ही थे। इसके सिवाय 'जयधवलाके जिस भागके लेखक आचार्य जिनसेन हैं उसकी एक गाथा (पणमह जिणवरवसह' नामकी) कुछ परिवर्तनके साथ तिलोयपण्णत्तिके अन्तमे पाई जाती है, और इससे तथा उक्त गद्य में 'अम्हे हि' पदके न होने के कारण वीरसेन स्वामी वर्तमान तिलोयपएणत्तिके कर्ता मालूम नहीं होते। उनके सामने जो तिलोयपरणेत्ति थी वह संभवतः यतिवृपभाचार्यकी रही होगी ।' 'वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके अन्तमे पाई जाने वाली उक्त गाथा ('पणमह जिणवरवसई) मे जो मौलिक परिवर्तन दिखाई देता है वह कुछ अर्थ अवश्य रखता है और उसपरसे, सुझाये हुए 'अरिस वसह' पाठके अनुसार, यह अनुमानित होता एवं सूचना मिलती है कि वर्तमान तिलोयपएणत्तिके पहले एक दूसरी तिलोयपरणत्ति आग्रंथके रूपमें थी, जिसके कर्ता यतिवृषभ स्थविर थे और उसे देखकर इस तिलोयपएणत्तिकी रचना की गई है।'
शास्त्रीजीके उत्त प्रमाणों तथा निष्कर्षों के सम्बन्धमे अव में अपनी विचारणा एव जॉच प्रस्तुत करता हूँ और उसमे शास्त्रीजीके प्रमाणोंको क्रमसे लेता हूँ:
(१) प्रथम प्रमाणको प्रस्तुत करते हुए शास्त्रीजीने जो कुछ कहा है उसपरसे इतना ही फलित होता है कि वर्तमान तिलोयपएणत्ति वीरसेन स्वामीसे बादकी बनी हुई है और उस तिलोयपण्णत्तिसे भिन्न है जो वीरसेन स्वामीके सामने मौजूद थी, क्योंकि इसमे लोकके उत्तर-दक्षिण मे सर्वत्र सात राजूकी उस मान्यताको अपनाया गया है और उसीका अनुसरण करते हुए घनफलोंको निकाला गया है जिसके संस्थापक वीरसेन है । और वीरसेन इस मान्यताके सस्थापक इस लिये है कि उनसे पहले इस मान्यताका कोई अस्तित्व नहीं था, उनके समय तक सभी जैनाचार्य ३४३ धनराजु वाले उपमालोक (प्रमाणलोक) से पॉच द्रव्योंके आधारभूत लोकको भिन्न मानते थे । यदि वर्तमान तिलोयपएणत्ति वीरसेनके सामने मौजूद होती अथवा जो तिलोयपएणत्ति वीरसेनके सामने मौजूद थी उसमे उक्त मान्यताका कोई उल्लेख अथवा ससूचन होता तो यह असंभव था कि वीरसेन स्वामी उसका प्रमाणरूपसे उल्लेख न करते। उल्लेख न करनेसे हो दोनोंका अभाव जाना जाता है।')अब देखना यह है कि क्या वीरसेन सचमुच ही उक्त मान्यताके संस्थापक हैं और उन्होने कहीं अपनेको उसका सस्थापक या आविष्कारक प्रकट किया है। जिस धवला टीकाका शास्त्रीजीने उल्लेख किया है उसके उस स्थलको देख जानेसे वैसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। वहाँ वीरसेनने, क्षेत्रानुगम अनुयोगद्वारके 'ओघेण मिच्छादिट्ठी केवडि खेत्ते, सव्वलोगे' इस द्वितीय सूत्रमे स्थित 'लोगे' पदकी व्याख्या करते हुए, बतलाया है कि यहाँ 'लोक' से सात राजु घनरूप (३४३ घनराजुप्रमाण) लोक ग्रहण करना चाहिये, क्योकि यहाँ क्षेत्र प्रमाणाधिकारमे पल्य, सागर, सूच्यगुल, प्रतरागुल, घनागुल, जगणी, लोकप्रतर और लोक ऐसे आठ प्रमाण क्रमसे माने गये हैं। इससे यहॉ प्रमाणलोकका ही ग्रहण है जो कि सात राजुप्रमाण जगश्रेणीके घनरूप होता है । इसपर किसीने शका की कि यदि ऐसा लोक ग्रहण किया जाता है तो फिर पॉच द्रव्योंके आधारभूत आकाशका ग्रहण नहीं बनता, क्योकि उसमे सात राजुके घनरूप क्षेत्रका अभाव है। यदि उसका क्षेत्र भी सातराजुके घनरूप माना जाता है तो 'हेट्ठा मज्झे उवरिं' 'लोगो अकिट्टमो खलु' और 'लोयस्स विक्खभो चउप्पयारो' ये तीन सूत्र-गाथाएँ अप्रमाणताको प्राप्त होती हैं । इस शंकाका परिहार (समाधान)करते हुए वीरसेन स्वामीने पुनः बतलाया है कि यहाँ 'लोगे' पदमें पच द्रव्योंके आधाररूप आकाशका ही ग्रहण है, अन्यका नहीं। क्योंकि लोगपूरणगदो केवली केवडि खेत्ते, सव्वलोगे' (लोकपूरण समुद्घातको प्राप्त केवली कितने क्षेत्रमे रहता है ? सर्वलोकमें रहता है) ऐसा सूत्रवचन पाया जाता है। यदि लोक सात राजुके धनप्रमाण नहीं है तो यह कहना चाहिये कि लोकपूरण समुद्घातको प्राप्त