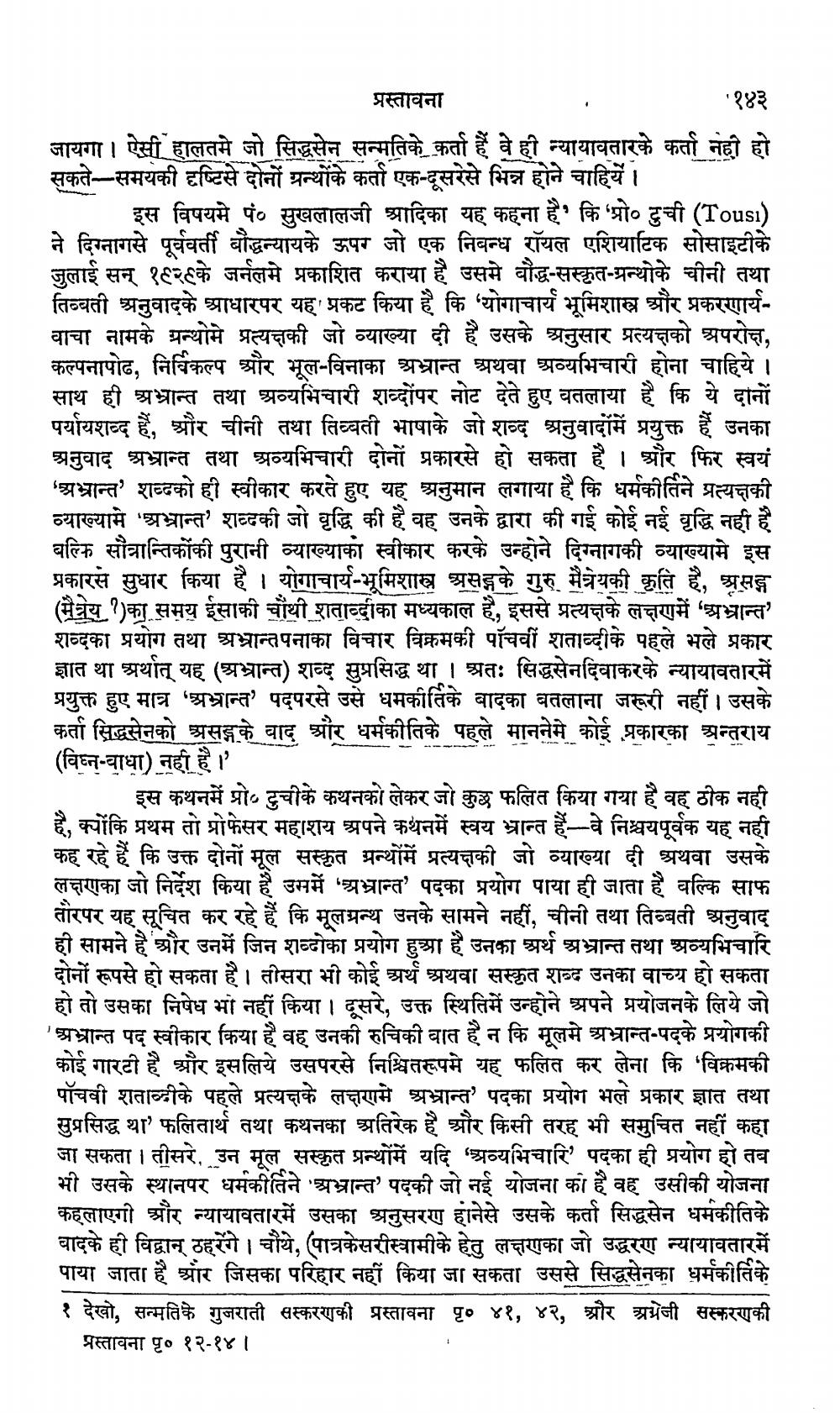________________
प्रस्तावना
१४३ जायगा । ऐसी हालतमे जो सिद्धसेन सन्मति के कर्ता हैं वे ही न्यायावतारके कर्ता नही हो सकते - समयकी दृष्टिसे दोनों ग्रन्थोंके कर्ता एक-दूसरे से भिन्न होने चाहिये ।
इस विषयमे पं० सुखलालजी आदिका यह कहना है' कि 'प्रो० टुची (Tousi) ने दिग्नागसे पूर्ववर्ती बौद्धन्यायके ऊपर जो एक निबन्ध रॉयल एशियाटिक सोसाइटीके जुलाई सन् १६२६के जर्नलमे प्रकाशित कराया है उसमे बौद्ध संस्कृत-ग्रन्थोके चीनी तथा तिब्बती अनुवादके आधारपर यह प्रकट किया है कि 'योगाचार्य भूमिशास्त्र और प्रकरणार्थ - वाचा नामके ग्रन्थोमे प्रत्यक्षकी जो व्याख्या दी है उसके अनुसार प्रत्यक्षको अपरोक्ष, कल्पनापोढ, निर्विकल्प और भूल - विनाका अभ्रान्त अथवा अव्यभिचारी होना चाहिये । साथ ही अभ्रान्त तथा श्रव्यभिचारी शब्दोंपर नोट देते हुए बतलाया है कि ये दानों पर्यायशब्द हैं, और चीनी तथा तिब्बती भाषाके जो शब्द श्रनुवादोंमें प्रयुक्त हैं उनका अनुवाद अभ्रान्त तथा अव्यभिचारी दोनों प्रकारसे हो सकता है । और फिर स्वयं 'अभ्रान्त' शब्दको ही स्वीकार करते हुए यह अनुमान लगाया है कि धर्मकीर्तिने प्रत्यक्षकी व्याख्यामे ‘अभ्रान्त' शब्दकी जो वृद्धि की है वह उनके द्वारा की गई कोई नई वृद्धि नही है बल्कि सौत्रान्तिकोंकी पुरानी व्याख्याको स्वीकार करके उन्होने दिग्नागकी व्याख्यामे इस प्रकारसे सुधार किया है । योगाचार्य - भूमिशास्त्र असके गुरु मैत्रेयकी कृति है, अ (मैत्रेय ?)का समय ईसाकी चौथी शताब्दीका मध्यकाल है, इससे प्रत्यक्षके लक्षण में 'अभ्रान्त' शब्दका प्रयोग तथा अभ्रान्तपनाका विचार विक्रमकी पांचवीं शताब्दी के पहले भले प्रकार ज्ञात था अर्थात् यह (अभ्रान्त) शब्द सुप्रसिद्ध था । श्रतः सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारमें प्रयुक्त हुए मात्र 'अभ्रान्त' पदपरसे उसे धमकीर्तिके बादका बतलाना जरूरी नहीं । उसके कर्ता सिद्धसेनको असङ्गके बाद और धर्मकीतिके पहले माननेमे कोई प्रकारका अन्तराय (विघ्न-बाधा ) नही है ।'
इस कथनमें प्रो० टुचीके कथनको लेकर जो कुछ फलित किया गया है वह ठीक नही है, क्योंकि प्रथम तो प्रोफेसर महाशय अपने कथनमें स्वय भ्रान्त हैं - वे निश्चयपूर्वक यह नही कह रहे हैं कि उक्त दोनों मूल संस्कृत ग्रन्थोंमें प्रत्यक्षकी जो व्याख्या दी अथवा उसके लक्षणका जो निर्देश किया है उसमें 'अभ्रान्त' पदका प्रयोग पाया ही जाता है बल्कि साफ तौरपर यह सूचित कर रहे हैं कि मूलग्रन्थ उनके सामने नहीं, चीनी तथा तिब्बती अनुवाद ही सामने है और उनमें जिन शब्दोका प्रयोग हुआ है उनका अर्थ अभ्रान्त तथा श्रव्यभिचारि दोनों रूपसे हो सकता है । तीसरा भी कोई अर्थ अथवा संस्कृत शब्द उनका वाच्य हो सकता हो तो उसका निषेध भी नहीं किया । दूसरे, उक्त स्थितिमें उन्होने अपने प्रयोजन के लिये जो 'अभ्रान्त पद स्वीकार किया है वह उनकी रुचिकी बात है न कि मूलमे अभ्रान्त - पदके प्रयोगकी कोई गारटी है और इसलिये उसपर से निश्चितरूपमे यह फलित कर लेना कि 'विक्रमकी पाँचवी शताब्दीके पहले प्रत्यक्ष के लक्षणमे अभ्रान्त' पदका प्रयोग भले प्रकार ज्ञात तथा सुप्रसिद्ध था' फलितार्थ तथा कथनका अतिरेक है और किसी तरह भी समुचित नहीं कहा जा सकता । तीसरे, उन मूल संस्कृत प्रन्थोंमें यदि 'अव्यभिचारि' पदका ही प्रयोग हो तब भी उसके स्थानपर धर्मकीर्तिने 'अभ्रान्त' पदकी जो नई योजना की है वह उसीकी योजना कहलाएगी और न्यायावतार में उसका अनुसरण होनेसे उसके कर्ता सिद्धसेन धर्मकीतिके बादके ही विद्वान् ठहरेंगे। चौथे, (पात्रकेसरीस्वामीके हेतु लक्षणका जो उद्धरण न्यायावतार में पाया जाता है और जिसका परिहार नहीं किया जा सकता उससे सिद्धसेनका धर्मकीर्ति के १ देखो, सन्मति के गुजराती सस्करणकी प्रस्तावना पृ० ४१, ४२, और अग्रेजी सस्करणकी प्रस्तावना पृ० १२-१४ ।