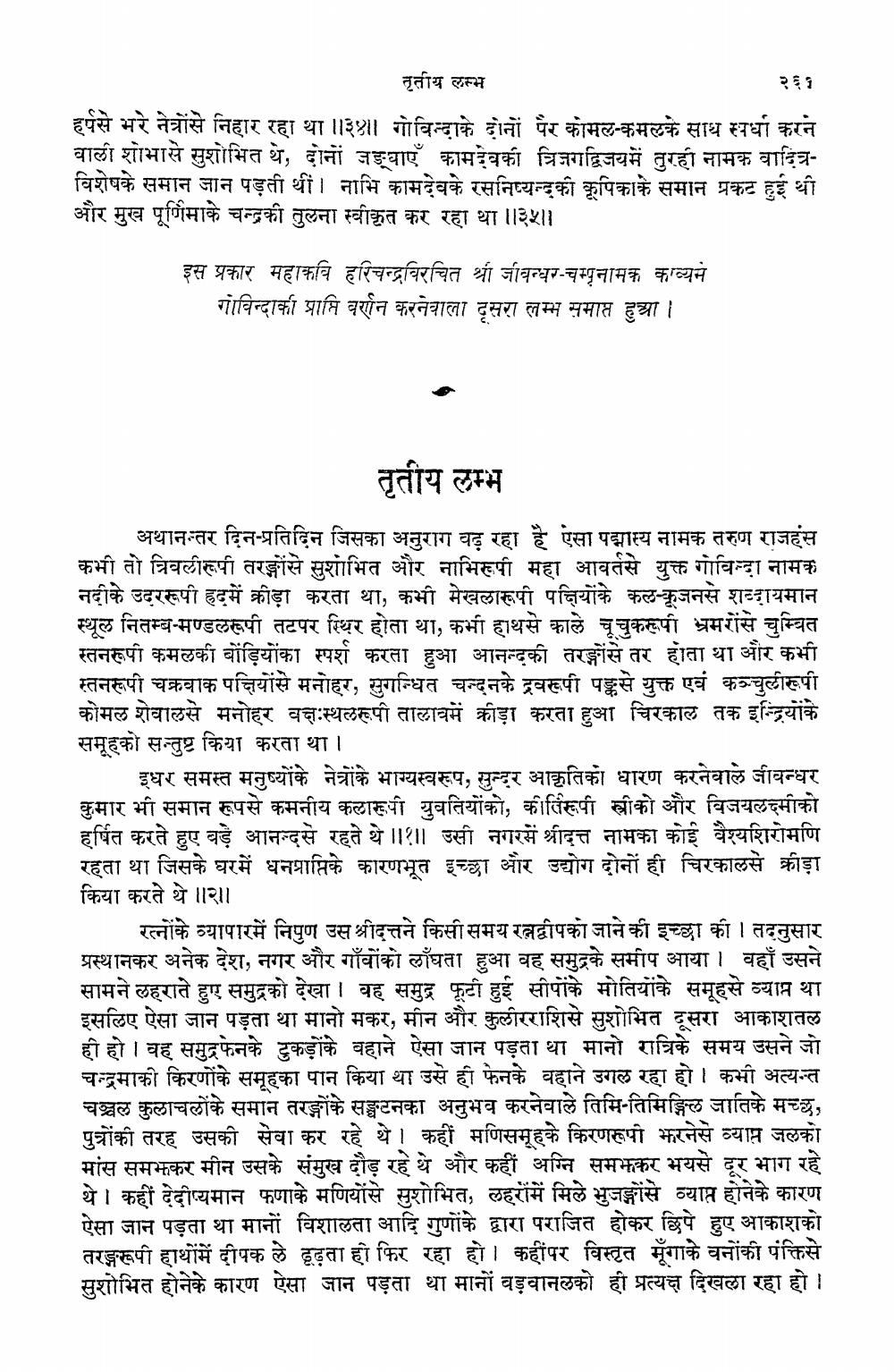________________
तृतीय लाभ
२६३ हर्पसे भरे नेत्रोंसे निहार रहा था ॥३४॥ गोविन्दाके दोनों पैर कोमल-कमलके साथ स्वर्धा करने वाली शोभासे सुशोभित थे, दोनों जवाएँ कामदेवकी त्रिजगद्विजयमें तुरही नामक वादित्रविशेषके समान जान पड़ती थीं। नाभि कामदेवके रसनिष्यन्दकी कूपिकाके समान प्रकट हुई थी और मुख पूर्णिमाके चन्द्रकी तुलना स्वीकृत कर रहा था ।।३।।
इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्रविरचित श्री जीवन्धर-चम्पृनामक काव्यने
गोविन्दाकी प्राप्ति वर्णन करनेवाला दुसरा लम्भ समाप्त हुआ।
तृतीय लम्भ अथानन्तर दिन-प्रतिदिन जिसका अनुराग वढ़ रहा है ऐसा पद्मास्य नामक तरुण राजहंस कभी तो त्रिवलीरूपी तरङ्गोंसे सुशोभित और नाभिरूपी महा आवर्तसे युक्त गोविन्दा नामक नदीके उदररूपी हृदमें क्रीड़ा करता था, कभी मेखलारूपी पक्षियोंके कल-कूजनसे शब्दायमान स्थूल नितम्ब-मण्डलरूपी तटपर स्थिर होता था, कभी हाथसे काले चूचुकरूपी भ्रमरोंसे चुम्बित स्तनरूपी कमलकी बोड़ियोंका स्पर्श करता हुआ आनन्दकी तरङ्गोंसे तर होता था और कभी स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोंसे मनोहर, सुगन्धित चन्दनके द्रवरूपी पङ्कसे युक्त एवं कञ्चुलीरूपी कोमल शेवालसे मनोहर वक्षःस्थलरूपी तालावमें क्रीड़ा करता हुआ चिरकाल तक इन्द्रियों के समूहको सन्तुष्ट किया करता था।
इधर समस्त मनुष्योंके नेत्रोंके भाग्यस्वरूप, सुन्दर आकृतिको धारण करनेवाले जीवन्धर कुमार भी समान रूपसे कमनीय कलारूपी युवतियोंको, कीर्तिरूपी स्त्रीको और विजयलक्ष्मीको हर्षित करते हुए बड़े आनन्दसे रहते थे ||१|| उसी नगरमें श्रीदत्त नामका कोई वैश्यशिरोमणि रहता था जिसके घर में धनप्राप्तिके कारणभूत इच्छा और उद्योग दोनों ही चिरकालसे क्रीड़ा किया करते थे ॥२॥
रत्नोंके व्यापारमें निपुण उस श्रीदत्तने किसी समय रत्नद्वीपको जाने की इच्छा की । तदनुसार प्रस्थानकर अनेक देश, नगर और गाँवोंको लाँघता हुआ वह समुद्रके समीप आया। वहाँ उसने सामने लहराते हुए समुद्रको देखा। वह समुद्र फूटी हुई सीपोंके मोतियोंके समूहसे व्याप्त था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो मकर, मीन और कुलीरराशिसे सुशोभित दूसरा आकाशतल ही हो । वह समुद्रफेनके टुकड़ोंके बहाने ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रिके समय उसने जो चन्द्रमाको किरणोंके समूहका पान किया था उसे ही फेनके बहाने उगल रहा हो। कभी अत्यन्त चञ्चल कुलाचलोंके समान तरङ्गोंके सङ्घटनका अनुभव करनेवाले तिमि-तिमिङ्गिल जातिके मच्छ, पुत्रोंकी तरह उसकी सेवा कर रहे थे। कहीं मणिसमूहके किरणरूपी झरनेसे व्याप्त जलको मांस समझकर मीन उसके संमुख दौड़ रहे थे और कहीं अग्नि समझकर भयसे दूर भाग रहे थे। कहीं देदीप्यमान फणाके मणियोंसे सुशोभित, लहरों में मिले भुजङ्गोंसे व्याप्त होनेके कारण ऐसा जान पड़ता था मानों विशालता आदि गुणोंके द्वारा पराजित होकर छिपे हुए आकाशको तरङ्गरूपी हाथोंमें दीपक ले दृढ़ता हो फिर रहा हो। कहींपर विस्तृत मूंगाके वनोंकी पंक्तिसे सुशोभित होनेके कारण ऐसा जान पड़ता था मानों वड़वानलको ही प्रत्यक्ष दिखला रहा हो ।