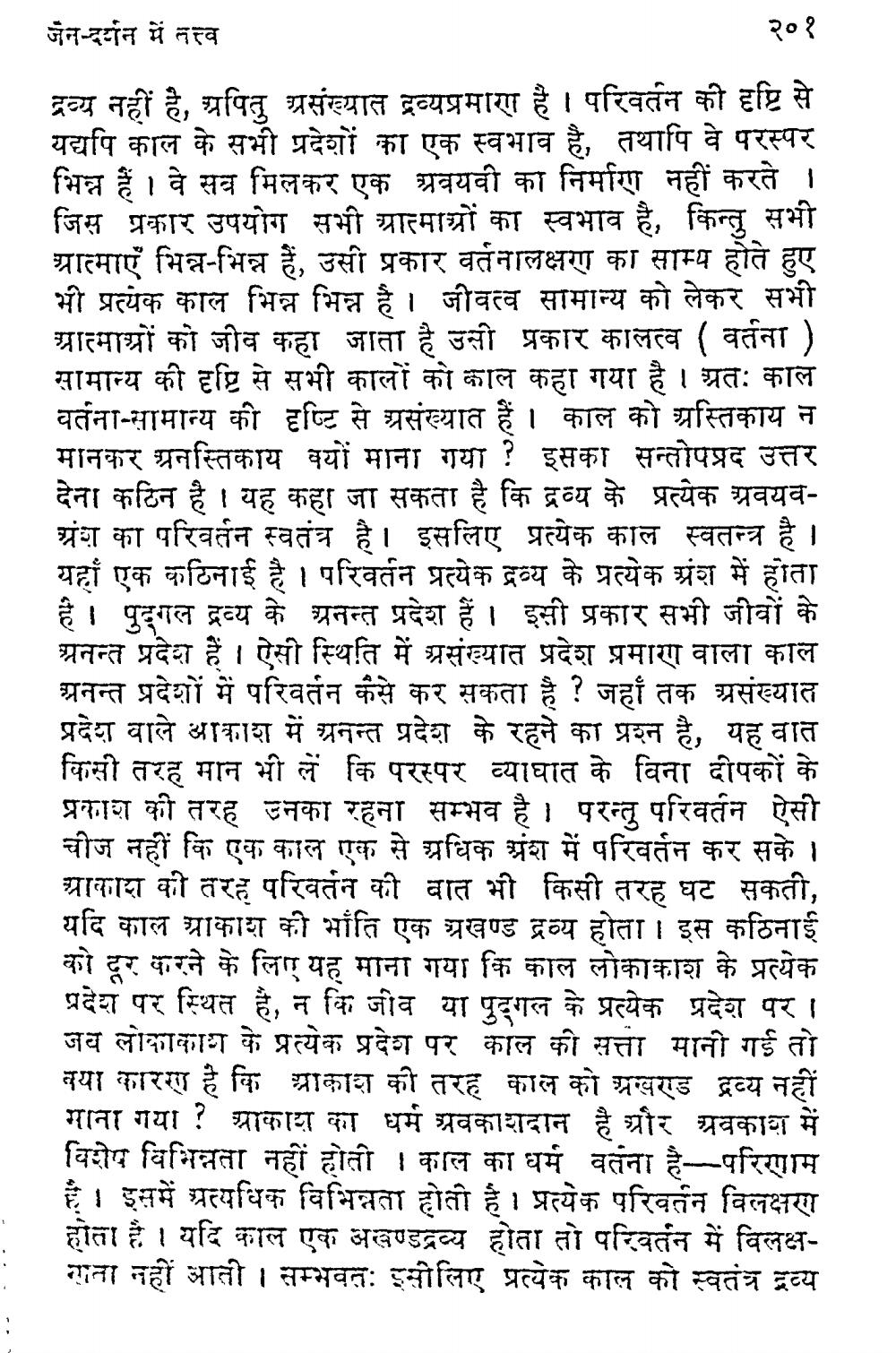________________
जैन-दर्शन में तत्त्व
२०१ द्रव्य नहीं है, अपितु असंख्यात द्रव्यप्रमाण है । परिवर्तन की दृष्टि से यद्यपि काल के सभी प्रदेशों का एक स्वभाव है, तथापि वे परस्पर भिन्न हैं। वे सब मिलकर एक अवयवी का निर्माण नहीं करते । जिस प्रकार उपयोग सभी प्रात्मानों का स्वभाव है, किन्तु सभी अात्माएँ भिन्न-भिन्न हैं, उसी प्रकार वर्तनालक्षण का साम्य होते हुए भी प्रत्येक काल भिन्न भिन्न है। जीवत्व सामान्य को लेकर सभी अात्मानों को जीव कहा जाता है उसी प्रकार कालत्व ( वर्तना ) सामान्य की दृष्टि से सभी कालों को काल कहा गया है । अतः काल वर्तना-सामान्य की दृष्टि से असंख्यात हैं। काल को अस्तिकाय न मानकर अनस्तिकाय क्यों माना गया ? इसका सन्तोपप्रद उत्तर देना कठिन है । यह कहा जा सकता है कि द्रव्य के प्रत्येक अवयवअंश का परिवर्तन स्वतंत्र है। इसलिए प्रत्येक काल स्वतन्त्र है । यहाँ एक कठिनाई है । परिवर्तन प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक अंश में होता है। पुद्गल द्रव्य के अनन्त प्रदेश हैं। इसी प्रकार सभी जीवों के अनन्त प्रदेश हैं । ऐसी स्थिति में असंख्यात प्रदेश प्रमाण वाला काल अनन्त प्रदेशों में परिवर्तन कैसे कर सकता है ? जहाँ तक असंख्यात प्रदेश वाले आकाश में अनन्त प्रदेश के रहने का प्रश्न है, यह वात किसी तरह मान भी लें कि परस्पर व्याघात के विना दीपकों के प्रकाश की तरह उनका रहना सम्भव है। परन्तु परिवर्तन ऐसी चीज नहीं कि एक काल एक से अधिक अंश में परिवर्तन कर सके । अाकारा की तरह परिवर्तन की बात भी किसी तरह घट सकती, यदि काल अाकाश की भाँति एक अखण्ड द्रव्य होता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह माना गया कि काल लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित है, न कि जीव या पुद्गल के प्रत्येक प्रदेश पर । जव लोकाकाग के प्रत्येक प्रदेश पर काल की सत्ता मानी गई तो क्या कारण है कि प्राकाश की तरह काल को अखण्ड द्रव्य नहीं माना गया ? नाकारा का धर्म अवकाशदान है और अवकाग में विशेप विभिन्नता नहीं होती । काल का धर्म वतंना है-परिणाम है। इसमें अत्यधिक विभिन्नता होती है। प्रत्येक परिवर्तन विलक्षण होता है । यदि काल एक अखण्डद्रव्य होता तो परिवर्तन में विलक्षगता नहीं आती । सम्भवतः इसीलिए प्रत्येक काल को स्वतंत्र द्रव्य