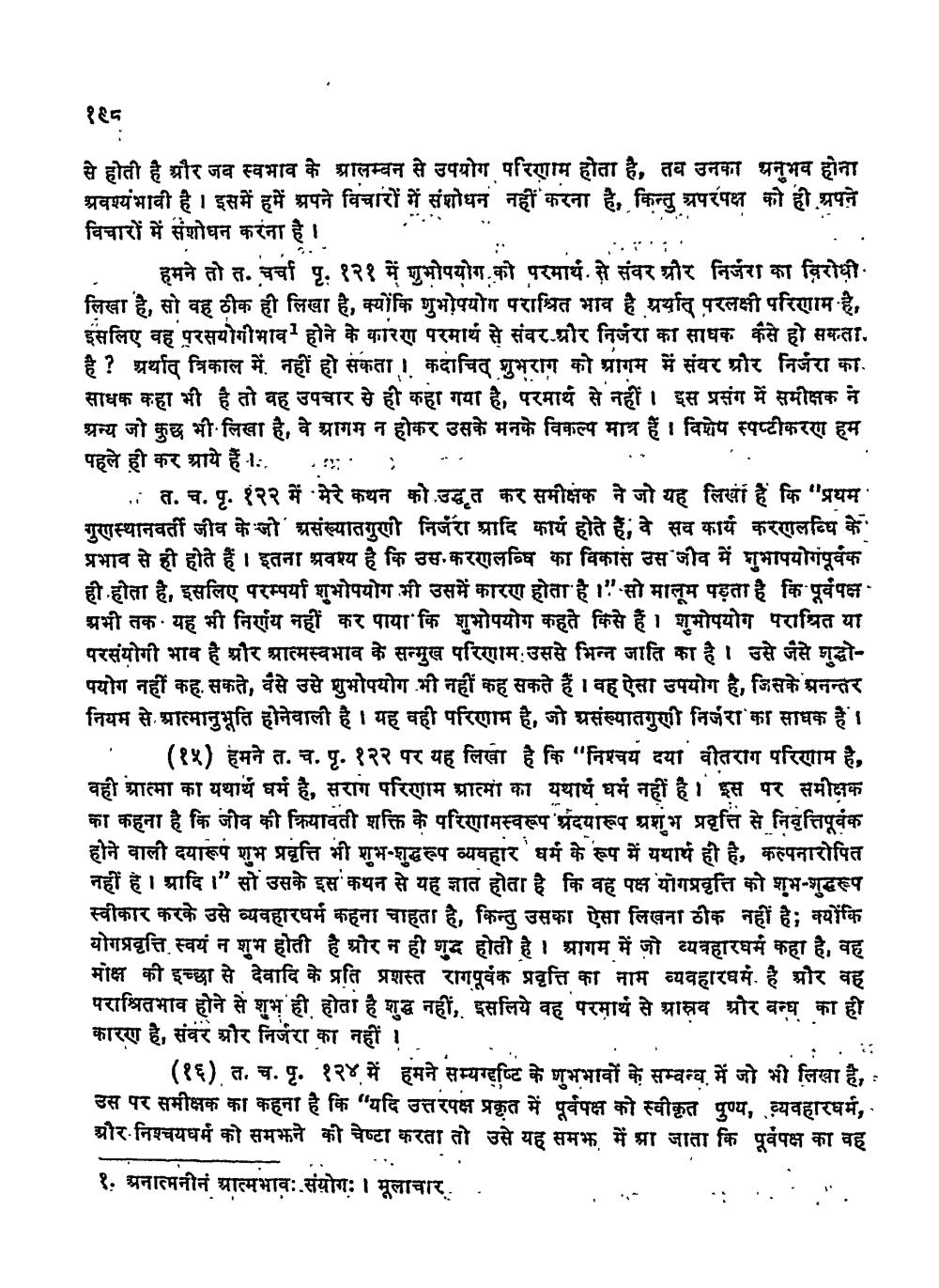________________
१६८ :
से होती है और जब स्वभाव के श्रालम्बन से उपयोग परिणाम होता है, तब उनका अनुभव होना श्रवश्यंभावी है | इसमें हमें अपने विचारों में संशोधन नहीं करना है, किन्तु अपरंपक्ष को ही अपने विचारों में संशोधन करना है ।
हमने तो त. चर्चा पृ. १२१ में शुभोपयोग को परमार्थ से संवर श्रीर निर्जरा का विरोधीलिखा है, सो वह ठीक ही लिखा है, क्योंकि शुभोपयोग पराश्रित भाव है अर्थात् परलक्षी परिणाम है, इसलिए वह परसयोगीभाव होने के कारण परमार्थ से संवर श्रीर निर्जरा का साधक कैसे हो सकता. है ? श्रर्थात् त्रिकाल में नहीं हो सकता । कदाचित् शुभराग को ग्रागम में संवर श्रौर निर्जरा का. साधक कहा भी है तो वह उपचार से ही कहा गया है, परमार्थ से नहीं । इस प्रसंग में समीक्षक ने श्रन्य जो कुछ भी लिखा है, वे श्रागम न होकर उसके मनके विकल्प मात्र हैं । विशेष स्पष्टीकरण हम पहले ही कर श्राये हैं 1.:.
C
त. च. पृ. १२२ में मेरे कथन को उद्धृत कर समीक्षक ने जो यह लिखा हैं कि " प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव के जो प्रसंख्यातगुणी निजरा आदि कार्य होते हैं, वे सब कार्य करणलब्धि के प्रभाव से ही होते हैं । इतना अवश्य है कि उस करणलब्धि का विकास उस जीव में शुभापयोगंपूर्वक ही होता है, इसलिए परम्पर्या शुभोपयोग भी उसमें कारण होता है ।" सो मालूम पड़ता है कि पूर्वपक्षअभी तक यह भी निर्णय नहीं कर पाया कि शुभोपयोग कहते किसे हैं । शुभोपयोग पराश्रित या परसंयोगी भाव है और आत्मस्वभाव के सन्मुख परिणाम: उससे भिन्न जाति का है । उसे जैसे शुद्धोपयोग नहीं कह सकते, वैसे उसे शुभोपयोग भी नहीं कह सकते हैं । वह ऐसा उपयोग है, जिसके अनन्तर नियम से आत्मानुभूति होनेवाली है । यह वही परिणाम है, जो प्रसंख्यातगुणी निर्जरा का साधक हैं ।
(१५) हमने त. च. पू. १२२ पर यह लिखा है कि "निश्चय दया वीतराग परिणाम है, वही आत्मा का यथार्थ धर्म है, सराग परिणाम आत्मा का यथार्थ धर्म नहीं है । इस पर समीक्षक का कहना है कि जीव की क्रियावती शक्ति के परिणामस्वरूप श्रदयारूप प्रशुभ प्रवृत्ति से निवृत्तिपूर्वक होने वाली दारूपं शुभ प्रवृत्ति भी शुभ शुद्धरूप व्यवहार धर्म के रूप में यथार्थ ही है, कल्पनारोपित नहीं है | आदि ।” सो उसके इस कथन से यह ज्ञात होता है कि वह पक्ष योगप्रवृत्ति को शुभ-शुद्धरूप स्वीकार करके उसे व्यवहारधर्म कहना चाहता है, किन्तु उसका ऐसा लिखना ठीक नहीं है; क्योंकि योगप्रवृत्ति स्वयं न शुभ होती है और न ही शुद्ध होती है । श्रगम में जो व्यवहारधर्म कहा है, वह मोक्ष की इच्छा से देवादि के प्रति प्रशस्त रागपूर्वक प्रवृत्ति का नाम व्यवहारघमं है और वह पराश्रितभाव होने से शुभ ही होता है शुद्ध नहीं, इसलिये वह परमार्थ से श्राव और बन्धु का ही कारण है, संवर और निर्जरा का नहीं ।
(१६) त. च. पृ. १२४ में हमने सम्यग्द्दृष्टि के शुभभावों के सम्वन्ध में जो भी लिखा उस पर समीक्षक का कहना है कि "यदि उत्तरपक्ष प्रकृत में पूर्वपक्ष को स्वीकृत पुण्य, व्यवहारधर्म, और निश्चयधर्म को समझने की चेष्टा करता तो उसे यह समझ में श्रा जाता कि पूर्वपक्ष का वह
१. अनात्मनीनं श्रात्मभावः संयोगः । मूलाचार
: